रवि नन्दन सिंह का आलेख 'हिंदी जमात के आखिरी उस्ताद: आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी'
 |
| आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी |
साहित्य मूलतः प्रतिबद्धता से जुड़ा वह कर्म है जो हमें मनुष्यता की तरफ अग्रसर करता है। यह हमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान तो प्रदान करता ही है सामाजिकता से भी गहरे तौर पर जोड़ता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ऐसे ही रचनाकार रहे हैं जिन्होंने 1903 ई से 1920 ई तक सरस्वती जैसी महत्त्वपूर्ण पत्रिका का संपादन किया। इस युग को सरस्वती पत्रिका का स्वर्ण युग माना जाता है। हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता की दुनिया में सरस्वती पत्रिका की भूमिका अहम थी। कवि आलोचक रवि नन्दन सिंह उचित ही लिखते हैं - 'द्विवेदी जी का हिन्दी साहित्य को दिया गया सबसे बड़ा अवदान यही है। उन्होंने एक समूची पीढ़ी को खड़ा कर दिया। उस पीढ़ी के मार्ग निर्देशक बन कर उभरे। उन्होंने संकेत किया और युगीन रचनाकारों ने उस संकेत सूत्र को पकड़ कर अपनी लेखनी चलायी और हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने साहित्य के उन स्थलों पर अँगुली रखी जहाँ अँधेरा था और उनकी पीढ़ी के रचनाकारों ने वहाँ लेखनी से प्रकाश भर दिया। द्विवेदी के मार्गदर्शन में अनेक रचनाकार अपनी सजग भूमिका के साथ खड़े हो गये। इनमें मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध', गोपाल शरण सिंह, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही', सत्य नारायण 'कविरत्न', नाथूराम शर्मा 'शंकर', राय देवी प्रसाद 'पूर्ण', रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी आदि रचनाकारों के नाम विशेष उल्लेखनीय है।' रवि नन्दन ने महावीर प्रसाद द्विवेदी पर एक महत्त्वपूर्ण आलेख लिखा है। आइए आज पहली बार पर हम पढ़ते हैं रवि नन्दन सिंह का आलेख 'हिंदी जमात के आखिरी उस्ताद: आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी'।
'हिंदी जमात के आखिरी उस्ताद: आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी'
रविनंदन सिंह
साहित्य, संगीत और कला की दुनिया कुछ मामलों में सामान्य दुनिया से अलग होती है, अत्यंत विशिष्ट होती है। विशिष्ट इस अर्थ में होती है कि वह सामान्य लोगों से अलग हट कर सोचती है। दुनियावी भौतिकता की दौड़ में शामिल नहीं होती। साधन की बजाय साधना का मार्ग चुनती है। जीवन का आनंद बाहर खोजने की बजाय अपने अंदर खोजती है। ’कस्तूरी कुंडली बसे’ के भाव को जीती हैं। साहित्य एवं कला की दुनिया अपने को भौतिक रूप से समृद्ध करने की बजाय आत्मिक रूप से समृद्ध करती है। जीवन की स्थूल चीजों से वास्ता रखने की बजाय अपनी भाव दशा में खो जाती है, इतना खो जाती है कि खुद को अपनी कला में विलीन कर लेती है। कला का यही सच है कि जो खुद को जिस अनुपात में विलीन करता है, उसी अनुपात में युगीन सत्य और सौंदर्य की निर्मिति करता है। ऐसी कला ही जीवन और जगत की विषमताओं का सही समाधान प्रस्तुत करती है।
यह बात सभी स्वनामधन्य रचनाकारों पर पूरी तरह लागू होती है। इसीलिए कलाकार या रचनाकार का जीवन बाहर से तो बिखरा हुआ दिखता है किंतु अंदर से अनुशासित रहता है। वह खुद अव्यवस्थित जीवन जीता है किंतु अंदर से उतना ही व्यवस्थित चित्त होता है। जीवन को भौतिक कसौटी पर नहीं जाँचता-परखता वरन व्यष्टि और समष्टि की मुक्ति के लिए छटपटाता रहता है। वह साधनों की खोज में नहीं उलझता बल्कि साधना की गहराई में उतरता है। उसे पता होता है कि बंदिश और अनुशासन में कला पनप नहीं सकती। इसीलिए हर रचनाकार सर्वदा स्वतंत्र और स्वछंद रहना चाहता है। आत्मिक मुक्ति की तलाश करता है।
मुक्ति की इसी भावना के अनुरूप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1904 ई. में अपनी दो सौ रुपए मासिक की नौकरी से इस्तीफा दे कर इंडियन प्रेस से मिलने वाले मात्र तेईस रुपए में गुजारा करना स्वीकार करते हैं। यद्यपि इस्तीफा देने के एक वर्ष पूर्व से ही वे सरस्वती का संपादन हाथ में ले चुके थे तथा जूही, कानपुर में अपने मित्र सीताराम के हाते में रह कर सरस्वती का संपादन करते लगे। इस संपादन के लिए उन्हें मात्र तेईस रुपए ही मिलते थे। आचार्य द्विवेदी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के संबंध में, अपने आत्मनिवेदन (मई, 1933 की सरस्वती में प्रकाशित) में लिखा है कि "अंग्रेज अधिकारी का हुक्म हुआ कि तुम इतने कर्मचारियों को ले कर रोज सुबह 8 बजे दफ्तर में आया करो और ठीक दस बजे मेरे कागज मेरे मेज पर मुझे रक्खे मिलें। मैंने कहा- मैं आऊँगा, पर औरों को आने के लिए लाचार न करूँगा। उन्हें हुक्म देना हुजूर का काम है। बस बात बढ़ी और बिना किसी सोच-विचार के मैंने इस्तीफा दे दिया। बाद में उसे वापस लेने के लिए इशारे ही नहीं, (मुझसे) सिफारिशें तक की गईं। पर सब व्यर्थ हुआ। क्या इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए, यह पूछने पर मेरी पत्नी ने विपण्ण हो कर कहा, "क्या थूक कर भी कोई उसे चाटता है?” मैं बोला, "नहीं, ऐसा कभी न होगा, तुम धन्य हो। तब उसने तो रोज तक की आमदनी से भी मुझे खिलाने- पिलाने और गृह-कार्य चलाने का दृढ़ संकल्प किया और मैंने 'सरस्वती' की सेवा से मुझे हर महीने जो 20 रु. उजरत, और तीन रु. डाकखर्च की आमदनी होती थी उसी से संतुष्ट रहने का निश्चय किया।"
इंडियन प्रेस से प्रथम परिचय कैसे हुआ इस संबंध में द्विवेदी जी ने अत्यंत रोचक बात लिखी है। उसके अनुसार जब वे झाँसी में थे तब वहां तहसीली स्कूल के एक अध्यापक ने उन्हें कोर्स की एक पुस्तक दिखाई। नाम था 'तृतीय रीडर' जो इंडियन प्रेस से छपी थी। उस अध्यापक महोदय ने उस पुस्तक में अनेक दोष दिखाए और द्विवेदी जी से आग्रह किया कि उसकी समालोचना कर दें। उस समय तक द्विवेदी जी की कुछ समालोचनाएँ प्रकाशित हो चुकी थीं। द्विवेदी जी ने पुस्तक पढ़ी और उस अध्यापक की शिकायत को ठीक पाया। नतीजा यह हुआ कि द्विवेदी जी ने उसकी समालोचना पुस्तकाकार प्रकाशित करा दी। यह समालोचना इंडियन प्रेस के खिलाफ़ थी किंतु चिंतामणि घोष प्रतिभा को पहचान लेते थे। इसी समालोचना की बदौलत इंडियन प्रेस से द्विवेदी जी का परिचय हुआ और कुछ समय बाद प्रेस ने उन्हें 'सरस्वती' पत्रिका का संपादन का दायित्व देने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। यह घटना रेल की नौकरी छोड़ने के एक साल पहले की है।
आचार्य द्विवेदी जब 13 वर्ष के थे, उन्हें रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी एवं फ़ारसी पढ़ने भेजा गया। आटा-दाल पीठ पर लाद कर घर से 36 मील दूर पढ़ने गए। रोटी बनाने नहीं आता था, अतः दाल में ही आटे की पीड़िया डाल कर किसी तरह पेट भरते थे। संस्कृत वहाँ अछूत समझी जाती थी। एक वर्ष बाद उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया। आगे पुरवा, फतेहपुर और उन्नाव के स्कूलों में पढ़ाई कर के चार वर्ष बाद स्कूल छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा वहीं समाप्त हो गयी। अजमेर में 15 रुपए महीने की नौकरी शुरू की, फिर पिता के पास बम्बई जा कर रेलवे में तार का काम सीखा और वहीं 20 रुपए मासिक पर तार बाबू बन गए। हरदा, होशंगाबाद, पुनः बम्बई होते हुए झाँसी पोस्टिंग हो गयी। नौकरी का जीवन जीने के लिए उन्होंने चार सिद्धांत निश्चित किए।
1-वक़्त की पाबंदी,
2-रिश्वत न लेना,
3-अपना काम ईमानदारी से करना तथा
4-ज्ञान वृद्धि के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना।
स्वाभिमान के प्रश्न पर 1904 में 200 रुपए मासिक वाली नौकरी से इस्तीफा दे दिया।'
द्विवेदी जी के नौकरी छोड़ने पर उनके कई मित्रों ने कई प्रकार से उनकी सहायता करने की इच्छा प्रकट की। किसी ने कहा- आओ, मैं तुम्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाऊँगा। किसी ने लिखा- मैं तुम्हारे साथ बैठ कर तुमसे संस्कृत पढूँगा। किसी ने कहा- मैं तुम्हारे लिए एक छापाखाना खुलवा दूँगा- इत्यादि। किंतु उन्होंने सबको अपनी कृतज्ञता की सूचना दे दी और लिख दिया कि अभी उन्हें उनकी सहायता की विशेष आवश्यकता नहीं। उन्होंने सोचा कि अव्यवस्थित-चित्त मनुष्य की सफलता में सदा सन्देह रहता है। उन्होंने अपनी सारी शक्ति सरस्वती में लगा दी। उन्होंने 'सब तज, हरि भज' की मसल को चरितार्थ किया। सरस्वती के संपादन में द्विवेदी जी के चार आदर्श और संकल्प थे
(1) वक्त की पाबंदी
(2) मालिकों का विश्वास-पात्र बनने की चेष्टा
(3) अपने हानि-लाभ की परवाह न करके पाठकों के हानि-लाभ का सदा ख्याल रखना और
(4) न्याय पथ से कभी विचलित न होना।
सरस्वती' के संपादन से मिलने वाले मात्र 23 रुपए मासिक में गुजारा करने लगे। 1903 से 1920 तक उन्होंने सरस्वती का संपादन किया जो एक ऐतिहासिक गौरव का विषय है। उनके पास साधन बहुत कम थे, किंतु उनकी साधना बहुत बड़ी थी।
नागरी प्रचारिणी सभा काशी के विद्वान एवं पांडुलिपियों के खोजी श्रीयुत केदार नाथ पाठक ने अपने एक संस्मरण में द्विवेदी जी से संबंधित रोचक बात बताई है। उसके अनुसार 1904 में श्याम सुंदर दास और द्विवेदी जी में कुछ मतभेद चल रहा था। उसी समय अक्तुबर 1904 की सरस्वती में नागरी प्रचारिणी सभा की एक खोज रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की गई थी। तब तक सरस्वती नागरी प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से ही प्रकाशित होती थी। प्रचारिणी सभा ने उस आलोचना का प्रतिवाद करते हुए इंडियन प्रेस के मालिक बाबू चिंतामणि घोष को एक पत्र लिख भेजा। इसकी प्रतिक्रिया में द्विवेदी जी ने दिसंबर 1904 की सरस्वती में ’सभा और सरस्वती’ शीर्षक से एक धारदार आलोचनात्मक लेख लिखा। उस लेख में श्याम सुंदर दास और केदार नाथ पाठक पर भी व्यंग्य किया गया था। उस समय केदार नाथ पाठक पन्ना, म प्र में पांडुलिपियों की खोज कर रहे थे। वहीं उन्होंने सरस्वती में द्विवेदी जी का लेख पढ़ा। श्याम सुंदर दास और अपने ऊपर ली गई चुटकी से पाठक जी बहुत क्षुब्ध हुए। नागरी प्रचारिणी सभा के अंदर बड़ी हलचल मच गई। सभा ने बैठक की और आगामी जनवरी 1905 से सरस्वती से अपना अनुमोदन हटाने का निर्णय लिया। इंडियन प्रेस को सूचना भेज दी गई। इंडियन प्रेस के संस्थापक बाबू चिंतामणि घोष स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने उस अंक के छपे कवर को रद्द करवा दिया और सभा के अनुमोदन वाला हिस्सा हटा कर पुनः नया कवर छपवा दिया। जनवरी 1905 से सरस्वती और प्रचारिणी सभा का संबंध समाप्त हो गया। सभा से सरस्वती की विदाई हो गई। इस पर द्विवेदी जी ने सरस्वती में ’अनुमोदन का अंत’ शीर्षक से एक शिष्ट और मार्मिक संपादकीय लिखा था। केदार नाथ पाठक उन्हीं दिनों द्विवेदी जी से जा कर जूही, कानपुर में मिले और उनसे सीधे तौर पर एक उग्र प्रश्न पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि ’सभा के कार्यों की कड़ी आलोचना का हमें किस रूप में प्रतिवाद करना होगा। क्या ’विषस्य विषमौषधम’ की नीति का अवलंबन करना पड़ेगा?’ तब द्विवेदी जी ने सज्जनता से कहा कि ’देवता! ठहर जाओ, मैं अभी आता हूँ।’ घर के अंदर गए। एक हाथ में गिलास, सुंदर तश्तरी में मिठाइयां और एक लौटा पानी ला कर सामने रख दिए। फिर उसी कमरे के एक कोने में रखी मोटी लाठी भी ला कर सामने रख कर मुस्कुराते हुए बोले- "सुदूर प्रवास से थके-माँदे आ रहे हो, पहले हाथ-मुँह धो कर जलपान करके सबल हो जाओ, तब यह लाठी और यह मेरा मस्तक है।" इस पर केदार नाथ पाठक शर्म से पानी पानी हो गए और उनके क्रोध का स्थान करुणा ने ले लिया। द्विवेदी जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव उमड़ पड़ा।
नवंबर 1905 की सरस्वती में द्विवेदी जी ने ’भाषा और व्याकरण’ शीर्षक से एक लेख लिखा। उसमें तत्कालीन धुरंधर लेखकों की रचनाओं से व्याकरण संबंधी अनेक दोषों को उद्धृत करके दिखाया गया था। उसमें कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली ’भारत मित्र’ पत्रिका के संपादक लाला बालमुकुंद गुप्त की रचना से भी एक उद्धरण दिया गया था। इससे क्षुब्ध हो कर बालमुकुंद गुप्त ने आत्माराम नामक छद्म नाम से ’भाषा की अस्थिरता’ शीर्षक निबंध में द्विवेदी जी का तीव्र प्रतिवाद किया। उन्होंने उस लेख में द्विवेदी जी पर अनेक तीव्र प्रहार किए। इस लेख की प्रतिक्रिया में पंडित गोविंद नारायण मिश्र ने कलकत्ता से ही प्रकाशित ’हिंदी बंगभाषी’ पत्रिका में "आत्माराम की टें-टें“ शीर्षक एक कटु निबंध लिखा। भारत मित्र' और 'सरस्वती' के बीच यह झगड़ा बरसों चलता रहा जिसमें हिंदी-बंगवासी, व्यंकटेश्वर-समाचार, सुदर्शन आदि पत्र-पत्रिकाएं अपने-अपने इष्ट-मित्रों का पक्ष ले रहीं थीं। इस वाद-विवाद में कुछ लोग सहृदयता, आपसी सौजन्य और शिष्टता का ध्यान एकदम भूल गए थे। पर विद्वान् द्विवेदी जी उस अवस्था में भी अपने विरोधियों का प्रतिवाद करने में सर्वदा शिष्ट और सहृदय बने रहे। अपने स्वाभाविक अभ्यास के कारण वे मर्यादा का ध्यान कभी नहीं भूले। पर कोई कहाँ तक सहन कर सकता है? सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। एक लेख में बालमुकुंद गुप्त ने बैसवारे की बोली में "हम पंचन के ट्वाला माँ" लिख कर द्विवेदी जी पर कटाक्ष किया। तब दिवेदी जी कुछ क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने 'कल्लू अल्हइत' के नाम से "सरगौ नरक ठेकाना नाहिँ" शीर्षक एक आल्हा अवधी में लिख डाला। उस पर बालमुकुंद गुप्त ने अपनी राय देते हुए लिखा कि 'भाई वाह! कल्लू अल्हइत का आल्हा खूब हुआ। क्यों न हो, अपनी स्वाभाविक बोली में है न।’ इस झगड़े ने हिंदी-साहित्य-संसार में बड़ी चहल-पहल मचा दी थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बालमुकुंद गुप्त एक बार कानपुर गए और उर्दू मासिक पत्र 'जमाना' के सुयोग्य संपादक मुंशी दया नारायण निगम से मिले। द्विवेदी जी से भी मिलना चाहते थे किंतु साहस नहीं कर पा रहे थे। तब निगम जी उन्हें ले कर द्विवेदी जी के पास जुही गए। निगम जी ने द्विवेदी जी का परिचय देते हुए कहा- "आप ही सरस्वती के सुयोग्य संपादक पं० महा. ..।" इतना कहना था कि बालमुकुंद गुप्त ने झट से द्विवेदी जी के पैरों पर अपना मस्तक रख दिया। द्विवेदी जी आश्चर्य में पड़ गए, उन्हें पहचानते नहीं थे। उन्होंने एक अपरिचित भद्र पुरुष को इस प्रकार पैरों पर माथा टेकते देख झट से उठा कर हृदय से लगा लिया। तब निगम महाशय ने बतलाया कि आप हैं ’भारत मित्र' के सुयोग्य संपादक लाला बालमुकुंद जी गुप्त।' गुप्त जी की आँखें भर आईं। उन्होंने कहा कि "मैं अपराधी हूँ और आपके सामने अपने उन अभद्रतापूर्ण व्यवहारों के लिये क्षमा माँगने भौर प्रायश्चित्त करने आया हूँ। आप विद्या में गुरु बृहस्पति, स्नेह में ज्येष्ठ भ्राता तथा करुणा में बुद्ध के सदृश हैं। आपके चरणों पर मैं बार बार अपना सिर रखता हूँ। अखबारनवीसी एक ऐसा काम है जिसमें अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में बहुधा ऐसी भूलें होती हैं। मैंने न्याय-संगत बातों का अनुचित रूप से उत्तर दिया है, जिसके लिये मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ।" तब से दोनों एक दूसरे के प्रशंसक हो गए।
 |
| बालमुकुंद गुप्त |
नागरी प्रचारिणी सभा काशी से ’द्विवेदी अभिनंदन ग्रन्थ’ छपा है। उसमें हरिभाऊ उपाध्याय का भी एक लेख है। हरिभाऊ उपाध्याय तीन वर्ष तक सरस्वती में द्विवेदी जी के सहायक रहे और बाद में गांधी के ’नवजीवन’ पत्र में चले गए। उनका लेख द्विवेदी जी के व्यक्तित्व को समझने में सहायक है। अपने लेख में हरिभाऊ उपाध्याय लिखते हैं कि “पूज्य द्विवेदी जी का स्मरण होते ही मेरे सामने पिता और गुरु की एक सम्मिलित मूर्ति खड़ी हो जाती है। जब मैं 'सरस्वती' में जाने लगा था, तब मुझको कुछ हितैषियों ने मना किया था कि 'द्विवेदी जी से तुम्हारी पटेगी नहीं, तुम वहाँ न रह सकोगे, वे बहुत कड़े और क्रोधी हैं। कोई सहायक उनके पास अधिक समय तक नहीं टिका है।' मैंने अपने मन में सोचा कि 'जब पूज्य द्विवेदी जी इतने विद्वान्, ऐसे सुयोग्य संपादक, और हिंदी-संसार में ऐसे मान्य पुरुष हैं, तब ऐसा कोई कारण नहीं कि मैं उनके अधीन काम करने में हिचकूं या किसी भावी भय को हृदय में स्थान दूँ। यदि वे कड़े हैं तो काम ही तो अधिक लेंगे; यदि क्रोधी होंगे तो कुछ भला-बुरा ही तो कह लेंगे, कोई अमानुषिक व्यवहार तो करेंगे नहीं। फिर मैं तो उनके प्रति बहुत श्रद्धा और गुरु-भाव रखकर जाना चाहता था। तो, मैंने मित्रों से कहा कि उनकी कड़ाई मेरे लिये अच्छे ट्रेनिंग का काम देगी और उनका क्रोध मेरे लिये वरदान होगा। बस, मैं चल पड़ा। प्रयाग में 'इंडियन प्रेस' के एक कमरे में मैं पूज्य द्विवेदी जी के सामने पहले-पहल पेश किया गया। मैं मन में कुछ सहम रहा था। उनका खासा लम्बा कद, विशाल और रोबदार चेहरा, बड़ी-बड़ी मूंछें-ये सब उनके तेजस्वी व्यक्तित्व की छाप डाल रहे थे। उनके सामने मैं दुबला-पतला अधमरा-सा युवक पहुँचा! पहुँचते ही उन्होंने मुझसे पूछा 'ओहो ! आप भी ऐनक लगाते हैं!’ मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने सोचा, क्या पहली परीक्षा में ही फेल होना होगा? उन्होंने और भी कुछ चुने हुए प्रश्न किए, जिनके उत्तरों में उन्होंने मुझे भीतर-बाहर सब अच्छी तरह समझ लिया। मैं खूब समझ रहा था कि मुझ पर जबरदस्त 'सर्चलाइट' पड़ रही है। लेकिन उस समय भी मुझे यही प्रतीत हो रहा था कि मैं एक सहृदय और सहानुभूतिशील बुजुर्ग के सामने हूॅं। अस्तु, कोई तीन वर्ष मुझे द्विवेदी जी के चरणों में रहकर 'सरस्वती' की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त रहा। मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि क्रोध करने की तो बात ही क्या, कभी तेज स्वर में भी द्विवेदी जी ने मुझे कुछ कहा हो।" ये बातें द्विवेदी जी के व्यक्तित्व को समझने में सहायक हैं।
 |
| हरिभाऊ उपाध्याय |
आचार्य द्विवेदी को आचार्य की पदवी नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने प्रदान की थी। 2 मई, 1933 में नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा अभिनंदन ग्रंथ प्रदानोत्सव के समय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक वक्तव्य दिया था जो मई, 1933 की सरस्वती में प्रकाशित भी हुआ था। उस वक्तव्य में उन्होंने अपने को ’आचार्य’ कहे जाने पर कहा कि 'मुझे आचार्य की पदवी मिली है। क्यों मिली है, मालूम नहीं है। कब, किसने दी है, यह भी मुझे मालूम नहीं। मालूम सिर्फ इतना ही है कि मैं बहुधा- इस पदवी से विभूषित किया जाता हूँ। शंकराचार्य, मध्वाचार्य्य आदि के सदृश किसी आचार्य के चरणरजःकण की बराबरी मैं नहीं कर सकता। बनारस के संस्कृत-कालेज या किसी विश्वविद्यालय में भी मैंने कभी कदम नहीं रखा। फिर इस पदवी का मुस्तहक मैं कैसे हो गया? विचार करने पर, मेरी समझ में, इसका एक-मात्र कारण मुझ पर कृपा करने वाले सज्जनों का अनुग्रह ही जान पड़ता है।
द्विवेदी जी सचमुच भाषा एवं साहित्य के आचार्य थे, उस्ताद थे। युगीन रचनाकारों को प्रेरणा दे कर, उनकी भाषा का संस्कार कर, रचनाकारों की रचनाओं को सँवार कर-तराश कर उन्होंने कुशल उस्ताद की तरह उनका मार्गदर्शन किया। उनके संकेत-सूत्र को पकड़ कर कई रचनाकार यशस्वी भी बने। मैथिली शरण गुप्त, निराला, प्रेमचंद जैसे अनेक रचनाकारों ने तो उन्हें अपना गुरू माना है। आज तो हिन्दी जगत में कोई शागिर्द नहीं हैं। सभी पैदाइशी उस्ताद हैं। उन्हें किसी गुरु से रचना-कौशल सीखने की आवश्यकता नहीं है। अब अर्जुन की तरह गुरु से सीखने वाले रचनाकार नहीं हैं। आज सब अभिमन्यु की तरह पहले से ही सीख कर पैदा हुए हैं। अब अपने वरिष्ठ रचनाकारों को अपनी रचना दिखा कर उनसे सलाह लेने वाले कहाँ हैं? स्थिति तो यह है कि यदि कोई सलाह दे भी दे तो लोग बुरा मान जाते हैं। इसीलिए सभी रचनाकार स्वघोषित रचनाकार होते हैं। हाँ यह ज़रूर होता है कि कोई रचनाकार अपनी साधना, अभ्यास, जिज्ञासा और सीखने की प्रवृत्ति से अपनी कलात्मक प्रतिभा में निखार ला देता है।
हिन्दी के रीतिकाल तक उर्दू की तरह हिंदी में भी एक उस्ताद की आवश्यकता होती रही या महसूस की जाती रही। आदिकाल एवं भक्तिकाल में गुरु का महत्त्व तो सर्वसिद्ध है। किन्तु आधुनिक काल में हिन्दी जगत के अकेले उस्ताद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ही हैं। द्विवेदी जी की दृष्टि बिल्कुल साफ थी। वे कला अथवा साहित्य की सामाजिक भूमिका को स्वीकार करते थे। वे 'कला कला के लिए' की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते थे। उनके लिए कला और साहित्य सामाजिक परिवर्तन के संवाहक थे। अतः वे साहित्य-कर्म के प्रति सजग और गम्भीर थे। द्विवेदी जी युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं। वे न सिर्फ़ स्वयं सजग थे बल्कि अपने समकालीन रचनाकारों को भी सामाजिक भूमिका के प्रति सजग करने में विश्वास करते थे। उनके लिए मुक्ति अकेले नहीं बल्कि सबके साथ होने में काम्य थी। इसलिए वे सबको प्रेरित करते हैं, सबको जागरूक करते हैं। साहित्य एवं समाज के प्रति सबको प्रतिबद्ध होने का आवाहन करते हैं। वे अपने युग में एक उस्ताद की भूमिका निभाते हैं। रचनाकारों को उनके कर्त्तव्य का भास कराते हैं। साहित्य कैसा हो, भाषा कैसी हो आदि प्रश्नों की कसौटी उनके पास थी उनके लिए सामाजिक उपादेयता महत्त्वपूर्ण थी। समाज का उत्थान ही राष्ट्र के उत्थान की पूर्वपीठिका है और इस उत्थान में साहित्य की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, द्विवेदी जी इस बात को बखूबी समझते थे।
साहित्य की सामाजिक भूमिका को द्विवेदी जी ने इतनी गहनता से महसूस किया कि इसके प्रति रचनाकारों को जागरूक बनाने के लिए अपने निजी हितों को ताक पर रख दिया। रेलवे की नौकरी छोड़ दी और एकान्तवासी रचनाकार की बजाय निर्देशक रचनाकार की भूमिका को अपना लिया। निजी साहित्य साधना करते तो उनकी कई कृतियाँ आ जाती। उनके साहित्य में कला और सौन्दर्य पैदा हो जाता। किन्तु उन्होंने कला और सौन्दर्य के ऊपर समाज और राष्ट्र के निर्माण को महत्त्व दिया। द्विवेदी जी का हिन्दी साहित्य को दिया गया सबसे बड़ा अवदान यही है। उन्होंने एक समूची पीढ़ी को खड़ा कर दिया। उस पीढ़ी के मार्ग निर्देशक बन कर उभरे। उन्होंने संकेत किया और युगीन रचनाकारों ने उस संकेत सूत्र को पकड़ कर अपनी लेखनी चलायी और हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने साहित्य के उन स्थलों पर अँगुली रखी जहाँ अँधेरा था और उनकी पीढ़ी के रचनाकारों ने वहाँ लेखनी से प्रकाश भर दिया। द्विवेदी के मार्गदर्शन में अनेक रचनाकार अपनी सजग भूमिका के साथ खड़े हो गये। इनमें मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध', गोपाल शरण सिंह, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही', सत्य नारायण 'कविरत्न', नाथूराम शर्मा 'शंकर', राय देवी प्रसाद 'पूर्ण', रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी आदि रचनाकारों के नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन रचनाकारों ने अपने उस्ताद की प्रेरणा से काव्य-भाषा एवं समाज-राष्ट्र के ज्वलन्त पक्षों पर गम्भीरता से अपनी रचनात्मक भूमिका निभाई।
द्विवेदी जी किस तरह साथी रचनाकारों को प्रेरित करते थे, इसका बस एक उदाहरण ही काफ़ी है और वह उदाहरण हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी के अनेक शागिर्दों में अग्रपांक्तेय ही नहीं प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने द्विवेदी जी को पूरा सम्मान देते हुए अपना उस्ताद माना। वे एक स्थान पर स्वयं लिखते हैं कि- "मेरी उल्टी सीधी प्रारम्भिक रचनाओं का पूर्णशोधन करके उन्हें सरस्वती में प्रकाशित करना और पत्र द्वारा मेरे उत्साह को बढ़ाना द्विवेदी महाराज का ही काम था।"
वस्तुतः द्विवेदी युग के पूर्व ब्रजभाषा ही कविता की भाषा थी। ब्रजभाषा में ही सभी रचनाकार अपनी लेखनी का चमत्कार पैदा करते थे। मैथिली शरण गुप्त भी 'रसिकेन्द्र' उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएँ लिखा करते थे। उन्होंने अपनी ब्रजभाषा की एक कविता 'सरस्वती' में छपने के लिए प्रेषित की। उस समय सरस्वती का सम्पादन द्विवेदी जी कर रहे थे। द्विवेदी जी ने गुप्त जी की कविता एक टिप्पणी के साथ वापस कर दी। उनकी टिप्पणी बहुत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा कि ’आपकी कविता पुरानी भाषा में लिखी गयी है जबकि हम सरस्वती में आमजन की भाषा में लिखी कविताएँ ही प्रकाशित करते हैं।’ द्विवेदी जी ने यह भी कहा कि ’अब 'रसिकेन्द्र' बनने का जमाना गया।’ अगर द्विवेदी जी की जगह दूसरा सम्पादक होता तो बिना किसी टिप्पणी के वह कविता लौटा देता। किन्तु द्विवेदी जी का तरीक़ा अलग था। वे एक युग निर्माता थे, उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रेरक था। अतः उन्होंने सकारात्मक सुझाव दिया कि अब रसिकेन्द्र बनने का जमाना गया, अगर कविता करना है तो आमजन की भाषा में कविताएँ कीजिए। दूसरा रचनाकार होता तो बुरा भी मान सकता था, किन्तु गुप्त जी अलग व्यक्तित्व थे। उन्होंने द्विवेदी जी की बात को सकारात्मक रूप से ग्रहण किया। द्विवेदी जी के मार्गदर्शन को स्वीकार कर उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखना आरम्भ किया। जब उन्होंने अपनी खड़ी बोली की ’हेमंत’ शीर्षक कविता सरस्वती में प्रकाशन हेतु प्रेषित की तो द्विवेदी जी ने उसमें काफ़ी संशोधन करते हुए प्रकाशित किया। कोई दूसरा रचनाकार इसे भी बुरा मान सकता था। आजकल किसी की कविता में संशोधन कर दीजिए तो आप सबसे बुरे हो जाते हैं। किन्तु गुप्त जी ने इसे शिरोधार्य किया क्योंकि यह उस्ताद की सीख थी।
एक बार द्विवेदी जी ने सरस्वती में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था 'कवि और कविता।' उस लेख में उन्होंने कवियों से आग्रह किया कि कविता लिखने के पूर्व उर्दू के श्रेष्ठ कवियों की रचनाएँ अवश्य पढ़ें। इसमें उन्होंने अल्ताफ हुसैन हाली तथा उनकी कृति 'मुसद्दस' का जिक्र किया। हाली ने अपने मुसद्दस में, मुस्लिम कौम के सामाजिक एवं नैतिक पतन को केन्द्र में रखते हुए प्रबंधात्मक रचना की है। अपने उस्ताद द्विवेदी जी के निर्देशानुसार गुप्त जी ने ’मुसद्दस’ मँगवाया और उसे आद्योपान्त पढ़ गए। पढ़ा ही नहीं बल्कि उससे प्रभावित भी हुए। मुसद्दस के प्रभाव से ही उन्होंने 'भारत-भारती' की रचना की, जिसमें भारतवर्ष के प्राचीन गौरव, उसके अधोपतन तथा उसकी जागृति के लिए सुन्दर उद्बोधन मिलता है। इस काव्य को उन्होंने तीन खण्डों-अतीत, वर्तमान और भविष्य में विभक्त किया गया है। अतीत खण्ड में भारत के प्राचीन गौरव, भारतीयों की वीरता, विद्या, बुद्धि, कला-कौशल, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य-दर्शन आदि का गुणगान किया है। वर्तमान खण्ड में भारत की वर्तमान अधोगति का चित्रण है। इस खण्ड में सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन, साहित्य, कला आदि की अवनति का चित्रण है। भविष्यत खण्ड में भारतीयों के प्रति उद्बोधन तथा देश के प्रति मंगलकामना की गयी है। यह कृति आचार्य द्विवेदी के मार्ग निर्देशन से ही फलीभूत हुई।
 |
| मैथिली शरण गुप्त |
आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती में एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था 'कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता'। इस लेख में आचार्य द्विवेदी ने कवीन्द्र रवीन्द्र से प्रभावित हो कर साहित्य में उर्मिला की उपेक्षा का प्रश्न उठाया था। अब तक रामकथा को केन्द्र में रख कर जो भी साहित्य सृजन हुआ, उसमें उर्मिला उपेक्षित पात्र ही रही। अगर कहीं उसकी चर्चा भी हुई तो वह प्रसंगवश ही हुई, ठहर कर या उसे केन्द्र में रख कर नहीं हुई। जबकि चौदह बरस के वनवास के दौरान उर्मिला ने जो त्याग, तप और साधना का जीवन जिया और पूरे परिवार को एक सूत्र में बाँध कर रखा, वह हर भारतीय के लिए प्रेरणादायी है। अपने उस्ताद के इस लेख की भावना को गुप्त जी ने न सिर्फ महसूस किया बल्कि उस पर ठहरकर विचार भी किया। उस विषय को गुना-बुना और इसकी क्षतिपूर्ति का संकल्प लिया। उनका यह संकल्प 'साकेत' के रूप में प्रतिफलित हुआ। इस महाकाव्य में उर्मिला का चित्रण एक मर्यादित, संयमित और त्याग की प्रतिमूर्ति नारी के रूप में हुआ है। प्रारम्भमें उर्मिला अनन्य प्रेमिका है किन्तु जब लक्ष्मण श्रीराम के साथ वनवास का निर्णय लेते हैं तब वह अपने प्रेम का बलिदान देती है। वह अपने प्रिय के मार्ग में बाधा नहीं बनती बल्कि त्याग और तपस्या का मार्ग वरण करती है। उसकी वेदना गहन है, विरह की पीड़ा अत्यन्त अथाह है, किन्तु वह द्वेषरहित है। इसलिए उसका विरह अत्यन्त मार्मिक बन जाता है। विरह काल में उसके हृदय का और भी प्रसार हो जाता है। वह एक अनन्य प्रेमिका है, आदर्श पत्नी है तथा सुसंकृत कुलवधू है। इस प्रकार 'साकेत' महाकाव्य का अवतरण भी उस्ताद आचार्य द्विवेदी की प्रेरणा से ही फलीभूत हुआ।
आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती में एक लेख लिखा- 'हिन्दी की वर्तमान दशा।' इस लेख में उन्होंने यह भावना प्रकट की कि हिन्दी में भी बंगला की प्रसिद्ध कृतियों- 'प्लासी का युद्ध', 'मेघनाद वध' तथा ’वृक संहार’ जैसी रचनाएँ होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने रचनाकारों का आवाहन भी किया। गुप्त जी ने गुरु के इस आदेश को शिरोधार्य करते हुए 'प्लासी का युद्ध' तथा 'मेघनाद वध' का हिन्दी में अनुवाद किया। यह उस्ताद और शागिर्द का हिन्दी साहित्य में अप्रतिम उदाहरण है।
गुप्त जी आजीवन अपने उस्ताद का उपकार मानते रहे और समय-समय पर इसके बारे में लिखा भी और कहा भी। साकेत महाकाव्य की भूमिका में गुप्त जी लिखते हैं कि, "आचार्य पूज्य द्विवेदी जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना मानो उनकी कृपा का मूल्य निर्धारित करने की ढिठाई करना है। वे मुझे न अपनाते तो आज इस प्रकार आप लोगों के समक्ष खड़े होने में भी समर्थ होता या नहीं, कौन कह सकता है।
करते तुलसी दास भी कैसे मानस नाद?
महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद।"
जिस समय द्विवेदी जी रचनाकारों को खड़ी बोली कविता के प्रति प्रेरित कर रहे थे, उस समय ब्रजभाषा की चारों तरफ धूम मची थी। लाला भगवानदीन लगातार नारेबाजी कर रहे थे कि, "खड़ी बोली का खड़ापन कान फाड़े डालता है।" इसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट की मान्यता थी कि, "खड़ी बोली में जो कर्कशपन है, उसके कारण कविता के काम में ला कर उसमें सरसता सम्पादन करना प्रतिभावान के लिए कठिन है।" इसके विपरीत आचार्य द्विवेदी के मार्गदर्शन में गुप्त जी, हरिऔध जी तथा अन्य कवियों ने खड़ी बोली कविता लिख कर यह सिद्ध किया कि इसमें सुन्दर कविता भी लिखी जा सकती है। हरिऔध ने खड़ी बोली कविता में तीन तरह प्रयोग किये-क्लिष्ट तत्सम प्रधान खड़ी बोली, सरल तत्सम प्रधान खड़ी बोली तथा ठेठ बोलचाल की खड़ी बोली। यद्यपि हरिऔध द्विवेदी मण्डल के कवि नहीं थे किन्तु उनका रूझान खड़ी बोली की तरफ़ द्विवेदी जी एवं उनके द्वारा सम्पादित 'सरस्वती' के कारण ही हुआ। उनका 'प्रियप्रवास' खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बना।
लक्ष्मीधर वाजपेई’ तथा ज्योति प्रसाद मिश्र ’निर्मल’ ने नागरी प्रचारिणी सभा के ’द्विवेदी अभिनंदन ग्रन्थ’ में एक निबंध लिखा था जिसका शीर्षक है–’आदर्श संपादक द्विवेदी जी’। इसमें एक टिप्पणी दृष्टव्य है - “द्विवेदी जी स्वयं तो लिखते ही थे, और संपादन-कार्य में घोर श्रम भी करते थे; परंतु साथ ही साथ वे नए-नए लेखक और कवि भी बनाते चलते थे। उनकी पैनी नजर उनके उन्नत ललाट की बड़ी-बड़ी भौंहों के नीचे के तेजस्वी नेत्रों की मर्मबेधिनी दृष्टि नहीं, बल्कि उनके मस्तिष्क के भीतर की पैनी दृष्टि- भारतवर्ष के हिंदी-संसार में बहुत दूर विदेशों के भी हिंदी जानने वालों में अपने लिए लेखक ढूंढ़ा करता था। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों में भी उन्होंने हिंदी-लिखने वालों को ढूंढ़ा और जो लोग विदेशों में रह कर हिंदी को भूले हुए थे, शायद हिंदी लिखना भी बहुत कम जानते थे, उनसे भी हिंदी के लेख लिखवा-लिखवा कर मंगाए। और, उन लेखों की भाषा अपने सांचे में ढाल कर लेखकों को ऐसा उत्साहित किया कि उनमें से कई लेखक आज भी हिंदी संसार में चमक रहे हैं। द्विवेदी जी ने सैकड़ों लेखकों को, जिन्हें कोई जानता भी न था, 'सरस्वती' द्वारा मैदान में लाकर खड़ा किया। श्री मैथिलीशरण गुप्त, 'शंकर' जी, हरिऔध जी, राय साहब 'पूर्ण' जी, पंडित रामचरित उपाध्याय, पंडित लोचन प्रसाद पांडेय, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, पंडित गिरिधर शर्मा 'नवरत्न', पंडित गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही', पंडित रूप नारायण पांडेय, ठाकुर गोपाल शरण सिंह आदि यशस्वी कवियों को प्रकाश में लाने वाले द्विवेदी जी ही हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु की 'भानु की झाँकी' द्विवेदी जो ने ही 'सरस्वती' में दिखलाई। द्विवेदी जी ने ही पहले-पहल 'श्रीधरसप्तक' लिख कर पंडित श्रीधर पाठक का गौरव बढ़ाया।" इसी लेख में उक्त लेखकद्वय आगे लिखते हैं कि “स्वनामधन्य 'भारतेंदु' जी के बाद अपने ढंग की भाषा-शैली द्विवेदी जी ने विशेष रूप से चलाई। व्याकरण-विशुद्ध भाषा लिखने पर सदैव जोर दिया। आजकल के सैकड़ों लेखक करीब-करीब उसी शैली पर चल रहे हैं। 'प्रताप' के तेजस्वी संपादक स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी तो द्विवेदी जी को अपना एक ही परम गुरु मानते थे और अपना प्रत्येक कार्य द्विवेदी जी का आशीर्वाद ले कर करते थे। वे द्विवेदी जी के ही अखाड़े में तालीम पाए हुए एक विशेष व्यक्ति थे।“
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आचार्य द्विवेदी यद्यपि कोई घोषित उस्ताद नहीं थे किन्तु युगीन रचनाकारों को प्रेरणा देकर, उनकी भाषा का संस्कार कर, कुछ रचनाकारों की रचनाओं को सँवार कर, तराश कर कुशल उस्ताद की तरह उनका मागदर्शन किया। उनके संकेत-सूत्र को पकड़ कर कई रचनाकार यशस्वी बने। अगर हिन्दी साहित्य में आचार्य द्विवेदी की तरह की भावना और उनके मण्डल के रचनाकारों की तरह का जिज्ञासु भाव बना रहता तो कुछ और बात होती। हिन्दी साहित्य में उस्ताद-शागिर्द की परम्परा अब नहीं है। किन्तु साहित्य में जब कभी जिक्र होगा, तो हिन्दी जमात का यह आख़िरी उस्ताद अपने सभी शागिर्दों के साथ साहित्य में ऐतिहासिक महत्त्व का अधिकारी होगा। सचमुच वे हिंदी जगत के आखिरी उस्ताद हैं।
********
(सरस्वती पत्रिका के हालिया अंक से साभार।)
सम्पर्क :
मोबाइल : 9454257709


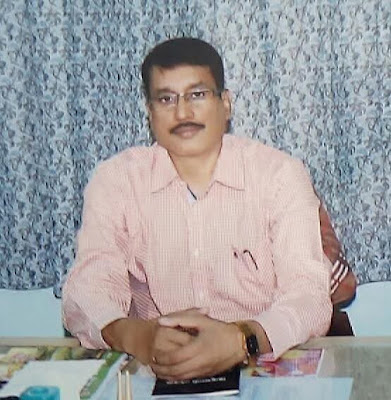



टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें