पंकज मोहन का आलेख 'हरदेवी कथा'
 |
| पंकज मोहन |
'सीमंतनी उपदेश' ऐसी किताब है जिसकी मूल प्रति में किसी भी लेखक का नाम नहीं है। शोधकर्ता चारु सिंह ने यह दावा किया कि उन्होंने ही पहली बार यह खोज किया कि इस किताब की लेखिका हरदेवी हैं। रमन सिन्हा और गरिमा श्रीवास्तव के गम्भीर आलेखों के आने के बाद उन पर स्रोतों के इस्तेमाल को ले कर आरोप भी लगाए गए। हाल ही में शोधकर्ता पंकज मोहन ने अपने अध्ययन के आधार पर उद्घाटित करते हैं कि " 'इन्डियन मैगजीन' के जून 1889 के अंक मे तीन हिन्दी-उर्दू पुस्तक की समीक्षा छपी, लेकिन समीक्षक का नाम सिर्फ तीसरी पुस्तक की समीक्षा के नीचे छपी। मेरी दृष्टि में तीनो पुस्तकों के समीक्षक पिन्काट थे। एक पुस्तक बालवाड़ी या किंडरगार्टन शिक्षा से सम्बद्ध थी जिसकी रचयिता हरदेवी थीं। इसी समीक्षा में फ्रेडरिक पिन्काट ने हरदेवी को "सीमंतनी उपदेश" नामक पुस्तक (जिसकी लेखिका का नाम पुस्तक में कहीं भी अंकित नहीं था) की रचयिता बताया। चारु सिंह अगर इस महत्वपूर्ण शोध सामग्री से परिचित होती, तो यह दावा नहीं करती कि "सीमंतनी उपदेश" की लेखिका की खोज सबसे पहले उन्होंने की। इसका श्रेय इन्डियन मैगजीन के हिन्दी-उर्दू पुस्तकों के समीक्षक फ्रेडरिक पिन्काट को जाता है।" पंकज जी का मानना है कि "कोई भी अर्थवान सारस्वत यज्ञ किसी एक व्यक्ति की प्रतिभा या परिश्रम के बल पर पूरी तरह सम्पन्न नहीं होता। विद्वान एक दूसरे के परिश्रम और अन्तर्दृष्टि का आदर करेंगे, तभी हरदेवी-विषयक शोधकार्य आगे बढेगा।" इस बात में सच्चाई भी है। तो आइए आज पहली बार पर हम पढ़ते हैं पंकज मोहन का आलेख 'हरदेवी कथा'।
'हरदेवी कथा'
पंकज मोहन
एशिया के दूसरे देशों में पितृसत्तात्मक समाज के अंकुश और अन्याय के विरोध में स्त्रियों ने अपने विरोध का परचम बीसवीं सदी के आरम्भ में फहराया, लेकिन भारत में उन्नीसवीं सदी के अंत में ही स्त्री-मुक्ति आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। हरदेवी स्त्रियों के हक के लिये संघर्ष करने वाली हिन्दी समाज की पहली महिला लेखिका हैं, लेकिन शोध सामग्री के अभाव में अभी तक उनके जीवन और कर्म पर ठोस काम नहीं हो पाया है। चारु सिंह ने 2015 में 'आलोचना' में प्रकाशित अपने लेख मे समय की रेत पर बिखरे हरदेवी के चरणचिह्न को खोजने का स्तुत्य प्रयास किया है और तदुपरांत रमण सिन्हा ने कुछ नई शोध सामग्रियों के आधार पर हरदेवी के जीवन पर नई रोशनी डाली है, लेकिन चूंकि अभी भी हरदेवी हमारे लिये एक पहेली ही बनी हुई हैं। चारु सिंह हरदेवी-विषयक अपने शोध को 'सेमिनल' मानती हैं, लेकिन उन्होंने हरदेवी के जीवन के अनेक महत्वपूर्ण प्रसंगों के बारे में जो लिखा है, वह भ्रामक है।
चारु सिंह के अनुसार विधवा हरदेवी रोशन लाल से लंदन में मिली, उनकी शादी 1890 ई में हुई, और विवाह के शीघ्र बाद इलाहाबाद के बैरिस्टर रोशन लाल ने लाहौर हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। चारु सिंह ने यह भी लिखा कि लाहौर में बसने के बाद रोशन लाल ने "ख़ुद को आर्यसमाज के सांगठनिक कार्यों से दूर ही रखा"। समय के अभाव के कारण आज मैं सिर्फ उपरोक्त विन्दुओं पर सिलसिलेवार ढंग से विचार करूंगा।
आर्यसमाज के स्त्रोत के अनुसार श्रीमती हरदेवी और रोशन लाल का विवाह कन्हैया लाल अलखधारी के प्रयत्न से सम्पन्न हुआ था। कन्हैया लाल अलखधारी ने 1877 में स्वामी दयानन्द सरस्वती की पंजाब धर्म-प्रचार यात्रा का आयोजन किया था और उनके भागीरथ प्रयत्न के बल पर ही पंजाब में आर्य समाज की सुदृढ आधारशिला तैयार हो पाई थी। कन्हैया लाल अलखधारी ने 1881 में हरदेवी की पहली पुस्तक "सीमंतनी उपदेश" प्रकाशित की थी, किन्तु इस पुस्तक के प्रकाशन के एक साल बाद ही वे स्वर्ग सिधार गये थे। मेरी दृष्टि में उन्होने अपनी मृत्यु के ठीक पहले 1881 में रोशन लाल जो उस साल लाहौर गर्वनमेंट कालेज में बी. ए. अंतिम वर्ष के छात्र थे, और आर्य समाज से गहराई से जुडे हुए थे, को पी. डब्लू. डी. के एक्जीक्युटिव इन्जीनियर कन्हैया लाल की पुत्री हरदेवी से परिचित कराया। वकालत की पढाई के निमित्त लंदन यात्रा करने के पूर्व दोनों शादी या सगाई कर चुके थे। संभवतः विवाह को गुप्त रखने की विवशता के कारण हरदेवी रोशन लाल के साथ लंदन नहीं गई, लेकिन इंग्लैंड की पत्रिका "इन्डियन मैगजीन" ने मई, 1886 के अंक में हरदेवी, उनके भाई सेवाराम, भाभी और उन दोनों की छोटी बेटी राधिका, जिनका विवाह कालांतर में पटना हाईकोर्ट के बैरिस्टर सच्चिदा नंद सिन्हा से हुआ, के लंदन प्रवास की खबर एक साथ छापी (WELCOME TO THE NEWLY ARRIVED HINDU LADIES IN LONDON)। लोकलाज के कारण विधवा की सगाई/ विवाह के समाचार को गुप्त रखा गया, लेकिन लंदन के लोगों की आंखों के आगे यह सम्बन्ध उजागर हो गया। चारु सिंह कहती हैं कि दोनो की शादी 1890 में हुई, लेकिन अगर ऐसा होता, तो 1888 में जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुन कर वह अपने भाई के साथ स्वदेश लौटीं, तो लाहौर में अपनी मां के पास क्यों नहीं रही? वह रोशन लाल के साथ रहने इलाहाबाद क्यों आयीं। इस संदर्भ में इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि उन्होने 1888 में इलाहाबाद से 'भारत भगिनी" पत्रिका के प्रकाशन का श्रीगणेश किया। 1932 में जब रोशन लाल की मृत्यु हुई, सच्चिदानंद सिन्हा की पत्रिका "Hindustan Review" ने लिखा कि हरदेवी के साथ उनका विवाह 1890 में सम्पन्न हुआ, लेकिन इसी पत्रिका में 1906 में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित था कि 1890 में उन दोनों की शादी का "announcement" या प्रचार हुआ और 1890 से ले कर 1892 तक बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेक अखबारों ने हिन्दू समाज की मर्यादा को तोड़ने वाली इस प्रबुद्ध दम्पति की भर्त्सना की। 1892 तक भी यह गुप्त विवाह पूरी तरह से प्रच्छन्न नही हो पाया। 1892 में आस्ट्रेलिया के अखबारों में प्रकाशित एक रिपोर्ट में हरदेवी का परिचय "भारत की दुखिया स्त्रियों के कल्याण के लिये प्रयासरत धनी विधवा" के रूप में दिया गया।
लाला रोशन लाल ने पांच अन्य कर्मठ कार्यकर्ताओं के सहयोग से 18 अप्रैल 1886 को लंदन में आर्य समाज की नींव रखी और इसी वर्ष जून में आयोजित आर्यसमाज के अधिवेशन में उन्होने आर्यसमाज के तीसरे नियम - वेद के अध्ययन-मनन के महत्व- पर व्याख्यान दिया। इस सभा में संस्कृत, उर्दू और हिन्दी के सुधी अध्येता फ्रेडरिक पिन्काट ने भी व्याख्यान दिया। फ्रेडरिक पिन्काट का जीवन चरित बाबू श्याम सुन्दर दास ने "हिंदी कोविद रत्नमाला" में और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 1908 में "सरस्वती" पत्रिका और कालांतर में "हिन्दी साहित्य का इतिहास" में प्रस्तुत किया। हरदेवी को लाहौर में प्रिंसिपल नवीन चन्द्र राय (आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक) की सुपुत्री हेमंत कुमारी देवी जो "सुगृहणी" पत्रिका की सम्पादिका थी, का सुखद सान्निध्य प्राप्त था और वह ब्रह्मसमाज की सभाओं में भाग लेती थीं, लेकिन कन्हैया लाल अलखधारी की प्रेरणा के फलस्वरूप वह निश्चित रूप से आर्य समाज से भी जुडी हुई थीं। चारु सिंह इस तथ्य को नजरअंदाज करती हैं। मेरा अनुमान है कि हरदेवी ने लंदन में आयोजित आर्य समाज की सभाओं में भाग लिया और यहीं उनकी भेंट पिन्काट साहब से हुई। हरदेवी ने उन्हें अपनी पुस्तकें भी दी होंगी। पिन्काट भारतेन्दु हरिश्चन्द्र समेत उन्नीसवीं सदी के सभी प्रमुख साहित्यिकों के मित्र थे। उन्होंने भारतेन्दु को ब्रजभाषा पद्य में एक पत्र लिखा था जिसकी आरंभिक पंक्ति है:
"वैस-वंस-अवतंस श्री बाबू हरिचंद जू।
छीर नीर कल हंस टुक उतर लिखि देव मोहि।।"
"हिंदी के यूरोपियन विद्वान: व्यक्तित्व और कृतित्व" पुस्तक मे अनुसार पिन्काट साहब "इंडियन मैगजीन' के हिंदी पुस्तकों के समीक्षक थे और इस रूप में उन्होंने "समकालीन साहित्य से बराबर परिचित रहने की चेष्टा की।" आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी यह लिखा है कि वे इंग्लैंड से निकलने वाले मैगजीन में हिन्दी साहित्यकारों की पुस्तकों का परिचय देते थे। 'इन्डियन मैगजीन' के जून 1889 के अंक मे तीन हिन्दी-उर्दू पुस्तक की समीक्षा छपी, लेकिन समीक्षक का नाम सिर्फ तीसरी पुस्तक की समीक्षा के नीचे छपी। मेरी दृष्टि में तीनो पुस्तकों के समीक्षक पिन्काट थे। एक पुस्तक बालवाड़ी या किंडरगार्टन शिक्षा से सम्बद्ध थी जिसकी रचयिता हरदेवी थीं। इसी समीक्षा में फ्रेडरिक पिन्काट ने हरदेवी को "सीमंतनी उपदेश" नामक पुस्तक (जिसकी लेखिका का नाम पुस्तक में कहीं भी अंकित नहीं था) की रचयिता बताया। चारु सिंह अगर इस महत्वपूर्ण शोध सामग्री से परिचित होती, तो यह दावा नहीं करती कि "सीमंतनी उपदेश" की लेखिका की खोज सबसे पहले उन्होंने की। इसका श्रेय इन्डियन मैगजीन के हिन्दी-उर्दू पुस्तकों के समीक्षक फ्रेडरिक पिन्काट को जाता है। उन्होंने ही इस तथ्य को पब्लिक डोमेन में लाया। "ideasofindia.org" डाटाबेस में इस समीक्षा का रेफरेंस उपलब्ध है, लेकिन लेखिका का नाम 'हरिदेवी' दिया हुआ है। सबसे पहले रमण सिन्हा ने अपने लेख में हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया।
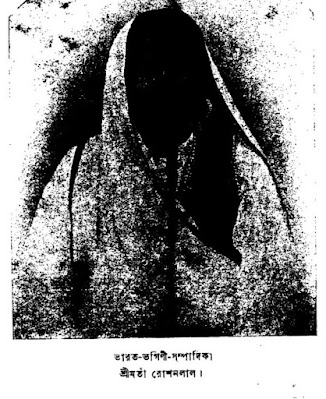 |
| ढाका से निकलने वाली पत्रिका "भारत महिला" (1910) मे हरदेवी का चित्र छपा था। संलग्न चित्र की छायाप्रति धूमिल है, लेकिन उसके नीचे "भारत- भगिनी-सम्पादिका श्रीमती रोशनलाल" अंकित है। |
चारु सिंह के अनुसार रोशन लाल और हरदेवी विवाह के शीघ्र बाद 1892 के आस पास लाहौर चले गये, लेकिन उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती। 1892 के बाद "भारत भगिनी" पत्रिका में प्रकाशन स्थान का नाम लाहौर छपने लगा, लेकिन अनेक साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1898 तक रोशन लाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते रहे और जैसा कि सच्चिदा नंद सिन्हा ने अपने एक लेख में लिखा रोशन लाल 1899 में लाहौर हाई कोर्ट में शिफ्ट हुये।
बंगला में एक पुस्तक है "ভারত-মুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অর্ধশতাব্দীর বাংলা" (भारत मुक्तिसाधक रामानन्द चट्टोपाध्याय और अर्धशताब्दी का बांग्ला)। इस पुस्तक में रामानन्द बाबू (1865-1943) के परिवार और हरदेवी-रोशनलाल के आपसी पारिवारिक सम्बन्ध का उल्लेख है। रामानन्द चट्टोपाध्याय बांग्ला और अंग्रेजी की सर्वाधिक लोकप्रिय पत्रिका, क्रमशः प्रवासी और Modern Review के संस्थापक-सम्पादक थे और उन्होने बाद में हिन्दी पत्रिका "विशाल भारत" भी निकाली। 1895 में वे इलाहाबाद कायस्थ पाठशाला के प्रिंसिपल नियुक्त हुये थे और 1897-98 में "इलाहाबाद के साउथ रोड में हरदेवी और रोशन लाल उनके पडोसी थे। रामानन्द चट्टोपाध्याय की धर्मपत्नी हरदेवी से हिलमिल गई थीं। जब दोनो महिलायें मिलती थीं, हिंदी और बंगाली साहित्य के बारे में कभी-कभी विचार-विमर्श करती थी। एक दिन हरदेवी ने कहा, "देखिए, कितना सुंदर हिंदी उपन्यास निकला है!" मिसेज चट्टोपाध्याय ने स्वाध्याय के बल पर हिंदी पढ़ना सीख लिया था। वे मुहावरेदार हिंदी बोल लेती थी और उनका उच्चारण भी शुद्ध था। हरदेवी से उन्होंने वह हिंदी किताब ली और देखा कि किताब का शीर्षक था "सास और पतोहू", और लेखक का नाम था गोपाल राम। कुछ ही पन्ने पढ़ने के बाद श्रीमती चट्टोपाध्याय समझ गईं कि गोपाल राम ने शास्त्री महाशय की पुस्तक "মেজ বৌ" को हिन्दी मे अनूदित कर उसे अपने मौलिक ग्रंथ के रूप मे छपवा लिया है। पुस्तक में मूल लेखक के नाम का जिक्र कही भी नहीं था। उन्होंने यह बात हरदेवी को बताई। हरदेवी को कुछ बंगाली आती थी। वे अपनी पत्रिका में बंगाली लेखों के अनुवाद को भी स्थान देती थीं। 1895 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट मे भी रोशन लाल का नाम वकील के रूप में अंकित है
1897 में मद्रास में आयोजित Theosophical Society के वार्षिक अधिवेशन के प्रतिभागी रोशन लाल का परिचय "बैरिस्टर फ्रौम इलाहाबाद" के रूप में मिलता है, लेकिन उन्होंने 1899 के पन्द्रहवें कांग्रेस अधिवेशन में "लाहौर हाईकोर्ट के बैरिस्टर आर्य समाज प्रतिनिधि" के रूप में हिस्सा लिया।
1899 में लाहौर में बसने के बाद रोशन लाल ने आर्यसमाज की सांगठनिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। 1992 में वे आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाव तथा सीमाप्रांत स्थान लाहौर के मंत्री बने। वे सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, परोपकारिणी सभा, गुरुकुल कांगडी विद्यालय आदि आर्यसमाज की संस्थाओं को नेतृत्व दिया और लाहौर आर्यसमाज के प्रधान भी रहे। बीसवीं सदी के आरंभिक वर्षों में ब्रिटिश पत्रकार Valentine Chirol जब पंजाब की राजनैतिक गतिविधियों पर रिपोर्ट तैयार करने लाहौर आया, लाला रोशन लाल ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की कि आर्यसमाज भारत के नैतिक और धार्मिक उत्थान के प्रति समर्पित है और राजद्रोह से उसका कोई सम्बन्ध नही है। इसकी चर्चा Chirol ने 1910 में प्रकाशित अपनी पुस्तक "Indian Unrest" में की।
हरदेवी के कार्य का उल्लेख बंगला की "वामाबोधिनी" पत्रिका या "भारत महिला पत्रिका" में ज्यादा हुआ। हिन्दी समाज हिन्दू मूल्य और मर्यादा पर कुठाराघात करने वाली हरदेवी के स्वागत के लिये तैयार नहीं था। जैसा कि रमण सिन्हा के लेख का शीर्षक है, वह भारत की विस्मृत समाज सुधारिका हैं। यह सुख का विषय है कि अहमदाबाद की चारु सिंह, जे एन यू के रमण सिन्हा और गरिमा श्रीवास्तव, दिल्ली विश्वविद्यालय की आरती मिनोचा और कोलम्बिया विश्वविद्यालय के अमन कुमार जैसे सुधी जन हरदेवी के व्यक्तित्व और कृतित्व के विभिन्न पक्षों को प्रकाश में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कोई भी अर्थवान सारस्वत यज्ञ किसी एक व्यक्ति की प्रतिभा या परिश्रम के बल पर पूरी तरह सम्पन्न नहीं होता। विद्वान एक दूसरे के परिश्रम और अन्तर्दृष्टि का आदर करेंगे, तभी हरदेवी-विषयक शोधकार्य आगे बढेगा।
पैतीस साल पहले अपने आक्सफर्ड प्रवास के दौरान धर्मवीर ने "सीमंतनी उपदेश" का उद्धार किया। गरिमा श्रीवास्तव ने 2019 में लन्दन की ब्रिटिश लाइब्रेरी से हरदेवी की दो पुस्तकें "लंदन यात्रा" और "लंदन जुबिली" खोज निकालीं और वहां उन्हे "स्त्रियो पै सामाजिक अन्याय" नामक निबन्ध भी मिला। हरदेवी के जीवन और कर्म से सम्बद्ध हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी सामग्रियां डिजिटल फार्म में साउथ एशियन आर्काइव, आर्काइव और्ग और अमेरिका-यूरोप के प्रमुख पुस्तकालयों में उपलब्ध है। कुछ पुराने समाचार पत्र और पत्रिकाएं नेहरू मेमोरियल म्युजियम ऐंड लाइब्रेरी (अब प्राइम मिनिस्टर म्युजियम) में उपलब्ध है। गरिमा श्रीवास्तव ने ब्रिटिश लाइब्रेरी मे उपलब्ध हरदेवी की दो पुस्तकों को प्रकाशित कर हिन्दी लोकवृत में रुचि रखने वाले शोधार्थियों का उपकार किया है। वीरभारत तलवार की पुस्तक या/ और चारु सिंह के शोध आलेख को पढ कर गरिमा श्रीवास्तव ने ब्रिटिश लाइब्रेरी जा कर हरदेवी की रचनायें ढूंढी होगी और अपने वरिष्ठ सहकर्मी रमण सिन्हा के साथ इन पुस्तकों पर चर्चा की होगी और कुछ वर्षों के बाद गरिमा श्रीवास्तव की पुस्तक को पढ कर आरती मिनोचा अपनी अनूदित तथा सम्पादित पुस्तक "The Travel Writings: London Yatra and London Jubilee" तैयार करने के लिए प्रेरित हुई होंगी। अगले वर्ष जब आरती मिनोचा की पुस्तक बाजार मे आयेगी, पश्चिम जगत के लोगो को भारतेन्दु काल की महिला की विश्वदृष्टि को गहराई के साथ जान पायेंगे। शोध के क्षितिज को विस्तार देने की यही प्रक्रिया है। शोधकर्ता फुटनोट में उत्कृष्ट शोध आलेख या शोधग्रंथ का रेफरेंस देते हैं लेकिन साथ ही मूल श्रोत के सम्यक विश्लेषण के आधार पर वे वर्तमान शोध की सीमा को रेखांकित करते हैं और अपने शोध की नूतन दिशा को नियमित करते हैं। मैंने भी इस लेख में हरदेवी के जीवन-प्रसंग पर प्रकाश डालने वाले एक शोध आलेख की सीमा को पहचाना, लेकिन मै यह भी मानता हूं कि हिन्दी और अंग्रेजी में हरदेवी पर लिखने वाले उपरोक्त सभी विद्वानों और विदुषियो ने अपने अपने ढंग से यात्रा साहित्य, जेन्डर अध्ययन आदि क्षेत्रों के विकास मे योगदान दिया है। आलोचना में प्रकाशित चारु सिंह के लेख, तद्भव में प्रकाशित रमण सिन्हा के लेख और समालोचन में प्रकाशित गरिमा श्रीवास्तव के लेख में प्रयुक्त अनेकानेक श्रोत समान हैं, इसलिए उनमें कुछ मुद्दों पर विचार साम्य है। कुछ पाठक यह कह सकते हैं कि इन आलेखों में असवाधानी या जल्दीबाजी के कारण एक-दो जगहों पर समुचित रेफरेंस नहीं दिये गये हैं, लेकिन मुझे सुनियोजित शोध कदाचार का प्रमाण नहीं मिला। मैं तीनो लेखों को पढ कर समृद्ध हुआ।
----------------------



टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें