अवंतिका प्रसाद राय की कविताएं
 |
| अवंतिका राय |
महानगरीय सभ्यता ने प्रकृति से ले कर मनुष्य सबको बुरी तरह प्रभावित किया है। निश्छल मन इससे आक्रांत होता है और खुद को बिलग महसूस करता है। विजय बैगा हो, सुदामा बंसफोर या फिर स्वयं कवि इन सारे बदलावों का साक्षी होते हुए भी हतप्रभ है। समय की सुई पीछे नहीं घूमती। वह हमेशा आगे ही देखती और चलती है। लेकिन यह बात मानीखेज है कि कुदरत के होने से ही इस समय और समय की सुई का अस्तित्व है। कवि अवंतिका राय ने कम लिखा है। और लिखने से भी बहुत कम छपे हैं। वे एक सजग, सतर्क और उस मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिसमें सबके लिए समान जगह और सम्मान बचा हुआ है। आइए आज पहली बार पर पढ़ते हैं कवि अवंतिका राय की कविताएं।
अवंतिका प्रसाद राय की कविताएं
बच्चे और खिड़कियां
मकानों में
खिड़कियां
ढूंढ़ ही लेते हैं
बच्चे
उठो
उठो
जैसे पूरब से उठता है
सूरज
पृथ्वी को
जीवन देते हुए
जैसे उठता है
कहानियों का नायक
चतुर्दिक
अपनी आभा
बिखेरते हुए
और
लड़ता है निर्णायक युद्ध
ऐसे उठो
जैसे
उठता है गुलाब
उठता है वृक्ष
असंख्य प्राणियों का आश्रय बन
अपने जीवन से
जीवधारियों का
प्राण स्पंदित करते हुए
उठो
जैसे उठता है शिक्षक
बच्चों को मंत्रमुग्ध करते हुए
लिखता है श्यामपट पर
और
स्मृतियों में बस जाती है
कोई बात
कोई कविता
कोई सिद्धान्त
या फिर
कोई कहानी
उठो
जैसे नचिकेता
जैसे ब्रूनो
गैलिलियो
राबिया या सुकरात उठे
नवोन्मेष के साथ
बनाते पृथ्वी को
निरन्तर सुन्दर और चेतस
ऐसे
जैसे
उठे थे राम
और वचन के लिए
निकल गये थे जंगल
उठना
जैसे
बच्चे को
कन्धे पर बिठाए
उठता है पिता
जैसे
उठती है मेह
प्यासी धरती को
तृप्त करते हुए
जैसे मां
ममता से भर
अपने छौने के लिए उठती है
और लगाती है
अपने स्तन से
ऐसे उठना
जैसे बुद्ध की आंखें उठीं
अपार करुणा से भर
ऐसे तो कत्तई न उठना
जैसे उठता है
अहंकारी
जैसे उठता है
अल्पज्ञानी
जैसे उठती है
गलाजत
जैसे लहरा कर
उठता है सांप
जैसे उठती है जड़ता
उठने के लिए तो
बांधना पड़ता है
अपने वेग को
जैसे अंकुर बांधता है, ललक के साथ
सूरज तक पहुंच
जाने के लिए
आत्मवृत्त
महसूसता हूं
इस बार की मार
अपने स्नायुतन्त्र पर
घेरती है स्नायविक कंपकंपाहट,
पीठ पर
झन्न झन्न करता है कुछ
आते हैं चक्कर गोल गोल
बैठता हूं
फिर उठता हूं
किसी से, कहीं भी नहीं कच्चा अपनापन
अज़ीब तरह का लेप पर लेप लगा हुआ इन्सान!
नहीं है किसी के
उद्बोधन में कोई शक्ति
एक टटकापन
न
नहीं बात करनी मुझे
पीठ दिखाते
निरुपाय
मनुष्यों से
अड़ कर
जो लड़ सके
ऐसा समूह
दिखा था
पंचनद के किनारे
क्या गंगा और यमुना में
सचमुच नहीं बचा है
कोई दम
या फिर
चुल्लू भर साफ पानी
रसोईघर से रसमंजरी
रसातल!!
हर तरफ भय का साम्राज्य
हर तरफ कालिख का कब्जा,
आदमी अपनी टुच्ची पिपासा में
नहीं देख पा रहा
दूर तलक
नहीं आते उसकी कल्पना में
सुलझे सुन्दर देश
बेशर्म
घिस गये फिल्मी गीतों पर बात करते
पुरस्कृत होते नराधम
कहते हैं
कमान संभालेंगे
जिन्हें शीर्षक देने का शऊर नहीं
वे नेतृत्व का दम भर रहे हैं,
अब कवित्त कहने से
बात नहीं बनेगी
ऐ मेरे कवि
लाओ
शब्दों में
गोली दागने का शऊर
(क्षमा आलोक धन्वा!)
लाओ
गोली दागने का शऊर
और निकल पड़ो
समाप्त होने तक
खून का ठंढापन
अपनी नदियों की मलिनता
अपनी कंपकंपाहट
व्यक्त करो!
व य क्त करो!!
व य क्त करो!!!
कहीं नहीं है आदमी
वह यहां नहीं
मर चुका है
विराट प्रकृति और जानवरों के बीच रहना ही
अब श्रेयस्कर है
जीवन पाता हूं
सिर्फ वृक्षों
चिड़ियों और
पांत के आख़िरी लोगों से,
शब्दों की कारीगरी
वाक्यों की लसलसाहट
और भावों की खरीद फरोख्त मे खो जाती है
सद्तर्क की पावन धारा!
वकालत की भाषा बोलते अनगिन लोग
हर मोड़ पर दिखते हैं
सेना, मशीन और फौजफाटे के बाद भी
उनका अवचेतन भरा हुआ है
ख़ौफ से
ऐसा लगता मानो पास का
सब कुछ बुझ गया हो
और आसमान से बहुत दूर
किसी नक्षत्र लोक से
झिलमिल
टिमटिमाता
दीख पड़े
प्रकाश
कहते हैं
सच्चे आह्वान से
फरिश्ते भी रूख कर लेते हैं
कुछ इसी उम्मीद पर
प्रकाशपुंज के स्वप्न
देखता है मेरा मनुष्य
फिर से बसे
उचट गया है मन
जैसे दीवाल छोडती है
वर्षों पुरानी रंगाई की पपडी
मन को फिर बसाना
कितना कठिन है इस महानगर में!
प्रकृति रंगरेज है
पर कितनी बची है इस महानगर में
ढूंढता हूं बूढा बरगद
ढूंढता हूं चिडियों को
ढूंढता हूं रंभाती गाय
ढूंढता हूं कुलांच मारते हिरन
ढूंढता हूं सफ्फाक बहती नदी
ढूंढता हूं आत्मीय आदिवासी
जिससे मन कुछ लसे
और उम्र के इस दौर में
एक बार फिर से बसे।
सुदामा बंसफोर
सुदामा बंसफोर अपने कुनबे के साथ
रहता है गाज़ीपुर के फ़खनपुरा गांव में
मिलता है निश्छल आत्मीयता से
'कैसे चलती है ज़िन्दगी सुदामा?'
'पांच बंसफोर एक दिन बांस की दउरी बनाते हैं,
बेचते हैं... तो एक दिन में
दो सौ रुपये मिलते हैं हाकिम!'
'कहां से आये सुदामा?'
'घुमंतु हैं हाकिम!'
'कोई कष्ट?'
'बांस नहीं मिलता... अऊर ई प्लास्टिक सौतन है हमारी!'
'का खाते हो?'
'कभी भात, कभी लिट्टी!'
'सुदामा! कुछ गा-बजा कर सुनाओगे?'
लजाता है सुदामा
'अब नहीं बजाते! पहले डफला बजाते थे!'
'सुनाओ ना डफले पर कोई गीत!'
'बहुत उदास मौसम है हाकिम! अऊर डफले को मूस ने कुतर दिया! का सुनायें?'
पास बैठी मेहरारू लोग मनुहार करती हैं
'सुनाये द हाकिम के!'
पन्नी के घर में घुसता है सुदामा
निकाल कर लाता है डफला
ढब-ढब बजाता है
और चकरघिन्नी हो जाता है
मेहरारू लोग कहती हैं
'ई अब कभी-कभी अकेल्ले बजाते हैं!
पहिले सब होते थे साथ'
बाजा बन्द होता है
'आप लोग कुछ खायेंगे-पियेंगे?'
नाहीं हाकिम! बस सरकार से कहियो कि
बांस बाहर ना भेजे!'
बचे बाकी बांस के झुरमुट से
हम बिदा लेते है,
मन ही मन बुदबुदाते हैं
कौन है सरकार?
विजय बैगा
विजय बैगा
बंभनी-सोनभद्र का निवासी था
जाहिर है आदिवासी था
उसे नहीं था कोई मोह
उसे नहीं था किसी से छोह
वह विज्ञापन से दूर था
जीवन-यापन में चूर था
वह थूरता नहीं था
घूरता सही था
वह था सरल
मनुष्यों में विरल
वह अपनों के साथ मिल-जुल कर करमा गाता था
मादल के थाप पर नाचता और नचाता था
रोज शाम को वह कच्ची महुआ पीता था
जिन्दगी को खूब-खूब जीता था
उसे यकीन था कुछ जादू-टोने पर
उसे नाज था अपने होने पर
यह तबकी बात है
जब उसके अगल-बगल झंगाठ पेड़ थे
पेड़ों में ढेर सारे खोते थे
बेशक खोतों में ढेर सारे चिड़िया चुरगुन और तोते थे
तब विजय बैगा जवान था
गोंड़ों में उसका मान-जान था
फिर एक दिन सपनीले शहर से ठेकेदार आया
बैग में भर कर जाने किसके कहने पर नोट और हार लाया
कहा 'तुम्हें नेता बनना है?
गर्मी में ठार बरसाने वाली इस कार में चलना है?"
विजय बैगा ने उस हार और कार को निहारा
धीरे-धीरे जाने क्या विचारा
फिर उस पर घोटुल की पहली रात जैसा नशा था
और वह ठेकेदार के जाल में फंसा था
फिर तो किस-किस ने उसे भरमाया
विजय बैगा खूब चकराया
अब वह राजधानी में है
उसके यार-दोस्त किसी केमिकल फैक्ट्री के जहरीले पानी में हैं
वह जिन दरख्तों को प्यार से सहलाता था
जिनके फलों को चाव से खाता था
वे ठेकेदार की मिल्कियत हैं
उसके संगी-संघाती की जमीन
कार्पोरेट की वसीयत है
जहां खिलते थे घनेरों फूल
वहां हवा में बिखरी रहती है धूल
उसके पहाड़ का अब यही हसर है
उसके सीने पर क्रसर है
चलेगी मेरी नाव!
उद्दाम लहरों पर
चलेगी मेरी नाव
लहरों से टकराते
हिचकोले खाते
पानी में गोता लगाते
बचते-बचाते
उद्दाम लहरों पर चलेगी मेरी नाव!
जहां क्षितिज से मिल रहा हो
अथाह सागर
उस पार को पतियाते
दूर किसी महानगर में बैठे दोस्त से
एकालाप में बतियाते
भूख में सुस्वाद्य रुखा सूखा खाते
उद्दाम लहरों पर चलेगी मेरी नाव!
ठोकते-बजाते
सागर की थाह पाते
चंचल हवाओं से
प्रीत लड़ाते
चन्द्रमा को आमन्त्रण दे दे कर
पास बुलाते
उद्दाम लहरों पर चलेगी मेरी नाव!
तुम कैसे लपझुन्ना
तुम कैसे लपझुन्ना मुन्ना
किस-किस का पुनपुन्ना
रात-दिन फेरे में रहते
कैसे हो धन दुन्ना मुन्ना
तुम कैसे लपझुन्ना?
तुम्हें ख़बर न दिन की मुन्ना
रात-रात करते तक-थुन्ना
तुम कैसे लपझुन्ना?
तिन्ना-तिन्ना करके रोते
बखरा लेते चौगुन्ना मुन्ना
तुम कैसे लपझुन्ना?
टेंट में रखते खोलनी घर की
और ज़िगर में चुन्ना मुन्ना
तुम कैसे लपझुन्ना?
कैसे निबहेगा घर-बाहर
तुम होते टुन-फुन्ना मुन्ना
तुम कैसे लपझुन्ना?
तुमसे है संसार में कचकच
तुम ठहरे झर-टुन्ना मुन्ना
तुम कैसे लपझुन्ना?
मधु की एक बूंद ना मन में
कैसे सुन्ना-सुन्ना मुन्ना
तुम कैसे लपझुन्ना?
रमुआ के गोलगप्पे
मिठाई की दुकान सजी है
पेट वालों की धूम मची है
सेठ मिठाई चांप रहा है
रमुआ कुछ-कुछ भांप रहा है
कितने रसगर हैं गोलगप्पे
सेठ के पेट में जाते नब्बे
बिन छीने ना काम बनेगा ओ
रमुआ रोज-रोज ललचेगा?
इक दिन उसने जुगत लगाई
कारिन्दों की सभा बुलाई
कहा कि तुमको होश नहीं है
मेहनत कर तुम सूख रहे हो
सेठ छानता रोज मलाई
फिर उसने प्रस्ताव किया कि
हक लेंगे अब पूरा भाई
सेठ को इसकी भनक लग गई
मेठ पर उसने चांप चढ़ाई
और मेठ को लालच दे कर
रमुआ को फटकार लगाई
रमुआ भी अब खूब अड़ा था
सबको ले कर खूब लड़ा था
इनके बीच में जो जो आता
कस कर जूते-लात वो खाता
अन्त में सेठ ने किया सरेन्डर
तब जा कर थम सका बवन्डर
रमुआ अब यह देख रहा है
गोलगप्पे का थाल पड़ा है
खट कर मार रहा गोलगप्पे
कारिन्दे बन गये हैं छब्बे
कैसे....कब छूटा? गिरीश बाबू!
भादो की सुबह
दिन में रात
जैसे वटवृक्ष
फुर्सत में
ढेर सारी बात
गति की अति
पूंजी जिसका पति
ऐसी रैन में भी चैन नहीं
लगा है नैन वहीं,
भादो की सुबह
चिडियों ने भी
बटोर रखे हैं
कोटर में दाने
आदमी अभागा!
चला है चबाने,
रिमझिम-रिमझिम
बरसता है पानी
गर्म है कोटर
कोटर को छू कर
गुजरती है ठंडी हवा
आदमी अभागा!
किस-किस फेर में पडा
अर्जी लेकर दौडता है,
विकास क्या धकचक और शोर है?
देखो न गिरीश बाबू
कितनी मनभावन
यह भादो की भोर है,
लखनऊ में एक नदी बहती थी
मां उसे गोमा कहती थी
भादो में
गोमा उफनती थी
अब क्या?
गिरीश बाबू!
गोमा में तुम्हारे
फेर का कलुष है,
भादो में
उछल उछल कर
गोमा में खेलना
कैसे......कब छूटा?
गिरीश बाबू!
याद करो
कब टूटा
यह सिलसिला
गिरीश बाबू!
(इस पोस्ट में इस्तेमाल की गई पेंटिंग्स विजेंद्र जी की है।)
सम्पर्क
मोबाइल - 07985325004
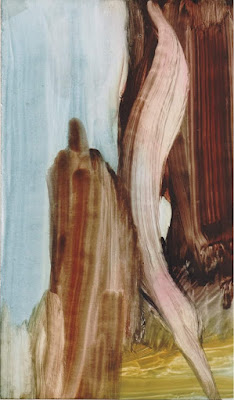





अद्भुत कविताएं हैं 🙏🙏
जवाब देंहटाएं