विनोद शाही का आलेख ‘नवजागरण: कबीर, प्रसाद और हम’।
मनुष्य की प्रगति में नवजागरण की एक विशेष भूमिका है। शाब्दिक अर्थ में ही नहीं, वास्तविक रुप में भी इसने हमें जागृत किया और वास्तविक अर्थों में हमें इंसान बनाया। हम मध्य काल से आधुनिक होने की राह पर बाकायदा चल पडे। लेकिन आधुनिकता की यह राह न तब आसान थी, न ही आज आसान है। हर जमाने में गैलीलियो जैसों को या तो अपनी खोज के लिए कट्टरवादियों के सामने माफी मांगनी पडती है, या फिर ब्रूनो जैसे जल कर मरने के लिए अभिशप्त होना पडता है। धर्म, ईश्वर, कर्मकाण्ड, चमत्कार, रहस्य वह भ्रम रचने में आज भी कामयाब हैं कि उस अलौकिक शक्ति की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यह अलग बात है कि जिन आविष्कारों और खोजों ने इस दुनिया को आज इतना बेहतरीन बना दिया है उसके पीछे मनुष्य ही है। भारतीय परिदृश्य में कबीर ने नवजागरण की शुरुआत की। तुलसी ने मानस के जरिए भक्ति को पुनर्स्थापित किया। आगे चल कर जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाधर्मिता के जरिए कबीर की आधुनिकता को रेखांकित करने का प्रयास किया। विनोद शाही एक अरसे से नवजागरण को केंद्र में रख कर गम्भीर और महत्त्वपूर्ण काम करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण आलेख लिखा है : ‘नवजागरण: कबीर, प्रसाद और हम’। इस आलेख को थम कर पढने की जरुरत है। आज पहली बार पर प्रस्तुत है विनोद शाही का आलेख ‘नवजागरण: कबीर, प्रसाद और हम’।
नवजागरण: कबीर, प्रसाद और हम
विनोद शाही
1986 में प्रकाशित अपने एक आलेख 'हिन्दी नवजागरण की समस्याएं' में नामवर सिंह ने अपने विश्लेषण का निष्कर्ष इस रूप में प्रस्तुत किया,
"न इतिहास कल्पवृक्ष है और न नवजागरण कामधेनु।"
इससे यह पता चलता है कि 1990 से पहले वाले दौर में यह विचार सामने आने लग पड़ा था कि हिन्दी नवजागरण की बात अब हमारे समय के लिए पिछले दौर की वस्तु बन गई है, जिससे भविष्य और वर्तमान की पुनर्व्याख्या के लिए अब अधिक मदद नहीं ली जा सकती।
नामवर सिंह तथा रामविलास शर्मा जिस हिन्दी नवजागरण की बात करते हैं, उसका सम्बन्ध वे 19वीं शती से जोड़ते हैं। परन्तु क्योंकि उस सन्दर्भ में की गई चर्चा भारतेंदु हरिश्चंद्र से आरंभ हो कर, महावीर प्रसाद द्विवेदी से होती हुई, रामचंद्र शुक्ल, निराला, प्रेमचंद और प्रसाद तक भी आती है, इसलिए यह माना जा सकता है कि उसका आखिरी छोर, आजादी से पहले के बीसवीं शती के पूरे कालखंड को स्पर्श करता है। तथापि इस सम्बन्ध में स्पष्ट समयक्रम का रेखांकन प्रायः नहीं हुआ है। तो सवाल उठता है कि उसके बाद के कालखंड को क्या हमें हिन्दी नवजागरण के उत्तर काल की तरह देखना चाहिए?
दूसरी समस्या 19वीं सदी से पूर्व वाले उस कालखंड के सांस्कृतिक परिदृश्य को नाम देने की है, जो 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद संन्यासी विद्रोह के रूप में प्रकट होता है। बंगाल के आधुनिक नवजागरण का आरंभ वहीं से मानना पड़ेगा। बंकिमचंद्र ने अपने उपन्यास 'आनंद मठ' में इसी ओर संकेत किया है।
हिन्दी नवजागरण को सभी चिन्तक बंगाल नवजागरण से प्रभावित मानते हैं। अंग्रेज़ राज हिन्दी पट्टी में आया भी देर से है। इसलिए उसका आरंभ 19वीं शती से मानने में अधिक दिक्कत नहीं।
पर ये सवाल खड़ा रहता है कि आजादी मिलने के बाद से ले कर 1990 तक का कालखंड किस सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित है? हम देख सकते हैं कि उस कालखंड में धर्मनिरपेक्षता, एक नई चेतना के विकसित होने का आधार हो जाती है।
परन्तु 1990 के बाद से भारत जैसे ही भूमंडलीकरण वाले नए दौर की ओर खुलता है, हालात बदलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम जितने भूमंडलीकृत होते हैं, उतने ही हम इस सवाल की ओर भी मुखातिब होते हैं कि हम दरअसल क्या हैं? एक राष्ट्र के रूप में, अपने ज्ञान के स्रोतों की नई समझ के रूप में, और विश्व में अपनी पहचान के बनने या बिगड़ने के रूप में, हम क्या हैं, यह सवाल अचानक केन्द्र में आ जाता है?
हमारा वर्तमान, हमें एक दफा फिर से, खुद को नए अर्थ में खोजने के लिए कहता प्रतीत हो रहा है। हम ऐसे हालात के रूबरू हैं, जहाँ एक तरफ हमें फिर से विश्व गुरु हो सकने के सपने दिखाये जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी चेतना जिन अस्मिताओं से निर्मित होती है, उनकी विविधता और बहुलता संकटग्रस्त स्थिति में है। पहली दिशा हमें 'सामाजिक एकरूपता' के सांचे में ढालने की ओर धकेल रही है, तो दूसरी दिशा 'ज्ञानात्मक एकरूपता' के तन्त्र में। यह बात कहने भर के लिए ठीक लगती है कि हमारे समय में विश्व पहले के मुकाबले में अधिक जनतान्त्रिक हुआ है। दलील दी जाती है कि इस जनतान्त्रिकता की वजह से अनेक प्रकार की जातीय अस्मिताएं अपने उभार के लिए अनुकूल हालात पा रही हैं।
जबकि हकीकत यह है कि सामाजिक एकरूपता का आधार बन कर प्रकट होने वाली नई तरह की राष्ट्रवादी चेतना, इन विविधताओं और बहुलताओं को अपने लिए एक तरह का खतरा मानती है। और वह जो भूमंडलीकरण वाला एक नया संसार हमारे सामने खुल रहा है, वह 'ज्ञानात्मक एकरूपता' के सहारे इनकी सांस्कृतिक विविधताओं को आत्मसात कर के आखिरकार खारिज ही कर रहा है।
राष्ट्रवादी चेतना का पूरा दारोमदार इस बात पर है कि समाज की बहुत तरह की अस्मिताओं को वह कैसे, तमाम भिन्नताओं के बावजूद, अपने जनतान्त्रिक जनाधार में बदल सकता है। प्रचलित भाषा में इसे 'वोट की राजनीति' कहा जाता है। इस तरह राजनीतिक 'मेंडेट' के आधार पर सामाजिक एकरूपता की छवि निर्मित की जाती है।
दूसरी तरफ भूमंडलीकरण जिस सूचना क्रान्ति के घोड़े पर सवार हो कर आया है, उसकी दिलचस्पी इस बात में है कि वह कैसे दुनिया भर की विविधताओं को अपने 'आभासी ज्ञान तन्त्र ' की भुजाओं में बदल सके। इस तरह सूचनाओं के 'डेटाबेस के हब्ज़' पर वर्चस्व के आधार पर यह भ्रम पैदा किया जाता है कि दुनिया भर में एक खास तरह की 'ज्ञानात्मक एकरूपता' स्थापित हो रही है।
भारत की बात करें, तो हमारे समय का मनुष्य, अब तक के इतिहास के सबसे गहन दिग्भ्रम में जी रहा है। वह समझ नहीं पा रहा है कि उसका वुजूद मूलतः स्थानीय है या वैश्विक? उसका मुख्य कर्म क्षेत्र निजी है या सार्वजनिक? उसका महत्व, उसकी अलग पहचान की वजह से है या सामूहिक पहचान के कारण? और यह भी कि उसका 'वास्तविक स्वरूप' सामाजिक समरसता वाले इतिहास-बोध को हासिल करने से प्रकट होगा, या वैज्ञानिक अध्यवसाय से अधिक कुशल और दक्ष होने पर ही निर्भर रहने के बजाय, अपनी ज्ञान परम्पराओं के मौलिक विकास से दुनिया में अग्रणी हो जाने से?
मौजूदा दौर में यह जो हमारे अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने की जरूरत से घिर जाने का मामला है, वह हमें इस प्रश्न की ओर ले जाता है कि क्या हम नवजागरण की एक और लहर के उठने के साक्षी हो रहे हैं? हम परम्परागत रूप में जिस तरह जी रहे होते हैं, वह बात अब हमारे काम की नहीं रह गई लगती है। हालात हमें जिस नयी तरह से जीने की ओर धकेल रहे हैं, वह हमें अपने 'मूल स्वरूप' से बहुत अलहदा मालूम पड़ती है। यह दुविधा समय के जिस कालखंड में, जब जब अपने अपने तरीके से प्रकट हुई है, तब तब हम एक खास तरह के नवजागरण के दौर में प्रविष्ट हो रहे होते हैं।
भारत के सन्दर्भ में इस बात को समझने की कोशिश करें, तो हमें इससे पहले की नवजागरण की लहरों की ओर देखना होगा। हम अपने वास्तविक स्वरूप की तलाश के सन्दर्भ में पहले 15वीं शती में जागे थे और फिर 19वीं शती में। 15वीं शती में मध्यकालीन नवजागरण का वह दौर सामने आया था, जिसे रामविलास शर्मा 'लोक जागरण' कहते हैं। 19वीं सदी में हमारा आधुनिक नवजागरण प्रकट हुआ था, जिसे 'सांस्कृतिक नवजागरण' और हिन्दी पट्टी को ध्यान में रखते हुए 'हिन्दी नवजागरण' कह दिया गया। यह जो दो कालखंड चिन्हित किए गए हैं, उनमें से पहले की भूमिका बनाने के लिए इस्लामी देशों के आक्रमण और उनकी संस्कृति की चुनौती को आधार के रूप में देखा जाता है। और आधुनिक नवजागरण के पीछे अंग्रेजों का साम्राज्यवादी शासन और ईसाइयत का खतरा आधार बनता है। मौजूदा दौर में इस तरह का कोई बाहरी हमला प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देता। परन्तु इसके पीछे, विकसित देशों के द्वारा लाये गयी सूचना क्रान्ति के पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया को अपना 'ज्ञान-सत्तात्मक उपनिवेश' बना लेने की, मंशा साफ देखी जा सकती है।
धर्म, संस्कृति और सभ्यता के संघर्ष वाले दौर अतीत की वस्तु हो गए हैं। अब हम इस सभ्यता-फंस्कृति मूलक परिदृश्य के एक नए 'ज्ञान-सत्तात्मक रूप' के आमने सामने हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने के सम्बन्ध में अब हमारा काम, अपनी संस्कृति सभ्यता या धर्म से जुड़ी परम्पराओं में वापसी करते हुए, या अपने इतिहास-बोध को नए रूप में उपलब्ध करते हुए चलने वाला प्रतीत नहीं होता। अब हमें अपने स्वरूप के ज्ञान-सत्तात्मक पक्ष की गहराई में उतरना पड़ेगा। अपने ज्ञान के स्रोतों की मौलिक पुनर्व्याख्या होगी। और मौजूदा दौर के ज्ञान विज्ञान के उच्च स्तर के मुकाबले में खड़े हो सकने वाले, अपने 'ज्ञान-विशिष्ट स्वरूप' को पहचानना होगा। और इस के साथ अपने भविष्य की उन संभावनाओं को खोजना होगा, जो सही अर्थ में प्रति-औपनिवेशिक (डी-कोलोनियलाइज्ड) होंगी।
यह एक तरह से अपने राष्ट्र की ही नहीं अपनी चेतना की दूसरी आज़ादी को पाने जैसा होगा।
अब हम इस खोज में निकल सकते हैं कि हमारे नवजागरण के पहले वाले दो उभारों में वे लोग कौन से हैं, जो वक्त से पहले एक भविष्योन्मुख सोच के साथ, उन समयों में भी, अपने 'ज्ञान विशिष्ट स्वरूप' को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान कर सामने आये थे। ऐसे भविष्यद्रष्टा ही आज हमारे लिए, हमारे मौजूदा दौर की चुनौतियों के बरक्स, हमारे प्रेरणास्रोत हो सकते हैं।
○○○
हमारे यहाँ घटित हुए 15वीं शती के नवजागरण का समग्रता में मूल्यांकन करते हुए लाल बहादुर वर्मा इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि
"15वीं शती में कबीर के साथ हम एक ऐसे मुकाम तक पहुंच गये थे, जो यूरोप के उस वक्त तक के रेनेसां से बहुत आगे प्रतीत होता है। वहाँ जिस तरह का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण नज़र आता है, वैसा तत्कालीन यूरोप के लिए भी समय से बहुत आगे की चीज़ था। लेकिन फिर हमारे यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि हमारा नवजागरण पटरी से उतर गया।"
अगर हम इस वक्तव्य की गहराई में जाएं, तो यह देख पाना कठिन नहीं कि हमारे अधिकांश विद्वानों ने मध्यकालीन नवजागरण को जिस तरह तुलसी केंद्रित रूप में देखने दिखाने की कोशिश की है, वह बात अगर असंगत नहीं, तो मौजूदा दौर की ज्ञान-सत्त्ता केंद्रित चुनौतियों के मद्देनज़र पुनर्विचारणीय अवश्य है।
ठीक इसी तर्ज़ पर अब हम 19वीं सदी वाले आधुनिक नवजागरण की पुनर्व्याख्या के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। उस दौर के बंगाल नवजागरण के चिंतकों के पीछे अखिल भारतीय स्तर पर एक दफा बहुत जबरदस्त ज्ञानात्मक स्फुरण हुआ था। इसने तर्क-न्याय और बुद्धि विवेक की कसौटी पर, उन तमाम बातों का विरोध किया था, जिनकी वैज्ञानिक व्याख्या संभव नहीं थी। नतीजतन केशव चंद्र सेन, राममोहन राय, रानाडे, विवेकानंद और फुले से ले कर उत्तर भारत में सक्रिय दयानंद सरस्वती तक, सभी के निशाने पर मूर्ति पूजा, अवतारवाद और सगुण भक्ति जैसी चीज़ें आ गयी थीं। यह काम बहुत हिम्मत वाला काम था। ऐसा करते हुए हम पश्चिम के ईसाइयत केंद्रित औपनिवेशिक सभ्यताकरण के चंगुल से बाहर आने के लिए बहुत दूर तक कामयाब हो चले थे।
लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, खास तौर पर उत्तर भारत के हिन्दी नवजागरण वाले रूप में, कि हमें फिर से पौराणिक वैष्णवता के भक्तिवादी रूप के प्रति नतमस्तक बनाने वाले रास्ते पर पुनः खड़ा कर दिया गया। इसके बावजूद हिन्दी नवजागरण वाले हमारे इस उत्तर भारतीय परिदृश्य में हमारी एक आखिरी उम्मीद की तरह एक रचनाकार अवश्य है। वह अपने 'ज्ञानात्मक स्वरूप' को बचाने लिए निरंतर संघर्षरत नज़र आता है। वह रचनाकार है, जयशंकर प्रसाद। लेकिन उनके असमय निधन के कारण, उनका वह प्रयास एक अधूरी रह गयी ज्ञानात्मक क्रान्ति जैसा हो कर रह गया।
तो आइए, एक कोशिश करें, पहले के नवजागरण के अपने इन दोनों रचनाकारों की मदद से अपने समय में भविष्य के गवाक्ष खोलने की। और उनके 'ज्ञानात्मक स्वरूप' की प्रेरणाओं को वर्तमान के ज्ञान-सत्तात्मक परिदृश्य में सकारात्मक हस्तक्षेप करने लायक बनाने की।
यहाँ यह स्पष्ट कर देना ज़रूरी लगता है कि यह काम परम्परावादी सोच रखने वालो में आक्रोश और विरोध के भाव पैदा कर सकता है। खास तौर पर उनमें, जिनकी सोच व्यक्ति पूजा पर ठिठकी होती है। वे व्यक्ति को बचाने के लिए मुद्दों व सरोकारों को हाशिये पर धकेल देते है। लेकिन हमें सच के करीब हो सकने के लिए यह सवाल तो उठाना ही पड़ेगा कि रामचंद्र शुक्ल का 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', कबीर को हाशिये पर रखने की कोशिश करता है और प्रसाद को अन्य छायावादी कवियों के संग, उनके रहस्यवाद की वजह से, 'अभारतीय' तक बता देता है। इन बातों के समाधान विशुद्ध साहित्यिक किस्म की अकादमिक बहसों के द्वारा संभव नहीं हैं। वहाँ तुलसी और शुक्ल के प्रति हिन्दी पट्टी का अति अनुराग, कदम-कदम पर हमारा रास्ता रोक कर खड़ा दिखायी दे सकता है। पर अगर हमें भारत के भविष्य की चिन्ता है और हमें मौजूदा दौर की चुनौतियों के बरक्स अपने वास्तविक स्वरूप की खोज में निकलना है, तो अपनी आस्थाओं को पूर्वाग्रह में बदलने से रोकना ही होगा।
○○○
19वीं शती में जब भारत यूरोप के रेनेसां से परिचित होना आरंभ हुआ, तब हमारे यहाँ यह खोज आरंभ हो गयी कि क्या भारत यूरोपीय सभ्यता के संपर्क में आने के बाद जागा है, या इस तरह का जागरण इससे पहले भी दिखाई देता रहा है?
जहाँ तक जागरण काल की बात है, वह यूरोप में ईसाई पूर्व काल वाले ग्रीको रोमन और सातवीं आठवीं शताब्दी के अरबी फारसी शामी उत्थान की तरह देखा जाता है। भारत में उसे अपने यहाँ के ईसा पूर्व कालीन औपनिषदिक एवं दार्शनिक उत्थान काल के रूप में पहचाना जाता है। फिर यूरोपीय रेनेसां 15वीं शती में घटित होना आरंभ होता है। वह वहाँ आधुनिक काल की आमद की सूचना देता है और निरंतर विकासमान होता नज़र आता है। बाद में वह 17वीं 18वीं शती में ज्ञानोदय में बदल जाता है।
तत्कालीन भारत को इस वैश्विक नवजागरण के आइने में दोबारा खोजते हुए हमारे इतिहासकार इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे यहाँ भी कबीर (1398-1518) के साथ 15वीं शती, एक महान नवजागरण की ओर खुलती है। अकबर (1542-1605) तक नवजागरण की वह प्रक्रिया विकासमान दिखाई देती है। 1582 में जब अकबर दीनेइलाही की बात करता दिखाई देता है, तो लगता है कि जैसा रामचंद्र शुक्ल ने 'तुलसीदास' पर विचार करते हुए लक्ष्य किया, कि 'कबीर के साथ 'हिन्दू मुसलमान के मिलजुल कर रहने' की जिस बात ने ज़मीन पकड़ी थी, उसका दायरा फैल रहा था। पर उसी दौर में कुछ ऐसा हुआ कि न केवल दीनेइलाही की बात ही अर्थहीन हो गयी, हिन्दू मुस्लिम समाज भी अपने धर्मों के साम्प्र दायिक पुनर्गठन में लग गये। इससे कबीर आदि से संबंधित ज्ञानधारा के, तत्कालीन साम्प्र दायिक जकड़बंदियों से आज़ाद होने के रास्ते में रुकावट पैदा हो गयी। नतीजतन उसके भीतर से विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना के विकास की संभावना का अन्त हो गया। भारत यहीं, इसी सन्दर्भ में, यूरोप से पिछड़ गया।
सत्रहवीं शती में यूरोप सत्ता पर धर्म के व्यापक नियन्त्रण को परे हटाता हुआ ज्ञान के मौलिक और स्वतन्त्र विकास की ओर अग्रसर हुआ था। ऐसा कर पाने की वजह से उसने विज्ञान के अभूतपूर्व विकास के दौर में दाखिल हो गया। लेकिन हम अपने परम्परावादी और रूढिवादी कोटि के भक्तिवादी और इस्लामी पुनरुत्थान में उलझ गये। इस वजह से हम 'अपने सीमित तरीके से मानवीय होने' और ' अपनी अपने तरह का लोकमंगल करने' के आदर्शों को, 'युग की मर्यादा' कह कर स्थापित करने में लग गये।
यहाँ इस तथ्य को नज़रंदाज़ करना उचित नहीं होगा कि हमारे देश के तत्कालीन हालात यूरोप से भिन्न थे। यूरोप हमारे मुकाबले, आर्थिक और सांस्कृतिक, दोनों धरातलों पर, पिछड़ा हुआ था। तीव्र विकास उनकी युगगत ज़रूरत की तरह उन्हें ठेल कर, पूरी दुनिया को अपने हित विस्तार के लिए खोजने की ओर ले गया था। जबकि हमारी स्थिति यह थी कि हमें खुद को संभालना भी था, आक्रांताओं के हाथों लुटने से बचाना भी था। हर्ष के मज़बूत साम्राज्य के टूटने बिखरने के बाद से हम मध्य एशियाई मुस्लिम हमलावरों के हाथों लगातार बार-बार अपनी संचित धन सामग्री को गंवाते चले आ रहे थे। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादाओं का पालन करने वाला जो समाज हमारे यहाँ विकसित हुआ था, वह अपनी इस व्यवस्था के विकास के शिखर को छू रहा था। पर विदेशी हमलों ने उस सामाजिक ताने बाने को बिखेर कर अव्यवस्था का माहौल पैदा कर दिया था। इतिहास हमें खीच कर सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा था। बिखराव ने निम्न वर्गों, हस्तशिल्पियों और छोटे काश्तकारों को भी विकास करने के अवसर देने आरंभ कर दिये थे। परम्परागत ज्ञान विज्ञान की सीमाएं स्पष्ट हो चली थीं। व्यापारिक पूँजीवाद अपने विकास के शिखर को छूने के बाद, अब यथास्थितिवादी हो रहा था। मुस्लिम हमलावरों की युद्धकला हमें पीछे छोड़ रही थी। मध्य एशिया आठवीं शती के बाद हमारे मुकाबले अधिक तेज़ी से विकासमान था। तो ऐसे हालात में 15वीं शती के आसपास हमारे समाज के निचले तबकों में एक नयी 'ज्ञानात्मक क्रान्ति' की मशाल जल उठी। मध्य एशियाई ज्ञान विज्ञान के नव उत्कर्ष से लैस, वहाँ के चिन्तनशील सूफी और फकीर, वहाँ से अपने विद्रोही तेवरों की वजह से उजड़ जाने को अभिशप्त हमारी ओर खिंचे चले आ रहे थे। वे हमारे नाथ योगियों में समय के मुताबिक रूपान्तरित होने की संभावनाओं को देख कर, उनसे घुल मिल गये थे।
रामचंद्र शुक्ल ने उस दौर के गोरखपंथियों की इस ज्ञान क्रान्ति को पहचान कर इनकी बाबत इस प्रसिद्ध कथन को उद्धृत किया है,
गोरख जगायो जोग
भक्ति भगायो लोग।
यह वह दौर था जब वर्णाश्रम व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने वाली 'भक्ति' को धत्ता बताते हुए भारत ने अपनी 'ज्ञानात्मक क्रान्ति' को, साहसपूर्वक जन-जन की वाणी में उतारना आरंभ कर दिया था। इससे भारत की उत्पादन मूलक रचनात्मकता का समाज के निचले तबकों तक विस्तार हो पा रहा था। पौराणिक वैष्णवता से बंधे हिन्दू समाज और मौलवी मुल्ला की गिरफ्त में कैद नवनिर्मित मुस्लिम समाज, दोनों के निचले तबकों ने अपने आपको इन सांस्कृतिक, धार्मिक सांस्कृतिक बंधनों से आज़ाद करना आरंभ कर दिया था। हिन्दू मुस्लिम आपसदारी के अब तक के सर्वाधिक मुक्त और उदार दौर को भारत ने न इससे पहले कभी देखा था और न बाद में।
15वीं शती इस लिहाज से सामाजिक समरसता का स्वर्णकाल मालूम पड़ती है और यही वह काल है जिसे हम अपने यहाँ बद्धमूल वर्णाश्रम मूलक मर्यादा वाले भक्तिभाव का ध्वंसकाल भी कह सकते हैं। कबीर कहते हैं।
"संतौं भाई आई ग्याँन की आँधी रे ।"
यहाँ ज्ञान से जन्म लेने वाले इस ध्वंस का जो रूपक बांधा गया है, वह देखने लायक है। इस आंधी में क्या क्या नहीं उड़ रहा है!... भ्रम, माया, द्वैत भाव, मोह, तृष्णा, कुबुद्धि, कूड़ कपाट और अंधकार… सब कुछ जो नकारात्मक है, ज्ञान विरोधी है, वह सब देखते देखते उड़ा जा रहा है:
"भ्रम की टाटी सबै उड़ानी, माया रहै न बाँधी॥
हिति चित्त की द्वै थूँनी गिराँनी, मोह बलिण्डा टूटा।
त्रिस्नाँ छाँनि परि घर ऊपरि, कुबुधि का भाण्डा फूटा॥
जोग जुगति करि संतौं बाँधी, निरचू चुवै न पाँणी।
कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जाँणी॥
आँधी पीछै जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भींनाँ।
कहै कबीर भाँन के प्रगटै, उदित भया तम खीनाँ॥"
यहाँ स्पष्ट शब्दों में द्वैत भाव को, जिसके बिना भक्ति का अस्तित्व नहीं है, कुबुद्धि के साथ रख कर उड़ा दिया गया है। इस 'ज्ञान ध्वंस' के बाद, 'ज्ञानात्मक जोग जुगत' से नयी खपरैल वाला एक नया घर खड़ा कर लिया गया है, ऐसा घर, जिसकी छत्त चूती नहीं। फिर जैसे ही यह आंधी रुकती है, प्रेम के जब की बारिश होने लगती है। फिर सूर्य निकल आता है और दुनिया में फैला अंधकार भाग खड़ा होता है।
कबीर के साथ भारत में ज्ञान की यह जो आंधी आयी थी, उसके बाद अब बारी थी, 'ज्ञानात्मक विकास' के अगले चरण के प्रकट होने की। वह प्रकट हो पाता, तो भारत तभी उसी दौर में अपने 'विज्ञान युग' में प्रवेश कर गया होता।
पर देखते-देखते प्रतिक्रान्ति घटित हो गयी। अमीर व्यापारी और देशी राजाओं को जैसे ही लगा कि वे अपने माल अफताब संभाल सकते हैं, वे फिर से मर्यादावादी वैप्णववाद का भक्तिवादी गठन करने में लग गये। शूद्र समाज के श्रम का उल्टे अब और शिद्दत से दोहन शोषण आरंभ हो गया। हस्त उद्योग और शिल्पियों के अन्तर्विकास की संभावनाएं जहाँ की तहाँ कुंठित हो गयीं। भक्ति लौट आयी और ये हुआ अकबर के काल में। हुआ यह कि वेद और कुरान जैसे पवित्र ग्रंथों को मानने वाले मुख्यधारा के लोक प्रचलित धर्म सत्ता में लौट आये। कबीर जैसे निरगुनिये, नाथ योगी और सूफी, जिन बातों से जन को निजात दिलाने चाहते थे, उन्होंने उल्टे और मज़बूती से उन्हें, उन्हीं से बांधना शुरू कर दिया। कबीर ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट समाज सांस्कृतिक विभाजन को रेखांकित किया था,
पाछे लागा जाइ था, लोक वेद के साथ
आगे ते सद्गुर मिल्या, दीपक दीया हाथ
'लोक वेद' के पीछे लगने का मतलब है, 'लोक' प्रचलित' 'वेद' विहित' धर्म संस्कृति के पीछे चलना। तो यह लोक वेद एक तरफ है और ज्ञान विवेक का 'दीपक' दूसरी तरफ है। चुनाव इन दो विकल्पों के दरम्यान करना है। तो कबीर ने ज्ञान को चुन लिया और वेद विहित कही जाने वाली लोक प्रचलित भक्ति को छोड़ दिया।
उसी भक्ति को कुछ ही समय के अन्तराल में तुलसीदास, 'नाना पुरान निगमागम सम्मत' बता कर वापिस ले आये। रामचंद्र शुक्ल ने इसे 'भारत भुवन में धर्म की पुनर्स्थापना' की तरह देखा है। निश्चित ही यह धर्म की पुनर्स्थापना थी, जिस पर अफसोस ज़ाहिर करते हुए जयशंकर प्रसाद ने लिखा कि 'तुलसी की रामायण', काव्य की तरह उतनी नहीं, जितनी एक तरह के 'धर्म ग्रंथ' की तरह लोक में प्रचलित होती है। यानी कबीर जिस 'लोक वेद' वाले रास्ते को छोड़ कर, ज्ञान विवेक के दीपक को जलाने की बात करते हैं, उसकी दिशा को तुलसीदास उल्टा कर, फिर से 'लोक वेद' की ओर मोड़ देते हैं।
कबीर और तुलसी के फर्क को अगर हम, नवजागरण के सरोकारों से न जोड़ कर, विशुद्ध 'काव्य' के तल पर ही देखने सुलझाने का प्रयास करेंगे, तो वह बात सीमित अकादमिक दायरे में घूमने वाली बात हो कर रह जायेगी। तथापि इस सम्बन्ध में अब तक ऐसा ही कुछ होता रहा है। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल प्रणीत 'हिन्दी साहित्य के इतिहास' के अधिकांश विवेचन हैं। या जैसे हाल में प्रकाशित कबीर के विशेष अध्ययन से जुड़ी पुरुषोत्तम अग्रवाल की 'अकथ कहानी प्रेम की' है। तो इससे सारी बहस अकादमिक हो कर लीक से उतर जाती है। और साहित्य की नवजागरण के सरोकारों को आगे ले जाने में जो भूमिका है, वह हाशिये पर चली जाती है।
नवजागरण के नुक्तेनिगाह से यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन कवि किस्से कितना बड़ा या छोटा है, महत्वपूर्ण यह है कि वह हमारे नवजागरण के लिहाज से कितना अग्रगामी है और कितना अवरोधक। तो, नवजागरण के कोण से सोचने की प्रक्रिया के तहत, जैसे ही कबीर के मुकाबले, तुलसी की भूमिका संदिग्ध हो जाती है, हिन्दी पट्टी के अधिकांश विद्वान अचानक यह कहते हुए तुलसी के पक्ष में आ खड़े होते हैं कि उनसे बड़ा कवि हिन्दी में कभी हुआ ही नहीं। इसलिए इस विवेचन में आगे बढने से पहले यह स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि किसी कवि का बड़ा होना और प्रबोधनकार होना, ये दो अलग बातें हैं। ज़रूरी नहीं कि जो बड़ा कवि हो, वह उतना ही रूपान्तरकारी भी हो। वह धार्मिक, सामाजिक व्यवस्था का पक्षधर, परम्परागत मूल्यों की मर्यादा का रक्षक और उन्हीं के मानवीय रूपों में लोकमंगल को खोजने वाला भी हो सकता है, जैसे कि हमारे महानतम कवि के पद पर आसीन गोस्वामी तुलसीदास हैं। ऐसा करते हुए अगर वे भारतीय 'नवजागरण के अग्रदूत' साबित नहीं होते, तो इससे उनके 'बड़े कवि' होने की बात पर कोई आंच नहीं आती। वे अपने प्रबंध कौशल, नाना मानवीय व्यवहारों के मर्मस्पर्शी अंकन और लोक व्यवहार की सामान्य नीतियों को पहचान सकने की अभूतपूर्व अन्तर्दृष्टि से युक्त होने के कारण, 'काव्य की श्रेष्ठता की कसौटी पर, बेजोड़ हैं।
लेकिन वही तुलसीदास अपने लोकमंगल के, मर्यादावादी होने की वजह से, यथास्थितिवादी होने का पता भी देते हैं। उनका लोकमंगल, 'दास्य भाव से युक्त भक्त समाज' के लोकमंगल का पर्याय हो जाता है, जिससे मनुष्य के आत्मचेतना से युक्त हो कर सत्य की खोज करने की स्वतन्त्र ता बाधित होती है। वह साहस, जो एक अन्वेषक के पास होता है, जो उसे 'गहरे पानी मैं पैठने' का आमंत्रण देता है, वह उन भक्ति भाव वाले 'बपुरों' के पास नहीं होता, जो 'किनारे पर बैठे' किसी अवतारी तारणहार के प्रकट हो ने की बाट जोहते हैं।
तुलसीदास स्पष्ट करते हैं कि 'सेवक सेव्य भाव बिनु' न 'भव से तरना' मुमकिन है, न वह भक्ति ही संभव है, जिसकी करुण कातर पुकार सुन कर त्रिभुवन में व्याप्त राम सगुण अवतारी रूप में उसकी मदद करने के लिए दौड़े चले आते हैं।
तो, ये दो दृष्टियां हैं। कबीर उस दृष्टि से सम्बन्ध रखते हैं, जो सब बंधनों से मुक्त कर के ज्ञान विज्ञान के विवेक सम्मत स्वतन्त्र अन्वेषण की ओर ले जाती है। दूसरी तरफ तुलसी की दृष्टि है, जो 'दास्य भाव' से युक्त है और दास का स्वामी के प्रति, बिना प्रश्न उठाये, समर्पण चाहती है। ऐसी दृष्टि से 'दास' बक्त, त्रिभुवन के स्वामी को पुकारता है, ताकि उसे 'प्रसाद' के रूप में वे सब ऋद्धियां सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जायें, जिन्हे 'ज्ञान की बड़ी कृष्ट साधना' से बमुश्किल पाया जाता है। ताकि सारा विकास, सारी प्रगति, बस 'नाम सिमरन' से पलक झपकते ही मुमकिन हो जाए।
तुलसी को हिन्दी के सबसे बड़े कवि के आसन पर बिठाने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को दिया जा सकता है। कवि के तौर पर वे जब तुलसीदास की व्याख्या करते हैं, तो किसी को उनके उस विवेचन से सहमत होने के रास्ते में कोई अड़चन महसूस नहीं होती। पर जब वे तुलसी को 'युग कवि' के आसन पर भी बिठाना चाहते हैं, तो सवाल उठ खड़ा होता है कि वे किस युग के किस जीवन दर्शन और समाज सांस्कृतिक रूपान्तर के सन्दर्भ में उन्हें महान बनाते हैं?
यहाँ दो बातें हैं, जिन पर शुक्ल जी बहुत बल देते हैं। वे हैं, एक, तुलसी की सामाजिकता, और दूसरी है, लोकमंगल और उसकी मर्यादा का प्रयत्न पक्ष। इनके सहारे वे 'रूपान्तर के लिए संघर्षशील होने' की बात को तुलसी के काव्य मूल्य के रूप में स्थापित करते हैं। अब हम इन बातों की गहराई में उतर सकते हैं।
तुलसी के रामकाव्य में वह जो संघर्षशीलता है, वह किसके खिलाफ है? उसके निशाने पर नाना प्रकार के लोग हैं, 'खल, कामुक, 'निशाचर' और वे लोग जो मर्यादा विहीन हो कर धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं। यहाँ उनके निशाने पर समाज के वे वर्ग और जनसमूह हैं, जिनमें ऐसे व्यवहारों के कारण 'रावणत्व' को देख पाना संभव हो सकता है। उनमें 'अलख जगाने वाले' योगी हैं, जो 'रामनाम को जपना' भूल गये हैं। इसलिए उन्हें 'नीच' कहा जा सकता है। वहाँ छल कपट करने वाले साधु भेषधारी लोग जैसे 'रावणत्व से युक्त लोग हैं, जो 'मर्यादा में रहने वाली सीताओं' को चुराने की बदनीयत से भरे 'खलकामी' हैं। मर्यादाहीन लोगों में 'अनपढ, गंवार, शूद्र और स्त्रियां' शामिल हैं, जिन्हें 'ताड़ना' से नियन्त्रित किया जाता है। तथापि सबसे ऊपर वे हैं, जो 'विधर्मी' हैं, जिनके संहार की सामर्थ्य केवल 'धनुर्धर राम' में है। भक्तों की पुकार सुन कर वे पुनः प्रकट हो सकते हैं और भारत में धर्म की मर्यादा की पुनः स्थापना कर सकते हों।
अब इन सभी कोटियों के तत्कालीन समाजशास्त्र को समझ लेते हैं। इनका सम्बन्ध मुसलमानों, नाथ योगियों, सूफियों और निरगुनियों के अलावा उस शूद्र समाज से है, जो विकासशील हो सकने की संभावनाओं की वजह से वेद विरोधी बातें करते हैं, जाति पाँति की धर्म मर्यादा को नहीं मानते और सत्य की खोज के लिए सिवाय आत्म विवेक के और किसी का शासन अनुशासन नहीं मानते। वे ऐसा इसलिए करते बताए गये हैं क्योंकि उन्हें भ्रम हो गया है कि ईश्वर उनके 'हिये में विद्यमान' है। स्पष्टतः तुलसी का यह सारा जीवन दर्शन और लोकमंगल मूलक संघर्ष तत्कालीन नवजागरण की अनेक बुनियादी प्रगतिशील प्रवृत्तियों के विरोध में जा खड़ा होता है।
जैसे ईश्वर को हृदय में विद्यमान मानने और देखने का सम्बन्ध प्रेम की जिस स्वतन्त्रता से है, तुलसी उसे स्वीकार नहीं कर पाते। वे उसे अनिवार्यतः सामाजिक पारिवारिक संबंधों के माध्यम से ही अभिव्यक्त हो सकने की वस्तु मानते हैं। निरगुनियों और सूफियों के बेशर्त प्रेम की अराजकता उन्हें स्वीकार्य नहीं है।
रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम के ऐसे रूप को 'अभारतीय' कह कर खारिज करने का प्रयास किया है। वे उसे आशिक माशूक के निर्लज्ज क्रीडा कलाप की तरह देखते हैं, जो पारम्परिक मर्यादावादी भारतीय समाज के अनुकूल नहीं है। 'पद्मावत' के प्रेम की प्रशंसा भी वे तभी कर पाते हैं, जब वह नासमझी की तरह एक भारतीय गृहिणी के मर्यादित विरह के रूप में अभिव्यक्ति पाता है। पर रतनसेन के पत्नी को पीछे छोड़ देने और पद्मावती के प्रति रूपासक्त हो उसे पाने के लिए निकल पड़ने में, जो पितृसत्तात्मक सामंतीय व्यवहार शूरवीरता देखी जाती रही है, उसे शुक्ल जी अपनी आलोचना का विषय नहीं बनाते। वहाँ उन्हें वैसी कोई निर्लज्जता दिखायी नहीं देती। प्रेम सम्बन्धी यह जो मर्यादावाद है, वह मूलतः स्त्रियों के पतिव्रता होने से सम्बन्ध रखता है। राम उनके महानायक हैं, क्योंकि वे पुरुष होते हुए भी संयमी हैं। लेकिन प्रेम की ऐसी संबंधाधारित विवध मर्यादाओं के अभाव में, किसी परम स्वतन्त्र प्रेम की मौजूदगी को वे संभव नहीं मानते।
भक्ति के लिए भी इसीलिए वे, सगुण अवतारी राम की हर काल में 'देह में उपस्थिति' का रूपक बांधते रहते हैं। शुक्ल जी अपने तुलसी को ऐसे ही भक्त के रूप में देखते हैं। तुलसी को चित्रकूट में राम के साक्षात देहगत दर्शन हुए थे, इस बात को वे 'सत्य' मानने का आग्रह तक करते हैं। शुक्ल जी तुलसी की जिस भक्ति को 'निगमागम सम्मत जीवन दर्शन' के रूप में भारतीय समाज के उच्चतम मूल्य की तरह स्थापित करते हैं, उसकी तर्कसम्मत व्याख्या तभी हो सकती है, जब हम यह मान लें कि सगुण अवतारी राम के दर्शन, दास्य भाव वाले मर्यादित प्रेम या 'प्रीति' से युक्त भक्तों को, सदैव सहज रूप में, होते रहते हैं। प्रेम के जिस रूप को दास्य भाव भक्ति की मर्यादा के तहत तुलसी और शुक्ल, भारतीय समाज के लिए उच्चतम मूल्य के रूप में अनुकरणीय बनाते हैं, उसका मनोविज्ञान उनकी निम्न धारणा में सूत्रबद्ध हो गया है,
'भय बिनु होय न प्रीति"
यह जो 'भय' है, वह तुलसी और शुक्ल के मर्यादावाद की मूलभूमि है। यह भय, भक्तों को प्रेम की मर्यादा में रखता है और दुष्टों का संहार करने की 'शक्ति' देता है। इस तरह वह शील और शक्ति की आधारभूमि बन कर, ऐसे प्रेम से उपास्य प्रभु की मूर्ति को नानाविध सौंदर्यपूर्ण छवियों से युक्त बनाता है।
"जाकी रही भावना जैसी
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी"
वह जो भयभीत होने से बचने के लिए मर्यादित है, वह उनसे प्रेम करता है और वह जो उनका शत्रु है, वह इस छवि मात्र से आतंकित, पराभूत या शांत हो कर बैठ जाता है।
स्पष्ट है कि इस मर्यादावादी प्रेम दर्शन को, तत्कालीन भारत में प्रकट समाज-सांस्कृति व राजनीतिक बिखराव और अव्यवस्था से निजात पाने के लिए, एक रास्ते की तरह चुन लिया गया। लेकिन इसने रचनात्मक प्रेम के स्वतन्त्र हो कर आत्म विकास करने की उन संभावनाओं को नष्ट कर दिया, जो भारत को ज्ञान आधारित मुक्ति पाने की ओर ले जा रही थीं। इसकी मंज़िल भारत में ज्ञान के ऐसे मौलिक रूपों के प्रकट हो सकने से संबद्ध हो सकती थी, जो हमें भी एक नये विज्ञान काल में प्रवेश के लायक बना सकते थे।
दास्य भाव भक्ति से फायदा यह हुआ कि अकबर के काल में ही देशी राजाओं ने स्वामी और दास के सापेक्ष संबंधों की बहुस्तरीय व्यवस्था को खड़ा कर लिया। यह व्यवस्था निम्न रूप में सामने आयी,
"खल्क खुदा का
हुक्म बादशाह का
अम्ल राजा का"
यह स्वामियों की कोटियों की हकीकत है। सबसे ऊपर भक्ति और इबादत की स्वीकृत पद्धतियां हैं। उनके बाद दिल्ली के तत्कालीन बादशाह का हुक्म है। फिर रियासतों के राजाओं और सुल्तानों का शासन है। सामान्यजन के लिए इन तीनों के प्रति दास्य भाव से भरे प्रेम से युक्त रहने के अलावा अपने भय से मुक्त होने का कोई विकल्प नहीं है। तो, जैसे ही यह व्यवस्था ज़मीन पकड़ती है, भारत में प्रकट हो रही नवजागरण मूलक प्रेम क्रान्ति खारिज हो कर, प्रतिक्रान्ति मे बदल दिये जाने के लिए, विवश हो कर रह जाती है।
आप देख सकते हैं कि कहाँ यह 'भय बिनु हो न प्रीति' का दर्शन है, और कहाँ कबीर का वह परम स्वतन्त्र प्रेम है, जिसे पाने के लिए उत्पादक, व्यापारी और राजा तक को 'सीस देन' की हद तक जाना पड़ सकता था। समाज के इन तीनों वर्गों के तत्कालीन स्वामियों की बाबत कबीर ने जो ललकार अपने समय में फेंकी थी, उसे उन्हीं के इस प्रसिद्ध दोहे के रूप में, अबकी दफा इन नये अर्थों को उसमें महसूस करते हुए दोबारा पढें,
"प्रेम न बाड़ी ऊपजे
प्रेम न हाट बिकाय
राजा प्रजा जेहि रुचे
सीस देय ले जाये।"
इस पूरे समीकरण में सिवाय प्रजा के सब संकटग्रस्त नज़र आते हैं। सीस बचा कर और सीस उठा कर चलने वाले तो केवल वही हैं, उत्पादक, व्यापारी सेठ और राजा लोग। प्रजा का क्या है, उसके सीस को तो रोज़ रोज़ इन्हीं तीनों कोटियों के स्वामियों के चरणों में दास्य भाव से झुकने, या फिर इरा देने का खेल चलता ही रहता है। उसे तो पता ही है कि सीस दे कर प्रेम कैसे पाया जाता है? यह एक कठिन प्रक्रिया है। अहम् से मुक्त हो कर खुद ब्रह्म हो जाने की, ताकि परम स्वतन्त्र हो कर सृष्टि की रचना और पुनर्रचना में हिस्सेदार हुआ जा सके।
पर 15वीं शती में, यह जो सामान्य प्रजा जनों में प्रेम की इतनी ऊंचाई को छू लेने की नयी 'ब्रह्म रीति' और 'ज्ञान रीति' बल पकड़ रही थी, यह 'गुसाइयों' के लिए बर्दाश्त से बाहर की बात हो गयी थी।। लेकिन थे तो वे उस वक्त 'डिफेंसिव' मुद्रा में ही। ऐसी नवजागरण मूलक हवाओं को बहने से रोकने के लिए वे नित नये तर्क ईजाद कर रहे थे,
"सगुनहिं अगुनहिं नहिं कछु भेदा" या
"अगुन बिनु जो सगुन कहै...
सो गुरु तुलसीदास"
इन तर्कों से स्पष्ट है कि उस दौर में वह जो 'ज्ञान की आंधी' आयी थी, वह क्या-क्या उड़ा कर अपने साथ लिए जा रही थी। ये तर्क इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि तुलसीदास के समय तक, गोरखपंथी जोग ने, सगुण भक्ति से लोगों को, वाकई बहुत दूर कर दिया था। इसलिए लोगों को यह समझाना ज़रूरी हो गया था कि निर्गुण और सगुण में कोई तात्विक अन्तर नही है।
लेकिन वह जो दलील है कि सगुण के बिना निर्गुण संभव नहीं, ज्ञान के विकासक्रम को सिर के बल खड़ा करने जैसी है। निर्गुण की बात सांख्य धारा के गुण विवेचन के अगले चरण के रूप में सामने आयी थी। वजह यह थी कि ज्ञान के लिए पदार्थ से कुछ अलहदगी तो होनी ही चाहिए। तो यह बात ज्ञाता के गुणातीत होने की ओर मुड़ गयी। ज्ञाता को स्वरूपतः निर्गुण और ज्ञेय को त्रिगुणात्मक मान लिया गया। इससे ज्ञान की दो कोटियां पैदा हुईं। पहली, ज्ञेय, जो ज्ञात के विस्तार से ताल्लुक रखती थी। इसे पूरी तरह निर्गुण नहीं कहा जा सकता। दूसरी कोटि अज्ञेय की थी। इसमें प्रवेश के लिए निर्गुण दशा में जाना ज़रूरी था। इस दशा में 'तत्वमसि' वाले अभेद का अनुभव संभव था। यह दशा अनादि अनंत सृष्टि के ज्ञान का प्रवेश द्वार कही जा सकती थी।
इस तरह हम देख सकते हैं कि 15वीं शती वाले नवजागरण काल में भारत ज्ञान की अनादि अनंत संभावनाओं के 'गहरे पानी में पैठने' के मंसूबे के साथ आगे बढता है। पर जल्द ही, यानी सोलहवीं शती के मध्य से इस रास्ते को अवरुद्ध करने के प्रयास होने लगते हैं। 'ज्ञान के सुविधावाद' से ताल्लुक रखने वाली भक्तिवादी दलीलों से इस ज्ञान यात्रा को रोक लिया जाता है।
भक्तिवादी यह बात पुरज़ोर तरीके से कहने लगते हैं कि अगुन और सगुन में कोई भेद नहीं होता। जिस ज्ञान को पाने के लिए निरगुनिये इतना खून पसीना बहाते हैं, उसे तो प्रभु राम के दास, 'नाम सिमरन' से जब चाहे, हासिल कर सकते हैं। रामनाम परम रसायन है, जो परम ज्ञान की दशा को सहज उपलब्ध करा सकता है। वे कहते हैं कि निर्गुण का सगुण के बिना होना संभव नहीं। यह दलील बड़ी मनोहारी है, पर अधूरी है। यह ठीक है कि पहले हमें त्रिगुणात्मक सृष्टि का ज्ञान होता है, फिर उसके बाद ही यह मुमकिन है कि ज्ञाता के स्वरूप का अनुभव, हमें निर्गुण से एकाकार होने की ओर ले जाए। यह ज्ञान के अन्तर्विकास का सही क्रम है। पर भक्तिवादी इसे उल्टा कर सैर के बल खड़ा कर देते हैं। वे कहते हैं कि निर्गुण का सगुणावतार संभव है। तो छोड़ो इस निगुने निर्गुण को, सीधे उसके सगुणावतार के दास हो जाओ। बात खत्म। ज्ञान साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं। सत्य को खोजने का झंझट क्या उठाना? सत्य खुद, प्रभु राम या नटखट कन्हैया की तरह तुम्हारे दरवाज़े पर खड़ा है। इन अवतारों ने अपनी कुंजी तुम्हारे हाथ पकड़ा रखी है। 'राम से बड़ा राम का नाम'। बस नाम जपो और पार हो जाओ। पर इसमें इतना ध्यान रखो। प्रेम के लिए बाबरे मत हो जाना। मर्यादित प्रेम करना। भारतीय रीति से। अज्ञात, अविगत, अगुन, अलख वगैरह सबको जानने का फल, सहज भाव से स्वतः मिल जायेगा।
भक्ति मार्ग की इस 'विशुद्ध भारतीय पद्धति' को रामचंद्र शुक्ल बड़े मनोयोग से इस तरह स्थापित करते हैं, मानो वही भारत का 'वास्तविक जातीय स्वरूप' हो। इसके अतिरिक्त हमारे काव्य में जो विशिष्ट है, उसे वे 'अभारतीय' कह कर अवांछित बना देते हैं। ये दो अभारतीय चीज़ें हैं, शामी देशों के प्रभाव से हमारे काव्य में प्रवेश करने वाला अराजक प्रेम, जो मनुष्य को परम स्वतन्त्र बनाता और अपनी आत्मा या सत्य को बिना किसी अवतारी पुरुष की मध्यस्थता के, सीधे हासिल होने लायक बनाता है। शुक्ल जी को वह अभारतीय लगता है, क्योंन्कि वह अमर्यादित व्यवहार है, क्योंकि वह निगमागम सम्मत प्रतीत नहीं होता, और क्योंकि उसका सामाजिक संबंधों मे अभिव्यक्ति का कोई तयशुदा रूप नहीं है। और दूसरी चीज़ जिसे वे खारिज करते हैं, वह है रहस्यवाद। यहाँ प्रकृति पर चेतना के आरोप की जो बात है, वह उन्हें ग्रीको रोमन प्रतिबिंबवाद या सूफियों के इलहाम की दशा के अनुभवों की याद दिलाती है। व्यक्ति चेतना के अन्य पदार्थों पर आरोप को वे बुद्धि विवेक सम्मत नहीं मानते। इसके बजाये वे यह कहते हैं कि अन्य पदार्थों और व्यक्तियों के साथ मनुष्य के सम्बन्ध, मूलतः 'भाव आधारित' हुआ करते हैं। इसलिए काव्य के भावन व्यापार को वे 'हृदय के विस्तार से जोड़ कर देखते हैं।
रहस्यवाद, इसके बजाय, 'चेतना या आत्मभाव के विस्तार' का सिद्धांत सै। अगर वे इस तरह के रहस्यवाद को स्वीकार कर लेते,, तो ऐसा मानने का अर्थ यह होता कि काव्य में भक्ति के भाववाद और अवतारवाद के लिए गुंजाइश समाप्त हो जाती।
अतः वे रहस्यवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि को ही नज़रंदाज़ कर देते हैं। अगर वे दार्शनिक दृष्टि से साहित्य को थाने की बात को स्वीकार कर लेते, तो प्रसाद की तरह उन्हें यह कहने में कोई दिक्कत नहीं होती कि रहस्यवाद का सम्बन्ध उपनिषदों से, तथा बौद्ध और शैव दर्शनों से है। उस ओर देखने से, जैसा जयशंकर प्रसाद ने दिखाने की कोशिश की, भारतीय संस्कृति का 'मूल स्वरूप', भक्ति के बजाय, भारतिय अध्यात्म के रूप में स्वीकार करना पड़ता।
दूसरे यही प्रेम और रहस्यवाद, चूकि कबीर और जायसी में अधिक उत्कर्ष को प्राप्त होता दिखायी देने लगता, तो कठिन हो जाता कि फिर कैसे वे, किस दलील के आधार पर, भारत की किस जातीय संस्कृति के किस मूल स्वरूप को, इस्लाम से अलहदा ही नहीं, बेहतर भी बता पाते।
शुक्ल जी का सांस्कृतिक एजेंडा स्पष्ट था। उन्हें इस्लाम को भारत के लिए खतरा बताने और साबित करने के लिए अपना चिन्तन खड़ा करना था। ऐसी भारतीय संस्कृति और साहित्य धारा का बचाव करना था, जिसमें हिन्दू पुनरुत्थान अपने मानवीय और लोकमंगलकारी रूप में मौजूद हो। और जिसे अन्य काव्यधाराओं से बेहतर बताया जा सके, खास तौर पर उनसे, जिनमें इस्लाम के प्रभाव के कारण अभारतीय प्रवृत्तियों ने जड़ें जमा ली थीं। कबीर, इसीलिए उनकी आलोचना के निशाने पर आ गये। उनका रहस्यवाद, उन्हें अमूर्त और आत्मनिष्ठ होने के कारण, अपर्याप्त विभावन व्यापार वाला मालूम पड़ता हैं। इससे, उन्हें लगता है, 'काव्योचित भाव सृष्टि' नहीं हो पाती है, जिससे सम्यक 'रस परिपाक' नहीं हो पाता। इस तरह वे अपने मत को, दार्शनिक दृष्टि की उपेक्षा करके, काव्यशास्त्रीय दृष्टि वाले मत की तरह स्थापित करते हैं। शुक्ल जी की यह चिन्तन पद्धति, बड़े सोचे समझे तरीके से, तमाम दार्शनिक विवेचनों को ही काव्य के लिए अग्राह्य बना देती है।
ऐसा किये बिना यह संभव नहीं था कि आठवीं शती से ले कर 15 वीं शती तक भारत में हिन्दू मुस्लिम संस्कृतियों के आपसी संवाद से, जिस नवजागरण के प्रकट होने के हालात ज़मीन पकड़ गये थे, उन्हें हाशिये पर डाला जा सकता।
15वीं शती के बाद के हालात ऐसे थे कि कबीर और रैदास के पीछे चलने वाले सामान्य जनों के विशाल जनसमूह, उनके नाम से प्रवर्तित 'पंथों' में शामिल होते जा रहे थे। रामचंद्र शुक्ल ने इन पंथों, मठों, संप्रदायों आदि की बहुतायत को चिन्ता का विषय बताते हुए, उन्हें भारत की जातीय संस्कृति के लिए इस्लाम के प्रभाव से उत्पन्न खतरे की तरह देखा है। पर इनकी चुनौती को देखते हुए लोगों को वैष्णव भक्ति मार्ग में फिर से लाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा था। सूर और तुलसी के सांस्कृतिक महत्व को वे इसी दृष्टि से साबित करते हैं।
भारत की इस वैष्णव भक्ति मार्ग में वापसी के लिए अकबर के दीने इलाही ने भी सहयोगी भूमिका निभायी थी। इस नये दीन धर्म की प्रतिष्ठा के इरादे से अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादतखाने में सभी धर्मों को एक मंच पर ला कर आपस में संवाद करने और किसी सांझे रास्ते को अपनाने के लिए कहा था। पर वह प्रयोग असफल हुआ। उस प्रयोग की असफलता का एक कारण यह लगता है कि वहाँ उन लोगों को नुमांइदगी नहीं दी गयी, जो पहले से ही ऐसे सांझे उलूम या धर्माचरण की दिशा में आगे बढ चुके थे। इस सन्दर्भ में निरगुन संत और सूफी सबसे आगे थे। दीने इलाही की धारणा उन्हीं के रास्ते को सत्ता समर्थन देने जैसी होती, तो उसकी सफलता में कोई सन्देह नहीं था। पर अकबर ने वहाँ बुलाया, वैष्णव हिंदुओं को, मुल्लाओं मौलवियों को, बौद्धों और जैनियों को। यानी वहाँ भारतीय समाज के कुलीन वर्गों के प्रतिनिधि पहुंचे, जिन्हें अपने अलग धर्मों को पुनर्गठित कर के, फिर से सत्ता परिदृश्य में महत्वपूर्ण होना था। दीने इलाही भारत के उस जन सामान्य की आवाज़ होता, जो नवजागरण की चेतना से अनुप्राणित थी, तो भारत का भविष्य कुछ और होता। संभवतः हम भी यूरोप की तरह अपने नवजागरण की संभावनाओं को ठोस वैज्ञानिक ज़मीन दे पाने लायक हो जाते। पर अकबर ने जो चाहा, तमाम नेक मंसूबों के बावजूद, उसके नतीजे उसकी उम्मीद के उलट निकले। वह एक उदारवादी बादशाह था, पर कुलीन समाज से घिरा था। आखिरकार मुख्यधारा की कुलीन धर्म संस्कृति की विजय हुई। जनजागरण की संभावनाओं को धीरे-धीरे हाशिये पर धकेला जाने लगा। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि सोलहवीं शती के भक्तिकाल से कबीरपंथ और रैदासी संप्रदाय के गद्दीनशीनों में भक्तिवादी लोगों की घुसपैठ हो गयी। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी 'घर जोड़ने की माया निबंध में बताते हैं कि मूर्तिपूजा और अवतारवाद विरोधी कबीर की मूर्तियां बन गयीं और उन्हें भी एक अवतारी पुरुष में बदल दिया गया। यही नहीं कबीर के नाम से अनेक ऐसे पद प्रचलित किये कराये गये, जो उनके भी भक्तिवादी होने का भ्रम पैदा कर सकें। एक पद तो जो उनका उपहास उड़ाने के लिए किसी वैष्णव भक्त ने रचा था, खुद कबीर के रचे पद के रूप में विख्यात हो गया,
"कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नांव
गले राम की जेवड़ी, जिस खींचे तित जांव।"
15वीं शती के हमारे नवजागरण का ऐसा दुखद अन्त, अन्ततः भारत के दुर्भाग्य का जनक सिद्ध हुआ। अकबर काल में ही देशी राजाओं ने वैष्णव भक्तिमार्ग के नवगठन के लिए प्रयास आरंभ कर दिये थे। यूरोप के सौदागर भारत आने लगे थे। जलमार्ग के रास्ते खुल रही विकास की इन्ही संभावनाओं का लाभ हमारे व्यापारिक पूँजीवाद को मिलना आरंभ हो गया था। परिदृश्य धीरे धीरे बदलने लगा था। दिल्ली दरबार के धीरे धीरे कमज़ोर होते जाने से, हिन्दू राजा और नबाब आपस में लड़ झगड़ कर व्यापारिक पूंजी का अधिकाधिक लाभ उठाने की फिराक में रहने लगे थे।
मध्यकालीन नवजागरण के ठुस्स हो जाने से सामान्य जन का, निचली जातियों और तबकों के शिल्प उद्योग और उत्पादन का हाल खराब होता जाता था। मुनाफाखोर व्यापारी उनका शोषण करने लग गये थे। ज़मीनी स्तर का आर्थिक विकास जहाँ का तहाँ रुका पड़ा था। विकास के लिए नयी वैज्ञानिक शोध और तकनीकों की ज़रूरत थी, पर हमारे हुक्मरान आपस में लड़ रहे थे। भारत अगर बचा हुआ था तो गांवों की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बल पर बचा हुआ था। पर राष्ट्रीय राजनीति और व्यापारिक पूँजीवाद अपने व्यक्तिगत हितों से आगे देखने की स्थिति में नहीं रह गये थे।
ऐसे में 18वीं शती के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक इरादों का राजनीतिक विस्तार करती हुई बंगाल पर काबिज़ हो जाती है। वहाँ के नबाब की पीठ पीछे खड़ी हो कर कंपनी जब वहाँ टैक्स या लगान वसूली के नाम पर सबको लूटने लगती है, तो हमारे लोगों की आंख अचानक खुलती है। मंदिरों के चढावों के एक हिस्से पर गुज़र बसर करने वाले दानाई संन्यासी तक ये देख कर हैरान हो जाते हैं, कि मंदिर तक सरकारी नियन्त्रण में चले गये हैं। मुफ्त का माल अब किसी के लिए नहीं बचा। तो संन्यासी विद्रोह करते हैं। भक्तिवाद की परीक्षा का समय आ जाता है। शंकराचार्य के पंचायतन विधि से पूजित अवतारों को, प्रकट होने के लिए पुकारा जाता है। सूर्यवंशी, वैष्णव, शक्तिसाधक, रामभक्त और तमाम अन्य अवतारों पर दृढ आस्था रखने वाले लोग, नबाब के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। बंकिम चंद्र इस बाबत 'आनंदमठ' में बताते हैं कि उन्हें यह लगता है कि उनके असल दुश्मन मुसलमान हैं। हिन्दू अवतारों ने अंग्रेज़ों को देवदूत बना कर, उन्हीं की मदद के लिए भेजा है। जब वे इस्लामी शासन का देश से अन्त कर देंगे, तो अंग्रेज़ उन्हें उनका देश सौंप देंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि अंग्रेज़ किस तरह की कूटनीति का सहारा ले कर हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा रहे हैं और अपना साम्राज्य विस्तार करते जाते हैं। अंग्रेज़ों की इस चाल को सबसे पहले बंगाल समझता है। फिर वह जागता है और वहाँ 19वीं शती का हमारा आधुनिक नवजागरण प्रकट होता है।
2
बंगाल नवजागरण को ध्यानपूर्वक देखने से यह बात आसानी से समझ में आ जाती है कि कैसे भारत एक दफा फिर से उसी रास्ते पर चलता दिखायी दिया, जिस पर कभी कबीर ने चलने की हिम्मत दिखायी थी। मूर्ति पूजा, अवतारवाद और भक्तिवाद, एक दफा फिर से हमारे नवजागरण के निशाने पर आ गये। हम साफ देख पा रहे थे कि हमारे अग्रविकास के रास्ते के मुख्य अवरोधक कौन से हैं? वह क्या है जो हमें हमारे ज्ञान के स्रोतों मे वापसी करने से और उनका मौलिक रूप में नव विकास करने से रोकता है? किस वजह से हम अपनी जिज्ञासाओं को खुला नहीं छोड़ पाते और परम्परागत धारणाओं व मान्यताओं पर साहसपूर्ण पुनर्विचार करने और उन पर प्रश्न उठाने का साहस नहीं जुटा पाते? अंग्रेज़ों को अपने बीच पा कर हमें समझ में आ गया था कि हमारी स्वतन्त्रता, विकास और प्रगति की कुंजी हमारे अपने हाथ में थी, पर हमने खुद उसे पराये हाथों में सौंप दिया था। हमें ज्ञान के मामले में परजीवी हो कर जीने की सुविधा ने घेर लिया था। हम 'भगवद् प्रसाद' की तरह पायी चीज़ों से ही सन्तोंष करके, जीने की आदत का शिकार हो चुके थे। भक्तिवादी मानसिकता वाले लोगों को इस बात से, कि उनका शासक कौन है, तब तक कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जब तक वह उन्हें, राज भक्त बने रहने के एवज में, सुख सुविधा देने का वादा निभाता है। भगवद भक्ति और राज भक्ति में आता कम फासला होता है कि आप उसे फ्वतन्त्र चेता हुए बिना देख पाने में समर्थ नहीं हो सकते। आज की तरह उस दौर में भी हम यह देख नहीं पा रहे थे कि अतीत में विश्वगुरु होने का दावा करने वाला भारत, अपनी बाबत उस छवि के मिथ्या निर्माण से ही खुश हुआ रह सकता है। अब उसके भीतर स्वयं अपने बूते ज्ञान का ऐसा विकास करने की ख्वाहिश तक मिट गयी थी कि वह विज्ञान के धरातल पर अब फिर से पूरी दुनियां से आगे निकल सकता है। ऐसे हालात में भारत को नींद से जगाना ज़रूरी था।
19वीं शती के हमारे नवजागरण के चिंतक देख पा रहे थे कि हमारी नींद की असल वजह, हमारे भक्तिभाव से आंखें बंद कर के यथार्थ से मुंह चुराने की प्रवृत्ति में छिपी थी। पर उस नींद को तोड़ने के लिए ज़रूरी था, हमारी मूर्तिपूजा और अवतारवाद में आस्था को छिन्न भिन्न करना। यह अवतारवादी भक्तिभाव अकबर कालीन हालात में प्रभुत्व में आ गया था। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के उद्भव पर विचार करते हुए, उसके प्रभुत्व में आने की वजह यह बतायी थी कि अपने इससे हमें, अपनी घोर निराशाओं से उबरने में मदद मिली थी। पर शुक्ल जी की यह धारणा 16वीं शती के मध्य में प्रकट राम भक्ति और कृष्ण भक्ति पर ही लागू होती है। तब से ले कर 19वीं शती तक इसका प्रभुत्व बना रहता है।
पर शुक्ल जी की भक्ति के उद्भव की धारणा के आधार पर हम कबीर जैसे निरगुन संतों और सूफियों की निर्भीक और ओजस्वी वाणी की व्याख्या नहीं कर सकते। वे किसी तरह की निराशा के शिकार दिखायी नहीं देते। उल्टे वे सत्ता के कंधों पर सवार हर तरह की परम्परागत धार्मिकता का, उनकी संस्थाओं और पूज्य ग्रंथों तक का खंडन करने का साहस दिखाते हैं। राजा तक को चुनौती देते हैं कि अगर उसे प्रेम से पाये जा सकने वाले सत्य की झलक चाहिए तो उसे अपना सिर उतार कर रख देने को तैयार होना पड़ेगा।
तब सवाल है कि शुक्ल जी का वह समाज कौन सा है, जो निराशा से युक्त हो कर भक्ति की शरण में चला गया था? ज़ाहिर है शुक्ल जी भारत के समान्य जन की कोटि में आने वाले हिन्दू मुसलमानों की चित्तदशा को नहीं, यहाँ सवर्णों और कुलीनों में व्याप्त भावों को, भय और निराशा के अंधकार में डूबने की तरह, पहचान रहे थे। उन्हें इस निराशा से बचाने के लिए भक्ति भाव में ठौर तब मिला, जब अकबर के उदार साम्राज्य में उन्हें, मनसबदारियां मिलनी आरंभ हो गयीं। तब वे अपनी अलग और विशिष्ट पहचान को अपने वैष्णववादी भक्तिवाद के रूप में उत्कर्ष की ओर ले गये। रामचंद्र शुक्ल इस महती कार्य को करने में सर्वाधिक मददगार साबित होने वाले सूर और तुलसी को इसीलिए पूरे हिन्दी के शिखर कवियों के रूप में स्थापित करने के लिए भगीरथ प्रयास करते हैं।
इस विवेचन से यह बात साफ हो जाती है कि शुक्ल जी की धारणा से मेल खाने वाली भक्ति का उद्भव काल 16वीं शती के मध्य का है, न कि 15वीं शती का। 15वीं शती को, इसके बजाये, हम भारत के पहले नवजागरण के उद्भव काल की तरह देख सकते हैं।
परन्तु यहाँ सवाल यह उठता है कि वह कार्य जो 16वीं शती के उत्तरार्द्ध में तुलसी और सूर को करने लायक लगा, उसका महत्व स्थापित करने के लिए रामचंद्र शुक्ल बीसवीं शती में क्यों इतनी गहन निष्ठा का परिचय देते हैं। वे यह काम उस दौर में करते हैं, जब उनके पीछे 19वीं शती के नवजागरण के चिंतकों की एक लंबी कतार है, जो इस भक्तिवाद,मूर्तिपूजा और अवतारवाद के विरोध में खड़ी है। ऐसे करते हुए नवजागरणकार, भारतीय समाज में सुधार कर सकने लायक होने का प्रयास करते हैं। सामाजिक सुधार के लिए वे वेद शास्त्रों, पुराणों और अन्य पवित्र माने जाने वाले बहुत से ग्रंथों की अनेक स्वीकृत धारणाओं को चुनौती दे रहे थे। उस आधार पर वे विधवा विवाह, वेश्या उद्धार, बाल विवाह विरोध, अस्पृश्यता विरोध, स्त्री शिक्षा, अन्तर्जातीय विवाह, जातिप्रथा विरोध आदि के लिए गुंजाइश पैदा कर रहे थे। स्पष्ट है कि ऐसा करते हुए वे तुलसी की बहुत सी मर्यादावादी धारणाओं के, उनके वर्णाश्रम समर्थन के, दास्य भावमूलक मानसिकता के, संबंधों के पितृसत्तात्मक रूप के और सेवक सेव्य भाव वाली स्वामिभक्ति जैसे मूल्यों के अगर सीधे विरोध में नहीं भी खड़े थे, तथापि वे इन सब से असहमत तो निश्चित ही दिखायी दे रहे थे। इस नवजागरण मूलक परिदृश्य में तत्कालीन हिन्दी साहित्य किस दिशा में आगे बडा, इस पर अभी गंभीरतापूर्वक विवेचन होना बाकी है।
हिन्दी पट्टी के उस दौर के सांस्कृतिक परिदृश्य को रामविलास शर्मा 'हिन्दी नवजागरण' कहते हैं। यह बंगाल और शेष भारत के नवजागरण से काफी अलग दिखायी देता है। यहाँ तक कि इसकी मुख्य प्रवृत्तियां शेष भारत के नवजागरण के सरोकारों से, कई दफा विचलन का शिकार होतीं और कई दफा उसकी धार को कुंद करती तक दिखायी देती हैं।
यही वजह है कि हमें नवजागरण के नुक्ते निगाह से उस काल पर विचार करते हुए रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद के पुनर्मूल्यांकन तक जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि जिसे हम हिन्दी जाति का नवजागरण कहते हैं, उसके शीर्ष पुरुष अपने व्यापक सरोकारों की वजह से यही दो लोग हैं। ये अपने उस दौर के अन्य रचनाकारों, जैसे प्रेमचंद और निराला की तुलना में, युग प्रवृत्तियों के अधिक समर्थ व्याख्याकार हो जाते हैं, हालांकि साहित्यिक महत्व की दृष्टि से उनकी चर्चा इनकी बनिस्बत अधिक नज़र आती है।
हिन्दी नवजागरण को सम्यक रूप में समझने के लिए नामवर सिंह के आलेख 'हिन्दी नवजागरण की समस्याएं' को देखा जा सकता है। इस आलेख में कुछ ऐसी बातें हैं, जिनसे हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि हिन्दी नवजागरण भारत के शेष भागों के नवजागरण के मुकाबले में लीक से थोड़ा नीचे उतरा क्यों नज़र आता है? बावजूद इसके कि जो दावा किया जाता है, वह यह है कि हिन्दी नवजागरण का सम्बन्ध ज्ञान के उत्कर्ष काल से है। नामवर सिंह लिखते हैं कि
"महावीर प्रसाद द्विवेदी की 'सरस्वती' ज्ञान की पत्रिका कही गई है और उनका गद्य हिन्दी साहित्य का ज्ञानकांड। इस प्रकार भारत का उन्नीसवीं शताब्दी का नवजागरण यूरोप के 'एनलाइटेनमेंट' अथवा 'ज्ञानोदय' की चेतना के अधिक निकट प्रतीत होता है।"
तथापि जैसे जैसे नामवर हिन्दी नवजागरण के ज्ञानकांड की गहराई में उतरते हैं, वे पाते हैं,
"हिन्दी नवजागरण में प्रखर बुद्धिवाद की प्रधानता भी संदिग्ध ही दिखाई पड़ती है।"
क्या कारण है? एक कारण यह है कि उत्तर भारत में कोई बड़ा नवजागरणमूलक चिंतक दिखाई नहीं देता। इस अभाव की पूर्ति हिन्दी के साहित्यकारों को करनी पड़ती है, जो बहुत अपर्याप्त सिद्ध होती है। इस सम्बन्ध में नामवर सिंह कहते हैं,
"हिन्दी प्रदेश में नवजागरण का कार्य मुख्यत: स्वयं लेखकों और साहित्यकारों को ही संपन्न करना पड़ा क्योंकि यहाँ बंगाल और महाराष्ट्र की तरह प्रखर समाज-सुधारक और विचारक अगुआई करने के लिए नहीं मिले। हिन्दी प्रदेश को मिले भी तो दयानंद सरस्वती जिनकी भूमिका का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उन्नीसवीं शताब्दी के बड़े हिन्दी लेखकों में से एक भी उनसे प्रभावित न हो सका।
जहाँ तक दयानंद सरस्वती के द्वारा उत्तर भारत में किये गये नवजागरण के प्रयासों का सम्बन्ध है, उनका इस क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर तो व्यापक प्रभाव दिखायी देता है, पर हिन्दी के लेखक साहित्यकार अगर उनसे प्रभावित नहीं हुए, तो यह बात साबित हो जाती है कि हिन्दी नवजागरण, नवजागरण की सामान्य लीक और चाल, दोनों से रहित था। दयानंद सरस्वती से प्रभावित हो कर लाला लाजपत राय और भगत सिंह जैसे लोग औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के खिलाफ जिस राष्ट्रीय चेतना से ओत प्रोत हो कर संघर्षशील हुए, उसका हिन्दी लेखकों साहित्यकारों की निगाह में कोई बड़ा मूल्य क्यों नहीं था? स्त्री शिक्षा के सुधारवादी काम में दयानंद सरस्वती की विरासत अभूतपूर्व परिणाम लायी थी। जिसे आज हम हिन्दी का आधुनिक खड़ी बोली वाला रूप कहते हैं,उसके विकास के लिए, हिन्दी को समर्पित आरंभिक छापेखानों में से एक, आर्यसमाज के प्रयासों से लाहौर में खोला गया था। और सबसे बढ कर बात यह है कि जिसे हम आधुनिक भारतीय नवजागरण का प्रखर बुद्धिवादी रूप कहते हैं, वह दयानंद सरस्वती के 'सत्यार्थ प्रकाश' के 'खंडन मंडन' वाले प्रसंग में, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। इसके निशाने पर वह पौराणिक वैष्णववाद भी था, जिसे दयानंद 'कपोल कल्पित' मानते थे। इसलिए हिन्दी पट्टी के लेखकों साहित्यकारों के लिए इस तरह के बुद्धिवाद से जुड़ने की बात, शायद जितने बड़े साहस की मांग करती थी, उसके लिए वे तैयार नहीं थे। वे इसके साथ खड़े होने के बजाये, अपनी परम्परागत कूप मंडूकता में आश्रय खोजने लग गये थे। नामवर सिंह ने इस सन्दर्भ में लक्ष्य किया है कि
"हिन्दी से उदाहरण लें तो भारतेंदु की वैष्णव-निष्ठा सर्वविदित ही है। सन् 1884 ई. में जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने 'वैष्णवता और भारतवर्ष' शीर्षक से एक लंबा लेख लिख कर सप्रमाण सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि 'वैष्णव मत ही भारतवर्ष का मत है और वह भारतवर्ष की हड्डी, लहू में मिल गया है।'
वैष्णव भक्तिवादी मनोवृत्ति के इस प्रभुत्व को, हिन्दी नवजागरण के लीक से उतर जाने के मुख्य कारण की तरह रेखांकित किया जा सकता है। इसी कारण हिन्दी पट्टी का साहित्यिक परिदृश्य दयानंद के विरोध मे खड़ा होता होता, आखिरकार बुद्धिवाद विरोधी परम्परावादी यथास्थितिवाद के प्रभाव को ग्रहण करता दिखायी देने लगता है। वह अपने नवजागरणमूलक स्रोतों तक की ठीक से पहचान करने में इसीलिए असमर्थ दिखायी देता है। इस सन्दर्भ में नामवर सिंह द्वारा उद्धृत एक रोचक प्रसंग नीचे उद्धृत किया जा रहा है,
"स्वयं भारतेंदु दयानंद की अपेक्षा बंगाल के केशव चंद्र सेन को श्रेयस्कर समझते थे। 1885 ई. में लिखित 'स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन' शीर्षक लेख में भारतेंदु दयानंद के बारे में यह निर्णय देते हैं कि उन्होंने 'जाल, को छुरी से न काट कर जाल ही से काटना चाहा,' जबकि केशव ने इनके विरुद्ध जाल काटकर परिष्कृत पथ प्रकट किया।' केशव चंद्र सेन के महत्तर होने का कारण यह है कि भारतेंदु के मन के अनुकूल केशव ने 'अपनी भक्ति की उच्छृखलित लहरों में लोगों का चित्त आर्द्र कर दिया।"
आश्चर्य है कि केशव च॔द्र सेन का बहाना बना कर दयानंद का विरोध करते वक्त भारतेन्दु को यह कैसे भूल गया कि केशवच॔द्र तो स्वयं मूर्तिपूजा, अवतारवाद और वैश्णववाद के विरोध में खड़े थे। प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज में निराकार ब्रह्म को पुकारने के लिए अगर वहाँ किंचित भावातिरेक की गुंजायश दिखायी दी, तो वे आर्यसमाज की यज्ञ पद्धति पर भी एक नज़र डाल लेते, जो अमीचंद के रस में सराबोर कर देने वाले भजनों के लिए विख्यात थी। उसके गाये 'अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में', जैसे भजनों की लोकप्रियता उस दौर में फिल्मी संगीत की ऊंचाई को छूती मालूम पड़ रही थी। लेकिन यह जो हिन्दी पट्टी का बुद्धिवाद विरोधी साहित्यिक नवजागरण था, वह अपने वैष्णव भक्तिवाद को सर्वोपरि मानने की वजह से, हिन्दूवादी पुनरुत्थान हो कर रह जाती है। नतीजतन यह हिन्दी नवजागरण, भारतीय नवजागरण को अपने यहाँ, हिन्दू और मुस्लिम नवजागरण के रूप में दोफाड़ कर देता है। नामवर सिंह ने इसे भी लक्ष्य किया है,
"हिन्दी प्रदेश के नवजागरण के संमुख यह बहुत गंभीर प्रश्न है कि यहाँ का नवजागरण हिन्दू और मुस्लिम दो धाराओं में क्यों विभक्त हो गया… हिन्दी प्रदेश का नवजागरण धर्म, इतिहास, भाषा सभी स्तरों पर दो टुकड़े हो गया।
स्वत्व रक्षा के प्रयास धर्म तथा संप्रदाय की जमीन से किए गए।"
पर ऐसा नहीं है कि हिन्दी नवजागरण अपनी समग्रता में, नवजागरण के रूपान्तरकारी सरोकारों के उलट जा कर खड़ा हो जाने की वजह से, साम्प्र दायिक कहा जा सकता है। इसके दो रूप दिखाई देते हैं। एक वह, जो वैष्णववादी भक्तिवादी हिन्दू पुनरुत्थान के लिए प्रयासरत था। इस धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष व्यक्तित्व के रूप में हम रामचंद्र शुक्ल को देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे साहित्यकार भी थे, जो शेष भारत के नवजागरण के मूल सरोकारों के साथ खड़े थे। वे विज्ञानवाद की अहमियत समझते थे। वे भारत के मूल स्वरूप की तलाश हमारे यहाँ मौजूद ज्ञानमूलक और दार्शनिक परम्पराओं के भीतर से कर रहे थे। और अपनी राष्ट्रीय चेतना के स्रोत के रूप में, 'वसुधैव कुटुंबकम' वाली समरसता मूलक दृष्टि को ग्रहण करके, हिन्दू मुस्लिम विभेद को कम करने का प्रयास करते थे। हिन्दी नवजागरण की इस धारा के प्रतिनिधि के तौर पर हम जयशंकर प्रसाद की बात कर सकते हैं।
यहाँ यह कहना ज़रूरी लगता है कि यह जो वैष्णव भक्तिवादी हिन्दू पुनरुत्थान वाला हिन्दी नवजागरण है, वह भारतेंदु को औपनिवेशिकता विरोध के मामले में भी दोफाड़ करता है। वे भारत दुर्दशा के कारण के रूप में अपने धन के विदेश चले जाने से चिन्तित हैं, पर 'अंग्रेज़ राज सुख साज सजे सब भारी' कह कर अपनी राजभक्ति का परिचय देना भी नहीं भूलते। इस धारा का यह जो अन्तर्विरोध है, उसे रामचंद्र शुक्ल में भी साफ पहचाना जा सकता है। इसके विस्तार में आगे सप्रमाण बात की जायेगी। फिलहाल यहाँ यह देखना दिलचस्प होगा कि नामवर सिंह हिन्दी नवजागरण के इस अन्तर्विरोध को किस रूप में देखते हैं,
"अंग्रेजी राज का घोर विरोध करने वाला वर्ग धर्म-संस्कृति आदि नैतिक-सामाजिक मान्यताओं में या तो मूलगामी है या फिर सुधारवादी। प्रथम भारतीय होने का दावा करता है तो दूसरा पश्चिमोन्मुख है।"
यहाँ जिस पश्चिमोन्मुख दूसरी धारा की बात है, वह इन्हीं वैष्णववादियों की है। पर हैरानी की बात यह है कि 'अंग्रेज़ी राज का घोर विरोध करने वाले दयानंद सरस्वती और जयशंकर प्रसाद जैसे पहली धारा के लेखक साहित्यकार, नामवर सिंह जैसे प्रगतिशील आलोचक को भी, 'मूलगामी' मालूम पड़ते हैं। ऐसा मुख्यतः इस वजह से है कि वैष्णवता विरोध वाली ज्ञानधारा कबीर से ले कर प्रसाद तक, हिन्दी नवजागरण के इस विशिष्ट परिदृश्य में बहुत से लेखकों के लिए दुविधा का कारण है, ऐसी दुविधा, जिसमें न रहते बनता है, न निकलते। नामवर सिंह अपनी इसी दुविधा के कारण, ताउम्र कबीर और तुलसी के बीच, कभी इधर, तो कभी उधर डोलते दिखाई देते हैं। 'दूसरी परम्परा की खोज' वाली अपनी किताब को वे गुरू के ऋण से उऋण होने की तरह देखते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि वे 'बुद्धि से खुद को कबीर के निकट पाते हैं, पर हृदय में तो तुलसी का ही वास है।'
लेकिन कबीर और तुलसी में विभाजित हो कर रह जाने से ताल्लुक रखने वाली यह दुविधा, हमारे समकालीन लेखकों के लिए तो अब एक बौद्धिक खेल हो सकती है, पर रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद के लिए यह युगबोधक संकट की तरह है। उसमें इधर या उधर होने का मतलब है, नवजागरण के सरोकारों से जुड़ना या अलग होने का निर्णय लेना।
19वीं शती में नवजागरण के चिंतकों के सामने मुख्य सवाल था, भारत के वास्तविक स्वरूप की खोज। अठारहवीं शती के आखिरी चरण में ही, यूरोप के अनेक देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने, भारत से आरंभ हुए व्यापार में भारी मुनाफे को देखते हुए, यह प्रयास करने आरंभ कर दिये थे कि हमारी सभ्यता और संस्कृति को ठीक से समझा जा सके। भारत से ताल्लुक बढाने के लिए भारत को जानना उनके लिए ज़रूरी हो गया था। भारत की अतीतकालीन संस्कृति के अध्ययन से वे यह देख कर चकित थे कि कभी भारत में ज्ञान विज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा था। पर अब वे ज्ञानोदय के उत्तरकालीन परिदृष्य में पूरी दुनिया के आधुनिक किस्म के सभ्यताकरण के एजेंडे के साथ फैल रहे थे। ईसाई् मिशनरी परोक्ष रूप में उनकी सहायता करते थे, ताकि जनसामान्य के बीच उनकी सभ्यता संस्कृतिमूलक श्रेष्ठता को स्थापित किया जा सके। भारत के प्राचयवादी अध्ययन के मुख्य केन्द्र कलकत्ता और लंदन मे काम करने लग पड़े थे। रायल एशियाटिक सोसायटी और फोर्ट विलियम कालेज आदि संस्थाएं इस काम में जुट गयी थीं कि कैसे हमारे अतीत की पुनर्व्याख्या करके हमें पश्चिम से हीन साबित किया जाये और हिन्दू मुस्लिम विभाजन को गहराने के लिए इतिहास का इस्तेमाल किया जाये। तो, जो रणनीति बनी, वह यह थी कि हमारे शास्त्रीय अतीत की महानता और श्रेष्ठता की अनदेखी की जाये और हिंदुस्तानी का हिन्दी व उर्दू में विभाजन कर के यहाँ की स्थानीय भाषाओं की सभ्यता व संस्कृति को उभारा जाये। वहाँ भी उस साहित्य और संस्कृति को महत्व दिया जाये, जिससे हिन्दू मुस्लिम विभाजन और गहरा हो सके। इतना ही नहीं यह कोशिश भी की जा सके कि उसमें ईसाइयत का प्रवेश हो सके। हीगेल, शोपनहावर, गिलक्रिस्ट और मैक्स मूलर जैसे विद्वानों के इस तरह के प्रयासों को भांप कर बंगाल और महाराष्ट्र में नवजागरण की जो लहर उठी, उसने भारत के 'वास्तविक स्वरूप' की खोज के लिए सीधे अपने स्वर्णिम अतीत के ज्ञान मूलक स्रोतों की ओर रुख किया। केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, रानाडे, ज्योतिबा फुले, विवेकानंद और उत्तर भारत में सक्रिय दयानंद सरस्वती आदि सब कितनों ने पौराणिक वैष्णववादी भक्ति के बजाये, वेद, उपनिषद, दर्शन, वेदांत आदि की ओर रुख किया। अंग्रेज़ विद्वान अपना काम करते रहे और हमारे चिंतक भारत के वास्तविक स्वरूप की सम्यक खोज और व्याख्या कर के उसे चुनौती देते रहे।
तो, अंग्रेज़ों का वह प्राच्यवादी एजेंडा शेष भारत में तो बहुत कामयाब नहीं हो सका, लेकिन हिन्दी पट्टी में, दयानंद सरस्वती की अस्वीकार्यता के कारण, और जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के प्रयत्नों के कारण, वह काफी हद तक अपने मंसूबों को कारगर बनाने में कामयाब हो गया। देखते-देखते हिन्दी पट्टी के अधिकांश लेखक आलोचक रचनाकार वही बोली बोलने लगे, जिसे हम ग्रियर्सन के लेखन में बीज रूप में विद्यमान पाते हैं।
अन्ततः ले दे कर एक प्रसाद ही ऐसे बड़े रचनाकार बचते हैं, जिनका रचनाकर्म शेष भारत के नवजागरण के सरोकारों से मेल खाता है और अंग्रेज़ों के द्वारा भारत को अपना सांस्कृतिक उपनिवेश बनाने के उनके एजेंडे के आड़े आ कर खड़ा हो जाता है। अपनी प्रतिरोधी चेतना और तेजस्विता की अभिव्यक्ति के लिहाज से वे अकेले ऐसे रचनाकार प्रतीत होते हैं, जिन्हें नवजागरण के प्रेरक स्तंभ के रूप में, कबीर के बाद प्रकट होने वाले दूसरे महानतम रचनाकार कह सकते हैं। वे अपनी अभिव्यक्ति और भाषा के रूपों में एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन नवजागरण की मशाल को घने अंधेरों के बावजूद जलाये रखने के लिहाज से, एक ही मंच पर आसीन हैं।
रामचंद्र शुक्ल की हिन्दी नवजागरण के सन्दर्भ में पुनर्व्याख्या से पूर्व यहाँ यह स्पष्ट कर देना ज़रूरी लगता है कि इसे उनके साहित्यिक अवदान के बारे में टिप्पणी की तरह न लिया जाये। साहित्य के विविध पक्षों पर उनके विचार मौलिक और उच्चस्तरीय हैं। रस का मौलिक विवेचन करके उसका अन्तर्विकास करने की दृष्टि से वे संस्कृत के महान आचार्यों की कोटि में रखे जाने लायक हैं, और हिन्दी में वे अकेले हैं, जिनका काव्यशास्त्रीय धारणाओं के अग्रविकास में इतना बड़ा योगदान है। दूसरी बात, जो उन्हें हिन्दी के अन्य सभी आलोचकों में शीर्ष स्थान पर वे जाती है, वह यह है कि हिन्दी साहित्य के विधिवत व्यवस्थित इतिहास की बेहद अपर्याप्त परम्परा के बावजूद उन्होंने इस कार्य को इतनी गहन अन्तर्दृष्टि और अध्यवसाय का परिचय देते हुए संभव कर दिखाया कि उनके बाद इस क्षेत्र में संस्थाओं से सामूहिक प्रयास भी, उनके ही इतिहास के पूरक और अनुपूरक ही सिद्ध होते हैं।
तथापि अपने इतिहास लेखन में उन्होंने जिन कवियों को कुछ अन्य कवियों तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बनाया और ऐसा करने के लिए हिन्दी नवजागरण के जिन सरोकारों को आधार की तरह ग्रहण किया, सवाल केवल उन्हें ले कर उठते हैं। खास तौर पर इसलिए, क्योंकि उनके ऐसे मूल्यांकनों के पीछे, अंग्रेज़ विद्वानों की वह नीति मौजूद नज़र आती है, जिसकी मदद से वे हिन्दी नवजागरण को हिन्दू और मुस्लिम नवजागरण में विभाजित करने का साम्प्र दायिक खेल खेल रहे थे। यह औपनिवेशिक दृष्टि, बरास्ते ग्रियर्सन, शुक्ल जी में प्रवेश करती देखी जा सकती है और ठीक यही बात है, जिसकी वजह से शुक्ल जी जयशंकर प्रसाद के निशाने पर भी आ जाते हैं और वे उनमें 'स्वरूप विस्मृति' के लक्षण तक देखने लगते हैं। इन बातों को समझने के लिए इनकी गहराई में जाना ज़रूरी लगता है।
○○○
आइए, पहले यह देखने का प्रयास करते हैं कि ग्रियर्सन इस सन्दर्भ में क्या कर रहे थे?? उनकी मुख्य धारणाएं, स्थापनाएं और सरोकार क्या थे? और किस तरह वे शुक्ल जी के लिए प्रेरक य आ अनुप्रेरक की भूमिका में चले गये?
ग्रियर्सन (1851-1941) ने 'द माडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर औफ हिंदुस्तान' (1889) लिख कर हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन के भविष्य की जैसे एक नयी परिपाटी तैयार कर दी थी। गार्सा द तासी के हिन्दी साहित्य के इतिहास में हिन्दी साहित्य का मतलब है, हिन्दी और उर्दू दोनों का साहित्य। ग्रियर्सन उसमें से उर्दू साहित्य को निकाल बाहर करते हैं।
दूसरी बात यह है कि वे हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्ति साहित्य को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हैं। वे हमारी भक्ति को 'ईसाइयत की देन' कहते हैं, जो हमारी तरह 'द्वैत भाव' वाली है। यह स्थापना कर के वे हमारे भक्ति आन्दोलन की व्याख्या निम्न रूप में करते हैं,
"‘समस्त धार्मिक मत-मतान्तरों के अंधकार पर बिजली सी कौंध दिखाई पड़ती है। कोई हिन्दू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई, किन्तु इतना तो निश्चित है कि समस्त भारतवर्ष ने इतना विराट आन्दोलन शायद ही कभी देखा हो।"
ग्रियर्सन के इस मत में ' समस्त मत मतान्तर का अंधकार' किस ओर इशारा करता है? वे जिस भक्ति की उन पर 'विजय' बात करते हैं, वह ईसाई धर्म की तरह द्वैतवादी यानी सगुण अवतारवाद से ताल्लुक रखने वाली भक्ति है। और जिन मत मतान्तरों को वे भारत के स्वरूप को तिरोहित करने वाला अंधकार कह रहे हैं, वे सिद्ध, नाथ, जोगी निरगुन और सूफी मत मतान्तर हैं। इनके माध्यम से भारत में सामान्य हिन्दू मुसलमान एक दूसरे के करीब आ कर भाईचारे के बंधन में बंध रहे थे। इसलिए वह सवर्ण 'हिन्दू' को उस अंधकार पर विजय दिलाने वाली 'सगुण भक्ति' की पैरवी कर रहे हैं।
उपर्युक्त दोनों बातों के ज़रिये ग्रियर्सन हिन्दी साहित्य के ऐसे इतिहास को लिखने और लिखवाने के काम में जुटे नज़र आते हैं, जो हिन्दू मुस्लिम को विभाजित कर दे। इस तरह वे ऐसे हिन्दी साहित्य के इतिहास की मदद से हिन्दी नवजागरण का एकांश में तो ऐसा इस्तेमाल कर ही सकते थे, जो शेष भारत के नवजागरण के मुकाबले, उनके औपनिवेशिक एजेंडे के अधिक अनुकूल हो। इस काम में उन्हें तब सफलता मिलती है, जब रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के पीछे काम करने वाली सांस्कृतिक दृष्टि बहुत दूर तक उनकी उपर्युक्त धारणाओं की पुष्टि करती दिखाई देने लगती है।
यहाँ सवाल यह उठता है कि शुक्ल जी के इतिहास के पीछे मौजूद उनकी सांस्कृतिक दृष्टि ग्रियर्सन से प्रायः मेल खाने वाली कैसे और क्यों हो गयी? क्या शुक्ल जी देख नहीं पाये कि ग्रियर्सन जैसे अंग्रेज़ विद्वानों की स्थापनाएं, अन्ततः अंग्रेज़ों के औपनिवेशिक एजेंडे को लागू करने करवाने की नीयत से भरी थीं? ऐसा लगता है कि इन दोनों संभावनाओं की तुलना में इस बात की संभावना अधिक है कि शुक्ल जी अपने तौर पर अपने मत का विकास कर रहे थे, पर उनकी वैष्णववादी दृष्टि उन्हें मुख्यतः हिन्दू की विचारधारा के पक्ष में और सामान्य हिन्दू मुसलमान को समन्वित करने की चाह रखने वाले मत मतान्तरों के विरोध में, खड़े होने की ओर ले गयी थी। तथापि वहाँ पीछे कहीं ग्रियर्सन खड़े भी अवश्य दिखाई दे जाते हैं, इस बात को सिरे से खारिज करना भी कठिन लगता है।
यहाँ इस बात को केवल एक संयोग कह कर ही टाला नहीं जा सकता कि शुक्ल जी का हिन्दी साहित्य का इतिहास, बाबू श्यामसुंदर दास द्वारा संपादित 'हिन्दी शब्द सागर' के नागरी प्रचारिणी सढा द्वारा प्रकाशन के बाद, उसी योजना की अगली कड़ी की तरह, प्रकाशित किया गया। 1900 में स्थापित इस नागरी प्रचारिणी सभा के पहले ही साल जो लोग इसके सदस्य बने, उनमें महामहोपाध्याय पं. सुधाकर द्विवेदी, इब्राहिम जार्ज ग्रियर्सन, अंबिकादत्त व्यास, चौधरी प्रेमघन जैसे ख्यातिलब्ध विद्वान थे। नागरी प्रचारिणी सभा के साथ ग्रियर्सन के इतने गहरे रिश्ते को अगर हम संयोग मान भी लें, तब भी इस बात को तो कदाचित कोई ही संयोग कह सकेगा कि नागरी सभा ने अपनी 'हिन्दी शब्द संग्रह वाली महत्वाकांक्षी योजना के तहत जिन आरंभिक ग्रंथों का प्रकाशन किया, वे ग्रियर्सन के द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का ही, उनकी अगली कड़ी के रूप में विस्तार प्रतीत होते हैं। 'हिन्दी शब्दसागर' (1916) की भूमिका में श्याम सुंदर दास लिखते हैं,
"भारत में पाश्चात्य कोशों और कोशकारों के संपर्क और प्रभाव से आधुनिक ढंग के कोशों का निर्माण प्रचलित और विकसित हुआ। हिन्दी के आधुनिक कोशों की चर्चा की जा चुकी है। प्रथम संस्करण की भूमिका में भी इसका सिंहावलोकन किया गया है।"
"इन्हें देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले के हिन्दी कांगों में प्रबम वा पादरी- आदम’ का हिन्दी कोश जो 1829 में ‘कलकत्ता से छपा । इसके पूर्व के कोश पाश्चात्यों द्वारा पाश्चात्य लिपि और भाषा के माध्यम से बने।"
"हिन्दी की विविध बोलियों के रूप स्थिर करने में ग्रियर्सन की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है।"
यहाँ ग्रियर्सन के जिस योगदान की बात की गयी है, उसका सम्बन्ध उनके 'लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इंडिया’ से है, जो अनेक खंडों में 1898 से ले कर 1928 के दरम्यान प्रकाशित हुआ। इससे पहले वे 1887 में बिहारी बोलियों का व्याकरण प्रस्तुत कर चुके थे।
ग्रियर्सन समेत बहुत से अंग्रेज़ विद्वान उन दिनों यह कोशिश कर रहे थे कि हिन्दी को उर्दू से अलहदा करने की बात पर वैज्ञानिक दृष्टि से मोहर लग जाये। हिन्दी के ऐसे शब्दकोश तैयार करवाये गये, जिनमें उर्दू शब्दावली को बाहर कर दिया गया। 'हिन्दी शब्द सागर' उसी कड़ी में सामने आया सर्वाधिक व्यवस्थित कार्य था।
अब बात यहाँ आ कर खड़ी हो गयी थी कि किसी तरह हिन्दी साहित्य के इतिहास को भी उर्दू और इस्लामी संस्कृति के मेलजोल और प्रभावों से अलहदा कर के, 'हिन्दू इतिहास' की तरह लिखा लिखवाया जाये। इस तरह के इतिहास को लिखने के रास्ते का जो सबसे बड़ा रोड़ा था, वह 15वीं शती के कबीर के रूप में सामने था। कबीर की लोकप्रियता, भारत के जन सामान्य के घर-घर में अपनी मौजूदगी का अहसास कराती नज़र आ रही थी। तब ग्रियर्सन की निगाह नाभादास के 'भक्तमाल' (1585) पर पड़ी। यह हिन्दी साहित्येतिहास को लिखने वह पहला प्रयास था, जिस में कबीर और अन्य निरगुनियों की गिनती भक्तों में की गयी थी। इसके आसपास कुछ पहले गुरू अर्जुन देव ने 'गुरू ग्रंथ साहिब' (1604) का जो संपादन किया था, उसमें कबीर की वाणी सर्वाधिक है, पर उन्हें वहाँ गुरू न कह कर 'भगत' कह दिया गया है। ज्ञानधारा को भक्ति का अंग बनाने और मानने की प्रक्रियाओं की शुरुआत इन्हीं ग्रंथों मे सबसे पहले दिखाई देनी आरंभ होती है। इससे पहले निरगुन धारा के लोगों को संत कहने का प्रचलन अधिक था। हालांकि वे विधिवत भक्त नहीं थे, जिनका सम्बन्ध सगुण भक्ति से होता है। पर 16वीं शती के मध्य तक आते आते जब सगुण भक्ति का वर्चस्व होने लगता है, संतों को भी भक्त कहा जाना आरंभ हो जाता है। शब्दों के व्यवहार प्रयोग अक्सर लचीले होते हैं। इसका फायदा ग्रियर्सन ने उठाया। नाभादास ने भक्त शिरोमणि के रूप में सूर और तुलसी की जो स्थापना कर दी थी, उस आधार पर ऐसे 'सूर और ससि' की तुलना में, कबीर आदि निरगुनियों को 'उडुगन' मात्र साबित किया जा सकता था। नतीजतन उनके व्यापक नवजागरणमूलक प्रभाव की उपेक्षा के आधुनिक अध्याय का लिखा जाना आरंभ हो गया।
वैष्णव भक्तिवाद को भारत की 'स्वरूप' निर्धारक वास्तविक चेतना का निर्माण करने वाली वस्तु में बदला जाने लगा।
दूसरी तरफ शैवों, नाथों, सिद्धों आदि से होती हुई वह संस्कृति चेतना, जो अब सूफियों के साथ रचाये गये संवाद के बाद, निरगुन धारा के रूप में, अपनी अनवरत विकास यात्रा को आगे बढ़ाती हुई प्रकट हुई थी, उसे ये ग्रियर्सन महोदय, 'मत मतान्तरों का अंधकार' कह कर नकारने की कोशिशों में लग गये। उनके इस सन्दर्भ में किये गये 'भक्तमाल' सम्बन्धी अध्ययन रायल एशियैटिक सोसायटी के जर्नल्स में 1909, 1910 और 1911 में प्रकाशित हुए। इनके आधार पर वे यह सिद्ध करने की भूमिका बनाते हैं कि तुलसी और सूर किस तरह भक्ति का एक 'विराट आन्दोलन खड़ा करते हैं, जो कबीर आदि के 'मत मतान्तरों के अंधकार में बिजली की तरह कौंधता' है।
15वीं शती के जिस नवजागरण को ग्रियर्सन इस तरह 'भारत का अंधकार काल' बना देते हैं, उसका कारण क्या है? इस सवाल के जवाब में वे मुसलमानों और इस्लामी संस्कृति के आक्रमण की ओर इशारा करते हैं। उनकी ये जो धारणाएं हैं, वे आगे चल कर शुक्ल जी के साहित्येतिहास में भक्तिकाल के विवेचन के अन्तर्गत निम्न स्थापना के रूप में पल्लवित हो जाती है।
“देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश ना रह गया। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था।”
शुक्ल जी की यह स्थापना, एक तरह से ग्रियर्सन के मत का विस्तार है, जो बाद में राम स्वरूप चतुर्वेदी, बाबू गुलाब राय और रामकुमार वर्मा का भी मत हो जाता है। लेकिन यहाँ यह सवाल अनुत्तरित छूट जाता है कि ऐसी हताशा और पौरुषविहीनता का नामोनिशान भी हमें उस कबीर की वाणी में क्यों नहीं मिलता, जो बाज़ार में लाठी ले कर खड़े तत्कालीन अर्थव्यवस्था और उसके बाज़ार को ललकार रहे हैं और लोगों को अपने घरबार का मोह त्याग कर अपने साथ चलने को कह रहे हैं, ताकि 'ज्ञानात्मक प्रेम' के दर्शन को संघर्ष करने और समाज को रूपान्तरित करने का अस्त्र बनाया जा सके। 'भगवान की भक्ति और करुणा में ही ध्यान लगाने के अतिरिक्त और कोई उपाय न देखने वाले तो तुलसी और सूर जैसे सगुण भक्त ही हैं, जिन्हें कबीर आदि की बलि चढा कर, हिन्दी साहित्य के शीर्ष पर ले जा कर बिठा दिया जाता है।
तुलसी को इतना अधिक महत्वपूर्ण बनाने का पहला प्रयास, उस दौर में ग्रियर्सन करते हैं। वे उन्हें 'दीन अथवा क्षुद्र ' हिन्दू समाज की 'तुतलाती आवाज' को सहृदयता पूर्वक सुनने वाले 'सुखदायी माता पिता' की तरह प्रस्तुत करते हैं,
Grierson presents Tulsidas "as a father and mother delight to hear the lisping practice of their little ones."
तुलसीदास को इतना महत्व देने के पीछे ग्रियर्सन की यह सोच काम कर रही थी कि उनके 'रामचरितमानस' का हिन्दू समाज एक धर्म ग्रंथ की तरह सम्मान करने लग पड़ा था। इसलिए तुलसी और मानस का इस्तेमाल मुलसमानों के विरूद्ध हिन्दू पुनरुत्थान को खड़ा करने के लिए किया जा सकता था। वे मानस की प्रशंसा करते हुए, अपने इस मनोभाव को छिपाते नहीं। अपने इतिहास में वे कहते हैं,
"यह दस करोड़ जनता का धर्मग्रंथ है और उनके द्वारा यह उतना ही भगवत्प्रेरित माना जाता है, अँग्रेज पादरियों द्वारा जितनी भगवत्प्रेरित बाइबिल मानी जाती है।''
यहाँ वे तुलसी और मानस के बहाने, हिन्दू ईसाई गठबंधन को मज़बूत करने की ओर आगे बढते दिखाई देते हैं। ग्रियर्सन के हिन्दी साहित्य में व्यक्त उनकी ऐसी धारणाओं का उनके बाद लिखे जाने वाले हिन्दी साहित्य के विभिन्न इतिहासों पर व्यापक प्रभाव नज़र आता है। किशोरी लाल गोस्वामी ने ग्रियर्सन के साहित्येतिहास का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कराया, तो भूमिका में लिखा,
"द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ने बाद में लिखे जाने वाले हिन्दी साहित्य के इतिहासों के रूप-रंग को सँवारा।"
अब हम यहाँ से रामचंद्र शुक्ल के 'हिन्दी साहित्य के इतिहास', की ओर सीधे आ सकते हैं। वहाँ हम जब उनके तुलसीदास के प्रति एकनिष्ठ अनुराग को देखते हैं, इस्लाम के हिन्दी साहित्य पर पड़ने वाले प्रभावों को अभारतीय कह कर निष्कासित कर देने की प्रवृत्ति को देखते हैं, कबीर आदि को साम्प्रदायिक मत-मतान्तरों के प्रचारक मान कर उन्हें काव्य की कसौटी पर गौण बना देने के प्रयास पर निगाह डालते हैं और सगुण वैष्णव भक्ति को भारत के सांस्कृतिक व्यक्तित्व के वास्तविक स्वरूप का पर्याय बना देने की बात पर उन्हें मोहर लगाता पाते हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि वे यह सब अपनी अंतःप्रेरणा से कर रहे थे, या ग्रियर्सन के प्राच्यवादी औपविशीकरण के एजेंडे के अधूरे रह गये कार्यों को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे थे?
इस सन्दर्भ में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उनके समकालीन जयशंकर प्रसाद की उन टिप्पणियों पर गौर करना होगा, जो उनके अतिरिक्त किसी अन्य आलोचक के बारे में कही गयी प्रतीत नहीं होतीं। उस दौर में वे ही थे, जो कबीर आदि निरगुनियों और सूफियों के प्रेम और रहस्यवाद को 'अभारतीय' घोषित कर के, उनके मुकाबले में तुलसी और सूर की भक्ति को 'भारतीय आत्मा' की प्रतिनिधि बना रहे थे और ऐसा कर के न केवल उन्हें हिन्दी साहित्य के शीर्ष पर बिठा रहे थे, हिन्दी नवजागरण को भी लीक से उतारने में परोक्ष हिस्सेदार हो रहे थे। उनके चिन्तन में घर कर गयीं इन बातों ने उन्हें जिस तरह के निष्कर्षों तक पहुंचाया, उन्हें नीचे दिये जा रहे कुछ उद्धरणों की मदद से आसानी से समझा जा सकता है,
1 "सिद्धों और योगियों की रचनाएँ साहित्य कोटि में नहीं आतीं और योगधारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती।"
2 "महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतन्त्र हिन्दू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे।"
3 ग्रियर्सन की उस धारणा का विस्तार, जिसमें वे भक्तिपूर्व भारत को 'मतमतान्तरों के अंधकार में घिरा' बताते हैं :
"शैवों, वैष्णवों, शाक्तों और कर्मठों की तू तू मैंमैं तो थी ही, बीच में मुसलमानों से अविरोध प्रदर्शन करने के लिए भी अपढ़ जनता को साथ लगाने वाले कई नए-नए पन्थ निकल चुके थे जिनमें एकेश्वरवाद का कट्टर स्वरूप, उपासना का आशिकी रंगढंग, ज्ञानविज्ञान की निन्दा, विद्वानों का उपहास, वेदान्त के चार प्रसिद्ध शब्दों का अनधिकार प्रयोग आदि सब कुछ था; पर लोक को व्यवस्थित करने वाली वह मर्यादा न थी जो भारतीय आर्यधर्म का प्रधान लक्षण है।"
4 "भक्तों के भी दो वर्ग थे। एक तो भक्ति के प्राचीन स्वरूप को ले कर चला था; अर्थात प्राचीन भागवत सम्प्रदाय के नवीन विकास का ही अनुयायी था और दूसरा विदेशी परम्परा का अनुयायी, लोकधर्म से उदासीन तथा समाजव्यवस्था और ज्ञान विज्ञान का विरोधी था। यह द्वितीय वर्ग जिस घोर नैराश्य की विषम स्थिति में उत्पन्न हुआ, उसी के सामंजस्य साधन में सन्तुष्ट रहा। उसे भक्ति का उतना ही अंश ग्रहण करने का साहस हुआ जितने कि मुसलमानों के यहाँ भी जगह थी।"
5 "यदि कोई पूछे कि जनता के हृदय पर सबसे अधिक विस्तृत अधिकार रखने वाला हिन्दी का सबसे बड़ा कवि कौन है तो उसका एक मात्र यही उत्तर ठीक हो सकता है कि भारतहृदय, भारतीकंठ, भक्तचूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास।"
6 "भूषण ने जिन दो नायकों की कृति को अपने वीरकाव्य का विषय बनाया वे अन्याय दमन में तत्पर, हिन्दू धर्म के संरक्षक, दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिन्दू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई।
7 "सारांश यह कि रहस्यवाद एक साम्प्रदायिक वस्तु है; काव्य का कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं”
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि रामचंद्र शुक्ल अपने 'हिन्दी साहित्य के इतिहास' को, हिन्दुओं के सांस्कृतिक पुनर्गठन के उद्देश्य को सामने रख कर लिख रहे थे। वे हिन्दी साहित्य को, 'हिन्दू साहित्य' के अर्थ में ग्रहण कर रहे थे और 'हिन्दी' की सांस्कृतिक चेतना को, 'हिन्दू की सांस्कृतिक चेतना' की तरह देखने दिखाने का काम कर रहे थे। इस तरह वे हिन्दी और हिन्दी संस्कृति का हिन्दूकरण करके उसके साम्प्रदायिक इस्तेमाल के लिए गुंजाइश पैदा कर रहे थे।
अंग्रेज़ अपने औपनिवेशिक ऐजेंडे के तहत, हिन्दू और हिन्दू संस्कृति का, साम्प्रदायिक इस्तेमाल कर के, उसे मुसलमानों के विरोध के लिए प्रेरित कर सकते थे। शुक्ल जी के उक्त उद्धरण सिद्ध करते हैं कि हिन्दू जाति और हिन्दू संस्कृति के गठन के लिए वे, हिन्दी साहित्य के इतिहास की जो व्याख्या करते हैं, वह मुसलमान और इस्लाम को विदेशी, अवांछित और हानिकारक सिद्ध करती है।
15वीं शती के कबीर केंद्रित नवजागरण को उनका साहित्येतिहास, सिरे से खारिज करता है, क्योंकि वहाँ मुसलमानों के प्रभाव के कारण, उनकी प्रिय और अनिवार्यतः वांछित भक्ति का, पर्याप्त विकास नहीं हो सका। ऐसा कर के वे भक्ति को भारत की 'स्वरूप विधायिनी' वस्तु में बदल देते हैं और उसे भारत के हृदय की धड़कन सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं।
हालांकि भारतीय दर्शन और वेदविहित औपनिषदिक परम्परा के माध्यम से, प्राचीन काल से निर्मित और विकसित भारत के 'वास्तविक स्वरूप' को, किसी तरह भी 'भक्तिवादी' नहीं ठहराया जा सकता।
जयशंकर प्रसाद इसी दिशा में आगे बढते हुए शुक्ल जी की धारणाओं का प्रत्याख्यान करते हैं। शुक्ल जी जब कबीर आदि की धारा को 'भक्ति की ही दूसरी धारा' कहते हैं, तो वे इस तथ्य की उपेक्षा करते हैं कबीरदास निरगुन संत ज्ञानमार्गी हैं, न कि 'अपूर्ण या अपर्याप्त भक्तिवादी'।
भक्तिवाद को ग्रियर्सन आदि प्राच्यवादी विद्वानों ने ईसाई धर्म के अनुकूल पा कर उसे, हिन्दी पट्टी की सांस्कृतिक चेतना के सार के रूप में स्थापित किया। इसकी वजह यह थी कि वहाँ वे मुसलमानों के प्रति हिंदुओं के विद्वेष को गहराने वाली भावभूमि ही नहीं देख रहे थे, वे इसमें लोगों को राजभक्त बना सकने की मूल्य चेतना की उपस्थिति भी देख पा रहे थे। रामराज्य के प्रतीक या पर्याय के रूप में अंग्रेज़ राज को प्रस्तुत करने का भ्रमपूर्ण प्रचार कर के वे, इस मकसद में कामयाब हो सकते थे। इससे पूर्व अठारहवीं शती के संन्यासी विद्रोह को ठुस्स करने में अंग्रेज़ों के इस प्रचार या षड्यंत्र की भी बड़ी भूमिका थी कि 'वे राम के दूत या देवदूत की तरह हिन्दुओं की मदद करने के लिए, हरि की इच्छा का पालन करते हुए भारत आये थे'। 'रामराज्य के सेवक' होने से 'भक्तजनों का उद्धार' होता है, इस विचार पर, इन प्राच्यविदों के भक्ति विवेचनों में, विशेष बल दिया गया था।
शुक्ल जी के भक्तिभाव विवेचन 'सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरिये उरगारि' की बात, पुरज़ोर तरीके से करते देखे जा सकते हैं। अंग्रेज़ों के औपनिवेशिक एजेंडे और शुक्ल जी के भक्ति विवेचन के बीच कोई सीधा रिश्ता या साठ गांठ है, यह कहना शुक्ल जी के साथ अन्याय करना होगा। तथापि इन दोनों बातों को जोड़ने वाले कुछ परोक्ष सूत्र अवश्य मिल जाते हैं, जिनके आधार पर हम, प्राच्यवाद के साथ उनकी वैचारिक एकसूत्रता को ले कर, कुछ हद तक सहमत होने के लिए अवश्य स्वतन्त्र ओ जाते हैं। जैसा कि निम्न उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है।
'भारत को क्या करना चाहिए।' शीर्षक से 'हिंदुस्तान रिव्यू' के 1905 के फरवरी अंक में प्रकाशित रामचंद्र शुक्ल के लेख का अंश:
"शिक्षा से मेरा मतलब सामान्य महत्व के मामलों के बारे में हमारे नेताओं की राय का अशिक्षित जनता तक संप्रेषण भी है, ताकि अवसर आने पर उनका [अशिक्षित जनता का] सहयोग मिलने से न रह जाए।"
शुक्ल जी की यह धारणा स्पष्ट करती है कि वे शिक्षा के 'राजनीतिक और राजभक्ति परिचालित' उद्देश्य से 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' और 'तुलसीदास' जैसी पुस्तकें लिख रहे थे। उनकी इस धारणा का महत्त्व इसलिए और बढ जाता है, क्योंकि वे स्वयं उच्च शिक्षा से जुड़े थे। हिन्दी साहित्य का इतिहास, अपने आरंभिक रूप में, छात्रों को दिये गये व्याख्यानों के नोट्स की तरह लिखा गया था। मतलब साफ है। वे हिन्दी साहित्य के इतिहास को इस तरह पढा रहे थे कि तत्कालीन अंग्रेज़ राज के 'नेताओं की राय का अशिक्षित जनता में संप्रेषण' हो सके, 'ताकि अवसर आने पर उनका सहयोग' राजसत्ता को मिल सके।'
हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्ति को, ज्ञान विज्ञान और दर्शन के सिर पर ला कर बिठा देने का, क्या दुष्परिणाम हो सकता है, इस बात को वे न सिर्फ जानते थे, भीतर भीतर शायद उससे बच कर निकलना भी चाहते थे। पर कोई विवशता थी, जिसके चलते वे अपने विवेचनों को भक्तिवाद के पक्ष में भुनाये जाने से खुद को बचा नहीं पा रहे थे। यह भी उनकी चिन्ता का विषय था कि इससे भारत में ईसाई धर्म को अधिक मज़बूत होने में मदद मिलेगी। यूरोप के इतिहास से वे परिचित थे। उन्हें पता था कि यूरोप में 15वीं शती में वह जो महान रेनेसां घटित हुआ, वह तभी मुमकिन हो सका, जब वहाँ के लोग और वहाँ की राजसत्ता ईसाइयों के और ईसाई धर्म के चंगुल से बाहर निकल गयी। इस सम्बन्ध में 'तुलसी की भक्ति पद्धति' नामक निबंध का एक अंश देखें,
"यूरोप में ईसाई धर्म के भक्त उपदेशकों द्वारा ज्ञान विज्ञान की उन्नति के मार्ग में किस प्रकार बाधा पड़ती रही है, यह वहाँ का इतिहास जानने वाले मात्र जानते हैं। हो सकता है। इस भावना का हिन्दू हृदय से बहिष्कार नहीं हो सकता। जहाँ हमें दिन दिन बढ़ता हुआ अत्याचार दिखाई पड़ा कि हम उस समय की प्रतीक्षा करने लगेंगे जब वह 'रावणत्व' की सीमा पर पहुँचेगा और 'रामत्व' का आविर्भाव होगा।"
संभव हो तो शुक्ल जी की इन पंक्तियों को तब तक बार-बार पढें, जब तक इनके पीछे मौजूद उनके हृदय के उस हाहाकार को सुनने में हम समर्थ न हो जायें, जो बुद्धि के विरोध में खड़ा होने के लिए विवश है और अपनी स्थिति के मिथ्यात्व को छिपाने के लिए किसी अनहोनी के चमत्कारपूर्ण तरीके से घट जाने का झूठा दिलासा दे कर खुद को बहला रहा है।
इतना ही नहीं, शुक्ल जी यह भी जानते थे कि जिस भक्ति मार्ग के रास्ते पर वे तुलसी दास की मार्फत, हिन्दी प्रदेश के लोगों को और व्यापक रूप में भारत को धकेले लिए जा रहे हैं, वह रास्ता ज्ञान विरोधी ही नहीं है, वह जनसाधारण को पाखंड, झूठ और चमत्कारमूलक अंधविश्वासों के गर्त तक में धकेल सकता है।
शुक्ल जी तुलसीदास में ऐसे झूठे और पाखंडपूर्ण दावों को देखते हुए भी, जाने किस विवशता और दबाव से, उस पर पर्दा डालने का असफल और अपर्याप्त प्रयास करते दिखाई देते हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए निम्न उद्धरण देखें,
"तुलसीदास जी को चित्रकूट में राम की एक झलक जंगल के बीच में मिली थी। इसका कुछ संकेत सा विनयपत्रिका के इस पद में मिलता है... प्रेम के इस झूठे दावे से, इस प्रकार के पाखंड से, अज्ञान के अनिष्ट प्रचार की आशंका नहीं।"
'अनिष्ट' की क्यों 'आशंका' नहीं? - क्योंकि, बकौल रामचंद्र शुक्ल, तुलसी दास तो 'अवतार' हैं, इसलिए वे जो करते या कहते हैं, उसे आंख मूंद कर मान लेना चाहिए। देखिए, शुक्ल जी किस रूप में तुलसी को एक अवतार की तरह प्रतिष्ठित करते हैं,
"...उसी समय भक्तवर गोस्वामी जी का अवतार हुआ जिन्होंने वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुलाचार, वेदविहित कर्म, शास्त्रप्रतिपादित ज्ञान इत्यादि सब के साथ भक्ति का पुन: सामंजस्य स्थापित करके आर्यधर्म को छिन्न-भिन्न होने से बचाया।"
इस प्रकार भक्ति मार्ग के पितृसत्तात्मक, ब्राह्मणवादी और सामंतवादी, 'झूठ, पाखंड और अज्ञान' पर पर्दा डालने से स्पष्ट है कि शुक्ल जी तत्कालीन दौर के ग्रियर्सन जैसे प्राच्यवादी लेखकों के प्रभाव को दरकिनार कर के, स्वतन्त्र लेखन कर पाने में कोई बाधा अनुभव कर रहे थे। यह भी हो सकता है कि इसके पीछे अकादमिक जगत को अंग्रेज़ी शिक्षा नीति के मुताबिक ढालने की कोशिशें उनसे वह सब लिखवा रही हों। दूसरों के कहे मुताबिक और दूसरों की विचारधारा के मुताबिक लिखने की इस तरह की विवशताओं को हमारे शीर्ष आलोचक अक्सर अनुभव करते रहे हैं, इसकी एक झलक नामवर सिंह के काशी नाथ को दिये गये एक साक्षात्कार में निम्न रूप में दर्ज है,
"मेरे गुरुदेव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मैं शूद्र जाति का ब्राह्मण हूँ। उसकी व्याख्या उन्होंने यों की है कि दूसरों के कहने पर ही मैं लिखता रहा हूँ। आचार्य शुक्ल ने अपने सारे लेखन को 'फरमाइशी' कहा है। फिर मैं किस खेत की मूली हूँ।"
तो यदि खुद रामचंद्र शुक्ल स्वीकार करते हैं कि उन्हें किसी की फर्माइश की पूर्ति के लिए लिखना पड़ा है, तो उनके तत्कालीन नवजागरण के सरोकारों से विवश विचलन को देख कर भी नकारना कहाँ तक संगत है?
समाज सांस्कृतिक रूपान्तर अधिक महान लक्ष्य है, उसकी पूर्ति के लिए अगर हमें अतीत के कुछ महान लेखकों-साहित्यकारों के प्रति अपने पूज्य भाव का परित्याग भी करना पड़े, तो हमें इसके लिए सहज सहर्ष तेयार रहना चाहिए।
○○○
प्रसाद इस बात को समझ रहे थे कि रामचंद्र शुक्ल की विचारधारा तत्कालीन भारतीय नवजागरण के बुनियादी सरोकारों से मेल नहीं खा रही थी। इसलिए उनका प्रतिवाद और प्रतिरोध करना उन्हें ज़रूरी लगता है।
प्रसाद ने 'काव्य और कला और अन्य निबंध' लिख कर ऐतिहासिक महत्व का जो काम किया, वह इसलिए भुला दिया गया, क्योंकि बहुत से विद्वानों और साहित्यकारों को यह लगा कि इसके पीछे उनकी मंशा खुद को बचाने की रही होगी। खुद को, यानी उस छायावाद और रहस्यवाद को, जो उनके अपने लेखन का मूल स्वरूप था।
तथापि, वस्तुस्थिति यह है कि संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त प्रेम और उसके ऐसे व्यापक अनुभव से संबद्ध रहस्यवाद को बचाते हुए, वे दरअसल भारत के सांस्कृतिक व्यक्तित्व के 'मूल स्वरूप' को बचा रहे थे। वे देख पा रहे थे कि भारत को 'बुद्धि विरोधी और ज्ञान विरोधी' भक्तिवादी 'रस के प्रवाह' में बहा कर डुबोया जा रहा था। पार निकलने या किनारे पर आ लगने के लिए ज्ञान विज्ञान के ऐसे स्रोतों में लौटने की ज़रूरत थी, जिनका पुनर्निर्माण हममें खुद अपने युगबोध के मुताबिक करना होता है।
प्रसाद देख पा रहे थे कि औपनिवेशिक दौर में हिन्दी नवजागरण किस तरह की भक्तिवादी प्रलय का साक्षी हो कर डूब रहा है। उनकी परेशानी यह थी कि अंग्रेज़ तो अंग्रेज़, खुद हमारे अपने अति सम्माननीय विद्वान, जिन्हें वे 'विज्ञ आलोचक' कहते हैं, भी उस राह पर चले जा रहे थे, जिसका आश्रय ग्रहण करने से हमारा डूबना तय था। भक्तिवाद की पुरज़ोर वकालत करने वाले ये 'विज्ञ आलोचक' कौन हैं, इस सम्बन्ध में अगर किसी को रामचंद्र शुक्ल के प्रति पूज्यभाव के कारण सच देखने में कुछ अड़चन हो, तो वे स्वयं तय कर सकते हैं कि प्रसाद और किसको 'विज्ञ' कह और मान सकते हैं?
खैर, पहले यह देख लेते हैं कि प्रसाद हिन्दी साहित्य और उसके इतिहास निर्माण की प्रक्रिया में वर्चस्वी हो गयी, पौराणिक भक्ति की व्याख्या किस रूप में करते हैं? वे उसे रस उपजाने वाली न मान कर, 'रसाभास' की अभिव्यक्ति करने वाली मानते हुए कहते हैं:
"यद्यपि भक्ति को भी इन्हीं लोगों ने (यानी तत्कालीन विज्ञ आलोचकों ने) मुख्य रस बना लिया था, परन्तु … जगत और आत्मा की अभिन्नता की विवृति उसमें नहीं मिलेगी। एक तरह से हिन्दी काव्य का यह युग संदिग्ध और अनिश्चित सा है। इसमें न तो पौराणिक काल की महत्ता है और न है काव्य-काल का सौंदर्य। चेतना, राष्ट्रीय पतन के कारण अव्यवस्थित थी। धर्म की आड़ में नए-नए आदर्शों की सृष्टि, भय से त्राण पाने की निराशा ने इस युग के साहित्य में, अवध वाली धारा में मिथ्या आदर्शवाद और ब्रज की धारा में मिथ्या रहस्यवाद का सृजन किया है।"
यहाँ भारत के अतीत को 'काव्य काल', और मध्यकाल को 'पौराणिक काल' कहा गया है। जिसे हिन्दी साहित्य के तत्कालीन इतिहासकार, ग्रियर्सन की देखादेखी, 'भक्ति काल' कहने लगे थे और उसे हिन्दी साहित्य व संस्कृति का 'स्वर्ण काल' मानने लगे थे, उसे प्रसाद 'भय से त्राण पाने की निराशा वाले युग' में प्रचलित 'अवध और ब्रज की धारा' कहते हैं। स्पष्ट है कि वे यहाँ रामभक्ति और कृष्णभक्ति की काव्यधाराओं की बात कर रहे हैं। उनके इस विवेचन के मुताबिक राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की ये काव्य धाराएं, 'मिथ्या आदर्शवाद और मिथ्या रहस्यवाद' की धाराएं हैं।
भक्ति काल की इतनी साहसिक और कटु आलोचना करने का साहस अगर प्रसाद में दिखायी देता है, तो वह उनके पास हिन्दी नवजागरण के महान उद्देश्यों और सरोकारों की पूर्ति कर सकने की चेतना के अलावा और कहीं से आया प्रतीत नहीं होता।
जिस दौर में वे अपने इन विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे थे, हिन्दी की अंग्रेज़ समर्थित अकादमिक दुनिया और आलोचना पर ग्रियर्सन और रामचंद्र शुक्ल जैसे 'बहुविज्ञ पंडितों' की तूती बोलती थी।
दूसरी ओर प्रसाद अकेले खड़े थे, अपने बूते, और भारतीय नवजागरण के तत्कालीन बुद्धिवादी और पौराणिक भक्तिवाद विरोधी स्वर में स्वर मिलाने के अपने संकल्प के बूते।
यहाँ इस बात की ओर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिसे वे 'पौराणिक काल' कहते हैं, उससे उनका तात्पर्य रामायण महाभारत काल से है। वह तुलसी और सूर के भक्तिवाद से अलग और विशिष्ट है।
तुलसी के काव्य में वे जब 'मिथ्या' हो गये 'शुद्ध आदर्शवाद' को देखते हैं, तो इस बात की उपेक्षा नहीं करते कि अकबर के काल से ले कर रामचंद्र शुक्ल के दौर तक आते आते तुलसी की 'रामायण' (रामचरित मानस) का महत्व जनसाधारण में लगातार बढा है। पर इसके पीछे वे उनके काव्य की श्रेष्ठता को न देख कर, हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान की सोच रखने वालों की भूमिका को काम करता अधिक पाते हैं। वे कहते है:
"इनका प्रभाव इतना बढा कि शुद्ध आदर्शवादी महाकवि तुलसीदास का रामायण, काव्य ना हो कर, धर्म ग्रंथ बन गया। सच्चे रहस्यवादी पुरानी चाल की छोटी-छोटी मंडलियों मैं लावणी गाने और चंग खड़काने लगे।
रहस्यवाद के 'सच्चे' पक्ष को प्रसाद भारतीय संस्कृति के 'वास्तविक स्वरूप' से उदभूत मानते हैं, परन्तु उन्हें इस बात का मलाल है कि तत्कालीन हिन्दी नवजागरण जिस तरह अपनी लीक से नीचे उतर गया था, उसमें उन जैसे ज्ञानधारा के रचनाकारों का उदात्त रहस्यवाद तक, छोटी छोटी सहृदय मंडलियों तक सीमित हो गया था। फिर भी वे 'एकला चलो रे' की भंगिमा के साथ अपने नवजागरण वाले ज्ञानोत्कर्ष को समर्पित मोर्चे पर डटे थे।
प्रसाद रहस्यवाद को 'अभारतीय' घोषित किये जाने का विरोध करते हैं। हम देख चुके हैं रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार रहस्यवाद को मैसेडोनिया और शामी देशों की सौगात मान कर, उससे अनुप्राणित कबीर की भारतीयता को ही सन्देहास्पद बना दिया था। कबीर के काव्य को सन्देहास्पद बनाने का मतलब था, 15वीं शती के भारतीय नवजागरण की मूलभूमि को सन्देहास्पद बना देना, ज्ञानधारा को भक्ति के मुकाबले हीन साबित करना और इस आधार पर कायम हो रही हिन्दू मुस्लिम एकता की ज़मीन को नष्ट कर देना। तो, यह मामला रहस्यवाद तक सीमित न हो कर, 15वीं शती के बाद में प्रकट हुए 19वीं शती के नवजागरण के सरोकारों को भी खारिज करने का मामल था। इसीलिए प्रसाद इसे ले कर इतने चिन्तित नज़र आते हैं। वे इसे विशुद्ध भारतीय वस्तु मानते हुए कहते हैं,
"साहित्य में रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है। इस से परोक्ष अनुभूति, समरसता और प्राकृतिक सौंदर्य के द्वारा अहम् का इदम् से समन्वय करने का सुंदर प्रयत्न हुआ है। वर्तमान रहस्यवाद की धारा भारत की निजी संपत्ति है, इसमें कोई सन्देह नहीं।"
इस सन्दर्भ में रामचंद्र शुक्ल के एक कथन की ओर स्पष्ट संकेत करती हुई उनकी एक अत्यन्त कटु एवं पीड़ा भरी टिप्पणी है,
"भारतीय रहस्यवाद ठीक मैसेडोनिया से आया है, यह कहना वैसा ही है, जैसा वेदों को 'सुमेरियन डौकूमेंट' सिद्ध करने का प्रयास।"
भारतीय रहस्यवाद की समुचित व्याख्या कर के प्रसाद मूलतः और मुख्यतः कबीर को हिन्दी नवजागरण के केन्द्र में लाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा करके ही यह संभव था कि तुलसी और भक्तिवाद के वर्चस्व वाले हिन्दी नवजागरण को उसकी लीक पर वापिस लाया जाता।
प्रसाद, कबीर के रूपान्तरकारी सरोकारों की ज़मीन को, सिद्धों की विद्रोही प्रवृत्तियों में खोजते हैं और इस तरह यह साबित करते हैं कि 15वीं शती के नवजागरण की भूमिका कबीर के प्रकट होने से कई सदियों पहले बननी आरंभ हो गयी थी। वे कहते हैं,
"सिद्धों ने भी वेद पुराण और आगमों का कबीर की तरह ही तिरस्कार किया है।"
'हिन्दी के आदि रहस्यवादियों' को प्रसाद, 'आनंद के सहज साधक' और 'बुद्धिवादी' कहते हैं। उनकी परम्परा में सामने आये निर्गुण सन्तों को' अन्ततः साहित्येतिहास में समुचित स्थान देना पड़ेगा, इस सन्दर्भ में प्रसाद का मत है:
"कबीर इस परम्परा के सबसे बड़े कवि हैं। कबीर में विवेकवादी राम का अवलंब है। वे 'साधो सहज समाधि भली' में सिद्धो की सहज भावना को दोहराते हैं। उन पर कुछ मुसलमानी प्रभाव पड़ा अवश्य, परन्तु शामी पैगंबरों से अधिक उन के समीप थे वेदिक ऋषि, तीर्थंकर नाथ और सिद्ध। कहना असंगत ना होगा कि उस समय हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद की इतनी प्रबलता थी कि स्वयं तुलसीदास को भी अपने महाप्रबंध में रहस्यात्मक संकेत रखना पड़ा।"
प्रसाद जब तुलसी पर कबीर के प्रभाव को चिन्हित करते हैं, तो उसका एक मकसद यह भी है कि हम इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करें कि इन दोनों में से हमें किसे ऊपर रखना चाहिए। वैसे भी तुलसी को ही यह कहने की ज़रूरत पड़ती है कि 'सगुनहिं अगुनहिं नहिं कछु भेदा'। यानी सगुण भक्ति को अपनी अपर्याप्तता को ढालने के लिए अपने आप को निर्गुण से अभिन्न बताना पड़ता है। जबकि ज्ञानधारा अपने पैरों पर आप खड़ी रहती है। उसे स्वयं को प्रमाणित करने के लिए किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ती।
परन्तु प्रसाद को यह बात चिन्तित करती है कि हिन्दी का तत्कालीन आलोचना परिदृश्य 'पश्चिमोन्मुख' होने की वजह से अपने नवजागरणमूलक दायित्व से भटक गया है। वह अपनी ज्ञान परम्पराओं को अभारतीय कहता है और औपनिवेशिक सरोकारों को प्रचारित करने में सहयोग देने वाली बातों के पक्ष में खड़ा होने के लिए 'भारतीयता की दुहाई' देता है।
"हिन्दी की आलोचना का दृष्टिकोण बदला हुआ सा लग रहा है। अब पश्चिम की विवेचन शैली का प्रभुत्व हो गया है। लेकिन ऐसी बातों के चुनाव में भारतीयता की दुहाई भी सुनी जाती है।"
"भारतीय साहित्य में सुरुचि सम्बन्धी विविधता के निदर्शन बहुत से मिलेंगे। उन्हें बिना देखे ही आजकल अत्यन्त शीघ्रता में अमुक वस्तु अभारतीय है अथवा भारतीय संस्कृति सुरुचि के विरुद्ध है, कह देने की परिपाटी चल रही है।"
"विज्ञ समालोचक भी हिन्दी की आलोचना करते करते, छायावाद रहस्यवाद आदि वादों की परिकल्पना कर के, उन्हें विजातीय विदेशी तो प्रमाणित करते ही हैं, यहाँ तक कहते हुए लोग सुने जाते हैं कि वर्तमान हिन्दी कविता में, अचेतन में, जड़ में चेतन का आरोप करना हिन्दी वालों ने अंग्रेजी से लिया है।"
"सच मानो यह आलोचकगण भारतीय संस्कृति के दो आलोक स्तंभों रामायण और महाभारत से अपनी आंख बंद कर लेते हैं। ये सब भावनाएं हमारे विचारों की सामान्यतः संकीर्णता से और प्रधानता स्वरूप विस्मृति से उत्पन्न है।"
जयशंकर प्रसाद यहाँ हिन्दी आलोचना के तत्कालीन परिदृश्य पर 'संकीर्णता' और 'स्वरूप विस्मृति' जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बात के निहितार्थ को समझना ज़रूरी है।
दरअसल यह बात उस दौर में 'विज्ञ समालोचक' समझे जाने वाले विद्वानों की, पश्चिमोन्मुख व औपनिवेशिक सरोकारों की ओर झुकी, उनकी उस विचारधारा को प्रश्नांकित करती है, जो भारतीय समाज और संस्कृति के वास्तविक स्वरूप को विस्मृत करके बैठ गयी है।
यहाँ हम यह सवाल उठा सकते हैं कि बरास्ते कबीर और प्रसाद, जब हम भारत के वास्विक स्वरूप की खोज करते हैं, तो हमारा कुल हासिल क्या होता है?
दरअसल यह खोज हमें अपनी ज्ञान परम्पराओं के स्रोत में वापसी की ओर ले जाती है, ताकि हम पश्चिमोन्मुख होने की विवशता से कुछ आज़ाद हो सकें और अपने तरीके से ज्ञान के ऐसे मौलिक विकास के नये संकल्प से युक्त हो सकें, जो ज्ञानमय होने के साथ साथ विज्ञानमय भी हो।
शुरुआत रचनाशीलता की आज़ादी से होती है। वहाँ साहित्य हमारी मदद करता है। फिर वह बात सोच और व्यवहार का मानक बन जाती है। प्रसाद के लिए काव्य का कुछ ऐसा ही मतलब है। वे कहते हैं,
"काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका सम्बन्ध विज्ञान, विश्लेषण, विकल्प से नहीं है। यह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है।"
यह जो 'रचनात्मक ज्ञानधारा' है, वह विज्ञानमय न हो कर भी, उसके पूरक की तरह अपना काम करती है। ज्ञान विज्ञान के बीच कोई विरोध नहीं है। विरोधी जोड़ा भाववाद और विज्ञानवाद का है। साहित्य और रचनाशीलता ऐसे विज्ञानवाद और भाववाद से निजात पा लेगी, तो विकास का आगे का रास्ता भी खुल जायेगा। यहाँ यह बात समझने लायक है कि प्रसाद विज्ञान और विकल्प को काव्य की वस्तु इसलिए नहीं मानते, क्योंकि वह रचनाशीलता को 'तथ्यवाद, यथार्थवाद और इतिहासवाद' मे उलझा सकती है। वे कहते हैं,
"यथार्थवादी, सिद्धांत से ही इतिहासकार से अधिक, कुछ नहीं ठहरता। क्योंकि यथार्थवाद इतिहास की संपत्ति है। किन्तु साहित्यकार न इतिहासकार होता है, न समाजशास्त्र प्रणेता। साहित्य इन दोनों की कमी को पूरा करने का काम करता है।"
प्रसाद यहाँ साहित्य और उसकी रचनाशीलता के मर्म को समझने के लिए हमें वहाँ ले जाते हैं, जहाँ इतिहास और समाजशास्त्र, साहित्य से कमतर साबित होते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रसाद साहित्य की समग्रता को कम करके आंकने वाले, किसी भी ज्ञानानुशासन के, उस पर वर्चस्व की बात को स्वीकार नहीं कर पाते।
यहीं वे पश्चिमपरस्त मानसिकता से उबरने के सूत्र तक पहुंचते हैं। पश्चिम का बुद्धिवाद, साहित्य को अपने ज्ञानानुशासनों से बांध कर, अपना पिछलग्गू बनाना चाहता है। वह इतिहास का मनमाना इस्तेमाल कर के तत्कालीन साहित्येतिहास को उसके वास्तविक स्वरूप से विच्छिन्न करने का खेल खेल ही रहा था। सामाजिकता को अतिरिक्त महत्व देकर वह हमें हमारी स्वरूपात्मक श्रेष्ठता से नीचे गिराने में लग गया था। इसे प्रसाद 'लघुता और क्षुद्रता के दर्शन’ की तरह देखते हैं। वे मानते हैं कि अभावग्रस्त वंचित जन समाज की 'वेदना की विवृत्ति' साहित्य में अवश्य होनी चाहिए, पर 'मनुष्यता के उच्चतर लक्ष्यों' का बलिदान देना किसी भी स्थिति में श्रेयस्कर नहीं। इसलिए वे अपने मनुष्यता धर्मी स्रोतों से जुड़े रह कर, वर्तमान के अभावों और वंचितों की पीड़ा का, ऐसा चित्रण साहित्य के लिए बेहतर मानते हैं, जो 'अहम् और इदम् की समरसता' तक ले जाये।
प्रसाद के लिए साहित्य की रचनाशीलता, उनके नवजागरणमूलक जीवन दर्शन का पर्याय है। उसे वे 'रचनात्मक ज्ञानधारा' कहते हैं। उसके एक ओर तुलसी और शुक्ल का भाववाद है, तो दूसरी ओर पश्चिम के वर्चस्व को स्थापित करने वाला विज्ञानवाद। ये दोनों भारतीय समाज, संस्कृति और जीवन पद्धति को अपने अपने सांचे में ढालना चाहते हैं। दोनों के सामने तयशुदा व्यवहार पद्धतियों को स्थापित करने के लक्ष्य हैं।
तुलसी के माध्यम से शुक्ल का भाववाद भारत को उस भक्ति की ओर ले जाना चाहता है, जो सेवक-सेव्य और स्वामित्व-दास्य भाव वाली मानसिकता वाले समाज का गठन करना चाहता है।
दूसरी ओर विज्ञानवाद भारत के इतिहास और संस्कृति की ऐसी व्याख्या कर रहा है, जिससे पश्चिम की श्रेष्ठता प्रमाणित हो और भारत अपने हीन भाव के साथ उनकी अधीनता स्वीकार कर ले।
प्रसाद की ज्ञानधारा इन दोनों का रचनात्मक इस्तेमाल करने के लिए अपनी स्वतन्त्रता को सब से ऊपर रखती है। वह भाव को 'आत्मा के अभिनय' के रूप में ग्रहण करती है और 'जड़ चेतन सभी के साथ एकाकार होने' के लिए स्वतन्त्र हो जाती है। इसलिए वह किसी आराध्य के सामने घुटने नहीं टेकती।
दूसरी ओर वह इतिहास के सामाजिक और वैज्ञानिक रूपों का विस्तार कर के उन्हें 'ज्ञात की सीमा के बाहर मौजूद अज्ञात' में ले जाती है, और मनुष्य के 'अपने तौर पर मनुष्य हो सकने' की स्वतन्त्रता की रक्षा करती है।
इस लिहाज से प्रसाद, प्रेमचंद से एक हद तक सहमत हो कर भी, वहीं, यानी 'ज्ञात की सीमा' में ही नहीं बंधते। वे सामाजिक इतिहास के पार मौजूद 'मानव जीवन के इतिहास' की ओर चले जाते हैं। प्रेमचंद ने उनके उप न्यास 'कंकाल' को पढा, तो उन्हें लगा कि वहाँ बहुत कुछ प्रशंसनीय है। पर वे प्रसाद के 'गड़े मुर्दे उखाड़ने' के अर्थ और महत्व को नहीं समझ पाये। प्रसाद ने अपनी एक कविता में इसे दधीचि के रूपक की मदद से स्पष्ट किया था। दधीचि के अस्थि शेष में लौटना, गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं है। वहाँ हम स्वेच्छा से किये गये अपने अस्थिदान से, राक्षसों के अन्त के लिए वज्र का निर्माण होता देखते हैं। वह मुर्दों को मुर्दों की तरह पीछे छोड़ना है, और उस जीवन-धारा से परिपूर्ण होना है, जो वहाँ अतीत से ले कर वर्तमान तक अबाध और अविरल रूप में अब तक हमारी देह में प्रवाहित है। वह इस ज्ञाताज्ञात इतिहास बोध से युक्त हो कर हर तरह के भाववादी पाखंड और विज्ञानवाद छल के मुकाबले में वज्र संघर्ष के लिए तैयार होना है।
हम देख सकते हैं कि आज हमारे मौजूदा उत्तराधुनिक दौर में, एक दफा फिर से भाववाद और विज्ञानवाद के नये रूप प्रकट हो कर, हमें अपने सांचों में ढालना चाहते हैं। भक्तिवादी भाववाद हमारी 'सामाजिक एकरूपता' को अपना नया लक्ष्य बना कर चल रहा है। इससे हमारे यहाँ, नयी जातीय अस्मिताओं का जो प्रजातान्त्रिक उभार हुआ, उनकी विविधता और बहुलता खतरे में पड़ गयी है। साहित्य इन अस्मिताओं के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखा रहा है। पर आलोचना परिदृश्य अभी तक उस नुक्तेनिगाह से अपने साहित्येतिहास की नवजागरण मूलक पुनर्व्याख्या के लिए कमर कस कर मैदान में उतरने से बच रहा है। दूसरी तरफ सूचना क्रान्ति वाले विज्ञानवाद की चुनौती है। वह भूमंडलीकरण के नाम पर हमारी 'ज्ञानात्मक एकरूपता' को स्थापित करना चाहता है। इससे तीसरी दुनिया अग्रविकास के लिए, हमेशा के लिए पश्चिम पर निर्भर हो जायेगी। हम भी अपने विश्वगुरु होने के भ्रम को पालते रहने के बावजूद, पश्चिम की गाड़ी में जुते एक डिब्बे से अधिक कुछ नहीं होंगे। यहाँ साहित्य को भी 'अपने वास्तविक और मौलिक ज्ञानात्मक स्वरूप को फिर से खोजने' की दिशा में गहन आत्म संघर्ष करने की ज़रूरत पडेगी।
प्रसाद की ओर इस सन्दर्भ में लौटते हुए हमें अनुमान हो सकता है कि हम पर अपने समय को नवजागरण की एक तीसरी लहर का हिस्सा हो जाने का दायित्व आयत है।
कबीर और प्रसाद, अब तक संभव हो सकीं,, नवजागरण की 15 वीं और र19वीं शती वाली पहले की, दो लहरों के महानायकों की तरह हमारे सामने उपस्थित हैं। उनके नवजागरणमूलक पुनर्पाठ, हमारे समय में प्रकट चुनौतियों के मुकाबले में हमें, अपने यहाँ घटित पहले के नवजागरणों के मूल्य बोध से लैस होने में हमारी मदद कर सकते हैं।
अब बात एक नयी तरह से अपनी जीवंत ज्ञानधारा के स्रोतों में रचनात्मक वापसी की ही नही, भविष्य के नक्शे बनाने की भी हो गयी है। शुरुआत के लिए हमें अपने साहित्य की नवजागरणमूलक पुनर्व्याख्या का काम अपने हाथों में लेना होगा। अकादमिक बहसों के और साहित्य में पांडित्य झाड़ने के मिथ्या ज्ञानाडंबर से मुक्ति पानी होगी। खुले में आना होगा, लेकिन कोरी सनसनीखेज़ सामाजिक मीडिया की बहसों में अपनी शक्ति को व्यर्थ गंवाने से भी बचना होगा।
कबीर से जुड़ने की तैयारी तो हिन्दी साहित्य के परिदृश्य में दिखायी दे रही है, पर अभी तुलसी व शुक्ल जी के प्रति श्रद्धावान हुए रहने का मोह भी हमें छोड़ नहीं रहा है। जयशंकर प्रसाद तक खुले मन से आने की तैयारी भी अभी कम ही दिखायी देती है। पर हालात संगीन होंगे, तो बर्फ भी ज़रूर पिघलेगी।
संपर्क:
ए 563 पालम विहार,
गुरूग्राम-122017
मोबाइल - 9814658098







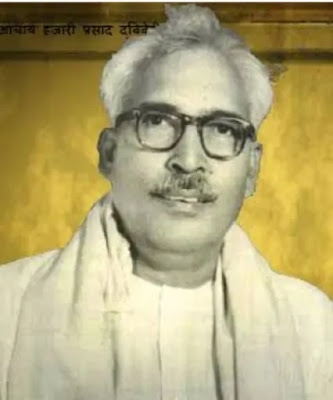





अद्भुत विश्लेषण।
जवाब देंहटाएं