कौशल किशोर का आलेख 'लघु पत्रिकाएं: कोशिश जारी है'
 |
| कौशल किशोर |
लघु पत्रिका आन्दोलन का विशिष्ट महत्त्व इसलिए भी है कि इसने नए नए रचनाकारों को परिदृश्य में आने का अवसर प्रदान किया। इस तरह हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि में प्रकारांतर से इनका अवदान मानीखेज है। छोटी छोटी जगहों से प्रकाशित होने वाली ये पत्रिकाएं स्थानीय रचनाकारों को सामने लाने का काम लगातार करती रहीं। हालांकि कई लघु पत्रिकाओं का सफर बहुत छोटा रहा लेकिन अत्यल्प अवधि में ही इन्होंने जो योगदान किया वह साहित्यिक पत्रकारिता की दुनिया में मील का पत्थर साबित हुआ। रेवांत पत्रिका के सम्पादक कौशल किशोर ने लघु पत्रिका आन्दोलन पर एक आलेख लिखा है। आइए आज पहली बार पर हम पढ़ते हैं कौशल किशोर का आलेख 'लघु पत्रिकाएं: कोशिश जारी है'।
'लघु पत्रिकाएं: कोशिश जारी है'
कौशल किशोर
साहित्य के क्षेत्र में पांच दशक से अधिक की यात्रा हो चुकी है। पीछे मुड़ कर देखता हूं तो स्मृतियां लघु पत्रिकाओं पर टिक जाती हैं। मेरी इस यात्रा में लघु पत्रिकाएं एक साथी के रूप में हमेशा मौजूद रही हैं। यह कहने में गुरेज नहीं कि यदि इनका संग-साथ न मिलता तो क्या यह यात्रा आगे बढ़ पाती। उसने मुझ जैसे नए रचनाकार को लिखने-पढ़ने की भूख पैदा की तथा छपने-छपाने का मंच प्रदान किया। यदि यह नहीं होता तो अपना लिखा डायरी या कॉपी में ही रह जाता। शायद वहीं विराम भी लग जाता।
1960 के दशक का उत्तरार्द्ध तथा 70 के दशक का पूर्वार्द्ध साहित्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौर में रचना और विचार की जमीन बदली। इसके पीछे नक्सलबाड़ी किसान आंदोलन की भूमिका थी। साहित्य आधुनिकतावाद-अराजकतावाद से मुक्त हो कर वामपंथी दिशा की ओर अग्रसर हुआ। बड़े पैमाने पर नये लेखक सामने आए। उन्हें अपने को अभिव्यक्त करने के लिए मंच चाहिए था। बड़ी व सेठाश्रयी पत्रिकाओं के बरक्स युवा लेखकों ने पत्रिकाएं निकालीं। ये बड़ी पत्रिकाओं के बरक्स निकली थीं, इसलिए ये लघु पत्रिका से जानी गईं।
उस दौर में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली आदि राज्यों से पत्रिकाएं निकलीं। शहरों ही नहीं छोटे-छोटे कस्बों और गांवों तक से इनका प्रकाशन हुआ। बिहार के गढ़हरा, बेगूसराय से 'द्वाभा' (संपादक - रामेश्वर प्रशांत), बगेन, आरा से 'प्रगति' (संपादक - विजेन्द्र अनिल), गिद्धौर, मुंगेर से 'लेकिन' (संपादक - विनय अश्म), कांकरोली, राजस्थान से 'संबोधन' (संपादक - क़मर मेवाड़ी) आदि दर्जनों गांवों-कस्बों से अनेक पत्र-पत्रिकाएं सामने आईं। हावड़ा/कोलकाता जैसे शहरों से दर्जन भर पत्रिकाएं सामने आईं। प्रिंट रूप में ही नहीं साइक्लो व लिथो प्रिंटिंग के द्वारा उनका प्रकाशन हुआ। इनकी संख्या सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में रही हैं। इनमें एक जिद्द, जुनून और प्रतिबद्धता थी जिसके कारण इसने स्वत: स्फूर्त आंदोलन का रूप ले लिया। सचमुच में यह लघु पत्रिका आंदोलन था। लेखकों के लिए पत्रिका लेखन का हथियार थी। समझ भी यही थी कि क्रांतिकारी दौर में इसी के माध्यम से उनकी सामाजिक भूमिका हो सकती है। आज वह सब बातें रूमानी लग सकती हैं। लेकिन उस दौर की यही सच्चाई है।
लघु पत्रिका को ले कर लेखकों और संपादकों के अपने-अपने अनुभव हैं। मेरे भी हैं, जिन्हें मैं संक्षेप में साझा करना चाहता हूं। बलिया से निकलने वाली पत्रिका 'युवा लेखन' की योजना 1972 में बनी। पहला अंक 1973 में आया। यह सोवियत रूस की अक्टूबर क्रांति के अवसर पर प्रकाशित अंक था। इसकी पहली कहानी चारू मजूमदार की शहादत को ले कर थी। पत्रिका का दूसरा अंक मशहूर कम्युनिस्ट नेता मुजफ्फर अहमद उर्फ काका बाबू की स्मृति को समर्पित था। पत्रिका के लेखकों में जगदंबा प्रसाद दीक्षित, राम निहाल गुंजन, विजेन्द्र अनिल, निर्भय मलिक, सकलदीप सिंह, रामेश्वर प्रशांत आदि शामिल थे।
1975 के जनवरी महीने में मैं लखनऊ आ गया। अब यही स्थाई निवास था और बन भी गया। मैं गांव व कस्बे से आया था इसलिए यहां के साहित्यिक-सामाजिक माहौल में हस्तक्षेप के लिए पत्रिका की जरूरत शिद्दत से महसूस हो रही थी। उस वक्त लखनऊ से नरेश सक्सेना व विनोद भारद्वाज के संपादन में 'आरंभ' निकल रही थी। 'कात्यायनी' (संपादक - अश्विनी कुमार द्विवेदी) जिसकी साहित्य जगत में अच्छी पहचान बन गई थी, वह बंद हो चुकी थी। शरद व शेषमणि पांडे 'अर्थ' निकाल रहे थे। गोपाल उपाध्याय ने 'उत्कर्ष' निकाला था। साहित्य पर अराजकतावादी दौर का असर भी था। हमने विनय श्रीकर के सहयोग से इमरजेंसी के दौरान 1976 में 'परिपत्र' का प्रकाशन शुरू किया। यह वाम विचारधारा की पत्रिका थी। इसके लेखकों में सव्यसाची, रमेश उपाध्याय, कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह, कुंवरपाल सिंह, नमिता सिंह, अलख नारायण, रामनिहाल गुंजन, विजेन्द्र अनिल, सुधीश पचौरी, मनमोहन, शलभ श्रीराम सिंह, महेंद्र नेह, शिवराम, मदन कश्यप, अरुण प्रकाश आदि शामिल थे। संपूर्ण नाटक 'जन सेवक नंबर दो' भी एक अंक में छपा।
इमरजेंसी के दौरान जिस तरह लिखने-बोलने की आजादी पर कुठाराघात हुआ था, उससे लोकतांत्रिक आकांक्षा प्रबल हुई। नई सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों का उदय हुआ। 1980 आते-आते लेखकों और सांस्कृतिक कर्मियों को संगठित करने के प्रयास शुरू हुए। लघु पत्रिकाओं की भूमिका एक संगठनकर्ता के बतौर उभरी। हमने अजय सिंह और अतुल सिन्हा के सहयोग से लखनऊ से 'जन संस्कृति' की शुरुआत की। यह नवजनवादी संस्कृतकर्मियों को संगठित करने वाला रचना और विचार का मंच बन गया। जन संस्कृति मंच के निर्माण के बाद यह मंच की पत्रिका थी। इसी तरह की भूमिका 'उत्तरार्द्ध' (संपादक - सव्यसाची) की रही है। नये लेखकों को जनवादी धारा में जोड़ने तथा जनवादी लेखक संघ में उन्हें ले आने में इसकी महती भूमिका है। भले ही 'कलम' और 'नया पथ' जलेस की आधिकारिक पत्रिकाएं हों लेकिन उतरार्द्ध ने संगठन के लिए वैचारिक जमीन तैयार करने का काम किया। कमोबेश यही भूमिका प्रगतिशील लेखक संघ को संगठित करने में 'पहल' (संपादक - ज्ञानरंजन) की है। वह घोषित रूप से प्रलेस की पत्रिका ना हो और आधिकारिक पत्र 'वसुधा' हो लेकिन 'पहल' की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र में वामपंथी सांस्कृतिक आंदोलन को मजबूत करने और उसे संगठित करने का काम किया। पत्रिकाएं संगठक के रूप में सामने आईं।
 |
| रमेश उपाध्याय |
आज 'लघु पत्रिका' नाम भी आम सांस्कृतिक व्यवहार से निष्कासित होने की स्थिति में है। इसकी जगह साहित्यिक पत्रिका का नाम लिया जाता है। लखनऊ से ही करीब आधा दर्जन से अधिक पत्रिकाएं निकल रही हैं। वे हैं - तद्भव, कथाक्रम, रेवान्त, लमही, समकालीन त्रिवेणी, कविता बिहान, शब्द सत्ता आदि। इनमें इक्का-दुक्का ही संसाधनों को जुटाने में सफल हुई हैं। इन्हें देख नहीं लगता कि पत्रिका निकालने में अर्थ कोई बाधा है। रचनाओं की समस्या दीगर बात है। कुछ को पत्रिका निकालने के लिए अपनी गांठ ढीली करनी पड़ती है। वहीं कुछ पीडीएफ रूप में आ गई हैं तो कई निकल भी रही हैं तो अनियतकालीन। इस तरह एक ही शहर में लघु पत्रिकाओं का मिला-जुला चेहरा सामने आता है। रचना और सरोकार के स्तर पर भी भिन्नता है। कमोबेश यही वर्तमान परिदृश्य है।
इस तरह लघु पत्रिका के पिछले 5-6 दशक की यात्रा का सार-संकलन करें, तो हम पाते हैं कि इसके तीन चरण हैं।
पहला चरण, बड़ी और सेठाश्रयी पत्रिकाओं के बरक्स नए लेखकों का पत्रिका-प्रकाशन के क्षेत्र में प्रवेश है। इसे नवलेखन के दौर से भी जाना जाता है। इसमें रचनाकारों में उत्साह और व्यवस्था विरोध प्रधान था।
दूसरे चरण में वैचारिक प्रतिबद्धता और जन सरोकार का प्रश्न मूल था। न सिर्फ युवा रचनाकारों बल्कि उस दौर के प्रतिष्ठित रचनाकारों ने भी लघु पत्रिकाएं निकालीं और लघु पत्रिका आंदोलन को एक नई ऊंचाई व पहचान प्रदान की। पत्रिकाओं की दिशा वाम और जनवादी थी। भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कण्डेय, ज्ञानरंजन, विष्णु चंद्र शर्मा, खगेन्द्र ठाकुर, नंदकिशोर नवल, सव्यसाची, डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, आनंद प्रकाश, रमेश उपाध्याय, चंद्रबली सिंह, विमल वर्मा, हरीश भदानी, सतीश जमाली जैसे प्रतिष्ठित लेखक लघु पत्रिकाओं से जुड़े और आंदोलन को आगे बढ़ाया। समारंभ, उत्तरार्ध, कथा, पहल, वाम, भंगिमा, विचार, सर्वनाम, सामयिक, अलाव, वातायन, युग परिबोध, सिर्फ, विनिमय, अभिव्यक्ति, इसलिए, पुरुष, युवालेखन, परिपत्र, जन संस्कृति, क्यों, धरती, सर्वनाम, आमुख, कलम, कथन आदि सहित बड़ी संख्या में पत्रिकाएं इस दौर में निकलीं। इनमें से अधिकांश बंद हो चुकी हैं। इक्का-दुक्का ही निकल रही हैं।
 |
| ज्ञानरंजन |
लघु पत्रिका आंदोलन के तीसरे चरण का आरंभ हम 1990 के आसपास मानते हैं। इस दौर में लघु पत्रिकाओं के चाल-चरित्र, चिंतन तथा उसके तेवर-कलेवर में बदलाव आया। इसके पीछे नवउदारवाद का सामाजिक-आर्थिक जीवन में प्रभाव तथा उग्र सांप्रदायिक उभार है। सामाजिक शक्तियों के उभार और उनकी जनतांत्रिक आकांक्षा के कारण साहित्य में अनेक स्वर उभरे और पत्रिकाओं में इनकी अभिव्यक्ति हुई। जहां पहले द्वंद्व की प्रकृति वर्गीय थी, वहीं सामाजिक हुई। वाम और जनवादी दौर में मार्क्सवाद साहित्य का प्रमुख प्रेरक विचार था, वहीं नवउदारवादी दौर में उत्तर आधुनिकतावादी विचारों का असर देखने को मिलता है। सामाजिक न्याय आंदोलन ने अस्मिता विमर्श के लिए आधार तैयार किया। साहित्य की जमीन बदली। नये विमर्श तथा स्त्री, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पर्यावरण जैसे विषय साहित्य के केंद्र में आये। बड़े पैमाने पर पूंजी, बाजार और नई तकनीक आदि का पत्रकारिता व मीडिया में प्रवेश हुआ। उनका चरित्र बदला। चौथे स्तंभ की भूमिका लोकतंत्र की निगरानी की ना होकर पूंजी व सत्ता के चाकर की बनती गई। हिंदी अखबार हिंदू अखबार तथा मीडिया ‘गोदी मीडिया’ बन गया। सोशल मीडिया की भूमिका भी बढ़ी। वह अभिव्यक्ति के नए मंच के रूप में उभरा। आज इसे भी नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले हुए।
इस दौर में लघु पत्रिकाओं में बदलाव दिखता है। वाम-जनवादी दिशा और तेवर की जगह अस्मिता विमर्श, सांप्रदायिकता का सवाल, उपभोक्तावाद, बाजारवाद आदि का प्रभाव है। विचार की जगह बाजार की प्रधानता है। साहित्य उत्सव व मेले-ठेले का जोर है। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पुरस्कारों आदि की ऐसी होड़ शुरू हुई जिसने मध्यवर्गीय महत्वाकांक्षा, व्यक्तिवाद, अवसरवाद जैसी पराई प्रवृत्तियों को बढ़ाने का काम किया। वस्तुपरकता का पहलू कमजोर हुआ। रचनाकारों में आत्मपरकता, आत्मश्लाघा, आत्मप्रशंसा, आत्मप्रचार बढ़ा। इस दौर की अधिकांश पत्रिकाएं व्यक्तिगत प्रयासों से निकली हैं/निकल रही हैं। सामूहिकता की भावना यानी जनवाद का पक्ष कमजोर हुआ है। ऐसे में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार आवश्यक है। ---
1. स्वतंत्र रूप से निकलने वाली पत्रिकाओं तथा सरकारी संस्थानों-अकादमियों से जो निकलती हैं, इनमें क्या कोई विशेष अंतर है? अगर नहीं है तो इसके क्या कारण हैं?
2. साहित्यिक पत्रिकाओं के चरित्र को देखें। जहां कुछ के पास संसाधनों का घोर अभाव है। उनके लिए एक-एक अंक के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। कहीं न कहीं उनका कमिटमेंट और जुनून है, जिसकी वजह से पत्रिकाएं निकलती हैं। वहीं, कुछ के पास संसाधनों और विज्ञापनों की कोई कमी नहीं। वह कलेवर में साहित्यिक दिखती हैं लेकिन संचालन में व्यवसायिक हैं। बहुत कुछ इनका नजरिया बकौल धूमिल ‘विरोध में हाथ भी उठा रहे और कांख भी ढ़की रहे’ रहता है। ऐसी पत्रिकाओं के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या हो?
3. क्या आज की पत्रिकाओं का एक ही चेहरा है? उनके बीच क्या फर्क है या किया जाना चाहिए?
4. साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं के चेहरे और चरित्र में आए बदलाव को देखते हुए क्या वर्तमान में उन्हें ‘लघु’ नाम देना उचित है ? लघु से हमारा आशय क्या है? इनकी प्रतिबद्धता क्या हो?
5. क्या कहीं कोई रोशनी दिख रही है? समयांतर, समकालीन जनमत, प्रेरणा अंशु, दस्तक, फिलहाल आदि पत्र-पत्रिकाएं निकल रही हैं। इनका मुख्य स्वरूप साहित्यिक-सांस्कृतिक है। यह हमारे समय के जटिल और जरूरी सवालों को संबोधित करती हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ पत्रिकाएं हैं, भले ही संख्या में कम हैं और उनमें लघु पत्रिका आंदोलन का तेवर है, इन सब से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? और उम्मीद कर सकते हैं तो इस दिशा में पहल कैसे की जाए? क्या इनका कोई मंच बन सकता है? क्या संभावना है?
6. कोशिश की जानी चाहिए। कोशिश होगी तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। मुक्तिबोध कहते हैं 'कोशिश करो /कोशिश करो /जीने की /जमीन में गड़कर भी'।
सम्पर्क
एफ -3144, राजाजीपुरम,
लखनऊ - 226017
मोबाइल - 8400208032
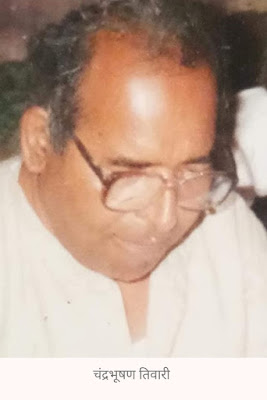



टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें