मन्नू भंडारी से ज्योति चावला की बातचीत
 |
| मन्नू भंडारी |
बीते 15 नवम्बर 2021 को प्रख्यात कहानीकार व उपन्यासकार मन्नू भण्डारी का निधन हो गया। मन्नू जी पचास के दशक की नई कहानी आन्दोलन से जुड़ी थीं। जीवन को देखने, मनोवैज्ञानिक रूप से समझने और उसे अभिव्यक्त करने का स्पष्ट नजरिया उन्हें और रचनाकारों से अलग खड़ा कर देता है।
मन्नू जी ने अनेक अप्रतिम कहानियाँ लिखीं। जिनमें कहानी 'एक प्लेट सैलाब' (1962), 'मैं हार गई' (1957), 'तीन निगाहों की एक तस्वीर', 'यही सच है', 'त्रिशंकु', 'आंखों देखा झूठ', 'अकेली ' महत्त्वपूर्ण हैं। आपका बंटी (1971), एक इंच मुस्कान (1962), 'महाभोज (1979) उनके महत्त्वपूर्ण उपन्यास हैं।
'यही सच है' पर 'रजनीगंधा' नामक फिल्म अत्यंत लोकप्रिय हुई थी और उसे 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था।
2007 में ज्योति चावला ने मन्नू भंडारी से 'शब्द संगत' के लिए एक साक्षात्कार लिया था। उस समय मन्नू जी गंभीर रूप से बीमार रहा करती थीं और रोज सेडेटिव लिया करती थीं। ज्योति ने उनसे यह साक्षात्कार कई बैठकों में लिया। बकौल ज्योति चावला 'साक्षात्कार के दौरान मन्नू जी राजेन्द्र जी के लिए अक्सर ज्यादा जोश में जो बोल जाया करती थीं उसे बाद में कटवा देती थीं।' बहरहाल मन्नू जी से ज्योति चावला का यह साक्षात्कार आज एक दस्तावेज की तरह है। मन्नू जी को नमन करते हुए आज हम पहली बार पर प्रस्तुत कर रहे हैं मन्नू भंडारी से ज्योति चावला की बातचीत।
मन्नू भण्डारी से ज्योति चावला की बातचीत
पुरुष हर जगह पुरुष ही होता है चाहे वह सवर्ण हो या दलित
ज्योति : आपकी महत्वपूर्ण रचनाएँ सन् 1950-60 के आसपास की हैं, जिस समय ‘नई कहानी’ का दौर चल रहा था। आप खुद उसका एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रही थीं, तो क्या ‘नई कहानी’ के बारे में कुछ बताएँगी?
मन्नू : मैंने सन् 1955-56 से लिखना शुरू किया था पर मेरी महत्वपूर्ण रचनाएँ तो सन् 1964 के बाद यानी दिल्ली आने के बाद आईं। हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि मेरे लेखन की शुरुआत ज़रूर ‘नई कहानी’ के दौर में ही हुई थी। पर उसके बारे में कुछ बताने से पहले मैं इस प्रचलित धारणा को ज़रूर ध्वस्त करना चाहती हूँ कि मैं उसका एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थी। ईमानदारी की बात तो यह है कि दो कहानी-संग्रह छपने तक तो मुझे नई कहानी का ककहरा भी नहीं आता था और न ही मेरा इससे कोई विषेष सरोकार था। मैं तो बस कहानियाँ लिखती थी, वे छपती थीं और पाठकों द्वारा स्वीकृत होती थीं और यही मेरा प्रमुख सरोकार था और सबसे बड़ा संतोष भी। अब क्योंकि मैं अपने लेखन के शुरुआती दिनों से ही राजेन्द्र, राकेश जी और कमलेश्वर जी के साथ रहती थी, जो नई-कहानी आन्दोलन के पुरोधा थे सो मेरा नाम भी इनके साथ जुड़ गया। यह भी हो सकता है कि मेरी कहानियों में भी वे सारी विशेषताएँ रही हों जो नई कहानी के साथ जुड़ी हुई थीं और इसलिये मुझे भी इसके झण्डे तले डाल दिया हो। आज सोचती हूँ तो यह भी लगता है कि उस समय इन लोगों के नामों के साथ जुड़ने से मुझे भी कुछ महत्वपूर्ण होने का बोध होता होगा इसीलिये मैंने भी तो कभी इसका मुखर विरोध किया ही नहीं पर महत्वपूर्ण होने का बोध होना और महत्वपूर्ण हस्ताक्षर होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। हस्ताक्षर होने के लिये जरूरी है कि आपका उस आन्दोलन के साथ गहरा सरोकार हो और उसे आगे बढ़ाने में निरन्तर सक्रिय भी हों। सरोकार क्या होता, बरसों तक तो मुझे इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी और बिना जानकारी के इसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का तो प्रश्न ही कैसे उठता भला?
अब ‘नई कहानी’ की कुछ विषेषताएँ - जिस विषय पर कुछ लोगों ने पुस्तकें लिख डालीं, उसे तुम मुझसे एक-डेढ़ पृष्ठ में जानना चाहती हो। तो बहुत मुश्किल, फिर भी बहुत मोटे रूप में कुछ बातें बताने की कोशिश करूँगी।
नए कहानीकारों ने घोषित रूप में अपने को प्रेमचन्द की परम्परा के साथ जोड़ा था। और इसे ही आगे बढ़ाना इनका लक्ष्य था। प्रेमचन्द की रचना दृष्टि और उनके लेखकीय मूल्य बहुत गहरे में समाज के साथ जुड़े हुए थे। समाज की विडम्बनाओं और विसंगतियों को उजागर करना, उन पर प्रहार करना ही उनकी रचनाओं के मुख्य विषय थे यानी कि समाज के बाहरी यथार्थ पर ही उनकी रचनाएँ केन्द्रित रहीं। इसीलिये नए कहानीकारों ने भी अज्ञेय, जैनेन्द्र की आन्तरिक यथार्थ वाली दृष्टि को छोड़ कर अपनी रचनाएँ भी समाज के बाहरी यथार्थ पर ही केन्द्रित कीं। इसके लिये उस समय बहुत ही अनुकूल अवसर भी था। गाँधीजी ने अपने समय में ही सामाजिक क्रान्ति की शुरुआत तो कर ही दी थी पर राजनैतिक आन्दोलन के चलते उस समय वह हाशिये में ही पड़ी थी। आज़ादी मिलते ही वह केन्द्र में आ गई जिससे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली। रूढ़िवादी, दक़ियानूसी समाज को बदलने के लिये विभिन्न स्तरों पर प्रयास ही नहीं होने लगे, उन पर प्रहार भी होने लगे। अब समाज का प्रमुख हिस्सा है परिवार और परिवार टिका है स्त्री-पुरुष या नई-पुरानी पीढ़ी के संबंधों पर सो इनके बदलाव अनिवार्य हो गये। महत्वाकांक्षी युवा अपना भविष्य बनाने के उद्देश्य से गाँव-कस्बे छोड़ कर शहर आ गये थे। शिक्षित होकर स्त्रियाँ भी शहरों में आकर नौकरियाँ करने लगीं तो अपने सहकर्मियों के साथ मित्रता होना स्वाभाविक था। इस स्थिति ने स्त्री-पुरुष संबंधों के बने बनाये ढाँचे को तोड़ कर नये आयाम सामने रखे और इसकी स्वाभाविक परिणति-प्रेम-प्रसंगों का सिलसिला भी चल पड़ा, जो दोनों पीढ़ियों के द्वन्द्व का कारण भी बना। शहरों में बसने के दौरान नई पीढ़ी का संघर्ष अपनी जगह और पुरानी पीढ़ी की उनसे उम्मीदें और निराशाएँ अपनी जगह। अपने आरम्भिक दौर की नई कहानियाँ मुख्यतः इन्हीं स्थितियों के विभिन्न पक्षों और पहलुओं पर केन्द्रित रहीं फिर जैसे-जैसे सामाजिक स्थितियाँ बदलती गईं, इनके विषय भी बदलते गये पर रहे वे सामाजिक स्थितियों पर ही केन्द्रित!
जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस दौर के अधिकतर कथाकार प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े हुए थे। गनीमत यही है कि इनमें से किसी ने भी अपनी रचनाओं पर इस विचारधारा को आरोपित नहीं होने दिया वरना इनकी रचनाएँ कलात्मक कृति न रह कर इस विचारधारा की प्रचारक हो जातीं।
इसमें कोई संदेह नहीं कि नये कहानीकारों का आग्रह मुख्यतः रहता कथ्य पर ही अधिक था पर उसके बावजूद किसी भी कथाकार ने शिल्प की उपेक्षा तो क़तई नहीं की। सब इस बात के प्रति पूरी तरह सचेत थे कि कलात्मक शिल्प ही किसी वास्तविक ब्यौरे को कला-सृजन में बदल सकता है और उनकी रचनाएँ अपने-अपने ढंग से इस बात का प्रमाण भी हैं।
वैसे जिस कथ्य पर कहानीकारों का आग्रह रहता था, उसके बारे में भी एक नारा उन दिनों काफ़ी प्रचलित था-भोगा हुआ यथार्थ या अनुभूति की प्रामाणिकता यानी कि वह कथ्य काल्पनिक नहीं बल्कि अपनी या किसी और की भोगी हुई वास्तविकता पर आधारित हो। हाँ, वह वास्तविकता कहानी बनने के दौरान यानी कि एक कलाकृति बनने के दौरान बदलेगी तो सही ही और कभी-कभी तो कहानी की ज़रूरत के हिसाब से इसका रूप इतना अधिक बदल जाएगा कि लेखक स्वयं नहीं पहचान पाएगा। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि बाहरी रूप चाहे कितना ही बदला हुआ हो पर उसका मूल-रूप ज़रूर किसी वास्तविकता पर ही केन्द्रित हो। कहानी के विश्वसनीय लगने के लिये यह अनिवार्य भी है। अब होने को तो और भी कई विषेषताएँ होंगी पर मैं अब अपने हिसाब से अंतिम पर सबसे महत्वपूर्ण बात कह कर इस प्रसंग को यहीं समाप्त करती हूँ। सच पूछा जाए तो यह प्रसंग नई कहानी की विशेषता के अंतर्गत तो आता भी नहीं है पर इस दौर की कहानी के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बात ज़रूर है।
इसमें कोई सन्देह नहीं कि नई कहानी आन्दोलन के दौरान एक से एक सशक्त कथाकार सक्रिय थे पर यह जुड़ गया मात्र तीन नामों के साथ - राजेन्द्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। इन्हें लोग नई कहानी की तिकड़ी भी कहते थे। कारण-अपने रचनात्मक लेखन के साथ-साथ इन तीनों ने पुरानी पीढ़ी की कहानी से इस दौर की कहानी की भिन्नता स्पष्ट करने के साथ इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि उजागर करते हुए भी बहुत कुछ लिखा। सबसे पहले राजेन्द्र यादव ने एक बहुत ही लम्बा सा लेख लिखा, जो इनके द्वारा ही सम्पादित नए कहानीकारों के संकलन ‘एक दुनिया समानान्तर’ की भूमिका के रूप में छपा। आज मैं क्या, कई लोग इसकी कुछ बातों से असहमत भले ही हों पर उस समय, या तो पहला होने के कारण या अपनी बातों के कारण इसने निस्सन्देह एक छाप तो छोड़ी थी। उसके बाद कमलेश्वर ने ‘नई कहानी की भूमिका’ नाम से एक पुस्तक ही लिख डाली। मोहन राकेश भी इन विषयों से संबंधित छिटपुट लेख लिखते ही रहते थे। अपने इन लेखों से राकेश जी और कमलेश्वर जी ने जब जहाँ मौका मिला अपने धुँआधार भाषणों से ‘नई कहानी’ का ऐसा दबदबा जमाया और उसे एक सक्रिय आंदोलन का रूप दे कर तीनों उसके पुरोधा भी बन बैठे। इधर रेणु, अमरकान्त, शेखर जोशी, भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियम्बदा जैसे अनेक एक से एक सशक्त कथाकार चुपचाप अपनी कहानियाँ लिखने में लगे हुए थे। आज इस सच्चाई से कौन इन्कार कर सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में ऐसे सक्षम और सशक्त कथाकार हिन्दी कथा-साहित्य के इतिहास में फिर कभी हुए ही नहीं। इसे मेरी पक्षधरता न समझा जाए तो यह भी सच है कि इतनी बड़ी संख्या में एक ही दौर में इतनी अच्छी कहानियाँ भी एक साथ फिर कभी शायद ही लिखी गई हों। ये मात्र स्वघोषित किये गये इन तीन पुरोधाओं का योगदान नहीं था बल्कि उस दौर के सभी कथाकारों का मिला-जुला योगदान था, जिसने उस समय कहानी को हिन्दी साहित्य की केन्द्रीय विधा बना दिया था।
ज्योति : समकालीन, ख़ासतौर पर उदय प्रकाश के बाद की कहानी कथ्य और शिल्प दोनों ही स्तर पर बहुत हद तक बदल गई है, जिसका अपना एक स्टाइल है, एक शिल्प है। क्या आपको नहीं लगता कि इस बदलाव के कारण आज की कहानी भी एक आन्दोलन की माँग करती है? इसका भी कोई नामांकन किया जाना चाहिए?
मन्नू : इसमें कोई संदेह नहीं कि अपनी पुरानी पीढ़ी की कहानियों से भिन्न होने के कारण ही हमारे दौर की कहानी को ‘नई कहानी’ कहा गया था पर यह तो तुम भी जानती हो कि ‘नई’ शब्द वैसे संज्ञा नहीं विषेषण है। यह तो जब कवि दुष्यंत कुमार ने इन कहानियों के नयेपन को देखते हुए इन्हें ‘‘नई कहानी’’ नाम दे दिया, जो बाद में स्वीकृत होकर संज्ञा की तरह चल पड़ा। अब नई कहानी के तीन प्रमुख कथाकारों (राजेन्द्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश) ने अपने रचनात्मक लेखन के साथ-साथ, पुरानी पीढ़ी की कहानी से अपने दौर की कहानी की भिन्नता और उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि को उजागर करते हुए भी बहुत कुछ लिखा (इसका संक्षिप्त उल्लेख मैं पहले कर चुकी हूँ, इसलिये दोहराऊँगी नहीं) और अपने ऐसे लेखन से ही धीरे-धीरे इन्होंने इसे एक आंदोलन का रूप भी दे दिया। यहाँ कहना मैं सिर्फ़ यह चाहती हूँ कि इस दौर की कहानी को नाम देना रहा हो या आंदोलन का रूप देना, जो कुछ भी किया इस दौर के रचनाकारों ने ही किया।
आज जब सामाजिक स्थितियाँ बदल गईं.... पूरा परिवेश बदल गया.... पारस्परिक संबंधों का स्वरूप भी बदल गया (इसके विस्तार में जाना तो संभव ही नहीं) तो स्वाभाविक है कि न पुराने मूल्य रहे होंगे.... न पुरानी संवेदनाएँ। अब ऐसे मूल्यहीन, संवेदनहीन परिवेश में जो कथाकार पनप रहे हैं, बहुत स्वाभाविक है कि उनकी रचनाओं के कथ्य भी बदलें क्योंकि हर रचनाकार अपने समाज में ... अपने परिवेश से ही तो अपनी सामग्री.... अपना कथ्य जुटाता है। और जब कथ्य बदलता है तो अपनी अभिव्यक्ति के लिये वह नए शिल्प की तलाश भी कर ही लेता है। अब अपनी पीढ़ी के कहानीकारों की पैरवी करते हुए तुम्हारा आग्रह है कि जब कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टि से अपनी पुरानी पीढ़ी की कहानी से समकालीन कहानी भिन्न हो गई तो क्या उसे भी नई कहानी की तरह एक नाम नहीं मिलना चाहिए या कि इसकी विशेषताओं के आधार पर इसके नाम से भी कोई आंदोलन नहीं चलाया जाना चाहिए?
सो ज्योति देवी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है... मैं सोचती हूँ शायद किसी को भी नहीं होगी.... पर करेगा कौन यह काम? कोई बाहर से तो आएगा नहीं। बेहतर तो होगा कि नई कहानी के रचनाकारों की तरह यह काम इस पीढ़ी के रचनाकार स्वयं करें। हाँ, इतना ध्यान जरूर रखें कि हर आंदोलन का एक वैचारिक धरातल जरूर होता है सो पहले वे अपनी कहानियों के इस वैचारिक धरातल की तलाश कर लें। रवीन्द्र कालिया के पहले ‘वागर्थ’ और अब ‘ज्ञानोदय’ के दो विशेषांकों ने और ‘कथा-देश’ के एक युवा-पीढ़ी विशेषांक ने इस काम को बहुत आसान कर दिया है। इन सारी कहानियों को एक साथ पढ़कर इनके वैचारिक धरातल और कुछ सामान्य विशेषताओं का अनुमान तो लगाया ही जा सकता है और उसी के आधार पर कोई चाहे और किसी को ज़रूरी लगे तो एक आंदोलन की शुरुआत भी की जा सकती है वरना कम से कम उसका नामांकन तो किया ही जा सकता है। इसमें किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है भला? पर करना यह काम युवा-पीढ़ी के रचनाकारों को ही होगा।
इस संदर्भ में एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी। तुम तो नई कहानी के बाद छलाँग लगा कर उदयप्रकाश का जिक्र करते हुए सीधे समकालीन कहानी पर आ गई। यह शायद भूल ही गई कि नई कहानी के बाद साठोत्तरी पीढ़ी की कहानी का दौर भी चला था। आज़ादी के मोहभंग की निराशा में लिपटी.... राजनीति और राजनीतिज्ञों के निरंतर पतन की प्रक्रिया का जीवन और संबंधों पर पड़ते प्रभाव को चित्रित करती इस युग की कहानियाँ क्या नई कहानी से बिल्कुल भिन्न नहीं थीं। इस दौर में ज्ञानरंजन, रवीन्द्र कालिया, दूधनाथ सिंह, काशी नाथ सिंह जैसे सशक्त कथाकार उभरे थे और बदले हुए इस परिवेश के चलते जिनका नज़रिया.... जिनकी संवेदना भी बिल्कुल बदल गई थी।
ज्योति : यहाँ बीच में ही एक बात पूछ लूँ? आप तो साठोत्तरी पीढ़ी की शुरुआत ही मोहभंग से मान रही हैं पर राजेन्द्र जी ने तो अपने लेख में इसे नई कहानी के साथ भी जोड़ रखा है। फिर?
मन्नू : इस बात के जवाब में अब मैं एक बात तुमसे पूछ लूँ? जब तुमने उस लेख को पढ़ा है तो उस संकलन (एक दुनिया समानान्तर) की कहानियाँ भी ज़रूर पढ़ी होंगी। अपने हिसाब से राजेन्द्र ने उसमें प्रमुख नये कहानीकारों की रचनाओं को ही संकलित किया है। अब तुम बताओ कि क्या उसमें से एक कहानी का कथ्य भी मोहभंग की मानसिकता पर आधारित है? हम कहानियों को आधार मानेंगे या लेख की बात को?
ज्योति : पर एक जिम्मेदार लेखक जब ऐसी बात लिखता है तो उसका कुछ आधार तो रहता ही होगा?
मन्नू : लगता है इस बात के चक्कर में हम अपनी बात के असली प्रसंग से ही भटक रहे हैं। चलो तुम्हारी इस बात का जवाब भी दे ही दूँ। असल में राजेन्द्र ने यह लेख सन् 64 में लिखा था और देश में मोहभंग का सिलसिला शुरू होता है सन् 62 में जब पहली बार काँग्रेस के राज्य को चुनौती देते हुए कुछ प्रान्तों में मिली जुली सरकारें बनी थीं। अब इस समय तक आते-आते तो नई कहानी के रचनाकार भी इस भावना से न तो वंचित थे न ही अप्रभावित और न ही उनका लेखन बंद हुआ था। पर उनकी रचनाओं का प्रमुख दौर तो मुख्य रूप से 50 से 60-65 तक ही माना जाता है.... उसके बाद तो साठोत्तरी पीढ़ी का दौर आ जाता है। अब राजेन्द्र जी ने क्योंकि यह लेख 64 में लिखा था तो मोहभंग की इस भावना से प्रभावित होना तो बहुत ही स्वाभाविक था पर ग़लती की तो यह कि इसे नई कहानी पर चस्पाँ कर दिया। एक बात यहाँ और स्पष्ट कर दूँ कि किसी भी दौर के कहानीकार का लेखन-समय तो कभी निश्चित किया ही नहीं जा सकता क्योंकि नये कहानीकार या साठोत्तरी पीढ़ी के या सचेतन कहानी के कथाकार आज भी लिख रहे हैं पर जब उनकी पीढ़ी की बात की जाती है तो उसके प्रमुख दौर को नज़र में रख कर ही की जाती है। सोचती हूँ तुम मेरी बात समझ गई हो। अब यह प्रसंग बंद और अपने असली प्रसंग पर ही लौटते हैं।
हाँ, तो बात चल रही थी कि नई कहानी के बाद कथ्य, शिल्प, भाषा, संवेदना सभी दृष्टि में भिन्न साठोत्तरी-पीढ़ी आई पर इस सारी भिन्नता के बावजूद न तो किसी ने उस समय इसके लिये किसी आंदोलन की माँग की न ही नामांकन की। वह तो बस अपने समय के हिसाब में साठोत्तरी-पीढ़ी कहलाई। पर सच्चाई यह है कि बिना किसी नाम और आंदोलन के इन कथाकारों ने हिन्दी कथा साहित्य के इतिहास में अपनी एक अमिट छाप तो छोड़ी ही। उसके बाद ‘सचेतन कहानी’ ‘अकहानी’ जैसे कुछ छिटपुट आंदोलन नाम के साथ भी आए तो जरूर पर न तो उनकी कोई पैठ बनी न ही कोई ख़ास पहचान। सो कहना मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि किसी भी युग की कहानियों की पहचान किसी आंदोलन या नामांकन से नहीं बनती... बनती है तो उस युग के कथाकारों की अपनी सृजनात्मक क्षमता और महत्वपूर्ण योगदान से। इसके बावजूद यदि तुम आंदोलन और नाम के प्रति आग्रही हो तो मुझे तो उसमें क़तई कोई आपत्ति नहीं। बस कुछ कथाकार मिल कर इस काम को सम्पन्न करें तो बेहतर होगा या फिर कोई समीक्षक करे यह काम।
ज्योति : एक सफल कहानीकार होते हुए आप कविता को क्या दर्ज़ा देती हैं? राजेन्द्र जी इसे साहित्य का प्रदूषण कहते हैं। कविता के पाठक कम हैं। एक उपेक्षा की दृष्टि रही है कविता को ले कर। आखिर क्या कारण है कि कविता की तुलना में कहानी को ज्यादा महत्व मिल रहा है? क्या आपने कभी कविताएँ लिखी हैं?
मन्नू : राजेन्द्र जी कविता के बारे में जो कुछ कहते हैं ज़रूरी नहीं कि वही धारणा मेरी भी हो। हालाँकि कविता में न मेरी रुचि है न गति। उसके बावजूद यह तो मैं मानती हूँ कि रचना के केन्द्रीय भाव को एक अच्छा कवि बहुत ही थोड़े शब्दों में बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से .... मारक ढंग से कह सकता है फिर हमारी तो परम्परा ही कविता की रही है। गद्य तो आधुनिक युग की देन है। रही उपेक्षा की बात सो यह धारणा तुमने उनकी बिक्री के आधार पर बना ली है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कविता की पुस्तकें कहानी की अपेक्षा बहुत ही कम बिकती हैं
क्योंकि कथा-तत्व एक आम पाठक को भी बाँध लेता है जबकि कविता के लिये एक विशेष साहित्यिक समझ की ज़रूरत होती है जो सबके पास तो होती नहीं। पर बिक्री की बात छोड़ दें तो साहित्यिक समझ की ज़रूरत होती है जो सबके पास तो होती नहीं। पर बिक्री की बात छोड़ दे तो साहित्यिक जगत में तो कविता की उपेक्षा है नहीं। साहित्य अकादमी के पुरस्कारों की सूची देखिए, कवियों को कहानीकारों की अपेक्षा कहीं अधिक पुरस्कार मिले हैं। नई कहानी आन्दोलन शुरू हुआ था जो ख़ूब प्रचलित भी हुआ, सो यह धारणा भ्रामक है कि कविता को ले कर उपेक्षा की दृष्टि रही है ... हाँ, उसका क्षेत्र जरूर साहित्यिक जगत तक ही सीमित है जो निरन्तर छोटा भी होता चला जा रहा है और कहानी के लिये ज़रूरी है मात्र शिक्षित होना .... और शिक्षितों की संख्या तो निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। पर इसके बावजूद प्रमुख कवि हमेशा पढ़े गये हैं और आगे भी पढ़े जायेंगे। इस तथ्य को क्या कहोगी कि अधिकतर लेखक अपना रचनात्मक-जीवन कविता से शुरू करते हैं। आखि़र कुछ सोच कर ही करते होंगे। मैंने जिन्दगी में न कभी कविता लिखी न ही लिखने की क्षमता है। पर यह उपेक्षा नहीं मेरे अपने सामर्थ्य की बात है। मेरा व्यक्तित्व शुरू से ही काव्यात्मक नहीं गद्यात्मक रहा है।
ज्योति : आपके ‘महाभोज’ उपन्यास की रचना 1979 में हुई थी जबकि कांशी राम ने तो दलितों की पार्टी बसपा की स्थापना 1984 में की थी। आश्चर्य है कि आपने कांशी राम द्वारा उठाये गये दलित शक्ति और दलित राजनीति के मुद्दे को को पहले ही समझ लिया और जान गईं कि दलित-वोट बैंक क्या चीज है और भारतीय राजनीति में उसकी क्या अहमियत है? इस जानकारी के प्रेरणा स्रोत?
मन्नू: लगता है तुमने इस उपन्यास को थोड़ा ग़लत समझ लिया है। हाँ, इस उपन्यास का प्रेरणा-स्रोत जरूर बेलछी-कांड रहा है और बेलछी में तेरह किसानों को पेड़ से बाँध कर जिन्दा जला दिया जाना, इस कांड का आधार था। एक पत्रिका में इसका वर्णन पढ़ कर मैं इतनी भाव-विह्वल रही और सोचा भी कि इस पर कुछ लिखूँगी पर तलाश थी किसी वैचारिक आधार की क्योंकि केवल भाव-विह्वलता के आधार पर तो कुछ लिखा नहीं जा सकता। कुछ महीनों बाद अपराधी-व्यक्ति के पैरोल पर छूट कर चुनाव लड़ने और थम्पिंग मैजोरिटी से जीतने पर मुझे वह आधार मिला-हमारे यहाँ की चुनाव-प्रक्रिया की जोड़-तोड़, उठा-पटक और तिकड़मबाजी! सो इस उपन्यास की का केन्द्रीय भाव दलित राजनीति से नहीं, यहाँ की चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। हो सके तो इस दृष्टि से एक बार उपन्यास फिर से पढ़ो.... बात साफ़ हो जाएगी।
ज्योति : यू. पी. में मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज दलितों की अपनी पार्टी की विजय तो हो गई लेकिन क्या यह प्रश्न आज भी बरकरार नहीं है कि अत्यंत दलितों की स्थिति का क्या होगा? ‘महाभोज’ के संदर्भ में कहूँ तो उन दलितों का क्या होगा जिन्हें जला दिया गया?
मन्नू : वैसे तो यह खुशी की बात है कि यू.पी. जितने बड़े प्रान्त की मुख्यमंत्री आज एक दलित महिला बनी। वैसे कुछ दलितों को मैंने इस बात पर आपत्ति करते ज़रूर सुना कि सवर्णों का सहयोग ले कर वे कांशीराम के लक्ष्य से ही च्युत हो गईं। व्यक्तिगत रूप से मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं दिखाई दी बशर्ते वे निम्न वर्ग के दलितों की स्थिति सुधारने के लिये कुछ ठोस काम करें।
ज्योति : वर्तमान में आप दलितों की स्थिति को कैसे देखती हैं?
मन्नू : ख़ुशी की बात है कि सदियों से असह्य-यातनाएँ सहता हुआ हाशिये पर पड़ा यह वर्ग धीरे-धीरे अब सभी क्षेत्रों में केन्द्र में आ रहा है। सांसदों और विधायकों की बढ़ती संख्या के साथ राजनीति में इसके बढ़ते प्रभुत्व से सभी परिचित हैं। यू. पी. जैसे बड़े प्रान्त की मुख्यमंत्री आज दलित वर्ग की महिला है। इधर आरक्षण द्वारा ऊँची शिक्षा पा कर ऊँचे ओहदों पर पहुँचना, अफसरशाही में इनकी स्थिति को उजागर करता है। अनेक कवि-कथाकारों ने अपनी रचनाओं में विशेषकर अपनी आत्मकथाओं से दलित-साहित्य की भी एक अलग पहचान बनाई है। ये सारी बातें इसी बात का प्रमाण हैं कि दलितों की स्थिति में (विशेषकर एक वर्ग के दलितों की) तो काफ़ी सुधार आया है। पर जहाँ तक इस वर्ग के लोगों की बात है, सामाजिक स्तर पर गाँव-देहात के अशिक्षित लोगों के बीच आज भी बराबरी का दर्ज़ा नहीं दिया जाता। एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करूँगी।
एक बार मुझे कालेज की छात्राओं के साथ सूखा पीड़ितों के राहत कार्य के लिये बीकानेर जाना पड़ा। कलेक्टर अन्दरूनी गाँवों में जाने की हमारी सारी व्यवस्था करवाने वाले थे, सो हम उनसे मिलने पहुँचे। उनके पास पहले से कोई बैठा हुआ था इसलिए हम बाहर इंतज़ार करने लगे। एकाएक एक लड़की ने उनकी नेम प्लेट देख कर ऐसे ही जिज्ञासावश पूछ लिया- अरे इन्होंने अपना सरनेम तो लगा ही नहीं रखा... अधूरी नहीं लग रही नेम प्लेट?
बाहर साफा बाँधे स्टूल पर बैठे चपरासी ने यह सुनते ही जिस हिकारत से कहा ‘‘अरे कैसे लगाएगा सरनेम... मीणा जो है।’’ वह बात आज तक मेरे मन पर खुदी हुई है। ओहदे में चपरासी पर अपने बास कलेक्टर के लिये मन में ऐसी हिक़ारत सिर्फ़ इसलिए कि वह मीणा है। और अशिक्षितों के बीच में आज भी यह एक हक़ीकत है जो शिक्षा के प्रचार के साथ ही दूर होगी।
अब एक शिकायत इस वर्ग से मेरी भी। जो लोग किसी क्षेत्र में आज ऊपर पहुँच गये हैं वे अपने से नीचे के दलितों को ऊपर उठाने की बजाए अपनी ही और और तरक्की की जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। एक बार भी नहीं सोचते कि दबा कुचला एक बहुत बड़ा वर्ग उनकी मदद की... उनके सहयोग की उम्मीद में आज भी नीचे ही पड़ा है। क्यों नहीं ये लोग उनके लिये भी कुछ करते हैं?
ज्योति : दलित जातियों में क्रीमीलेयर का भी एक मुद्दा है। आपकी इस बारे में क्या राय है?
मन्नू : मुद्दा तो शायद क्रीमीलेयर के आरक्षण का है। जानती हूँ इस बारे में मुँह खोलते ही मुझ पर आरोपों की बौछार होने लगेगी पर अब इससे चुप रहना भी तो मेरे लिये संभव नहीं है। सच बात तो यह है कि क्रीमीलेयर में आने वाले दलित सभी स्तर पर सुविधासम्पन्न हैं - चाहे राजनीति हो, अफ़सरशाही हो या आर्थिक स्तर, दलितों के नाम पर मिलने वाली सारी सुविधाएँ - ये अपनी ही झोली में तो डालते रहे हैं आज तक। वंचित रहा है तो अन्त्योदय वर्ग, इसीलिये उसकी स्थिति में आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इस वर्ग का शोषण करने में भी क्रीमीलेयर के दलितों को आरक्षण? अब आज यदि लालू यादव या मुलायम सिंह यादव के बच्चों को इस आधार पर आरक्षण मिले तो इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? इस बारे में मेरी बहुत स्पष्ट धारणा है कि दलितों में भी आरक्षण का आधार आर्थिक ही होना चाहिए। इस स्थिति में क्रीमीलेयर के दलित अपने आप इस सुविधा से वंचित हो जाएँगे।
ज्योति : पहले हिन्दी साहित्य की रचनाओं पर फ़िल्म बनने की एक परम्परा रही है, जैसे प्रेमचन्द, कमलेश्वर, राजेन्द्र यादव, और आपकी रचनाएँ। आज ऐसा कम देखने को मिलता है-इसका कारण? साहित्य और फ़िल्म की इस बढ़ती दूरी को आप कैसे देखती हैं? फ़िल्मे ज़्यादा कमर्शियलाइज्ड हो गई हैं या साहित्य ज़्यादा कठिन?
मन्नू : हिन्दी कथा साहित्य के इतने लम्बे दौर में पाँच-सात फ़िल्में बन गईं तो इसे परम्परा नहीं अपवादस्वरूप ही कहा जाएगा। हाँ, बंगला में ज़रूर साहित्यिक रचनाओं पर फ़िल्मे बनने की परम्परा है और शरत चन्द की रचनाएँ तो हिन्दी तक में बराबर बनती रही हैं। उनकी देवदास तीन बार और परिणीता अभी दूसरी बार बनी। कारण, एक तो इनकी रचनाओं में दृश्य तत्व बहुत हैं यानी विजुअल में बड़ी आसानी से ट्रान्सफार्म हो सकते हैं जो फ़िल्म के लिये बहुत ही आवश्यक गुण हैं.......दूसरा उनकी कहानी में दर्शकों को अपने साथ बाँध सकने की अद्भुत क्षमता भी है। हिन्दी में तुमने जिन फ़िल्म के नाम गिनाए उनमें प्रेमचन्द की केवल शतरंज के खिलाड़ी चर्चित रही पर शुद्ध सत्यजीत रे के नाम की वजह से या बदले हुए अन्त पर कुछ विवाद चला पर आर्थिक रूप से तो यह भी सफल नहीं रही। राजेन्द्र के ‘सारा आकाश’ ने नाम कमाया केवल इसलिए कि एक सही सफल कलात्मक फ़िल्म की शुरुआत हुई थी इस फ़िल्म से। पर चली यह भी कुछ बड़े शहर के मार्निंग शो में ही। कमलेश्वर की फ़िल्म तो कमलेश्वर की कहानी पर ही बलात्कार थी....चली भी नहीं। केवल मेरी ‘यही सच है’ कहानी पर बनी फ़िल्म ‘रजनीगन्धा’ .....एक साल तक डिब्बों में बन्द रहने के बाद चली तो फिर केवल सिल्वर जुबली ही नहीं बनाई बल्कि कई अवार्ड भी जीते। मात्र एक अपवाद, सो तुम इस तकलीफ़ से तो मुक्त हो ही जाओ कि पहले की रचनाओं पर तो फ़िल्म बनने की परम्परा थी और समकालीन रचनाओं पर फ़िल्म बनने का कोई सिलसिला ही नज़र नहीं आता। वास्तविक स्थिति तो यह है कि हिन्दी की साहित्यिक कृतियों पर फ़िल्म बनने की बंगला की भाँति कोई नियमित परम्परा कभी रही ही नहीं हालाँकि इतना तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हिन्दी में भी कुछ रचनाएँ तो ऐसी जरूर होंगी जो फ़िल्म बनने की सारी ज़रूरतों को पूरी कर सकें। उसके बावजूद यदि नहीं बनती तो इसे निर्देशक और साहित्य के बीच का अन्तराल ही कहा जाएगा। अच्छी फ़िल्मे तो हिन्दी में भी आती रहती हैं। अभी अभी कुछ अच्छी फ़िल्में आई हैं जिन्हे कमर्शियल भी नहीं कहा जा सकता जैसे ‘इक़बाल’, ‘ब्लैक’ और ‘तारे जमीन पर’। ये निर्देशक की क्षमता तो प्रमाणित करती हैं पर साहित्य के साथ उनका रिश्ता नहीं, क्योंकि इनमें से तो एक भी फ़िल्म साहित्यिक कृति पर आधारित नहीं है। इन प्रसिद्ध निर्देशकों के अकाउण्ट में कोई और साहित्यिक फ़िल्म भी नहीं मिलेगी क्योंकि साहित्य के प्रति इनका कोई रुझान नही नहीं है।
ज्योति : ‘आपका बंटी’ एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसमें आपने दिखलाया है कि आधुनिकीकरण और शहरीकरण की देन एकल-परिवार में से परिवार नामक संस्था से जो आस्था ख़त्म हो रही है उसके क्या दुष्परिणाम हैं और आज तो यह समस्या अपने विकराल रूप में है। परिवार-संस्था में आप कितना विश्वास रखती हैं?
मन्नू : इसमें कोई संदेह नहीं कि बंटी की समस्या परिवार के टूटने यानी माता-पिता के अलग होने से आरम्भ होती है पर वह विकराल रूप तो धारण करती है माँ के पुनर्विवाह से। पिता से अलग होने पर भी वह माँ के साथ प्रसन्न है। वहाँ उसका घर है, फूफी है, बगीचा है, माली काका हैं। माँ के नया-परिवार बसाते ही एक-एक कर के सब उसकी ज़िन्दगी से निकलते हैं और वह अपने और माँ के लिए एक साथ समस्या बन जाता है। यहाँ बात परिवार में आस्था की नहीं है क्योंकि परिवार तो अजय और शकुन दोनों ही फिर से बसाते हैं। तुम्हारा प्रश्न होना चाहिए कि आधुनिकीकरण के बावजूद (स्वेच्छा से शादी जिसमें निहित है) पति पत्नी में तलाक की नौबत क्यों आती है और दुर्भाग्य से जिनकी संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती ही जा रही है। वैसे तो हर पति-पत्नी के अलग होने के अपने निजी कारण तो होते ही होंगे पर मैं यहाँ संक्षेप में कुछ सामान्य कारणों की बात ज़रूर करना चाहूँगी। पिछले 50-60 सालों में शिक्षित आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अपनी अस्मिता के प्रति पूरी तरह सचेत होने से स्त्री की स्थिति में निरन्तर सुधार आता रहा है या कहूँ कि वह सही अर्थों में आधुनिक बोध से युक्त हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े ओहदों पर कार्यरत हो कर उसका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ा है। अब इनकी तुलना में पुरुषों में कम परिवर्तन आया है। सारी शिक्षा-दीक्षा और आधुनिकता के बावजूद वे आज भी अपने सामन्ती संस्कारों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए हैं। आधुनिक से आधुनिक व्यक्ति की ज़रा सी खाल खींचिए एक सामन्ती पति बैठा मिलेगा। अब ऐसे पुरुष के साथ जिसका जामा तो आधुनिक हो पर संस्कार सारे सामन्ती हों अपनी सारी कोशिशों के बावजूद सही अर्थों में आज की आधुनिक स्त्री के लिये तालमेल बैठाना मुश्किल होता जा रहा है। परिणाम तलाक।
ज्योति : अभी हाल ही में संडे-पोस्ट में राजेन्द्र जी ने कहा कि मात्र एक कप काफी माँगना भी मन्नू को मेरा फ्यूडल व्यवहार लगता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
मन्नू : अपनी असली हरकतों को छिपाने के लिये ऐसी बातों के आवरण डालते रहना राजेन्द्र की मजबूरी है सो डालते रहते हैं। अभी जुमा-जुमा आठ दिन ही तो हुए हैं मेरी किताब आए। जिन्होंने उसे पढ़ा होगा वे ये सारी असलियत जानते ही होंगे। मुझे ऐसी बातों पर कुछ नहीं कहना।
ज्योति : आप भारत के संदर्भ में विवाह-संस्था को कैसे देखती हैं?
मन्नू : मेरे ख्याल में तुम भारत के संदर्भ में विवाह-संस्था के भविष्य के बारे में जानना चाहती हो...तो इतना समझ लो कि सारे आधुनिकीकरण के बावजूद कुछ सदियों तक तो इसे कोई ख़तरा नहीं है लेकिन इसके स्वरूप को ज़रूर बदलना होगा। इसके परम्परागत दक़ियानूसी रूप ने तो इसे परिवार में पुरुष के वर्चस्व का आधार बना रखा है, जिसमें स्त्री के लिये विवाह संबंध नहीं, मात्र बंधन बन कर रह गया है। अब आज की आधुनिक स्त्री इस बंधन को स्वीकार करने को तैयार नहीं, परिणाम जैसी कि अभी हमारी बात हुई थी तलाक की बढ़ती संख्या। ऐसी स्थिति में विवाह की जरूरत पर ही प्रश्न उठने लगे हैं। आजकल विशेष रूप से महानगरों में ‘लिव-इन’ परम्परा की जो शुरुआत हुई है वह एक तरह से विवाह संस्था का नकार ही है। जब तक संबंध अच्छी तरह निभा, साथ रहे ...जैसे ही संबंध गड़बड़ाया अलग। यहाँ तलाक की उस बेहूदी और झंझटिया प्रक्रिया से गुज़रने की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि युवा लोगों का इसकी ओर रुझान बढ़ रहा है। पर बच्चों का इससे एक तरह से नकार ही है और यदि स्वीकार है तो अलग होने पर उनकी समस्या फिर बंटी वाली ही होगी। अब बच्चों के लिये जो समस्याग्रस्त हैं ‘लिव-इन’ की वह परम्परा इस देश में जड़ें जमा पाएगी भला? संभव ही नहीं है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज-स्वीडन, फिनलैंड, नार्वे में कोई तीन पीढ़ियों से लिव-इन की परम्परा चल रही है पर मात्र चालीस पैंतालिस प्रतिशत लोग ही इस तरह रहते हैं। इन आँकड़ों की मेरी जानकारी बहुत प्रमाणिक नहीं है कुछ कम ज़्यादा हो सकती है पर इतना तो तय है कि वहाँ भी आधी जनता के क़रीब तो विवाह कर के ही रहती है। अब हमारा तो परम्परावादी देश है। यहाँ से तो विवाह संस्था के समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। बस जैसा कि मैंने पहले कहा विवाह के रूप को बदलना होगा और महानगरों में तो इसका सिलसिला शुरू भी हो गया है जो धीरे-धीरे आगे भी फैलेगा।
ज्योति : सिंगल पेरेण्ट्स की अवधारणा ज़ोर पकड़ती जा रही है। सुष्मिता सेन इसका ताज़ा उदाहरण हैं। क्या परिवार को तोड़ कर हम समाज की कल्पना कर सकते हैं?
मन्नू : अभी तो सिंगल पेरेण्ट्स की स्थिति न के बराबर है। सुस्मिता सेन भी उस बच्चे को गोद लिया हुआ कहती हैं। केवल नीना गुप्ता ने यह साहस दिखलाया है। देखो; एक समय में विधवा विवाह वर्जित था आज बच्चे के साथ विधवा स्त्री से विवाह किया जा रहा है या नहीं? लिव-इन परम्परा में तो ऐसी स्थितियों की पूरी संभावना है। जब यह स्थिति बढ़ेगी तो इसके समाधान भी निकलेंगे वैसे अभी मैं ऐसी लड़कियों की..... थोड़ी बहुत अभी वे जहाँ कहीं भी हैं प्रशंसा ही करती हूँ जो लड़कों के डिच कर देने पर बच्चे को अपने बलबूते पर पाल रही हैं.... समाज के सारे आरोप और लांछन सहने के बावजूद।
ज्योति : हिन्दी में जो स्त्री विमर्श है उसको लाने का श्रेय बहुत हद तक राजेन्द्र जी को जाता है। हिन्दी का स्त्री विमर्श महज तीन चार स्त्री साहित्यकारों के साहित्य को ही स्त्री विमर्श का पुरोधा मानता है जिसमें रमणिका गुप्ता, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, जैसी रचनाकार हैं। स्त्री विमर्श की जो परिभाषा हिन्दी में बन रही है वह है देह से मुक्ति। डा. धर्मवीर की पुस्तक ‘तीन द्विज हिन्दू स्त्रीलिंगों का चिंतन’ में इन तीनों पर विचार किया गया है कि ये तीनों अपनी अनैतिकताओं को छिपाने का एक माध्यम ढूँढ रही हैं। स्त्री विमर्श में आप देह की महत्ता को किस तरह समझती हैं?
मन्नू : एक ही प्रश्न में तुम कई बातें मिला देती हो इसलिए मेरे लिये मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। फिर भी कोशिश करती हूँ कि सिलसिलेवार उत्तर दूँ।
हिन्दी साहित्य में तो स्त्री की दयनीय स्थिति, उसके अधिकारों की बात उस समय से लिखी जा रही थी जब विमर्श शब्दकोष में कहीं दबा पड़ा था। यह तो कोई पन्द्रह-एक साल पहले एकाएक कोश से निकला और फिर तो चारों ओर अपना परचम पहराते हुए इसने सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया, ‘नामवर सिंह के विमर्श’ ‘अशोक वाजपेयी के विमर्श’ ‘दलित विमर्श’ ‘स्त्री विमर्श’। साहित्य में तो बरसों पहले लिखी गई महादेवी वर्मा की ‘श्रृंखला की कड़ियाँ’ क्या स्त्री विमर्श की पुस्तक नहीं है? इसीलिए हिन्दी साहित्य में स्त्री विमर्श की पुस्तक नहीं है? इसीलिए हिन्दी साहित्य में स्त्री विमर्श का श्रेय राजेन्द्र को मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ, हंस द्वारा प्रचारित स्त्री विमर्श का श्रेय ज़रूर राजेन्द्र यादव को जाता है। यदि अपने स्त्री विमर्श के प्रचार-प्रसार के लिये उन्होंने मात्र तीन महिला-साहित्यकारों को इसके केन्द्र में रखा है तो यह उनका अधिकार है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना।
डा. धर्मवीर की पुस्तक मैंने भी देखी है....उन्होंने इन तीन महिलाओं के बारे में जो निष्कर्ष निकाले हैं वह उनकी अपनी राय है और व्यक्ति को किसी भी विषय पर अपनी राय रखने और उसे लिखित रूप में व्यक्त करने का भी पूरा अधिकार तो है ही। उन्होंने बस वही तो किया है। बेहतर होगा हम असली बात पर चर्चा करें यानी कि स्त्री विमर्श का वास्तविक रूप।
मेरे हिसाब से ‘हंस’ का जो स्त्री विमर्श है वह ‘कथनी’ का स्त्री-विमर्श है....मात्र बौद्धिक विलास और मेरा विश्वास है ‘करनी’ के स्त्री विमर्श पर। आज दूर-दूर के कस्बों गाँवों में बेपढ़ी लिखी स्त्रियाँ कुछ संस्थाओं की मदद से जिस प्रकार अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो कर उन्हें पाने के लिये सक्रिय हो रही हैं वह ‘करनी’ का विमर्श है। उदाहरण के लिये राजस्थान के अनेक गाँवों में चलाई जा रही साथिन संस्था। कैसे गाँव की स्थियाँ पहले सुन-समझ कर अपने अधिकारों के प्रति सचेत होती हैं और फिर उन्हें पाने के लिये....स्त्रियों के प्रति होने वाले किसी भी अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सामूहिक मोर्चा बाँधती हैं। इसी तरह हरियाणा की सरपंच महिलाओं का किस्सा पढ़ा। कैसे पहले तो वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुईं और फिर हिम्मत जुटा कर निष्क्रिय पड़े उस सरकारी तंत्र की कलाई मरोड़ कर उसे सक्रिय किया और औरतों को रोज़ चार-पाँच किलोमीटर से पानी लाने की यातना से मुक्ति दिलाई। पति या ससुराल द्वारा प्रताड़ित स्त्री का मुक़दमा सामने आया नहीं कि सबके अन्याय को ठिकाने लगाते हुए फैसला स्त्री के पक्ष में। ऐसे ही कई शहरों में स्त्रियों की काउन्सलिंग करने वाली संस्थाएँ पहले बातचीत से पतियों को रास्ते पर लाने की कोशिश करती हैं बाद में स्त्रियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दे कर ज़रूरत पड़ने पर उनके पतियों को कोर्ट में भी घसीटती हैं। इस तरह आज हर प्रान्त के शहरों में, गाँवों में बिना किसी प्रचार-प्रसार के स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिये कई संस्थाएँ सक्रिय हैं और मेरे लिये यही असली स्त्री विमर्श है।
ज्योति : पर ये सारे उदाहरण क्या स्त्री सशक्तीकरण के नहीं हैं?
मन्नू : तुम क्या स्त्री सशक्तीकरण को स्त्री विमर्श से भिन्न मानती हो?
ज्योति : अच्छा, अब देह की मुक्ति पर आप क्या सोचती हैं?
मन्नू : बेहतर तो होता कि राजेन्द्र खुद स्पष्ट करते कि उनका इससे क्या तात्पर्य है? अपनी बात मैं स्पष्ट कर देती हूँ। इस पुरुष प्रधान समाज में सदियों से स्त्री के शरीर के साथ पवित्रता का जो तमगा लटका रखा है उससे स्त्री की मुक्ति क्योंकि इसके चलते ही तो आज तक विधवा तलाक़शुदा या बलात्कार की शिकार स्त्रियाँ त्याज्य मानी जाती थीं किसी एक के साथ संबंध जुड़ने पर फिर वह किसी और के साथ संबंध रखने लायक मानी ही नहीं जाती थी..... क्योंकि उस स्थिति में उसका शरीर अपवित्र माना जाता था। पुरुष चाहे दस जगह मुँह मारता फिरे उसके लिये पवित्रता का ऐसा कोई बन्धन कभी रहा ही नहीं पर स्त्री को केवल एक पुरुष यानी पति के साथ ही सारा जीवन गुज़ारना होता था। पति की मृत्यु के बाद वैधव्य-जीवन की यातनाओं से कौन परिचित नहीं? सो मेरा भी आग्रह है कि स्त्री के शरीर को पवित्रता के इस तमगे से बिल्कुल मुक्त किया जाए और जो अधिकार पुरुष को प्राप्त हैं वे उसे भी मिलें।
हाँ, देह की मुक्ति अगर किसी के लिए सेक्स की मुक्ति का पर्याय हो यानी कि स्त्री को एक साथ कई जगह सेक्स संबंध रखने की छूट हो तो उससे मेरी असहमति है। कम से कम इस देश में तो यह संभव भी नहीं क्योंकि इसके लिए एक संबंधहीन जीवन अनिवार्य है और आज तक तो हमारे देश का स्त्री विमर्श न पति-परिवार निरपेक्ष है...न संतान-निरपेक्ष। हाँ, इतनी छूट तो उसके लिये अनिवार्य है कि एक या पति के साथ संबंध गड़बड़ाने पर वह उसे छोड़ कर दूसरे के साथ संबंध जोड़ ले.... पर कइयों के साथ सेक्स संबंध साथ-साथ चलने वाली स्थिति कम से कम मुझे तो स्वीकार्य नहीं, क्योंकि संबंधों की भी अपनी एक नैतिकता होती है, एक गरिमा होती है।
ज्योति : स्त्री विमर्शकारों की जब भी चर्चा होती है तो आप उसकी गिनती में नहीं आना चाहतीं। जबकि सच यह है कि आपका साहित्य और आपका जीवन स्त्री विमर्श के कई आयामों को उठाता है। अभय कुमार दुबे भी अपने तद्भव वाले लेख में इस ओर इशारा करते हैं। क्या स्त्री विमर्श किसी झण्डे तले इकट्ठे होने का नाम ही है?
मन्नू : स्त्री विमर्श की धारणा को अपने साहित्य और जीवन में ढालने के लिये इस झण्डे के नीचे आना क्या ज़रूरी है? सच पूछो तो मैंने तो विमर्श नाम ही कोई दस वर्ष पहले ही सुना होगा। इसके पहले तो न लेखन न भाषण में इसका कहीं अता-पता ही नहीं था। पर मैं तो अनभिज्ञता के अपने उसी पुराने ठीये पर ही खड़ी रही। नाम तो जान लिया पर उसके साथ और लोगों की तरह जुड़ नहीं सकी। पर बिना जुड़े ही मुझे जो लिखना है, लिखूँगी और जो करना है सो करूँगी तो सही ही। अरे मेरी बात छोड़िये....मैंने अभी क़स्बों गाँवों की जिन बेपढ़ी लिखी स्त्रियों का जिक्र किया था जो कैसे धीरे-धीरे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो कर उन्हें पाने के लिय सक्रिय भी हो रही हैं; वे भी तो न इस झण्डे के नीचे हैं.... न ही इसका नाम जानती हैं। पर स्त्री विमर्श में उनका योगदान कम तो नहीं।
ज्योति : दलित विमर्श और स्त्री विमर्श दोनों ही हाशिये पर के विमर्श हैं। पर जब हम दलित साहित्य को देखते हैं तो उसमें स्त्रियों की स्थिति उतनी ही बदतर है। ऐसे में स्त्री दोहरी मार खा रही है। मोहनदास नेमिश्यराय का एक महत्वपूर्ण लेख भी है इस संदर्भ में - ‘दोनों गाल पर थप्पड़’। ऐसा क्यों है कि ये दोनों अस्तित्ववादी विमर्श एक साथ नहीं चल पाते?
मन्नू : ज्योति, समझ नहीं आता कि तुम्हारे इस प्रश्न पर हँसू या तुम्हारी अनभिज्ञता पर चकित होऊँ। अरे, इस बात को कौन नहीं जानता कि पुरुष हर जगह पुरुष ही होता है, वह चाहे सवर्ण वर्ग का हो या दलित वर्ग का। हाशिये में पड़े दलित वर्ग का पुरुष अपनी अस्मिता के लिये.... अपने अधिकारों के लिये सवर्ण वर्ग से चाहे लोहा लेता रहे पर हाशिये में पड़ी, दोहरी मार झेलती स्त्री के अधिकारों की बात.....उसके सुख की बात तो कभी भूल कर भी नहीं सोचेगा। सोचना मतलब अपने अधिकारों में कटौती करना, ऐसा भला वह क्यों चाहेगा? ऐसी बातें सोचना तक उसके दायरे के बाहर की बात है। शिक्षित हो कर आज स्त्रियाँ ही इस दिशा में कुछ सचेत होने लगी हैं। निर्मला पुतुल की कविताएँ इस बात का प्रमाण हैं। जैसे-जैसे स्त्रियों में यह चेतना बढ़ेगी वे खुद अपने अधिकारों के लिये लड़ेंगी और वह दिन भी अब बहुत दूर नहीं है। यह भी सच है कि जैसे उनकी यातना दोहरी है वैसे ही उनकी लड़ाई भी दोहरी होगी- पहले अपने वर्ग के पुरुषों से बाद में सवर्णों से।
ज्योति : एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, आज एक बहुत ही आम धारणा बना दी गई है कि यदि आप बौद्धिक हैं तो प्रगतिशील हैं और यदि प्रगतिशील हैं तो आपको धर्म, पूजा-पाठ और त्यौहार आदि इन सब चीज़ों से कटे रहना पड़ेगा। सही मायने में यदि पूरी तरह खुद को धर्म से काट लिया जाए तो जीवन से अनुराग ही ख़त्म हो जाएगा। एक ख़ालीपन आ जाएगा। ईश्वर और कट्टरता से अलग कर के भी तो इसे देखा जा सकता है। ईश्वर में आस्था संघर्ष के दिनों का सबसे बड़ा साथी है। बड़े-बड़े विकसित देशों में भी धर्म प्रभावहीन तो नहीं हुआ है। आपकी इस बारे में क्या राय है। रिचर्ड डाकिन्स की पुस्तक ‘द गाड डिल्यूजन’ तथा भारत में CSDS का धर्म में लोगों की आस्था का सर्वेक्षण एक अलग तरह से सोचने की माँग करता है।
मन्नू : यह प्रगतिशील लोगों की नहीं बल्कि प्रगतिवादी लोगों की धारणा है जो लोगों को ईश्वर और धर्म से कटने के लिये प्रेरित करती है। उनके हिसाब से व्यावहारिक स्तर पर धर्म लोगों के जीवन में अफ़ीम का काम करता है। प्रश्न करने की उनकी बुद्धि को कुन्द कर के उनके विकास को एक तरह से अवरुद्ध ही कर देता है। पर यही प्रगतिवादी मार्क्सवादी-कोलकाता में जहाँ सरकार भी उन्हीं की है और बहुसंख्यक जनता भी दुर्गापूजा के समय किस क़दर पगला जाते हैं यह तो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। दुर्गा की स्थापना से ले कर भसान तक ये शायद अपनी घोषणाएँ भूल जाते हैं। दुर्गा पूजा इनका धार्मिक आयोजन भी है और शायद वर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार है। किसी भी धर्म के सिलसिले में कट्टरता के बिना भी तो ईश्वर में, धर्म में एक आस्था रखी जा सकती है और मेरा विश्वास है बल्कि अनुभव है कि यह आस्था संकट के दिनों में आपको एक अनाम सी शक्ति देती है। मैंने आज तक कभी पूजा पाठ नहीं किया, मन्दिर नहीं गई, जैनी होने के बावजूद कोई व्रत उपवास तक नहीं किया उसके बावजूद ईश्वर में मेरी अटूट आस्था है। बड़े से बड़े संकट के समय यदि कोई मुझे याद आता है तो या तो ईश्वर या फिर माँ जो मृत्यु के बाद मेरे लिये ईश्वर का ही पर्याय बन गई है। कौन नहीं जानता कि इस देश की बेहद गरीब संकटग्रस्त जनता अपने सारे दुखों को भगवान भरोसे ही तो झेलती है।
जहाँ तक त्यौहारों की बात है, जीवन की उबाऊ एकरसता को तोड़ने के लिये त्यौहार भी अनिवार्य हैं। हालांकि बाज़ारवाद के चलते आज उनका रूप काफी विकृत हो गया है।
रही ‘द गाड डिल्यूजन’ पुस्तक की बात या भारत में CSDS के सर्वेक्षण का संदर्भ सो फ़िलहाल तो मैं दोनों ही-बातों से अनभिज्ञ हूँ।
ज्योति : यह तो सच है कि राजेन्द्र यादव ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत ‘हंस’ से की। जितने चर्चित वे एक लेखक के रूप में हुए उससे कहीं अधिक सम्पादक के रूप में। आखि़र हंस में ऐसा क्या ख़ास और नया था कि हंस भी इतनी सफल पत्रिका हुई और राजेन्द्र जी भी इतने सफल सम्पादक?
मन्नू : इसमें कोई संदेह नहीं कि हंस ने राजेन्द्र को अपनी प्रतिष्ठा के चरम तक पहुँचाया। अब हंस में ऐसा क्या था, यह तो उसके पाठक बताएँगे। मेरा जहाँ तक ख़्याल है पाठकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इसके संपादकीय का घोर प्रशंसक है। अनेक पाठकों के पत्र तो इसी आशय के आते हैं कि हम आपके संपादकीय के लिये ही हंस लेते और बढ़ते हैं। हालाँकि यह मेरी अपनी राय क़तई नहीं है।
ज्योति : हंस का भविष्य क्या है?
मन्नू : यह हंस के लोगों से पूछो मैं कैसे बता सकती हूँ?
ज्योति : आपका और राजेन्द्र जी का संबंध अब बहुत हद तक खुल कर आ गया है। दो छोटे छोटे प्रश्न जो अब भी खुल नहीं पाए हैं उसमें एक तो यह कि राजेन्द्र जी के वर्तमान जीवन पर, दिनचर्या और हंस के दफ़्तर पर क्या आप अब बिल्कुल विचार नहीं करतीं? दूसरा यह कि आपके संबंध अब क्या बिल्कुल समाप्त हो गये हैं?
मन्नू: ज्योति, इस तरह के साक्षात्कारों में अपने व्यक्तिगत जीवन पर बात करना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। जितना लिखना था लिख दिया ..... अब बस।
ज्योति : अपने समकक्ष साहित्यकारों में राजेन्द्र जी के अलावा नामवर जी जीवित हैं जिनसे आपका पारिवारिक संबंध रहा है। नामवर जी का जितना राजेन्द्र जी से संबंध रहा उतना ही आपसे भी। उनके पत्रों में आपका उल्लेख भी देखने को मिलता है। राजेन्द्र जी तो उन्हें कभी अपना अच्छा मित्र नहीं मान पाये पर आप अपने को उनके कितना क़रीब मानती हैं?
मन्नू : मैं नामवर जी को अग्रज की तरह माना और आज भी वैसे ही मानती हूँ। कुछ बरसों पहले तक जो घरेलू गोष्ठियाँ होती थीं उसमें वे आते थे और उसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी बातें मुझे बहुत इंसपायरिंग लगती थीं। अब गोष्ठियाँ ही समाप्त हो गईं तो मिलना भी बंद सा ही हो गया पर राजेन्द्र की तरह उनसे मेरी अंतरंगता तो कभी रही ही नहीं। यह तुम्हारी ग़लत धारणा है कि राजेन्द्र कभी उन्हें अपना अच्छा मित्र नहीं मान पाए। मित्रता का यह मतलब तो नहीं कि विचारों में भी असहमति न हो और उसे खुल कर व्यक्त न किया जाए। राजेन्द्र बोलने के साथ-साथ उसे लिख कर भी व्यक्त करते हैं, नामवर जी केवल बोलकर, इसीलिये उनका विरोध ज़्यादा प्रकट होता है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रियंवद को साक्षात्कार देते हुए नामवर जी ने कहा था कि ‘राजेन्द्र ही मेरे एकमात्र मित्र हैं।’ राजेन्द्र गद्गद् हो कर इसका उल्लेख करते रहते हैं। अब यह मित्रता इस हद तक तो एकतरफा हो ही नहीं सकती पर मेरे साथ अंतरंग मित्रता वाली बात न पहले थी न आज है। हाँ, वक़्त ज़रुरत कभी फ़ोन पर बात हो जाती है पर मात्र एक दो मिनट की और वह तो हमेशा रहेगी ही। इतना जानती हूँ कि मेरे मन में यदि उनके लिये सम्मान है तो उनके मन में भी मेरे लिये थोड़ा स्नेह तो अवश्य है।
ज्योति : उन्हें आप बिल्कुल शुरुआत से देख रही हैं। उन पर यह आरोप लगता रहा है कि वे स्थिति को देख कर अपना विचार बदल देते हैं। पंत वाला विवाद उनमें सबसे ताज़ा है। आपको क्या लगता है?
मन्नू: पिछले कुछ वर्षों से लिखित और मौखिक रूप से बराबर नामवर जी पर यह आरोप लगता रहा है तो यह निराधार तो होगा नहीं। मैंने तो पिछले कुछ वर्षों से उनके भाषण सुने ही नहीं पर पंत वाला भाषण संयोग से वसुधा में पढ़ने को मिला। महादेवी जी की शतवार्षिकी का अवसर, तो उन्हें ऊपर तो उठाना ही था... तो उनके पद्य गद्य और व्यक्तिगत जीवन को आधार बना कर जितना चाहते उठाते... पंत को गिराना क्या ज़रूरी था? इसमें कोई सन्देह नहीं कि पंत की बाद की रचनाएँ उनकी आरम्भिक रचनाओं की अपेक्षा बहुत ही हल्की हैं..... उनके बारे में नामवर जी ने कोई नकारात्मक टिप्पणी की तो इसे कुछ बहुत अनुचित तो नहीं कहा जा सकता। विचार हैं ये उनके, जिन्हें अभिव्यक्त करने की उन्हें पूरी स्वतंत्रता भी है। पर कूड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग? नामवर जी जैसे दिग्गज समीक्षक से भाषा के संयम की अपेक्षा तो की ही जाती है। कूड़ा कह देने से महादेवी जी ज़्यादा बड़ी हो जाएँगी?
कवि कवि की तुलना तो ख़ैर फिर भी वाजिब है मुझे हँसी तो तब आई और हँसी से भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ जब महादेवी जी को उठाने के लिये उनहोंने एक दूलत्ती मुझ पर झाड़ दी। वे पंक्तियाँ ज्यों की त्यों कोट करूँगी तभी बात समझ में आएगी :
‘‘सम्पूर्ण लेखन में कहीं भी महादेवी जी ने जिस व्यक्ति से उनकी शादी हुई थी उसके बारे में एक भी कटु शब्द नहीं लिखा। आजकल दो कहानीकारों स्त्री और पुरुष के बीच जो लिखा पढ़ी हो रही है वह आप पढ़ ही रहे होंगे। कोई बख्शता नहीं है। इसलिये महादेवी के स्त्री-विमर्श पर बात करते हुए ये बात बराबर ध्यान में रहे।’’ अगर महादेवी जी कुछ समय के लिये भी पति के साथ रहतीं..... उनकी ज्यादतियों और उनके अनैतिक संबंधों को बर्दाश्त करतीं और फिर भी कभी मुँह नहीं खोलतीं तो तुलना करना बिल्कुल वाज़िब होता। पर इस स्थिति में....ख़ैर छोड़िये इस प्रसंग को।
ज्योति : आपकी पुत्री रचना के बारे में बहुत कम जानकारी है। आपका बंटी में कहीं आपकी बेटी की भी छवि है?
मन्नू : उपन्यास की भूमिका में ही मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि किन तीन बच्चों की प्रेरणा से मैं यह उपन्यास लिख पाई। अंततः जब ये तीनों बच्चे गड्डमड्ड हो कर एक सामाजिक समस्या के रूप में परिवर्तित हो गये तभी बंटी का जन्म हुआ था। उपन्यास लिखते समय रचना की उम्र भी बंटी के बराबर ही थी और मैं कुछ-कुछ उन्हीं हालात से गुज़र रही थी, इसलिये कहीं अचेतन में उसकी भी कोई परोक्ष सी छवि उपन्यास में आई है, तो नहीं कह सकती पर प्रत्यक्ष रूप से तो वह कहीं नहीं है।
ज्योति : आपके मना करने के बावजूद एक प्रश्न जरूर पूछना चाहती हूँ। कभी-कभी लोग जब कहते हैं कि पैंतीस साल तक तो साथ रह लीं..... राजेन्द्र जी से जितना फ़ायदा उठाना था उठा लिया और अब यह अलग होने की मुद्रा। आपको भी बुरा तो ज़रूर लगेगा पर मैं चाहती हूँ कि आप इसका उत्तर ज़रूर दें।
मन्नू: नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मान रही। पर उत्तर (कुछ देर सोचने के बाद) आत्मीय संबंधों के दौरान भी कभी-कभी मनुष्य को यंत्रणाओं से - असह्य यातनाओं के बीच से गुज़रना पड़ता है, पर उस सबके बीच भी उम्मीद की डोर पकड़े कैसे वह आशा-अपेक्षाओं के बीच डूबता उतरता ही रहता है। मनुष्य-मन की इन बारीकियों की....भावनाओं की.....इस तरह ऊहापोह को जो लोग बिल्कुल समझ ही नहीं पाते....उसे हमेशा लाभ-हानि, फ़ायदा नुकसान की तराजू पर ही तौलते रहते हैं, उनकी बात का भी कोई जवाब हो सकता है क्या? छोड़ो इस बात को।
ज्योति : लेकिन अंततः फिर आपने संबंध तोड़ा ही।
मन्नू: जीवन में एक बिन्दु ऐसा आता है, जब महसूस होता है कि बस। अब और आगे नहीं, और वही जीवन का निर्णायक क्षण होता है।
ज्योति : बेटी ने इस अलगाव को किस तरह लिया?
मन्नू: बहुत ही सहज रूप में लिया। तब तक उसकी शादी हो चुकी थी और आज उसके हम दोनों से अलग-अलग और बहुत अच्छे संबंध हैं।
ज्योति : अभी हाल ही में कृष्णा सोबती को व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई, और उन्होंने सम्मान ठुकरा भी दिया। आप इसे कैसे देखती हैं?
मन्नू: उन्होंने इंकार करके बहुत ही सही क़दम उठाया। व्यास सम्मान तो उन्हें बहुत पहले मिलना चाहिए था। उनका क़द बहुत ऊँचा है। व्यास सम्मान देने वाली समिति को यह सोचना चाहिए था। कृष्णा जी ने अस्वीकार करके अपने व्यक्तित्व की गरिमा के अनुकूल ही क़दम उठाया।
ज्योति : कृष्णा जी कहती हैं कि ये सम्मान अब युवाओं को दिया जाना चाहिए।
मन्नू : यह तो और भी अच्छी बात है। साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता के बाद कोई सम्मान बाक़ी रह भी नहीं जाता। युवाओं के पक्ष में उनका यह निश्चय निश्चित रूप से सराहनीय है।
ज्योति : बार-बार इस घोषणा के बावजूद कि आपका लिखना बंद हो गया। कुछ वर्षों से टुकड़ों टुकड़ों में लिखी जा रही आपकी ‘एक कहानी यह भी’ पुस्तक अंततः हमें पढ़ने को मिल ही गई। ऐसी ही कोई और रचना तो नहीं चल रही...जो निकट भविष्य में हमें पढ़ने को मिल सकेगी?
मन्नू: हाँ, लिखना मुझे अब पक्का शुरू करना है। अपने पिता पर और कमलेश्वर पर शब्द चित्र लिखना है। कमलेश्वर की मृत्यु के बाद लोगों ने उन पर बहुत लिखा क्योंकि मृत्यु के बाद हर व्यक्ति महान बन जाता है। मुझे भी कई लोगों ने कहा कि मैं भी कुछ लिखूँ पर कमलेश्वर की पूजा अर्चना का दौर ज़रा ख़त्म हो जाए। मैं उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर लिखूँगी।
रिंकी भट्टाचार्य (विमल राय की बेटी) ने कुछ समय पहले अलग-अलग क्षेत्रों की छः महिलाओं से कहा कि अपने पिता का यदि एसेसमेंण्ट करें तो क्या जाएँगी। मुझे भी लिखने को कहा गया। मैंने हिन्दी में लिखा, सुधा अरोड़ा ने उसका अनुवाद किया, और मीनाक्षी मुखर्जी ने उसकी समीक्षा की, और मुझे कटिंग भी भेजी और कहा कि आपका हिस्सा सबसे बढ़िया है।
नामवर जी ने जब ‘एक कहानी यह भी’ पढ़ी तो उसकी ख़ूब तारीफ़ की और शुरू के हिस्से के बारे में कहा कि मैं अपने पिता और उज्जैन वाले हिस्से पर विस्तार से लिखूँ। सही बात तो यह है कि पिता जी के जीवनकाल में उनसे वैचारिक विरोध तो बहुत रहा, उनसे ख़ूब लड़ी भी, पर आज बैठ कर देखने पर उनके कई प्लस प्वाइंट्स दिखाई देते हैं। कई कहानियाँ हैं, जो पूरी करनी हैं लेकिन आज कल तो क़लम तक पकड़ना भारी लग रहा है। अब तो तुम लोग बस यही दुआ करो कि जल्दी से जल्दी मुझे इस बीमारी से मुक्ति मिले, रोज़ इस सेडेटिव की इतनी मात्रा न खानी पड़े।
ज्योति : मैं तो हार्दिक रूप से आपके स्वास्थ्य की दुआ करूंगी ही, पर विश्वास रखिये आपके पाठक भी यही दुआ करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर पहले की तरह सक्रिय होंगी, जिससे हमें फिर से आपकी रचनाएँ पढ़ने का मौक़ा मिले।
सम्पर्क
ज्योति चावला
ईमेल : jtchawla@gmail.com


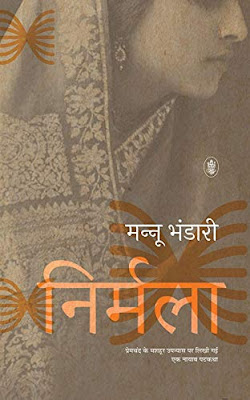








टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें