अरुण माहेश्वरी
(चित्रः गूगल के सौजन्य से)
अज्ञेय शताब्दी समारोहों के बहाने
सात मार्च 1911 को जन्मे अज्ञेय जी का शताब्दी वर्ष पूरा हो गया। हिंदी जगत में उनके लिये श्रद्धा-सुमनों की कोई कमी नहीं रही। अलग-अलग शहरों में कई आयोजन हुए। अखबारों, पत्रिकाओं में कुछ छोटी-मोटी टिप्पणियां आयीं। उनके निकट के मित्रों, संबंधियों ने एक-दो किताबें भी निकाली। कुछ स्वघोषित ‘सांस्कृतिक दूतों’ के शहर-शहर फेरे लगे। लेकिन गौर करने की बात यह है कि कुल मिला कर यह पूरा वर्ष बिना किसी वैचारिक उत्तेजना और सामाजिक-सांस्कृतिक व्यग्रता के एक स्निग्ध और शान्त, तनाव-रहित वातावरण में बीत गया।
रवीन्द्रनाथ, प्रेमचंद, और मुक्तिबोध तो जाने दीजिये, यहां तक कि तुलसी जयंती भी आज तक सामाजिक-सांस्कृतिक सवालों पर कुछ वैचारिक उत्तेजना पैदा करती है। लेकिन हाल के वर्षों तक हिन्दी में सबसे विवादास्पद समझे जाने वाले अज्ञेय की शताब्दी कोई मामूली वैचारिक आलोड़न भी पैदा नहीं कर पाये, यह स्थिति किस बात का संकेत है?
क्या यह अज्ञेय पर या आज के समय पर या दोनों पर ही कोई विशेष टिप्पणी है?
जिन नामवर जी की अज्ञेय के साथ एक मंच पर उपस्थिति से “वैचारिक रक्तपात” का कयास लगाया जाता था, उन्होंने भी इस शताब्दी वर्ष में दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थनाएं भर करके अपना काम चला लिया। और जो ‘अज्ञेयपंथ’ का झोला लिये घूमते रहे हैं, उनके पास पहले भी कहने के लिये सिर्फ श्रद्धा और भक्ति ही थी, शताब्दी वर्ष के समारोहों में भी उसी का प्रदर्शन किया गया। वैसे भी, आज के ‘समाजवाद-विहीन’ वैश्वीकरण के युग में अज्ञेय के विचारों के दो प्रमुख फलक, कम्युनिस्ट-विरोध और पूरब-पश्चिम द्वैत वाली पंडिताई के खरीदार कहां बचे हैं! कुल मिला कर इस पूरे साल ‘अज्ञेयपंथ’ और ‘नामवरपंथ’ की खूब छनी। सब कुछ भले-भले निपट गया।
इस ‘भले-भले’ ने ही आज हमारे लिये यह प्रश्न छोड़ दिया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? किसी जमाने में हिंदी में प्रगतिशील साहित्य आंदोलन के बरक्स अज्ञेय का प्रयोगवाद (परिमल) विचारधारा के एक दूसरे धुर का मंच हुआ करता था। पचास के दशक के शीत युद्ध के जमाने में एक ओर जहां सोवियत-प्रेरित समाजवाद, जनतंत्र और शांति का आंदोलन था तो दूसरी ओर अमेरिका के तत्वावधान में ‘कांग्रेस फार कल्चरल फ्रीडम’ का ‘समाजवादी निरंकुशता’ के खिलाफ ‘विचारधारा की समाप्ति’ के नारे के आधार पर तैयार किया गया पश्चिमी बुद्धिजीवियों का विरोधी मंच था। अज्ञेय जी ‘कांग्रेस फार कल्चरल फ्रीडम’ के मंच से जुड़े हुए थे, इसके अनेक साक्ष्य हिंदी में चर्चित हो चुके हैं। किसी भी वजह से प्रगतिशील साहित्य आंदोलन के साथ निर्वाह करने में असमर्थ लेखकों के लिये परिमल एक अलग मोर्चे की भूमिका अदा कर रहा था। इसीलिये स्वाभाविक तौर पर हिंदी में उस काल की सारी साहित्यिक-वैचारिक बहसों के केंद्र में अज्ञेय हुआ करते थे। लेकिन आज वह सारा विवाद कहां रफ्फू-चक्कर हो गया?
यही एक प्रश्न किसी को भी आज की साहित्यिक दुनिया के सच पर गहराई से नजर डालने के लिये प्रेरित कर सकता है।
आजादी के पहले की और शीत युद्ध के पूरे जमाने की बात छोड़ दीजिये। तब वास्तव में दुनिया दो शिविरों में बंटी हुई थी- साम्राज्यवादी और समाजवादी। 80 के दशक तक समाजवादी शिविर की अनेक बुनियादी कमजोरियों और बिखराव के उजागर होने पर भी धरती पर सोवियत संघ की मौजूदगी मात्र से विचारों की दुनिया में शीतयुद्ध का तनाव बना हुआ था। इसीलिये, तब तक भी भारत सहित बहुत से नवस्वाधीन विकासशील देशों में साम्राज्यवाद-विरोधी गुट-निरपेक्षता, गैर-पूंजीवादी विकास की संभावनाओं के आधार पर जनतंत्र और उसके विस्तार की लड़ाई की एक खास ‘समाजवादी’ दिशा थी। चीन का ‘नया जनवाद’ ढेरों नयी वैचारिक उद्भावनाओं का स्रोत था। हिंदी में तभी प्रेमचंद शताब्दी के दौरान प्रेमचंद को केंद्र में रख कर चंद्रबली सिंह ने ‘आलोचनात्मक’ और ‘समाजवादी’ यथार्थवाद के साथ ही यथार्थ की एक और, तीसरी श्रेणी ‘जनवादी क्रांतिकारी यथार्थवाद’ की अवधारणा रखी। प्रगतिशील लेखक संघ वस्तुतः बिखर गया गया लेकिन हिंदी-उर्दू के लेखकों के एक नये संगठन, जनवादी लेखक संघ (1982) का उदय हुआ। जनतंत्र का सवाल केंद्रीय सवाल बना और भारत की जनता की जनतंत्र की लड़ाई के मोर्चे की जो इंद्रधनुषी तस्वीर पेश की गयी उसमें डा. रामविलास शर्मा से लेकर अज्ञेय तक, सबके लिये समान स्थान का आश्वासन था। यह एक अलग विचार का प्रश्न है कि व्यवहार में ऐसा मोर्चा कभी भी संभव हुआ या नहीं हुआ? जाहिर है कि इस पूरे घटनाचक्र की पृष्ठभूमि में 1975 का आंतरिक आपातकाल और 1977 में जनता पार्टी तथा तीन राज्यों में वामपंथियों की भारी जीतों के अनुभव की भी बड़ी भूमिका थी। ष्
आंतरिक आपातकाल के पहले और बाद के इस दौर में अज्ञेय जीवित ही नहीं, खासे सक्रिय थे। 1965 में वे बर्कले के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लौट कर तीन सालों तक टाइम्स आफ इंडिया के हिंदी साप्ताहिक ‘दिनमान’ के संस्थापक संपादक की भूमिका निभाने के बाद 1973-74 के दौरान जयप्रकाश नारायण के साप्ताहिक ‘एवरीमैन्स वीकली’ के संपादक (1973-74) रहे और 1977-80 तक नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक का काम संभाला। वह पूरा दौर भारत में जनतंत्र की रक्षा के लिये सबसे तीव्र संघर्ष का दौर था और जयप्रकाश के साथ जुड़ कर अपने अखबारों के जरिये अज्ञेय ने उस पूरी लड़ाई में अपनी एक भूमिका अदा की थी।
फिर भी आज तक कोई यह प्रश्न क्यों नहीं उठाता है कि जनवादी लेखक संघ के वैचारिक परिप्रेक्ष्य के इंद्रधनुषी दायरे में अज्ञेय को उनके जीवित काल में कभी क्यों नहीं शामिल किया जा सका?
इस एक सवाल के जवाब से जहां प्रलेस-जलेस की विचारधारात्मक प्रतिश्रुतियों और निष्ठाओं की सचाई की परख हो सकती है, वहीं अज्ञेय की भी ‘जनतांत्रिक प्रतिबद्धताओं’ की वास्तविकता को समझा जा सकता है। कहना न होगा कि आज जहां जलेस-प्रलेस प्रकार के संगठन पार्टी की जकड़नों से बेदम होकर अस्तित्वीय संकट के गह्वर में हांफ रहे हैं, और लेखक क्रमशः जयपुर उत्सव की तरह की साहित्य-मंडियों में अपनी कीमत लगवाने को व्याकुल हो रहे हैं, वहीं अज्ञेय की ‘जनतांत्रिक प्रतिबद्धताओं’ का भी आज कोई दो-कौड़ी का दाम लगाने के लिये तैयार नहीं है। अज्ञेय शताब्दी वर्ष के आयोजनों की रपटों से तो कम से कम यही जाहिर होता है।
सचमुच यह एक अनोखी विडंबना है। नामवर का लोप ही अज्ञेय का भी लोप है। ऐसे ही ‘विचारधारा का अंत’ विचार मात्र के अंत का भी सबब बनता है।
अरुण माहेश्वरी
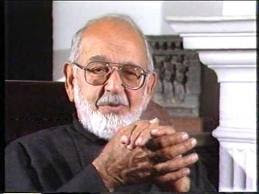




इस टिप्पणी को एक ब्लॉग व्यवस्थापक द्वारा हटा दिया गया है.
जवाब देंहटाएं