लाल बहादुर वर्मा का आलेख ‘प्रथम विश्व युद्ध जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।’
इसमें कोई दो राय नहीं कि मनुष्य इस धरती का
सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यह सर्वश्रेष्ठता उसने अपने ज्ञान और कौशल के चलते हासिल
की है। आज दुनिया की जो तस्वीर पूरी तरह बदल गयी है उसके पीछे मनुष्य के ज्ञान-
विज्ञान की ही बड़ी भूमिका है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। अपनी
सर्वश्रेष्ठता जताने के लिए वह युद्ध की तरफ उन्मुख हुआ। आधुनिक दौर में जाने के
बावजूद वह अपनी इस मनोग्रंथि से मुक्त नहीं हो पाया है। इसी वजह से दुनिया में आज
भी युद्धों का दौर जारी है। इस क्रम में मानव इतिहास का प्रथम सर्वाधिक भीषण युद्ध
प्रथम विश्व युद्ध था। दुनिया भर के राजनेताओं ने इसके बाद शान्ति बैठकें की और
युद्ध को समाप्त करने के दिखावटी प्रयास किए। इसका अंजाम दुनिया को दूसरे विश्व
युद्ध के रूप में भुगतना पड़ा। आज भी दुनिया में जगह जगह पर युद्ध लगातार हो रहे
हैं। कब कौन सा युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले ले, कहा नहीं जा सकता। यानी कि
बरबादियों के बावजूद हमने युद्धों से कोई सबक नहीं सीखा। पिछले वर्ष दुनिया ने
प्रथम विश्व युद्ध की शतवार्षिकी मनाई। इस अवसर पर प्रख्यात इतिहासकार प्रोफ़ेसर
लाल बहादुर वर्मा ने एक आलेख लिखा ‘प्रथम विश्व युद्ध जो खत्म होने का नाम नहीं ले
रहा।’ तो आइए ‘पहली बार’ पर आज पढ़ते हैं प्रोफ़ेसर लाल बहादुर वर्मा का यह
सुचिन्तित आलेख।
प्रथम विश्व युद्ध की शतवार्षिकी पर
प्रथम विश्व युद्ध जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा...
लाल बहादुर वर्मा
सौ साल
बीत गये! 1914 में, युद्ध का भूमंडलीकरण शुरू हुआ-ऐसा विध्वंस, पूरी धरती को, धरती ही नहीं धरती पर बसने वाले सबसे
प्रबुद्ध प्राणी मानव को भी, झुलसा
कर रख दिया था। बड़ी कोशिशें हुई कि ऐसा फिर न होने पाये। जैसे आदमी-आदमी के बीच के
झगड़े निपटाने के लिए न्यायालय बने हैं वैसे ही देशों के बीच झगड़े निपटाने के लिए
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय बने हैं। पर कुल बीस साल बाद पहले से भी अधिक भयानक
बर्बर और विध्वंसक द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध का अन्त होते-होते
मनुष्य ने परमाणु बम बना लिया था। और बना लिया था तो उसका प्रभाव देखना भी जरूरी
था। इसलिए उसे निर्दोष हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर गिरा कर उन्हें विलुप्त कर
दिया- ऐसा विध्वंस कि आज सत्तर साल बाद तक उसका दुष्प्रभाव पूरी तरह नष्ट नहीं
हुआ।
जब
आदमी-आदमी के बीच कुछ स्वाभाविक टकराहटें निहित स्वार्थ के झगड़ों में बदलने लगीं
तो तरह-तरह के नियम-कानून और संस्थाएँ बने। राज्य नामक सार्वभौम और सर्वशक्तिमान
संस्था का भी विकास हुआ। पर ये झगड़े हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते-बल्कि बढ़ते ही
जा रहे हैं और भयानक और भयानक रूप लेते जा रहे हैं, इसी तरह समुदायों के बीच भी टकराहटें बढ़ती गयीं। बारूद के आविष्कार
ने व्यक्तियों और समुदायों के बीच के झगड़ों को और हिंस्र और विध्वंसक बना दिया।
17वीं शताब्दी में यूरोप में युद्ध और राजनीति के बदनीयत सामन्वय से एक ऐसा
अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध शुरू हुआ जिससे मध्य यूरोप में त्राहि-त्राहि मच गयी। तभी
हॉलैंड के विचारक ग्रोशियस ने यह सोचा कि देशों के बीच झगड़ों को निपटाने के लिए
कोई न कोई उपाय तो होना ही चाहिए और उसने एक किताब लिखीं ‘राष्ट्रों के बीच युद्ध
और शान्ति के नियम’ (‘ऑन लाज ऑफ वॉर एण्ड पीस एमंग नेशंस’)। ग्रोशियस एक शान्ति
प्रिय व्यक्ति था इसलिए चाहता था कि राज्यों में आपसी सम्बन्धों का आधार कुछ नियम
हों और युद्ध की स्थिति हो सके तो आने ही न पाये और आ भी जाये तो विनाश और संहार
कम से कम हो और यथासंभव शान्ति की स्थापना हो सके। इसीलिए उसे अन्तर्राष्ट्रीय
कानून का प्रवर्तक (फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ) कहा जाता है। बहरहाल युद्ध तो बन्द नहीं
हुए, बल्कि उनका विस्तार होता गया और बीसवीं
शताब्दी में रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रथम विश्व युद्ध हो गया।
 |
| 1914 में यूरोप का मानचित्र |
युद्ध
के दौरान ही अमरीका के राष्ट्रपति इतिहासकार वुड्रो विल्सन ने प्रस्ताव किया था कि
देशों के बीव सम्बन्धों को संचालित करने के लिए एक ‘लीग ऑफ नेशंस’
बनायी जाए। उसी के प्रयासों से युद्ध
के बाद हुई पेरिस की संधियों का इसे अनिवार्य शर्त बना दिया गया और जेनेवा में एक
अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ‘लीग ऑफ नेशन’ का गठन हो गया। कुछ उत्साहित राजनेताओं ने
महत्वकांक्षी होकर ‘युद्ध पर प्रतिबंध’ लगाने की बात सोची। पर शान्ति के सारे
सपने दस साल के अंदर ही ध्वस्त हो गये और युद्ध की तैयारियां शुरू हो गयी। द्वितीय
विश्वयुद्ध अक्षरशः विश्व युद्ध साबित हुआ, क्योंकि
करीब-करीब अधिकांश विश्व बारूद की चपेट में आ गया। अब एक और शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रीय
संस्था ‘यूनाइटेड नेशंस’ का गठन हुआ। पर युद्ध खत्म होते ही
शीतयुद्ध शुरू हो गया, सैनिक गुटबंदियां शुरू हो गयी। कभी
कोरिया तो कभी वियतनाम तो कभी मध्य-पूर्व में युद्ध होते ही रहे। ऐसे भी समय आये
हैं जब जब लगा कि तीसरा विश्वयुद्ध बस शुरू ही होने वाला है। युद्ध है कि कभी यहाँ
तो कभी वहाँ चलते ही रहते हैं। अमरीका के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, जो भारत में अमरीका के राजदूत भी रहे
थे, जॉन गालग्रेथ ने दो टूक लिखा है कि
युद्ध बंद हो जायेंगे तो युद्ध/उद्योग कैसे चलेगा। अमरीका में राजनेताओं, युद्ध/उद्योग के संचालकों और पुराने
जनरलों के बीच सांठ-गांठ चलती ही रहती है। विश्वविख्यात
पुस्तक ‘साइंस इन हिस्ट्री के लेखक जे.डी.बर्नाल ने कई दशकों पूर्व शोध
करके बताया था कि दुनिया के अधिकांश प्रयोगशालाओं में शोध के केन्द्र में युद्ध
होता है।
सारांश
यह कि तमाम विध्वंसकता के बावजूद, सामान्य
जनता की शान्ति के लिए उत्कट आकांक्षा के बावजूद, शान्ति के पक्ष में बढ़ रही दलीलों और शान्ति-विमर्श के बावजूद, आज कोई भी दिन नहीं जाता जब कहीं न
कहीं युद्ध न हो रहा हो धरती पर।
ऐसा
क्यों? क्या मानव समाज मृत्यु की
आकांक्षा (डेथ-विश) के रोग से ग्रस्त है? क्या
युद्ध अ-निवार्य है? ये प्रश्न तब से पूछे जाने लगे हैं जब
से युद्ध बेलगाम और बेहद विनाशक हो गये हैं। वरना पहले तो युद्ध को गौरवान्वित
किया जाता रहा है। भारत में तो कुछ समुदायों में यह विश्वास भी घर कर गया था कि
मनुष्य जीवन मे सबसे बड़ी कीर्ति है युद्ध की बलिवेदी पर बलिदान हो जाना। ऐसे भी
शोध हुए हैं, जिन्होंने यह प्रमाणित किया है कि मानव
सभ्यता के विकास में युद्धों का भारी योगदान है, क्योंकि, खासतौर से आधुनिक काल में अधिकांश शोध
युद्ध में श्रेष्ठता और अजेयता पाने के लक्ष्य के लिए ही किये जाते रहे हैं।
समकालीन विश्व में भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अधिकांश चमत्कार युद्ध में वरीयता
पाने के लिए ही आविष्कृत हुए थे।
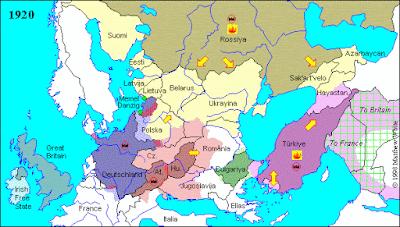 |
| Europe after the First World War |
ऐसे
में, युद्ध के स्रोत कहाँ हैं? कुछ लोग युद्ध का स्रोत मनोविज्ञान में
ढूँढते हैं। उनके अनुसार एक कहावत है कि मनुष्य एक ‘झगड़ालू प्राणी’ है (Pugnatious Animal) अगर मनुष्य का लड़ना स्वभाव ही है तो
वह किसी न किसी कारण से लड़ेगा है, कभी
व्यक्ति के रूप में, तो कभी समुदाय और देश के रूप में भी।
समाजवादी सारे इतिहास को वर्ग संघर्ष का इतिहास बताते हैं और युद्ध संघर्ष का ही
एक व्यापक रूप है। इसलिए जब तक वर्ग संघर्ष यानी मनुष्य के हित टकराते हैं तब तक
तो युद्ध होता ही रहेगा। विख्यात इतिहासकार अर्नाल्ड टॉयनबी ने लिखा है कि युद्ध
मनोविज्ञान नहीं टेक्नोलॉजी का विषय है (Matter Of Technology, Not of Psychology) यानी युद्ध विकसित हो रहे टेक्नोलॉजी
की ही अभिव्यक्ति होते हैं। तो क्या युद्धों का कभी अन्त नहीं होगा ? तो क्या युद्धों का अन्त नहीं होगा तो
मनुष्य जाति के अन्त को रोका जा सकेगा, ऐसी
पृष्ठभूमि में ही आज सौ साल बाद प्रथम विश्व युद्ध को समझने की आवश्यकता है ताकि
आज के युद्धग्रस्त समाज को युद्धोन्माद के रोग से मुक्त किया जा सके। समय आ गया है
कि आक्रामकता में मानव आवेगों की संतृप्ति को एक आत्महंता रोग के रूप में चिन्हित
किया जाए।
प्रायः
विश्वयुद्ध की जिम्मेदारी जर्मनी के सिर मढ़ दी जाती है। इसी कारण प्रथम विश्वयुद्ध
के बाद जब संधि हुई तो युद्ध की सारी जिम्मेदारी जर्मनी और उसके मित्र देश
ऑस्ट्रिया, इटली, बुल्गारिया और तुर्की के सिर मढ़ दी गयी और उन पर सारे युद्ध की
क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी लाद दी गयी। यह सच है कि ऊपर से देखने पर जर्मनी की, खासतौर से उसके तत्कालीन शासक कैसर
विलियम द्वितीय की आक्रामक नीति की तात्कालिक रूप से जिम्मेदारी थी। पर इसके कारण
इतिहास में मिलते हैं। पन्द्रहवीं, सोलहवीं
शताब्दी में जब उत्पादन के तरीके बदले और पूँजीवाद का जन्म हुआ तो इंग्लैण्ड, फ्रांस, नीदरलैण्ड आदि पश्चिमी यूरोप के देश आगे बढ़ गये, क्योंकि वहाँ पूँजीवादी विकास के लिए
आर्थिक और राजनीतिक रूप से अनुकूल परिस्थितियाँ थी। जर्मनी का क्षेत्र यूरोप में
आर्थिक रूप से सबसे अधिक संपन्न क्षेत्रों में से है। पर संयोग यह था कि यह
क्षेत्र छोटे-बड़े सैकड़ों राज्यों में विभाजित था। सोलहवीं शताब्दी में राष्ट्रवाद
के साथ-साथ पूँजीवाद का भी जन्म हुआ था और दोनों का विकास एक-दूसरे पर निर्भर रहा
होगा। जब सोलहवीं शताब्दी में धर्म सुधार का आंदोलन चला तो वह भी पूँजीवाद और
राष्ट्रवाद का पोषक साबित हुआ। जर्मनी का पहला राष्ट्र नायक मार्टिन लूथर प्रमुखतः
धर्म सुधारक था। उसने कैथोलिक चर्च ही नहीं जर्मनी के अधिकांश भू-भाग पर काबिज
पवित्र रोमन साम्राज्य का भी विरोध किया था। राष्ट्रवाद की पोषक एक राष्ट्र भाषा
भी होनी चाहिए। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा को आधुनिक विचारों का माध्यम बनाया और
जर्मनी में राष्ट्रवाद की लहर उठने लगी। पर विभिन्न कारणों से फ्रांस और इंग्लैण्ड
की तरह जर्मनी एक संगठित आर्थिक और राजनीतिक इकाई नहीं बन पाया। उसे एक होने में
तीन सौ साल लग गये। इस दौरान वहाँ राष्ट्रवाद कुंठित होता रहा और कुंठित
राष्ट्रवाद रोगी और महत्वाकांक्षी हो ही जाता है।
जर्मनी
के सबसे बड़े राज्य प्रशा और उसके प्रधानमंत्री बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी
उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ही एक हो पाया। बिस्मार्क समझ यह थी कि
जर्मनी का मूलभूत और पारंपरिक शत्रु फ्रांस है और चूंकि जंगल के एक क्षेत्र में दो
शेर नहीं रह सकते, रहेंगे तो टकरायेंगे ही, इसलिए बिस्मार्क ने फ्रांस को नीचा
दिखाना जर्मनी के गौरवान्मयन के लिए अनिवार्य समझा। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन ने
जर्मनी के राज्यों को रौंद डाला था। इसलिए बिस्मार्क ने भी जर्मनी के एकीकरण के
ठीक पहले फ्रांस से युद्ध मोल लेकर उसे बुरी तरह पराजित किया और फ्रांस की राजधानी
पेरिस में ही जर्मन राज्य नहीं ‘साम्राज्य’ की घोषणा की। 1871 के बाद बिस्मार्क की
विदेश नीति का एकसूत्रीय कार्यक्रम था फ्रांस का एकाकीकरण। इसके लिए एक तो उसने
फ्रांस के दूसरे पारंपरिक दुश्मन ब्रिटेन से मित्रता कर ली और दूसरे ऑस्ट्रिया और
इटली के साथ गुप्त रक्षात्मक संधि कर ली। इस तरह यूरोप के मध्य में इटली ऑस्ट्रिया
और जर्मनी ने एक दीवार खड़ी कर दी। जिसके एक ओर फ्रांस कुंठित होता रहा और दूसरी ओर
रूस का पूँजीवादी विकास बाधित होता रहा।
यह
कहा जा सकता है कि शीतयुद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद नहीं वास्तव में उन्नीसवीं
शताब्दी के अंतिम दशकों में ही शुरू हो गया था। शीत-युद्ध में शामिल सभी देश अपने
को आक्रांत महसूस करते हैं और लगातार संभावित युद्ध की तैयारी में जुटे रहते हैं।
यूरोप में ऐसा ही हो रहा था। यूरोप के अन्य बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस और रूस बिस्मार्क द्वारा की गयी
गुप्त सैनिक संधियों की अपने-अपने हिसाब से आकलन करते और उनका जवाब देने के लिए
लगातार तैयारियाँ करते। इस तरह यूरोप उसी समय वास्तव में दो गुटों में बट चुका था।
जो लगातार एक-दूसरे के विरुद्ध अपने को शस्त्र-सज्जित करते जा रहे थे। इस अर्थ में
ऐसा माहौल बनाने की मुख्य जिम्मेदारी बिस्मार्क की ही थी।
बिस्मार्क
के नेतृत्व में बीस वर्षों में जर्मनी की असाधारण प्रगति हुई। उस समय औद्योगीकरण
के लिए लोहा और कोयला को आधार स्तंभ समझा जाता था। ये दोनों ही जर्मनी में भरपूर
मौजूद थे। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण ही नहीं किया था एक ‘लौह नीति’ के माध्यम से जर्मनी में जनवाद और
समाजवाद के विकास पर अंकुश लगाते हुए तेजी से जर्मनी को एक शक्तिशाली देश बनाया
था। भारत में सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क
मानने की प्रवृत्ति है। पटेल से बिस्मार्क अधिक बड़ा संगठनकर्ता और शक्तिदाता था।
पर सरदार पटेल निश्चित ही बिस्मार्क से अधिक जनतांत्रिक थे।
पूँजीवाद
की प्रकृति में है विस्तारवाद, क्योंकि
जैसे ही पूँजीवाद एक देश के बाजार को एकीकृत और संगठित कर लेता है उसे अपने बाजार
को विस्तार देने के लिए दूसरे क्षेत्र चाहिए। इसीलिए जिन-जिन देशों में पूँजीवाद
सबसे पहले विकसित हुआ उन्होंने सबसे पहले उपनिवेश के रूप में नये बाजार बनाये।
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक यूरोप के समृद्ध देशों में सारे विश्व को-मुख्य रूप
से एशिया और आफ्रीका और अपने उपनिवेशों और प्रभाव क्षेत्रों को अपने-अपने यानी
बाजारों में बांट लिया था। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में जब जर्मनी और दक्षिण में
इटली एकीकृत होने के बाद प्रौढ़ हुए तो उन्हें भी बाजारों की सख्त ज़रूरत महसूस हुई।
पर तब तक तो बाजार बंट चुके थे। इस बाजार के बॅटवारें में जब जर्मनी ने अपना हिस्सा
लेने आक्रामकता दिखाई तो टकराहट अनिवार्य होती गयी।
 |
| Map_Europe_alliances_1914-fr.svg |
इसीलिए
प्रथम विश्वयुद्ध को बाजारों के पुनर्वितरण के लिए किया गया युद्ध कहा जाता है।
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में विलियम द्वितीय जर्मनी
का सम्राट बना। यह युवा सम्राट बेहद महत्वाकांक्षी था। वह बिस्मार्क का उसी तरह
सम्मान करता था जिस तरह अकबर ने बैरम खॉ का किया होगा, क्योंकि बैरम खॉन ही हूमायु की मृत्यु
के बाद मुगल साम्राज्य को अकबर के लिए सुरक्षित बनाया था। पर एक बार साम्राज्य
सुरक्षित हो जाने के बाद अकबर के लिए बैरम खा व्यवधान बनने लगा था और उसे हज करने
के लिए भेज कर अपने रास्ते से हटा दिया था। इसी तरह विलियम द्वितीय ने भी अपनी
वैश्विक नीति (Welt Politik) के लिए बिस्मार्क एक व्यवधान था। उसकी
महत्वाकांक्षा यूरोप महाद्वीप तक सीमित थी। वह कहता था कि जर्मनी हाथी है और
ब्रिटेन व्हेल- एक स्थल का राजा तो दूसरा पानी का। दोनों में टकराहट की गुंजाइश ही
नहीं। यानी जर्मनी यूरोप में अपनी सर्वोच्चता से संतुष्ट था और ब्रिटेन का राज
दुनिया भर के समुद्रों पर था। दोनों के हित टकराते नहीं थे। पर विलियम द्वितीय जिस
जर्मनी का सम्राट हुआ था वह विश्व बाजार के लिए लालायित था। ऐसे में उसकी
इंग्लैण्ड से टकराहट स्वाभाविक थी। इसलिए विलियम ने बिस्मार्क को रास्ते से हटा
दिया और खुल कर विश्व राजनीति में घुसपैठ करने लगा। बीसवीं शताब्दी के पहले दशक
में मानो यूरोप पर राष्ट्रवादी उन्माद छा गया।
प्रथम
विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों के बीच भावनात्मक
युद्ध छिड़ गया। जर्मन गुट के मुकाबले इंग्लैण्ड और फ्रांस तथा रूस और इंग्लैंड के
बीच पारंपरिक प्रतिस्पर्धाएं भुला कर तीनों देश एक गुट की तरह नजदीक आ चुके थे।
दोनों गुटों के बीच प्रचारात्मक युद्ध बढ़ता ही जा रहा था। दोनों गुटों के अखबार
एक-दूसरे के खिलाफ आग उगलते जा रहे थे।
अब
यह स्पष्ट हो गया था कि पूँजीवादी विकास में राष्ट्र एक इकाई बन गये हैं और हर
राष्ट्र एक-दूसरे को प्रतिद्वंद्वी समझने लगा है।
इसलिए प्रत्यक्षतः भले ही आक्रामकता की पहली
जिम्मेदारी जर्मनी की हो पर मूल में तो संपत्ति के बंटावारे की टकराट ही थी।
इतिहास बताता है कि व्यक्तियों के बीच टकराहटों का अधिकांशतः कारण निजी संपत्ति, उसका विस्तार, उसकी प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा आदि
ही होती है। इसी तरह समुदायों और देशों के बीच भी टकराहटों का मुख्य कारण संपत्ति
की प्राप्ति, विस्तार और बॅटवारा ही रहे।
व्यक्तियों की तरह देशों के बीच भी टकराहट का
एक करण सुरक्षा का सवाल भी होता है। लोग अपनी कमजोरी के कारण तो असुरक्षित होते ही
हैं, दूसरों की बढ़ती शक्ति के कारण भी
असुरक्षित हो जाते हैं इसीलिए इतिहास में शक्ति संतुलन (Balance Of Power) एक निर्णायक कारक रहा है। युद्धों का
एक महत्पूर्ण और निर्णायक कारण रहा है देशों का अपने को असुरक्षित समझना। अपनी
सुरक्षा बढ़ाने के लिए देश कुछ भी करते हैं और देशों के बीच एक शीतयुद्ध और
शस्त्रास्त्रों की होड़ शुरू हो जाती है। जिसे हम भारत, पाक सम्बन्धों के माध्यम से समझ सकते
हैं कि कैसे दोनों एक-दूसरे से असुरक्षित महसूस करते हुए आज दोनों ही परमाणु बम
धारक देश बन गये हैं।
प्रथम
विश्वयुद्ध के पहले जर्मनी द्वारा अकेला कर दिये जाने के बाद फ्रांस के सामने
असुरक्षा की तलवार लटकने लगी थी और उसने अपने आस-पास के देशों के साथ संधियाँ करते
हुए अन्ततोगत्वा जर्मन गुट के समानान्तर एक प्रतिस्पर्धी गुट बनाने में सफलता
प्राप्त कर ली। प्रथम विश्व युद्ध इन्हीं दोनों गुटों के बीच शुरू हुआ। युद्ध का
तात्कालिक कारण बाल्कन प्रायद्वीप में राष्ट्रवादी प्रतिस्पर्धा और उसमें यूरोप की
महाशक्तियों का कूद पड़ना शामिल था। यूरोप में उस समय महाशक्तियाँ थीं- ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और रूस। इतिहासकारों ने बिस्मार्क
को एक कूटनीतिक बाजीगर कहा है जो हवा में महाशक्तियों को गेंद की तरह उछालता रहता
था। दो गेंदे उसके हाथ में रहती और शेष हवा में उछली रहती यानी उन्हें अपने आधार
का पता ही नहीं होता। ये सारी महाशक्तियाँ बाल्कन प्रायद्वीप में अपने-अपने हित
पोषण के लिए हस्तक्षेप का प्रयास करती। वास्तव में बाल्कन प्रायद्वीप पर सदियों तक
तुर्क साम्राज्य का कब्जा रहा। जब तुर्क साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो उसे ‘यूरोप का बीमार’ कहा जाने लगा। जैसे कोई सम्पत्तिवान
रोगग्रस्त होता है तो उसके सभी संभावित वारिस ताक में रहते हैं कि जितना संभव हो
क्षींट लिया जाय। उन्नीसवीं शताब्दी में जब तुर्की का प्रभाव कम होने लगा तो यूरोप
की सभी महाशक्तियाँ विविध कारणों से वहाँ घुसपैठ करने लगीं। इसमें सबसे प्रबल दावा
रूस का होता, क्योंकि वह यह कहता कि जैसे बाल्कन
प्रायद्वीप में स्लाव जातियाँ रहती हैं। वैसे ही रूस भी एक स्लाव देश है। इसलिए
उसका फर्ज बनता था कि वह बाल्कन प्रायद्वीप के स्लाव लोगों की सरपस्ती करे। यह उसी
तरह का तर्क कि पाकिस्तान भारत के मुसलमानों और भारत पाकिस्तान के हिन्दुओं की
सरपरस्ती की बात करें। इसी बहाने रूस काला सागर और भूमध्य सागर तक अपनी नौसेना का
विस्तार करना चाहता था। दूसरी ओर ब्रिटेन रूस को अपना प्रतिद्वंदी समझता था, क्योंकि उसे रूस के लगातार दक्षिण में
विस्तार से अपने भारतीय साम्राज्य के लिए खतरा महसूस होता था। भारत में अधिकांश
विदेशी हमले पश्चिमोत्तर से खैबर दर्रे से होते रहे थे। इसलिए ब्रिटेन रूस के डर
(रशोफोबिया) से ग्रस्त रहता था। इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस
फार्मूले के हिसाब से ब्रिटेन, रूस
के दुश्मन तुर्की को अपना दोस्त समझता था और तुर्क साम्राज्य की हर तरह से मदद
करके रूस के विस्तार पर नियंत्रण रखना चाहता था। इसलिए बाल्कन प्रायद्वीप में
मुख्य प्रतिद्वंदिता इंग्लैण्ड और रूस की थी। पर फ्रांस और ऑस्ट्रिया भी घुसपैठ की
घात लगाए रहते। अब चूंकि सशस्त्र गुटबंदी हो चुकी थी इसलिए बाल्कन एक ज्वलनशील
क्षेत्र हो गया था।
फ्रांसीसी
क्रान्ति के बाद सारे यूरोप में
राष्ट्रवाद की हवा चल पड़ी और बाल्कन प्रायद्वीप में भी विभिन्न राष्ट्र अपना-अपना
हक जताने लगे। (यहाँ हम यह समझ ले कि इसी क्षेत्र में बीसवीं शताब्दी में मार्शल
टीटो के नेतृत्व में एक बहुराष्ट्रीय देश यूगोस्लाविया का उदय हुआ था। जिसने
गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जवाहर लाल नेहरू के साथ बड़ी भूमिका निभाई थी बाद में टीटो
की मृत्यु के बाद यह राज्य बिखर गया और पहले की तरह आज सर्बिया मोंटेनेग्रो, बोस्निया आदि देशों के रूप में फिर
विवादों में फँसे हुए हैं)। इस क्षेत्र में सबसे पहले राष्ट्रवादी बिगुल यूरोप के
सबसे पुराने देश यूनान ने बजाया और तब से एक के बाद एक क्षेत्रों में राष्ट्रवादी
उत्थान होता रहा। बीसवीं शताब्दी के शुरू में यह तो तय था कि इस क्षेत्र में कई
देश उभरने वाले हैं। पर उनकी सीमा क्या हो? यह
निश्चित नहीं था। इन्हीं को लेकर लगातार झड़पें होती रहतीं और महाशक्तियाँ अपनी हित
पूर्ति के लिए अवसर ढूढ़ती रहतीं।
बीसवी
शताब्दी के दूसरे दशक में यूरोप की स्थिति कैसी थी इसका अंदाजा ब्रिटिश विदेशमंत्री ग्रे के एक कथन से लगता है
‘चिराग बुझते जा रहे हैं, शायद हम अपने जीवन काल में इन्हें फिर
जलता न देख पाये।’ यूरोप बारूद का ढेर बन चुका था। कोई भी
चिंगारी विस्फोट कर सकती थी।
 |
| 4 August 2014 marks the 100th anniversary of the day Britain, having declared war on Germany, entered the First World War. |
वह
चिंगारी से सर्वियारायोवा के नामक नगर में आ गिरी। तनावपूर्ण माहौल में वहाँ
आस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गयी। ऑस्ट्रिया ने धमकी दी कि अगर चौबीस घंटे
के अन्दर हत्यारे को नहीं पकड़ा गया तो वह सर्बिया पर हमला कर देगा। हत्यारा नहीं
पकड़ा जा सका और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया। स्लाव बिरादर की मदद करने
के लिए रूस युद्ध में कूद पड़ा। ऑस्ट्रिया की जर्मनी से रक्षात्मक संधि थी। जिसके
अनुसार एक पर आक्रमण दूसरे पर भी आक्रमण समझा जाता। इसलिए ऑस्ट्रिया की मदद के लिए
जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रूस की मदद के लिए इंग्लैण्ड और
फ्रांस भी कूद पड़े। सारा यूरोप धू-धू कर जलने लगा। जर्मनी की पनडुब्बियाँ दूर-दूर
तक मार करने लगीं। धीरे-धीरे महाशक्तियों के उपनिवेश भी युद्ध में कूद पड़े। जब
जर्मन पनडुब्बी ने एक अमरीकी जहाज को डुबा दिया तो अमरीका भी युद्ध में कूद पड़ा और
युद्ध वास्तव में विश्वयुद्ध बन गया।
यहाँ
हमें विश्वविख्यात चिंतक की एक बहुत दिलचस्प टिप्पणी याद आती हैः
प्रथम
विश्वयुद्ध टैंको से शुरू हुआ और उसका अन्त हवाई जहाजों से हुआ। दूसरा विश्वयुद्ध
हवाई जहाजों से शुरू हुआ और उसका अन्त परमाणु बम से हुआ। लगता है तीसरा महायुद्ध
परमाणु बम से ही शुरू होगा और उसके बाद के युद्ध लाठी-डंडे से लड़े जायेंगे। इस
टिप्पणी में दो बातों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो यह कि युद्ध के दौरान
शस़्त्रास्त्रों को लगातार और अधिक कारगर बनाया जाता है और उनकी विध्वंसकता बढ़ती
जाती है और दूसरा यह कि अगर तीसरा विश्वयुद्ध हुआ तो विध्वंस इतना व्यापक होगा कि
सभ्यता ही नष्ट हो जायेगी और लोग प्रागैतिहासिक काल में चले जायेंगे।
शुरू
के वर्षों में जर्मनी लगातार विजयी होता रहा। क्योंकि युद्ध में पहला वार करने
वाले और पहले से तैयारी करने वाले की स्थिति बेहतर होती है। पर धीरे-धीरे
इंग्लैण्ड और फ्रांस भी अच्छी लामबंदी करने में सफल हुए। इस विश्व युद्ध में
ब्रिटेन की ओर से भारतवासियों की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। भारतियों
ने ‘वार-फन्ड’ में करोड़ों रुपया चंदा दिया और भारत के
सैनिक मध्य-पूर्व से यूरोप तक लड़ते हुए मारे गये। युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस का
सहयोगी रूस अन्त तक नहीं संभल पाया और लड़खड़ाते रूस में 1917 में क्रान्ति हो गयी। क्रान्ति के नेता लेनिन ने पहले से ही कहना शुरू कर दिया
था कि यह युद्ध पूँजीपतियों के बीच का युद्ध है। राष्ट्रवादियों को इससे कुछ नहीं
लेना-देना। इसलिए रूस को इस युद्ध से अलग हो जाना चाहिए। क्रान्ति के बाद लेनिन ने
जर्मनी से समझौता कर लिया और रूस युद्ध से अलग हो गया।
जर्मनी
को थोड़ी राहत मिली तो उसने और आक्रामक रूख दिखाया। पर उसकी एक चूक ने अमेरिका को
भी युद्ध में उतार दिया।
अमरीका
सैकड़ों वर्षों से, जिस दौरान यूरोप लगातार युद्धों में
ध्वस्त हो रहा था, निरंतर अपनी अनन्त संभावनाओं को उजागर
करता हुए एक महान शक्ति बनता जा रहा था। अमेरिका के युद्ध में कूदने से ब्रिटेन और
फ्रांस को अनन्त स्रोत उपलब्ध हो गये। अमरीका ने जर्मनी के खिलाफ लड़ने वालों की
बेहिसाब मदद की और स्वयं भी मोर्चा संभाला।
इस
समय ब्रिटेन ने दो बड़े कारगर नारे दियेः
1.
It is a war to make the world safe for Democracy.
2.
It’s
a war to end war.
(1). यह युद्ध दुनिया को जनतंत्र के लिए
सुरक्षित करने के लिए है
(2). यह युद्ध युद्धों का अन्त कर देने के लिए
है।
जाहिर
है कि ये दोनों ही नारे आदर्शवादी आहृवान थे। उपनिवेशों में, जैसे भारत में, किसी न किसी रूप में राष्ट्रवादी आंदोलन
शुरू हो गये थे आशा की किरण दौड़ गयी कि हो सकता है विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद
उन्हें स्वायत्तता या स्वतंत्रता मिल जाय। दूसरे युद्धों का अन्त कर देनी की बात
सभी शान्तिप्रिय लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आदर्शवादी उत्प्रेरणा थी। नतीजा यह हुआ
कि उपनिवेशों से भारी मदद मिलने लगी और जर्मनी का पलड़ा हल्का पड़ने लगा।
सबसे
पहले इटली ने जर्मनी का साथ छोड़ा और विरोधी गुट से जा मिला। इसके बाद जर्मनी
द्वारा विजित क्षेत्रों में राष्ट्रवादी उभार शुरू हुआ और अन्ततः स्वयं जर्मनी में
जहाँ युद्ध के पहले मजदूर आंदोलन यूरोप में सबसे अधिक तेज था। सम्राट विलियम
द्वितीय की हालत कमजोर पड़ने लगी। अन्ततः विलियम अपने परिवार के साथ भाग खड़ा हुआ।
अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन ने युद्ध के दौरान ही चौदह सिद्धांतों की घोषणा की थी
जिनके आधार पर दुनिया में फिर से शान्ति बहाल की जा सकती थी। इन्हीं चौदह
सिद्धांतों को आधार बनाया गया और युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस में शान्ति
वार्ताएँ शुरू हुई।
इस
युद्ध ने संवेदनशील लोगों का मोहभंग कर दिया था। इतना विनाश, इतनी निर्बन्धता, इतनी बर्बरता क्या हो गया है मानव को।
लड़ने वाले अधिकांश महत्वपूर्ण देश ईसाई धर्म के अनुयायी थे। क्या हुआ उस मानव
प्रेमी और अहिंसा के पुजारी ईसा मसीह की शिक्षाओं का? उसने कहा थाः ‘जो तुम्हारे बाएँ गाल पर तमाचा मारे
उसके सामने दायाँ गाल भी कर दो’ और
उसके अनुयायी निर्दोष लोगों की बर्बर हत्यायें कर रहे थे। 1915 में ही फ्रांत्ज़ काफ्का
ने एक छोटा सा उपन्यास लिखा - Metamorphosis (कायांतर)। इस उपन्यास का मुख्य पात्र ग्रेगोर एक सुबह बिस्तर से उठना
चाहता है तो पाता है कि वह तो कॉक्रोच (तिलचट्टा) हो गया है। हम सबने एक उलट गये
लाचार तिलचट्टे को देखा होगा जो लगातार अपनी टाँगे हिलाता हुआ अपने जीने को
प्रदर्शित तो करता है। पर लाख कोशिशों के बावजूद पलट कर सीधा नहीं हो पाता। इस
असाधारण रूपक ने मनुष्य की दुदर्शा और लाचारी को हृदय विदारक रूप में उजागर कर
दिया। काफ्का की यह रचना आज तक प्रासंगिक बनी हुई है, क्योंकि मनुष्य उस लाचारगी से कहाँ उबर
पा रहा है? इस रूपक पर विविध कलारूपों में रचनाएँ
हुई हैं। फिल्में बनी हैं। यहाँ तक कि रॉक बैन्ड ने भी इसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि पिछले सौ वर्षों से यह रचना
मानव समाज को असहायता से उबरने की प्रेरणा देती रही है।
फ्रांस
में विख्यात लेखक अल्बेर काम्यू ने एक कालजयी रचना रची ‘द प्लेग’। उस समय प्लेग का अन्त नहीं हुआ था और
वह हर साल महामारी में लाखों लोगों की जान ले लेती। यह बीमारी चूहों द्वारा फैलती
थी और उसकी कोई दवा नहीं थी। इस उपन्यास में अगणित चूहों का मानव शरीर पर रेलम पेल
मचाना इस तरह दिखाया गया कि पाठक अपने शरीर पर भी चूहों का रेंगना महसूस कर सकता
है। कुल मिला कर काम्यू ने भी मानव समाज को रोग ग्रस्त बताया और युद्ध को एक
महामारी करार दिया। युद्ध ने जो कुछ किया था उसका एक प्रमाण मिलता है ओसवाल्ड
स्पेन्गलर की विश्व विख्यात हो गयी किताब ‘डिक्लाइन
ऑफ द वेस्ट।’ स्पेन्गलर कोई बड़ा इतिहासकार नहीं था पर संवेदनशील शिक्षक स्पेन्गलर को युद्ध से इतना आघात पहुँचा कि उसने इसमें
समस्त पाश्चात्य सभ्यता का पतन देखा। उसने प्रतिपादित किया कि जैसे व्यक्ति जन्म
लेता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है और फिर
वृद्धवस्था के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है वही हाल सभ्यताओं का होता है और अब
लगता है कि पाश्चात्य सभ्यता भी मरणासन्न है।
इस
विषय को और विस्तृत और विद्वतापूर्ण ढंग से ब्रिटिश इतिहासकार अर्नाल्ड टायनबी ने
अपनी विराट पुस्तक ‘स्टडी ऑफ हिस्ट्री’ में प्रतिपादित किया। उनका स्वर इतना
निराशापूर्ण नहीं था पर सभ्यता के पतन की बात उन्होंने भी चिन्हित की।
कुल
मिला कर युद्ध ने लोगों को विचलित कर दिया। विराटता की ओर अग्रसर सभ्यता से मोहभंग
का दौर अभी तक जारी है। पर उसमें विस्तार से जाना इस लेख के दायरे में संभव नहीं।
इस
घटाटोप में आशा की एक ही किरण थी कि 1917 में रूस में दो बार क्रान्ति हुई और
दूसरी क्रान्ति के बाद सदियों से कल्पित मजदूरों का राज्य कायम हो गया। पर वह
तत्काल एक गृह युद्ध में लिप्त हो गया। रूस की प्रक्रियावादी शक्तियों की दुनिया
की सभी महाशक्तियाँ मदद करने लगीं और दो साल तक ऐसा गृह युद्ध नगर-नगर और सड़क, सड़क पर लड़ा गया कि लगता था कि दुनिया
अभी किसी क्रान्ति कारी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं।
उधर
पेरिस में विजेता पराजित देशों के शासकों नहीं पूरे देश को अपराधी बना कठघरे में
खड़ा किए हुए थे। इंग्लैण्ड में नारे लग रहे थे- ‘जैसे को तैसा’,
‘एक-एक पैसा
वसूला जाए।’
पेरिस
में पराजित देशों के साथ समझौता वार्ता शुरू हई। विश्व युद्ध के बाद यह वास्तव में
एक विश्व शान्ति सम्मेलन था। इसका पता इसी से चल सकता है कि भारत उस समय एक
स्वतंत्र देश नहीं था। पर भारत की युद्ध में बड़ी भूमिका थी इसलिए भारत के
प्रतिनिधि को भी पर्यवेक्षक के रूप में बुलाया गया था। वैसे तो सभी प्रतिनिधियों
से सलाह-मशविरा चलता रहा पर निर्णायक भूमिका पाँच प्रमुख विजेता देशों- ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमरीका, इटली
और जापान के शासन प्रमुखों की थी। इन पाँचों में भी सबसे निर्णायक भूमिका ब्रिटेन
के प्रधानमंत्री लॉयड जार्ज तथा फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लमांशो की थी। ये दोनों
ही मानो जर्मनी का खून चूस लेना चाहते हों। इन दोनों देशों की जनता भी आक्रांता
जर्मनी से बेहद नाराज थी और राजनेताओं को कुछ ही दिनों में ऐसी जनता के सामने ही
वोट माँगने जाना था। इसलिए ‘पब्लिक
मूड’ के अनुसार ही व्यवहार करना जरूरी समझा
जा रहा था। इन दोनों पर थोड़ा बहुत अंकुश लगा भी सकता था तो इनका सबसे बड़ा मददगार
अमरीका का राष्ट्रपति विल्सन। परन्तु विल्सन एक आदर्शवादी नेता था और वैसे भी
अमरीकी नेता यूरोप की कुटिल कूटनीतिक चालों से अभी पूरी तरह परिचित नहीं थे। दूसरे
विल्सन किसी भी कीमत पर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति संगठन ‘लीग ऑफ नेशंस’ का गठन करवा लेना चाहता था। इसलिए वह
लॉयड जार्ज और क्लमांशो की बदला लेने की नीति पर कोई प्रभावी अंकुश नहीं लगा सका।
 |
| President Woodrow Wilson |
ले दे
के वही हुआ जिसे रसेल ने ‘रीवॉस’ (Rivanche) यानी प्रतिहिंसा और बदले की भावना कहते हैं।
लेखक के अनुसार जर्मनी और फ्रांस के बीच बदले की इस भावना ने एक-दूसरे को नीचा
दिखाने के लिए बड़ी-बड़ी हिंसाएँ करवायीं। लेखक ने यहाँ इतिहास बोध और इतिहास
ग्रस्तता के बीच अन्तर चिन्ह्ति किया। इतिहास बोध का अर्थ होता है इतिहास से सबक
लेकर पुरानी गलतियों को दोहराने से बचना। जबकि इतिहासग्रस्तता का मतलब होता है
इतिहास के बोझ को ढोते रहना। इससे वैमनस्य की यादें ताजा रहती हैं और सकारात्मक
पक्ष भुला दिया जाता है। इसे हम भारत के इतिहास में हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों और
अब भारत-पाक सम्बन्धों में कार्यरत देख सकते हैं। बदले की भावना व्यक्ति और समुदाय
को संकीर्ण और आत्मघाती बनाती है।
पेरिस
की संधियों में इसी बदले की भावना ने सबसे बड़ा नुकसान यह किया कि शासकों को
जिम्मेदार करार देने के बजाय पूरे देश को जिम्मेदार ठहरा दिया और युद्ध की सारी
जिम्मेदारी पराजित देशों पर थोप दी। यह एक नितांत आपराधिक निर्णय था। सामान्य लोग
ऐसा ही करते हैं कि दुश्मनी हो जाए तो पुश्त-दर-पुश्त उसे ढोते हैं और दुश्मन ही
नहीं उसकी जाति, धर्म और उससे जुड़ी हर चीज से दुश्मनी
निभाते हैं। यह प्रवृत्ति भी हम भारतीय समाज में भली-भाँति चरितार्थ होते देखते
हैं। किसी घटना या व्यक्ति के दोष के लिए पूरी जाति और पूरे धर्म के अनुयायियों को
कितनी आसानी से यहाँ अपराधी मान लिया जाता है। अगर जर्मनी अपराधी था भी तो सम्राट
तो भाग खड़ा हुआ था और युद्ध के सारे निर्णय अधिकांशतः उसी ने लिए। फिर जनता को
क्यों दोषी ठहराया जाय? परंतु पेरिस की संधियों में युद्ध का
सारा खर्चा वसूलने के लिए क्षतिपूर्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया।
क्षतिपूर्ति कमीशन ने क्षति का आकलन किया वह रकम इतने खरबों में थी कि पराजित देश
शायद सैकड़ों वर्षों में ही जुर्माने को भर पाते। वास्तव में जुर्माना कौन देता? निरापराध जनता और वह भी
पुश्त-दर-पुश्त। इस नीति ने ही जर्मन समाज में ऐसा क्षोभ और असंतोष पैदा किया
जिसका लाभ उठाते हुए हिटलर जर्मनी पर फॉसीवाद लादने में सफल हो गया।
जुर्माना
वसूल करने के लिए जो शर्तें लगाई गयी थी उनमें वर्षों तक जर्मनी में हुआ सारा
उत्पादन इंग्लैण्ड और फ्रांस हड़पते रहे। जर्मनी के सारे उपनिवेश छीन लिये गये पर
ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध के बाद जनतंत्र का आहृवान करने के बावजूद उपनिवेशों से
मिली मदद को धता बताते हुए अपने उपनिवेश नहीं आजाद किए। भारतवासियों को तो भारी
मदद के बदले रौलेट एक्ट और जलिया वालां बाग का नरसंहार मिला था।
यह
अनोखी संधि वार्ता थी, जिसमें वार्ता हुई ही नहीं, संधि पत्र पर बन्दूकों के साये में
पराजित देशों से हस्ताक्षर करा लिया गया। क्लमांशों
लगातार धमकाता रहा, ‘हमारी तोपों का मुँह अभी भी जर्मनी की ओर ही है।’
ऐसी
अपमानजनक संधि के बाद व्यंग्य किया जाने लगा- ‘युद्ध
का अन्त करने वाला युद्ध समाप्त हो गया। अब शुरू हो रही है शान्ति जो शान्ति का
अन्त कर देगी।’ एक अनुभवी सेनाधिकारी जनरल
फोश ने कहा ‘यह शान्ति नहीं बीस साल का युद्ध स्थगन है’। और निश्चित ही ठीक 20
साल बाद 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हो गया।
यहीं
हम इसे उल्लेखनीय मानते है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विजेताओं ने प्रथम
विश्वयुद्ध के बाद के अनुभवों से लाभ उठाया और पराजित देशों को अपराधी घोषित करने
के बजाय युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर बाकायदा मुकदमा चला कर उन्हें
भिन्न-भिन्न सजाएँ दी गयी। इस सम्बन्ध में ‘नूरेम्बर्ग
ट्रायल्स’ का उल्लेख किया जा सकता है। युद्ध का
अन्त होने से पहले ही हिटलर ने तो आत्महत्या कर ली थी। पर उसके सहयोगी अधिकारियों
का अपराध सुनिश्चित कर उन्हें भिन्न-भिन्न सजाएँ दी गयी और ‘मार्शल प्लान’ के अन्तर्गत जर्मनी के पुनर्निर्माण के
लिए मदद की गयी। नतीजा यह हुआ कि धीरे-धीरे स्वयं जर्मनी के समाज ने भी मान लिया
कि अपराधी हिटलर और उसकी पार्टी थी और वे शर्मिदा हुए और हैं कि उन्होंने ऐसे
अपराधियों का साथ दिया। ऐसी नीति के कारण ही बार-बार नौबत आने पर भी तीसरा
विश्वयुद्ध अभी तक टलता रहा है। यहाँ यह कह देना उचित ही होगा कि युद्ध में जर्मनी
पराजित हुआ इसलिए उसके शासकों पर मुकदमा चला। पर अगर वह जीत जाता तब?...
 |
| बेल्जियम में हमले के दौरान जर्मन सैनिक आंटवर्प में जहाज़ से उतरे |
प्रथम
विश्वयुद्ध में पचपन लाख से अधिक व्यक्ति मारे गये और करोड़ों घायल हुए। जेनेवा में
हम युद्ध में आहत लूले, लंगड़े, अंधे, क्षत-विक्षत लोगों का भारी प्रदर्शन
हुआ तो लोगों का बुरा हाल हो गया। सम्पत्ति की तो जितनी हानि हुई थी उसका जायजा ही
लेना मुश्किल था। एक जर्मन पत्रकार ने इस विषय पर एक बड़ी सटीक टिप्पणी कीः-
‘प्रथम विश्वयुद्ध में सम्पत्ति का
जितना नुकसान हुआ उससे अधिक मानस का हुआ था। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सम्पत्ति
का अकूत नुकसान हुआ। पर मानो समाज का रोगग्रस्त मन स्वस्थ हो गया-तभी तो प्रथम विश्वयुद्ध
के बाद फॉसीवाद का उदय हुआ था और दुनिया एक-दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दी गयी थी।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद लगता है फॉसीवाद का खतरा टल गया।’
प्रथम
विश्व युद्ध ने वैसे तो सारी दुनिया को गहराई से प्रभावित किया पर यूरोप को तो
मानो उलट-पलट कर रख दिया। इस युद्ध में चार साम्राज्यों का अन्त हो गया- जर्मन, ऑस्ट्रियन, रूसी और तुर्की। यह सच है कि विजेता
ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने उपनिवेशों को बचा लिया। पर वहाँ भी स्वतंत्रता आंदोलन
ने गति पकड़ ली। इसे हम भारत के उदाहरण से समझ सकते हैं। युद्ध में सरकार की मदद करने
वाले गाँधी जी युद्ध के बाद खिलाफत और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने लगे और भारत
ही नहीं सभी उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन तेज होता गया। इसके लिए युद्ध को
श्रेय नहीं दिया जा सकता पर यह तो सच ही है कि युद्ध ने ही ऐसा माहौल पैदा किया और
ऐसी चेतना विकसित की जिसमें वंचित लोगों में एक उभार पैदा हुआ।
युद्ध
का एक अनअपेक्षित पर सबसे बड़ा परिणाम तो यही दिखाई देता है कि युद्ध के दौरान ही
1917 में रूस में दो क्रान्तियाँ हुईं और रूस में मेहनतकश का राज कायम हो गया।
निश्चित ही ऐसा इसीलिए संभव हुआ कि रूस युद्ध में लगातार पराजित हो रहा था और रूस
की सरकार इतनी कमजोर और जर्जर हो गयी कि वह पहले सुधारों और फिर क्रान्ति की आंधी को बर्दाश्त नहीं कर पायी।
विश्वयुद्ध जैसे नकारात्मक परिघटना के भी बहुत
से परोक्ष, किन्तु सकारात्मक परिणाम निकले। उन्हें
भी चिन्ह्ति करना आवश्यक है।
इतने बड़े पैमाने के युद्ध में युद्धरत देशों की
सारी युवाशक्ति खप गयी। युद्ध में भर्ती के लिए नीचे की उम्र घटाई और ऊपर की उम्र
बढ़ायी जाने लगी। इसका मतलब सारे युवक जो कोई काम कर सकते थे युद्ध सम्बन्धी कामों
में ही लग गये। फिर भी वे पूरे नहीं पड़ सकते थे। इसलिए घर की चौहद्दी टूटने लगी।
औरतों को भी कामों पर लगाया जने लगा। हालांकि औद्योगीकरण के बाद ही सस्ते श्रम के
रूप में औरतों का इस्तेमाल शुरू हो गया था पर वे प्रायः कारखानों में मजदूरी
करतीं। अब तो हर क्षेत्र में औरतों को प्रवेश मिलता गया। इससे नारी की दिनचर्या
बदली। यहाँ तक कि आचार-व्यवहार भी बदलने लगा। बड़े-बड़े बाल और भारी घाघरों के साथ
भाग-दौड़ की नौकरी नहीं की जा सकती थी इसलिए नारी का रूप-स्वरूप ही बदलने लगा।
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद हम मजदूर आंदोलन के साथ नारी आन्दोलन में भी तेजी आते देख
सकते हैं।
शिक्षा-साहित्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन
दिखायी पड़ता है। युद्ध के पहले, दौरान
और बाद में तकनीकी शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाने लगा। साहित्य में अब बड़े
उपन्यास और महाकाव्य पढ़ने का समय नहीं था किसी के पास। इसलिए कहानियों और एकांकी
नाटकों का जोर बढ़ा। इसमें जॉन गालसवर्गी के लिखे लघु
नाटक ‘द लिटिल मैन’ ने महानायकों की जगह
सामान्य व्यक्ति के महत्व को बढ़ाना शुरू किया। बाद में इसकी झलक हिन्दी साहित्य
में ‘लघु मानव’ की अर्थवत्ता बढ़ाने के
प्रयास में देखी जा सकती। अंग्रेजी साहित्य की प्रवृत्ति अर्नेस्ट हेमिंग्वे के दो
उपन्यासों में देखी जा सकती है। स्पेन में होने वाले गृहयुद्ध की पृष्ठभूमि पर
लिखे गये ‘फॉर हूम द बेल टाल्स’ और ‘फेयरवेल टू आर्म्स’ में देखी जा सकती है।
सबसे सटीक समीक्षा बर्नर्ड शॉ के नाटक ‘आर्म्स एण्ड द मैन’ में देखी जा सकती है। शॉ शेक्सपीयर के बाद अंग्रेजी के
सबसे बड़े नाटककार माने जाते हैं। उन्होंने अपने बहुचर्चित नाटक ‘आर्म्स एण्ड द मैन’ में एक सूत्र कहलाया है
अपने नायक ब्लंटश्ली ब्लेड श्लिी सेः Romantic Love is
Lust and Romantic War is Butchery. (रूमानी प्रेम कामेक्षा है और रूमानी युद्ध संहार)
पात्र ने प्रेम और युद्ध का रूमानियत के नाते गौरवान्यन की आलोचना की। इस कथन में
यहाँ यह प्रासंगिक है कि युद्ध को प्रायः शासक लोग देशभक्ति, देश-रक्षा या ‘मर्दान्गी’ आदि के बहाने अपने हित
का उपकरण बनाते हैं।
युद्ध से दुनिया इस तरह आक्रांत थी कि हर कीमत
पर-तुष्टिकरण की कीमत पर भी, शान्ति
बनाये रखना चाहती थी। शान्ति के लिए ‘लीग
ऑफ नेशंस’ तो बना ही था पर उसे पर्याप्त न मान कर
शान्ति के लिए तरह-तरह की वार्ताएँ और संधियाँ की जाने लगी। निरस्त्रीकरण के
प्रयास होने लगे। निरस्त्रीकरण सम्मेलनों पर जॉन व्हिटेकर नामक पत्रकार ने एक बहुत
अच्छा व्यंग्य किया था। उसने अपनी पुस्तक ‘फीयर
केम ऑन यूरोप’ (भयाक्रांत यूरोप) में दो छोटी-छोटी
कहानियाँ लिखीं जो आज भी प्रासंगिक हैं। पहली कहानी में जंगल में जानवरों का एक
सम्मेलन हुआ। यह चिन्ता प्रकट की गयी कि अगर जानवर एक-दूसरे का इसी तरह संहार करते
रहे तो जानवर समाप्त हो सकते हैं। इसलिए प्रस्ताव हुआ कि जानवर अपने खतरनाक अंगों
का इस्तेमाल न करें। तब हाथी ने कहा पंजों का इस्तेमाल वर्जित किया जाना चाहिए।
शेर ने कहा सूड़ पर प्रतिबंध लगना चाहिए...। यानी हर जानवर दूसरे जानवर के उस अंग
पर प्रतिबंध लगाना चाहता था जो अपने लिए खतरनाक समझता था। इसी तरह देश दूसरे देशों
के उन हथियारों पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे जो उनके पास नहीं थे या कम थे।
दूसरी कहानी और छोटी पर और दिलचस्प है। उसे
भारतीय संदर्भ में कहें तो इस तरह कहेंगेः-
‘एक
आदमी के पास एक रुपया था। वह दुकान पर जाकर उसकी रेजकारी (खुदरा) लेता। फिर दूसरे
दुकान जाकर रुपया लेता और फिर रेजकारी और फिर रुपया। उसके साथी ने पूछा तुम
बार-बार यह क्या कर रहे हो ? उस
आदमी ने जवाब दिया मुझे विश्वास है कि कभी न कभी कोई न कोई भूल करेगा...’ यानी दूसरों की भूल या गलतियों का
फायदा उठाने का प्रयास। समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार होने वाले सम्मेलनों
में क्या आज भी दूसरे पक्ष द्वारा गलती का इंतजार नहीं किया जाता?
वास्तव में निरस्त्रीकरण हुआ नहीं, क्योंकि सभी देशों में असुरक्षा का भाव
विद्यमान था। फिर भी युद्ध के बाद के पहले दशक के दौरान लगातार प्रयास होते रहे।
यहाँ तक कि युद्ध पर पाबंदी लगाने की भी सदिच्छा व्यक्त हुई। इन प्रयासों ने
शान्ति के पक्ष में ऐसा माहौल बनाना शुरू किया कि इनके लिए अमेरिकी विदेशमंत्री
केलॉग और फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रियां को नोबेल शान्ति पुरस्कार से नवाजा गया।
पर यह प्रयास वास्तव में खोखले थे, क्योंकि
युद्ध की जड़ों पर कोई प्रहार नहीं कर रहा था।
युद्ध के समाप्त होने के तीन वर्ष बाद ही इटली
में फॉसीवाद के प्रवर्तक मुसोलिनी ने इटली पर कब्जा कर लिया। फॉसीवाद एक उत्कट राष्ट्रवाद
तथा विकृत पूँजीवाद है। वह तब तक पैदा हो चुके समाजवादी विकल्प को पूरी तरह नकारते
हुए देश का पूरी तरह सैन्यीकरण कर राष्ट्रवादी उन्माद फैलाता है। मुसोलिनी इसी राह
पर अग्रसर हुआ। पर फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध से इतने डरे हुए थे कि उन्होंने
मुसोलिनी के प्रति तुष्टिवादी नीति अपनाई। इटली ने उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में
साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए अफ्रीका के सबसे पुराने देश
अबीसीनिया पर हमला किया और पराजित हुआ था। मुसोलिनी ने उस युद्ध का बदला लेने के
लिए पूरे देश को लामबंद किया और अबीसीनिया को पराजित कर इटली का उपनिवेश बना लिया।
फिर भी दुनिया के तथाकथित जनतांत्रिक देश नहीं चेते। लीग ऑफ नेशंस में मामला उठाया
गया। पर वह संस्था दंतहीन साबित हुई। वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं हुई।
इसी तरह पूरब में जापान में चमत्कार हुआ था।
उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक एक पिछड़ा सामंती देश तेजी के साथ पश्चिम, विशेषकर अमरीका, के संपर्क में आया और इतनी तेजी से
प्रगति की कि उसे इतिहास में जापानी चमत्कार (Japanese Miracle) कहा जाता है। उसने अपने दो विराट पड़ोसियों चीन और रूस को पराजित
किया और इंग्लैण्ड की प्रतिष्ठित कार्टून पत्रिका ‘द पंच’ ने उसे ‘जैक द जायंट किलर’ घोषित
कर दिया। जापान को ‘पूरब का ब्रिटेन’ कहा जाने लगा। ब्रिटेन ने जापान के साथ
बराबरी की संधि कर ली और प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने ब्रिटेन का साथ दिया, लेकिन पेरिस की संधियों में जापान को
वह लाभ नहीं मिला जो ब्रिटेन और फ्रांस का इसलिए वह बेहद असंतुष्ट हो गया।
जापान टापुओं का देश है और वहाँ की सबसे बड़ी
पूँजी वहाँ का प्रतिभाशाली मनुष्य है। वहाँ की जनसंख्या के लिए पर्याप्त रिहाइशी
जमीन तक उपलब्ध नहीं है। अब तो टेक्नोलॉजी के विकास के कारण गगनचुम्बी इमारतें
समस्या का एक हद तक समाधान करती हैं पर उस समय तो बढ़ते औद्योगीकरण और बढ़ी जनसंख्या
के लिए उपनिवेश चाहिए थे। जापान भी फॉसीवादी रास्ते पर चल पड़ा और उसने चीन के
उत्तर में मंचूरिया पर कब्जा कर लिया और इस बार भी प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले
शक्तिशाली देश कुछ भी नहीं कर सके।
फॉसीवाद का सबसे आक्रामक और बर्बर उभार जर्मनी
में हुआ। जर्मनी यूरोप का सबसे संभावना-सम्पन्न देश है। वहाँ की साहित्यिक और
दार्शनिक परंपराएँ विश्व विख्यात हैं पर विभाजित होने के कारण 1870 तक वह पनप नहीं
पाया था। पर पनपते ही बाजार की प्रतिस्पर्धा में वह विश्वयुद्ध का कारक बन गया था।
पराजय के बाद उसे इतना अपमानित और प्रताड़ित किया गया था कि पेरिस की संधियों की
अवहेलना के बिना वह सांस नहीं ले सकता था। सामान्य विकास से वह अपने बंधन नहीं तोड़
सकता था। उस वक्त जर्मनी की मानो ऐतिहासिक आवश्यकता थी एक असामान्य राष्ट्रवादी
उधार।
यह प्रदान किया उस व्यक्ति ने जिसकी भाषा तो
जर्मन थी पर वह जर्मनी नहीं ऑस्ट्रिया का निवासी था। उसी ने ‘नेशनल सोशलिस्ट पार्टी (नात्सी पार्टी)
का गठन किया। शुरू से ही आक्रामकता के कारण उसे जेल भी जाना पड़ा और जेल में ही
हिटलर ने युवा अवस्था में ही अपनी आत्मकथा लिख डाली, ‘मेरा संघर्ष’
(Mein Kamph). एक
कुंठाग्रस्त व्यक्ति की अनंत महत्वाकांक्षाओं को एक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत
किया गया। इसमें यहूदियों को जर्मनी की सारी मुसीबत, यहाँ तक प्रथम विश्वयुद्ध में पराजय तक, के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और
विजेताओं को ललकारते हुए जर्मनी को एक ‘आर्य’ यानी श्रेष्ठ जाति करार दिया गया था और
यही प्रतिपादित किया गया था कि जो श्रेष्ठ है उसे ही शासन करने का अधिकार है।
इसलिए जर्मनी ही विश्व का श्रेष्ठ शासक हो सकता है। हिटलर की बातों में अपमानित और
उत्पीड़ित जर्मन, समाज विशेषकर युवाओं, को एक सम्बल मिला और हिटलर ने अपनी
पार्टी को इतने तामझाम और इतनी आक्रामकता के साथ संगठित किया कि जर्मनी की लड़खड़ा
रही जनतांत्रिक सरकार को 1933 में हिटलर को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना
पड़ा। तब से अगले बारह वर्षों का समय यूरोप ही नहीं सारी दुनिया के लिए एक विध्वंसक
सुनामी से गुजरने के अनुभव जैसा रहा। थोड़े ही समय में उसने आरोपित संधि की
धज्जियाँ उड़ा दीं और तेजी से जर्मनी का सैन्यीकरण करता हुआ भावी खतरे का आगाज करता
गया। उसने इटली और जापान की फॉसीवादी शक्तियों से हाथ मिला लिया और स्पेन में चल
रहे गृह युद्ध में वहाँ की फॉसी शक्तियों की मदद करने लगा।
स्पेन में जनतांत्रिक तरीके से एक समाजवादी
सरकार स्थापित हुई थी। यह दुनिया के इतिहास में अप्रत्याशित और अभूतपूर्व था। इसका
स्पेन की सामंती और प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने भरपूर विरोध किया और जनरल फ्रांको
उनका नेतृत्व करने लगा। इटली और जर्मनी की फासिस्ट सरकारों ने फ्रांको की भरपूर
मदद की। पर जनता द्वारा चुनी हुई वैध सरकार की किसी जनतांत्रिक सरकार ने मदद नहीं
की थी। मानवता के सामने आसन्न खतरे को सरकारों ने नहीं पर सारी दुनिया के
बुद्धिजीवियों ने महसूस किया। कुछ बेहद प्रतिभाशाली युवा लेखकों जैसे क्रिस्टोफर
कॉडवेल, ने कलम छोड़कर हथियार पकड़ लिये और
जनतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध में कूद पड़े। भारत के लेखकों में भी उथल-पुथल मचनी
शुरू हुई। कांग्रेस के युवा नेता जवाहर लाल नेहरू ने स्पेन की जनतांत्रिक शक्तिओं
को नैतिक समर्थन दिया। पर अन्ततः ये शक्तियाँ पराजित हो गयी और स्पेन में भी एक
फॉसीवादी सरकार कायम हो गयी। तब भी दुनिया की जनतांत्रिक सरकारें नहीं चेती।
पर दुनिया के प्रगतिशील लेखकों ने फॉसीवाद के विरुद्ध
एक प्रगतिशील जनतांत्रिक मोर्चा बनाने का निर्णय लिया और प्रगतिशील लेखक संघ का
जन्म हुआ। वहीं से प्रेरणा लेकर भारत के युवा लेखक
सज्जाद ज़हीर ने भारत में भी एक ऐसा संगठन बनाना ज़रूरी समझा। इलाहाबाद में शुरू हुए
इस प्रयास का नतीजा तब निकला जब लखनऊ में भारत पहले ‘प्रगतिशील लेखक संघ’ का
अधिवेशन हुआ और उसकी अध्यक्षता के लिए हिन्दी के सबसे लोकप्रिय लेखक प्रेमचन्द को
बुलाया गया। ऐसे संगठन की पहल कम्युनिस्टों ने की थी और अधिकांशतः इस संगठन का
संचालन उन्हीं के हाथ में रहा। पर शुरू में इसे एक प्रगतिशील मोर्चे की तरह चलाया
गया। इसका सबसे बड़ा सबूत था कि अध्यक्ष प्रेमचन्द को बनाया गया जो कम्यूनिस्ट नहीं
थे। प्रेमचन्द ने लखनऊ में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने जोर
दिया कि साहित्य राजनीति के आगे-आगे चलने वाली मशाल हो सकता है और होना चाहिए। बाद
में इसमें विश्व विख्यात रवीन्द्र नाथ टैगोर जैसे लोग भी शामिल हुए और फॉसीवादी
विरोधी भावना के विस्तार में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस की सहकर्मी
जनलोक नाट्य मंच पर (इप्टा) रंगकर्मी को प्रगतिशील राह पर ले चली।
हिटलर की आक्रामकता बढ़ती जा रही थी। पर ब्रिटेन
और फ्रांस की सरकारें किसी भी कीमत पर युद्ध को टालने के भयाक्रांत नीति के कारण
हिटलर को बार-बार ‘अपीज’ करती जा रही। हिटलर ने पेरिस संधि को नकारा चेकोस्लोवाकिया पर हमला
किया, ऑस्ट्रिया पर हमला किया। पर न तो ‘लीग
ऑफ नेशंस’ कुछ कर सकी न उसके संचालक फ्रांस और ब्रिटेन। उल्टे ब्रिटेन के
प्रधानमंत्री ऑस्टिन चेम्बरलेन जर्मनी में म्यूनिख नामक नगर में गये और हिटलर से
वार्ता कर इस भ्रामक दंभ के साथ लंदन लौटे कि अब शान्ति स्थापित हो गयी है।
इन्होंने लंदन के हवाई अड्डे पर घोषणा कीः ‘आई
ब्रिंग पीस विथ ऑनर’ (मैं अपने साथ सम्मानजनक शान्ति लेकर
लौटा हूँ)। यह वक्तव्य इतिहास के सबसे हास्यास्पद वक्तव्यों में से साबित हुआ है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद विश्व
द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका में झोंक दिया गया।
करीब छह वर्षों तक दुनिया धू-धू कर जलती रही। ऐसे
विध्वंस की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक-एक कर सारे देश युद्ध में शामिल होते
गये। सभी महाद्वीप प्रभावित हुए। नियमों को कौन कहे, मर्यादाएँ तक तोड़ी गयी। पूरे
के पूरे नगर और क्षेत्र जला दिये गये। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियारों का
इस्तेमाल शुरू ही हुआ था। इस बार उनका धड़ल्ले से प्रयोग होने लगा। जर्मनी दोहरे
संहार में लगा हुआ था। एक ओर तो वह विश्वव्यापी संहार कर ही रहा था। पर ऐसा तो
युद्ध में शामिल दूसरे देश भी कर रहे थे। जर्मनी का सबसे जघन्य अपराध था, करीब साठ लाख यहूदियों का नस्लवाद के
नाम पर भीषण संहार- महज इसलिए कि वे यहूदी थे और हिटलर की निगाह में निम्न कोटि के
प्राणी। यह प्रवृत्ति तो मानव मात्र में पायी जाती है जिसने अपने को श्रेष्ठ समझा
वह औरों को निम्मतर समझ उसे नगण्य मानने लगता है। भारत में सवर्णों द्वारा दलितों
का अपमान और उत्पीड़न इसका ऐतिहासिक उदाहरण है। पर हिटलर ने इसे अपने नकारात्मक चरम
पर पहुँचा दिया और बच्चे,
बूढ़े तक निर्ममतापूर्वक भट्टियों में
झोंक दिये गये।
युद्धों के पहले और युद्ध के दौरान यहाँ तक कि
शीतयुद्ध के दौरान भी विध्वंसक हथियारों की खोज तेज हो जाती है। सभी शक्तिशाली देश
ऐसे हथियारों की खोज में थे जो शत्रु को पंगु बना दे। वर्षों से इसके लिए परमाणु
ऊर्जा का प्रयोग करने के प्रयास हो रहे हैं। अन्ततः अमरीका ने एक परमाणु बम बना ही
लिया। तब तक मुख्य शत्रुओं में इटली हथियार डाल चुका था। जर्मनी भी पराजित हो चुका
था। बस बचा हुआ था जापान और वह भी हथियार डालने ही जा रहा था। सभी शत्रु पराजित हो
जाते तो परमाणु बम का वास्तविक परीक्षण कहाँ होता? इसलिए अमरीका के राष्ट्रपति टूमन ने ताबड़तोड़ हिरोशिमा और नागाशाकी पर
परमाणु बम गिरा दिये और यह प्रमाणित हो गया कि यह नया हथियार अभूतपूर्व ढंग से
संहारक और विध्वंसक है। जिसने ने भी ‘हिरोशिमा
के फूल’ पढ़ा होगा या वाशिंगटन स्थित, ‘हालोकास्ट म्यूजियम’ देखा होगा उसकी आत्मा तक कॉप गयी होगी।
इस युद्ध में ऐसे हथियार बन गये थे, जिनका
परिणाम तात्कालिक तो होता ही था। परमाणु बम से निकली रेडियोधर्मिता इतनी विकराल है
कि दूर-दूर तक जहाँ भी उसका असर होता है वहाँ ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जारी रहती है
जो उस क्षेत्र में हो रहे किसी भी उत्पादन को, चाहे
वह मनुष्य का हो या वनस्पतियों का, उसे
नकारात्मक रूप से प्रभावित करती चली जाती है।
 |
| This file picture of a post card released by the Historial de Peronne |
इतने विध्वंस के बाद एक संभावना यह थी कि शायद
दुनिया के शासक कॉप जाएँ और ऐसे हथियारों पर अंकुश लग जाए। जिस पायलट ने हिरोशिमा
पर बम गिराया था वह अपराधबोध से विक्षिप्त हो गया। जिन वैज्ञानिकों ने इसे बनाने
में सक्रिय भूमिका निभाई,
जैसे ओपेनहाईमर वह आजीवन शान्ति-शान्ति
का पाठ करते रहे। पर नहीं प्रभावित हुए तो ट्रूमन और उनकी शासक बिरादरी। ऐसे
हथियारों और दूर-दूर तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों का विस्तार होता गया और
ऐसे शस्त्रों का निर्माण करने वाली बिरादरी में जल्दी ही ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और कुछ दिनों बाद चीन भी शामिल हो गया। अब तो ऐसे ‘समर्थ’ देशों में भारत और पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं जहाँ की आधी जनता
दोनों जून पेट भी नहीं भर पाती-और हथियार भी ऐसे जिसके सामने जापान पर गिराये गये बम पटाका लग सकते हैं।
इसी विषय पर शोध करने वालों के अनुसार ऐसे
हथियारों का इतना बड़ा जखीरा तैयार हो चुका है कि सारी धरती को कई-कई बार नष्ट किया
जा सकता है। अब तो ABC हथियारों का जमाना है यानी, ‘एटामिक बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों का’ और इन हथियारों का शिकार हो जाने के
लिए अपराधी होना आवश्यक नहीं। पहले हम कहानी में सुनते थे कि झरने के ऊपर बैठा शेर
नीचे पानी पीते भेड़ से कह सकता था कि वह उसका पानी जूठा क्यों कर रहा है। यानी
आक्रमण के लिए बे सिर पैर के बहाने बनाये जा सकते हैं। हम इराक में देख चुके हैं
कि आक्रमण के लिए कैसे बहाने बनाये जा सकते हैं। यह कहना भी स्थिति को उजागर नहीं
करता कि मनुष्य पाशविक होता जा रहा है, क्योंकि
कोई भी पशु दूसरे पशु को अकारण नहीं मारता।
खतरनाक यह ही नहीं है कि देश लगातार
शस्त्रास्त्रों के भण्डार बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि समाज में भी
युद्धोन्माद बढ़ता जा रहा है। पहले सामान्यतः झगड़े होते भी थे तो लाठी-डंडे से लोग
एक-दूसरे का हाथ-पैर तोड़ देते थे। अब तो बात-बात में पिस्तौल और बम चल जाते हैं।
ज़्यादातर लोग गुस्से में दिखायी देते हैं और अपने से कमजोर मिला नहीं कि हाथ उठ
जाता है। वह व्यक्ति पत्नी और अपना ही बेटा भी हो सकता है। जिन-जिन बातों पर
व्यक्ति, समुदाय और देश आपस में लड़ पड़ते हैं और
संहार तक पहुँच जाते हैं,
वह संवेदनशील लोगों की नींद हराम कर
सकता है।
ऐसे में हम कैसे कहे कि 1914 में शुरू हुआ
भूमंडलीकृत युद्ध यानी विश्वयुद्ध समाप्त हो गया था। तो क्या मान लिया जाय कि
मनुष्य हिंस्र, आत्महंता और मानसिक रोग से ग्रस्त हो
गया है और रोग संक्रामक होता जा रहा है तथा ला-इलाज लग रहा है ?
पर ऐसा कैसे हो सकता है? आस्तिक लोग मानते हैं कि मनुष्य उस
परमनियंता की संतान है। फिर वह इतना हिंस्र कैसे हो सकता है? ऐसा करने से तो स्वयं ईश्वर पर उंगली
उठ जाती है और नास्तिक मनुष्य तो इतने तर्क-बुद्धि से लैस होने चाहिए कि युद्ध को
आत्महंता समझे और उससे बचने के उपाय ढूंढे। पर ऐसा हो तो नहीं रहा। ऐसा कैसे होगा? जब तक आक्रामक प्रतिस्पर्धा और युद्ध
के कारण बने रहेंगे और वे मनुष्य का मनोविज्ञान तक प्रभावित करते रहेंगे। युद्ध का
प्रमुख कारण है असमानता और अन्याय। स्वतंत्रता, समानता
और भाईचारे को दुनिया का श्रेष्ठतम जीवन मूल्य माना जाता है। पर केवल अपने लिए।
फ्रांस की क्रान्ति जहाँ ये सिद्धांत
जन्में वहाँ भी सभी नागरिकों को समान नहीं माना गया। फ्रांस दुनिया भर में अपने
उपनिवेश बनाता और बढ़ाता गया। ब्रिटेन जो जनतंत्र का गढ़ माना जाता रहा है। पर वह
दुनिया का सबसे बड़ा उपनिवेशवादी देश रहा है। जहाँ-जहाँ जनतंत्र कायम भी हो गया है
जैसे-भारत वहाँ भी समाज के अधिकांश को सामाजिक न्याय नहीं प्राप्त है।
इतनी सभ्य और सशक्त होती जा रही दुनिया में भी
शोषण, उत्पीड़न और दमन न केवल संभव है कभी-कभी
उसे आवश्यक भी बताया जाता है। जो भी व्यक्ति शोषित, उत्पीड़ित और दमित होगा उसके मन में आक्रोश तो पलता ही रहेगा। अब
दुनिया इतना आगे बढ़ ही चुकी है कि की नियतिवाद के भारी दुष्प्रचार के बावजूद लोग
जानते जा रहे हैं कि उनकी दुर्दशा के कारण नियति में नहीं परिस्थितियों में हैं।
दूसरी ओर, श्रेष्ठता और असमानता को प्राकृतिक
मानते हुए जो लोग और देश शक्तिशाली है वह शक्ति को ही श्रेष्ठता का मानक बनाये
रखना चाहते ही हैं। ऐसे में सामान्य लोगों में भी श्रेष्ठ बनने के लिए किसी न किसी
तरह शक्तिशाली बनना जीवन की सबसे बड़ी उत्प्रेरणा बन जाए यह स्वाभाविक है। शक्ति
इतनी निर्णायक है कि नियमों का उल्लंघन किया जा सकता है। नियमों की अपने अनुकूल
व्याख्या की जा सकती है और वे आड़े आयें ही तो उन्हें बदला जा सकता है। जब शक्ति
इतनी निर्णायक हो और उसका व्यवस्थित ढंग से लगातार गौरवान्वयन होता हो तो सभी
शक्तिशाली बनने की चूहा-दौड़ में शामिल होते जाये क्या यह स्वाभाविक नहीं लगता ?। पर क्या यह भी स्वाभाविक नहीं कि
समझदार होने का दावा करने वाली आज की दुनिया यह भी समझे कि अन्ततः चूहा-दौड़ में
सभी चूहे मर जाते हैं।
ऐसा नहीं है कि यह बात समझी नहीं जा रही। आज भी
मुख्यतः शान्ति की श्रेष्ठता मानी ही जाती है। कुछ न कुछ प्रयास भी होते ही रहते
हैं। आज भी युद्ध विरोधी,
विश्वविख्यात चित्रकार पिकासो रचित
दुनिया की सबसे विख्यात युद्ध विरोधी पेटिंग ‘गेरनिका’ युनाइटेड नेशंस की दीवार पर टंगी ही
हुई है। युद्ध की भर्त्सना करने वाला साहित्य तो लिखा ही जा रहा है। पर युद्ध को
अ-निवार्य बताने वाला साहित्य भी तो लगातार लिखा जा रहा है। देशभक्ति के लिए युद्ध
तो आज भी गौरवांवित है।
पर एक दिन यह एकदम उजागर हो ही जाएग कि युद्ध और
शान्ति के बीच सह-अस्तित्व संभव नहीं। युद्ध अब
इतना विनाशक हो गया है कि जब तक उसका अन्त नहीं होगा तब तक वह दीमोक्लीज की तलवार
की तरह मानवता के सर पर लटकी ही रहेगी। आशा की किरण इस बात से पैदा होती है कि
मानव जाति ने बार-बार असंभव को संभव कर दिखाया है। उसने कितने चमत्कारी
आविष्कार और विचार दिये हैं तो क्या वह युद्ध जैसे संहारक रोग का निदान नहीं ढूढ़
सकता? युद्ध जीवन विरोधी है और सारी मानवता
आत्महंता नहीं हो सकती-अभी तो उसे जीवन को उच्चतर स्तर तक ले जाना है!
सम्पर्क-
मोबाईल - 09454069645
(इस पोस्ट में सभी चित्र गूगल के सौजन्य से प्रस्तुत किए गए हैं.)








अच्छा आलेख।
जवाब देंहटाएंअच्छा आलेख।
जवाब देंहटाएंकमाल का आलेख है। ज्ञानवर्धक और आंखें खोलने वाला इतिहास!
जवाब देंहटाएंशानदार आलेख...
जवाब देंहटाएंपूरी सदी को युद्ध इतिहास के रूप में चित्रित करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर वर्ग को इस चित्र से गायब कर दिया गया है। प्रथम विश्वयुद्ध की विभीषिका के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के विद्रोह से उपजी अक्टूबर क्रान्ति और उसकी युगान्तरकारी भूमिका का लेखक के लिए कोई महत्त्व नहीं है। यह बिलकुल ओझल कर दिया गया है क़ि विजयी अक्टूबर, भावी युद्धों के विरुद्ध सबसे बड़ी गारंटी था जिसे स्टालिनवादी प्रतिक्रान्तिकारियों की गद्दारी ने डुबो दिया।
जवाब देंहटाएंपूरी सदी को युद्ध इतिहास के रूप में चित्रित करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर वर्ग को इस चित्र से गायब कर दिया गया है। प्रथम विश्वयुद्ध की विभीषिका के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के विद्रोह से उपजी अक्टूबर क्रान्ति और उसकी युगान्तरकारी भूमिका का लेखक के लिए कोई महत्त्व नहीं है। यह बिलकुल ओझल कर दिया गया है क़ि विजयी अक्टूबर, भावी युद्धों के विरुद्ध सबसे बड़ी गारंटी था जिसे स्टालिनवादी प्रतिक्रान्तिकारियों की गद्दारी ने डुबो दिया।
जवाब देंहटाएंपूरी सदी को युद्ध इतिहास के रूप में चित्रित करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर वर्ग को इस चित्र से गायब कर दिया गया है। प्रथम विश्वयुद्ध की विभीषिका के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के विद्रोह से उपजी अक्टूबर क्रान्ति और उसकी युगान्तरकारी भूमिका का लेखक के लिए कोई महत्त्व नहीं है। यह बिलकुल ओझल कर दिया गया है क़ि विजयी अक्टूबर, भावी युद्धों के विरुद्ध सबसे बड़ी गारंटी था जिसे स्टालिनवादी प्रतिक्रान्तिकारियों की गद्दारी ने डुबो दिया।
जवाब देंहटाएंमुझे इस Blog के बारे में पता नहीं था। मैंने "पहली बार" नाम की इस ब्लॉग को पहली बार ही पढ़ा है। लेखक ,इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता लाल बहादुर वर्मा को पढ़ने का एक अलग अनुभव ही प्राप्त होता है ।
जवाब देंहटाएंमुझे इस Blog के बारे में पता नहीं था। मैंने "पहली बार" नाम की इस ब्लॉग को पहली बार ही पढ़ा है। लेखक ,इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता लाल बहादुर वर्मा को पढ़ने का एक अलग अनुभव ही प्राप्त होता है ।
जवाब देंहटाएंयकीन नहीं होता कि इतने सरल शब्दों में भी इतना शानदार आलेख लिखा जा सकता है। आपकी और रचनाएँ पढ़ने को उत्सुक हूँ...
जवाब देंहटाएं