पंकज बोस का आलेख ''दूसरी परम्परा के नामवर सिंह : खोज के कुछ बिन्दु"।
 |
| नामवर सिंह |
नामवर सिंह का नाम लेते ही विद्वता के प्रति हमारा मन आदर और सम्मान से झुक जाता है। अपनी अध्ययनशीलता से नामवर जी ने साहित्य को जाँचने-परखने का जो प्रतिमान गढ़ा वह आज भी अत्यन्त मानीखेज़ है। हालांकि द्विवेदी जी को ले कर लिखी गयी महत्त्वपूर्ण पुस्तक को वे ख़ुद ही विनम्रता से 'अन्तरिम रिपोर्ट' कहते हैं। आगे चल कर नामवर सिंह ने उस 'वाचिक शैली' को अपनाया जो हमारी भारतीय परम्परा के मूल में है। इस वाचिक परम्परा के जरिए वे आजीवन अपना काम करते रहे। शायद यही वजह है कि नामवर जी को सुनना रोचक हुआ करता था। उनको पढ़ना आज भी ख़ुद को पढ़ने जैसा होता है।
पंकज बोस युवा आलोचक हैं और अपने आलोचनात्मक-शोधपरक लेखन के लिए जाने जाते हैं। हालांकि पंकज ने कम लिखा है लेकिन बेशक यह कहा जा सकता है कि 'जी लगा कर लिखा' है। उन्होंने नामवर जी पर एक महत्त्वपूर्ण आलेख लिखा जो 'आलोचना' के अंक-62 (अक्टूबर-दिसम्बर 2019) में प्रकाशित हो चुका है। आज नामवर जी के जन्मदिन पर उनकी स्मृति को नमन करते हुए 'पहली बार' पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं पंकज बोस का आलेख ''दूसरी परम्परा के नामवर सिंह : खोज के कुछ बिन्दु"।
दूसरी परम्परा के नामवर सिंह : खोज के कुछ बिंदु
पंकज कुमार बोस
किसी आलोचनात्मक कृति को पढ़ते समय बहुधा हम शीर्षक के अनुरूप उसमें आलोचक के विश्लेषण को पढ़ने के आदी होते हैं। ऐसा करते हुए विवेच्य विषय की मूल समस्याओं को समझ लेने पर भी उससे सम्बद्ध आलोचक के निजी आशयों पर ध्यान नहीं दे पाते। वस्तुनिष्ठता का दवाब इतना अधिक होता है कि उसके पीछे आलोचक के आत्मीय सरोकारों की ओर उन्मुख नहीं होते। ‘आत्मीय’ यानी आलोचक की व्यक्तिगत दृष्टि या आलोचना के लिए उसकी निजी तैयारी। इस अर्थ में जो आलोचक विवेच्य विषय के प्रतिपादन और आलोचना की भाषा को ले कर जितना सचेत होगा, पाठकों से उसकी तैयारी को समझने के लिए उतनी ही तत्परता अपेक्षित होगी। यानी यदि हमें यह समझना है कि प्रस्तुत आलोचना लिखने में आलोचक की मूल प्रवृत्ति और उद्देश्य क्या रहा है तो उसमें निहित आत्मीयता या वैयक्तिकता के अन्तःसूत्रों की खोज करनी होगी। यह खोज भी अपने आप में आलोचना का ही एक काम होगा।
‘दूसरी परम्परा की खोज’ हिन्दी आलोचना की एक लघु प्रबंधात्मक कृति है जो हमें इस चुनौती का अवसर देती है। अब तक इस पर जितना अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, उन सबमें ‘दूसरी परम्परा’ को समझने-समझाने का ही उपक्रम हुआ है। बहुधा अध्येता ‘दूसरी परम्परा’ से इतने आक्रान्त रहे कि उसकी नातिदीर्घ व्याख्या कर उन्होंने अपने कार्य की इतिश्री मान ली। ‘खोज’ की ओर ध्यान दिया ही नहीं। यदि ‘खोज’ की ओर किसी ने ध्यान दिया भी तो उसे ‘दूसरी परम्परा’ से जोड़ कर ही देखा। अधिक से अधिक उसे अध्ययन-विश्लेषण या आलोचना का पर्याय मान कर छुट्टी पा ली। असल में ‘खोज’ इतना साधारण और इकहरे अर्थों वाला शब्द नहीं, विशिष्ट और बहुअर्थी पद है। नामवर सिंह की आलोचनात्मक तैयारी का सार और आलोचक के रूप में उनके आत्मसंघर्ष की कुंजी है। ज़रूरत है इस आत्मसंघर्ष के उन्मेष को पकड़ने की। इस दृष्टि से यदि हम केवल इसी कृति का अध्ययन करें तो ‘दूसरी परम्परा’ पद के साथ-साथ ‘खोज’ का अध्ययन भी अनिवार्य हो जाएगा। विश्लेषण-मूल्यांकन में अपेक्षित संतुलन की दृष्टि से भी यह उचित होगा।
दूसरी परंपरा : किसकी ?[i]1
हिन्दी में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के बाद या उनसे भिन्न दूसरी परम्परा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। लेकिन किस अर्थ में? इसका उत्तर हमें परम्परा के एक गौण अर्थ की ओर ले जाता है। लेकिन जो लोग इस ‘दूसरी परम्परा’ को आचार्य शुक्ल की नितांत विरोधी (परम्परा) समझते हैं, उनके लिए पहले इसी गौण अर्थ से निकलने वाले व्यंजित अर्थ को समझना बेहतर होगा। राम चन्द्र शुक्ल की एक लम्बी शिष्य परम्परा रही है। इसके आधार पर उनकी “कम-से-कम दो परम्पराएँ” रही हैं और इसका मतलब है कि “शुक्ल जी में गहरे अंतर्विरोध हैं।”[ii]2 अपनी पुस्तक में नामवर सिंह ने इस शिष्य परम्परा का संकेत मात्र किया है लेकिन स्पष्ट है कि शिष्यों या परवर्तियों में एक परंपरा उनके अनुगामियों की है तो दूसरी प्रतिगामियों की। अनुगामियों और प्रतिगामियों की भूमिका शुक्ल जी के आलोचनात्मक अवदान की सराहना-सहमति और असहमति-विरोध की है, व्यक्तिगत प्रशंसा या विरोध की नहीं। यदि हम इस सामान्य-सी बात को ध्यान में रखें तो अनुमान लगा सकते हैं कि एक धारा नंद दुलारे वाजपेयी की है जो शुक्ल जी के समय में ही उनकी (कुछ) स्थापनाओं का विरोध कर रहे थे और दूसरी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है जो शुक्ल जी के समय और उनके बाद भी उनका समर्थन करते रहे, उनकी मान्यताओं का अनुसरण करते रहे। एक ही गुरु के दो तरह के शिष्यों का यह केवल एक-एक उदाहरण है। उद्धरणों की यह शृंखला आगे भी बढ़ायी जा सकती है, लेकिन अभिप्राय केवल यही है कि दो अलग-अलग प्रस्थान-बिंदुओं को ले कर चलने वाले शिष्यों ने गुरु के अंतर्विरोध के अलग-अलग पहलुओं को पकड़ा है। यदि नंद दुलारे वाजपेयी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, शुक्ल जी का विरोध और समर्थन करते हुए भी उनकी परम्परा (की दो धाराओं) का विकास करते हैं तो ‘खोज’ के लेखक का कहना है कि “ऐसी स्थिति में देखना होगा कि द्विवेदी जी, शुक्ल जी की किस परम्परा से सम्बद्ध हैं? तभी इस बात का निर्णय हो पाएगा कि द्विवेदी जी ने उसका विकास किया या नहीं।”[iii]3 यहाँ ध्यान देने वाली बात है ‘परम्परा का विकास’। यदि परम्परा का अनुसरण कर के उसका विकास किया जा सकता है तो विरोध कर के क्यों नहीं? द्विवेदी जी यही कर रहे हैं। परम्परा का विरोध कर के उसका विकास कर रहे हैं। इसलिए ‘दूसरी परम्परा’ का एक अर्थ यदि शुक्ल जी की विरोध करने वाली परम्परा है, तो दूसरा अंतर्निहित अर्थ दूसरी धारा या शाखा के रूप में उस परम्परा का विकास करना भी है। इस अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए ‘दूसरी परम्परा’ का अध्ययन किया जाय तो उक्त विरोध (जो विरोध के माध्यम से परम्परा को आगे बढ़ाता है) के अन्य संदर्भ भी उजागर हो सकते हैं।[iv]4
‘विरोध’ को यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी की शब्दावली में कहें तो वह है—‘अस्वीकार’। उदाहरण हैं कबीर।
इस संबंध में द्रष्टव्य है ‘दूसरी परम्परा की खोज’ पुस्तक का ‘अस्वीकार का साहस’ शीर्षक निबंध। इसमें नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर संबंधी विवेचना पर ध्यान केन्द्रित किया है। वस्तुतः इसमें न तो कबीर का और न ही हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन किया गया है बल्कि अगले मूल्यांकन-पुनर्मूल्यांकन के लिए कुछ सूत्र छोड़े गए हैं। स्वयं द्विवेदी जी ने ‘कबीर’ पुस्तक की भूमिका में लिखा है, “कबीर दास बहुत-कुछ को अस्वीकार करने का अपार साहस ले कर अवतीर्ण हुए थे।” और आगे, “उन्होंने तत्काल प्रचलित नाना साधन-मार्गों पर उग्र आक्रमण किया है।”[v]5 नामवर सिंह ने अपने निबंध में द्विवेदी जी के इस संकेत को विस्तार दिया है। सोचना चाहिए कि ‘अस्वीकार का साहस’ क्या केवल कबीर में ही है? द्विवेदी जी में नहीं है? और क्या नामवर सिंह में भी नहीं है? या अपने समय में आचार्य शुक्ल में नहीं था? उन्होंने भी तो कबीर को अस्वीकार करना चाहा था! यदि कबीर ने प्रचलित साधन-मार्गों का विरोध किया है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी प्रचलित आलोचना-दृष्टि को अस्वीकार किया है। और यह सहज ही लक्षित किया जा सकता है कि द्विवेदी जी के समय में एक प्रचलित आलोचना-दृष्टि राम चंद्र शुक्ल और उनकी (शिष्य) परम्परा की भी थी। नामवर सिंह भी अपने समय में प्रचलित समीक्षा-दृष्टि को अस्वीकृत करते आ रहे हैं। इसी अस्वीकार के साहस की परिणति हैं उनकी दो कृतियाँ—‘कविता के नए प्रतिमान’ और ‘दूसरी परम्परा की खोज’। उदाहरण और भी हैं लेकिन प्रबंधात्मक कृति होने के कारण इन दोनों के नाम लिए गए हैं। यों हम कह सकते हैं कि यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल की परम्परा से भिन्न एक स्वस्थ परम्परा के लिए मार्ग बनाया या नामवर सिंह ने एक स्वस्थ आलोचना-परम्परा का विकास किया तो इसका अर्थ यह है कि आलोचना-दृष्टि के विकास के लिए ही नहीं, आलोचना- परम्परा के विकास के लिए भी ‘अस्वीकार का साहस’ अनिवार्य है। इस अस्वीकार में वैयक्तिक या वैचारिक विरोध के मामले गौण हो जाते हैं, परम्परा और उसके विकास का मुद्दा बेहद ज़रूरी हो जाता है। नामवर सिंह ने जहाँ-जहाँ विरोध किया है, वहाँ-वहाँ परम्परा के प्रति उनका यही दृष्टिकोण मुखर रहा है। उन्होंने कई जगहों पर, यहाँ तक कि अपने ‘आत्मकथ्य’ में भी इस तथ्य की याद दिलाई है जहाँ थियोडोर एडोर्नो को लगभग आत्मविश्वास के अंदाज में उद्धृत किया गया है—“One must have tradition in oneself, to hate it properly.” उद्धृत करने के तुरंत बाद उन्होंने लिखा, “जैसे यह बिजली की एक कौंध सी थी मेरे अपने समूचे जीवन और लेखन के लिए।”[vi]6
खोज-प्रक्रिया से पहले, प्रचलित आलोचना-दृष्टि (कबीर के संदर्भ में ‘नाना साधन-मार्गों’) के विरोध या अस्वीकार का एक और प्रसंग। ‘दूसरी परम्परा की खोज’ के आरंभिक अध्यायों में नामवर सिंह ने स्पष्ट किया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रवीन्द्र नाथ की प्रेरणा से कबीर का नया मूल्यांकन किया है। आगे उन्होंने लिखा है, “कबीर के माध्यम से जाति-धर्म-निरपेक्ष मानव की प्रतिष्ठा का श्रेय तो द्विवेदी जी को है ही। एक प्रकार से यह दूसरी परम्परा है।”[viii]8 तुरंत हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर जाता है कि आचार्य शुक्ल ने कबीर का ही नहीं बल्कि छायावाद के संदर्भ में रवीन्द्र नाथ के व्यापक प्रभाव का भी नकार के स्वर में विरोध किया है। यहाँ कबीर के व्यापक प्रभाव से आंदोलित हैं रवीन्द्र नाथ और पुनः रवीन्द्र की प्रेरणा से कबीर की ओर अग्रसर हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यों विरोध की दशा में और सहमति की स्थिति में भी यदि हमारी कुछ उपलब्धि है तो वह है : परम्परा की दो धाराओं या दो शाखाओं का विकास। कबीर दास और रवीन्द्र नाथ की व्यापकता का प्रभाव दूरगामी है। नामवर सिंह ने रवीन्द्र नाथ की ‘विश्व-दृष्टि’ की चर्चा करते हुए बतलाया है कि कैसे उससे द्विवेदी जी की आलोचना में एक खुलापन या व्यापकता आई। इस खुलेपन या उन्मुक्तता का रचनात्मक उपयोग उन्होंने न केवल अपने निबंधों या उपन्यासों में, बल्कि सूर, कबीर और कालिदास से सम्बद्ध अपनी आलोचना में भी किया है। ‘दूसरी परम्परा’ ऐसी ही उन्मुक्त और भविष्योन्मुखी आलोचना-दृष्टि की एक संज्ञा हो सकती है। ‘खोज’ का लेखक कहता है—“नए इतिहास के साथ आलोचना का एक नया मान भी दृष्टि-गोचर होता है। ‘कबीर’ के साथ इतिहास की एक भिन्न परम्परा ही नहीं आती, साहित्य को जाँचने परखने का प्रतिमान भी प्रस्तुत होता है।”[ix]9 स्पष्ट है कि ‘भिन्न परम्परा’ पद विरोध या अस्वीकार का समानधर्मा है जबकि ‘प्रतिमान’ उस परम्परा के विकास का। नामवर सिंह की ऐसी स्थापनाएँ पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हैं। लेकिन ‘दूसरी परम्परा की खोज’ में रेल की दो पटरियों की तरह इस वस्तुनिष्ठता के समांनातर आत्मपरकता की उपस्थिति भी उनके आलोचनात्मक आत्मसंघर्ष को समझने का मार्ग प्रशस्त करती है।
 |
| राम चंद्र शुक्ल |
संतुलन बिंदु : आत्म और वस्तु
आलोचना-कर्म में ज्यों-ज्यों हम वस्तुनिष्ठता की सीढियाँ उतरते हुए आत्मपरकता की गहराई तक पहुँचते हैं, दोनों की परस्परता का एहसास होने लगता है। आलोचक की आलोचना- प्रक्रिया और उसके आत्म-संघर्ष का भेद खुलने लगता है। यों वस्तुनिष्ठ विवेचन और आत्मीयतापूर्ण प्रस्तुति का अध्ययन भेद और अभेद का परस्पर अध्ययन हो जाता है : दार्शनिक निहितार्थों में नहीं, शुद्ध व्यावहारिक आलोचना के संदर्भ में। ‘दूसरी परम्परा की खोज’ के लेखक नामवर सिंह ने द्विवेदी जी की परम्परा का अनुसंधान किया है — यह उनका वस्तुनिष्ठ विवेचन है। उन्होंने अनुसंधान करते-करते स्वयं को ‘दलित द्राक्षा की भाँति निचोड़ कर’ उड़ेल दिया है—यह उनकी आत्मीयतापूर्ण प्रस्तुति है। स्वयं ‘खोज’ की ‘भूमिका’ इसका साक्ष्य है जिसके अनुसार इस पुस्तक में न आलोचना है और न ही मूल्यांकन, “अगर कुछ है तो बदल देने वाली उस दृष्टि के उन्मेष की खोज, जिसमें एक तेजस्वी परम्परा बिजली की तरह कौंध गयी थी। उस कौंध को अपने अन्दर से गुजरते हुए जिस तरह मैंने महसूस किया, उसी को पकड़ने की कोशिश की है। सफल कहाँ तक हो सका, इसका उत्तर परम्परा की ‘दूसरी खोज’ ही देगी। सम्भव है, इसमें मेरी अपनी खोज भी मिल जाय!”[x]10
उन्होंने केवल भूमिका में ऐसी सूचना दी है (ऐसी और भी सूचनाएँ हैं जो नितांत वैयक्तिक हैं)। दूसरी ओर, पूरी पुस्तक में विवेचन की शैली वस्तुनिष्ठ है जबकि स्थान-स्थान पर आत्मीय प्रस्तुतियाँ हैं। नामवर सिंह ने जिस बात को दिल से स्वीकार किया—“जिस तरह मैंने महसूस किया” और जिस बात की संभावना जतलाई—“सम्भव है, इसमें मेरी अपनी खोज भी मिल जाय”—उसपर परवर्ती अध्येताओं का ध्यान गया ही नहीं। वे दूसरी परम्परा की मनोरम अरण्याणी में ही भटकते रह गए। जबकि सच तो यह है कि नामवर सिंह के इन सूत्रों को पकड़ कर हम साहित्य-समालोचना के किसी भी बीहड़ जटिल अरण्य में घूम / भटक सकते हैं और अपने गंतव्य तक पहुँच भी सकते हैं। हालाँकि ये सूत्र आत्मीयतापूर्ण हैं और बहुधा आलोचना के क्षेत्र में ‘आत्मीयता’ या ‘आत्मपरकता’ जैसे शब्दों को प्रासंगिक नहीं माना जाता। ख़ास तौर पर मार्क्सवादी आलोचना में किसी भी प्रकार के ‘ट्रीटमेंट’ के लिए इस प्रजाति के शब्द तो जैसे वर्जित ही हैं!
फिलहाल नामवर सिंह की आलोचना-प्रक्रिया में इन प्रवृत्तियों के उन्मेष को पकड़ने के पीछे मंशा यह नहीं है कि किसी तरह उन्हें गैर-मार्क्सवादी आलोचक साबित किया जाय, बल्कि केवल यही कि किसी भी प्रकार के आलोचना-कर्म में एक संतुलन-बिंदु की खोज की जाय। आलोचना में ऐसे संतुलन-बिंदुओं की खोज एक अल्पविवेचित पहलू है जिसे उजागर करने के सूत्र स्वयं नामवर सिंह देते हैं। पूरी पुस्तक में ये सूत्र ‘बिजली की कौंध’ की तरह हैं जिनका आभास पढ़ते-पढ़ते कुछ क्षणों के लिए ही सही, होता है। नामवर सिंह ने तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की तेजस्वी परम्परा के ‘विद्युत-तडितों’ को बहुत पहले ही अपने भीतर भाँप लिया था। ‘दूसरी परम्परा की खोज’ से भी बहुत पहले। अपनी आलोचना के निर्माण-काल में ही। आरंभ से ही वे कौंध से चमत्कृत नहीं होते, उसे अपने भीतर महसूस करते हैं। इसका प्रमाण है उनके आरंभिक दौर की ललित निबंधों की पुस्तक ‘बकलम ख़ुद’ जहाँ द्विवेदी जी के ललित निबंधों की छाप है जिसे कोई चाहे तो अनुसरण भी कह सकता है।[xi]11 हालाँकि परम्परा की व्याख्या करते हुए नामवर सिंह मानते हैं कि आलोचना-कर्म में मौलिक कुछ नहीं होता है। एक दृष्टि से देखें तो सब कुछ नकल ही है। नकल या अनुकरण का अर्थ व्यंजना में लेना चाहिए। यानी पूरी परम्परा को अपने भीतर जज्ब कर के उसे पुनःप्रस्तुत करना।
नामवर सिंह की आरंभिक आलोचना में ठीक उसी तरह राम चंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का छायाभास है जिस तरह अज्ञेय, मुक्तिबोध और शमशेर की आरंभिक कविताओं में छायावाद की छाया। यह छाप नकारात्मक नहीं है। ‘बकलम ख़ुद’ को प्रकाशित होने के बाद भी प्रायः साठ वर्षों तक अप्रकाशित रखने के पीछे यही संकोच तो नहीं था (?)—नकारात्मक प्रभाव के प्रकट होने का संकोच। यदि यह कृति प्रथम अल्पज्ञात प्रकाशन के बाद भी प्रकाशित होती रहती तो नामवर सिंह के आलोचक-व्यक्तित्व की बुनावट को समझना संभवतः और सरल होता। उनके अनुकर्ताओं के लिए नहीं, उनके वृहत्तर और वास्तविक पाठकों के लिए। ‘देर आयद दुरुस्त आयद’ को मानते हुए कह सकते हैं कि उस बुनावट को पकड़ना अभी भी कठिन तो है, असंभव नहीं। असल में आलोचक व्यक्तित्व की इस बुनावट की उधेड़बुन की प्रक्रिया का गहरा संबंध ‘खोज’ या खोज के उन्मेष की प्रक्रिया से भी है।
खोज का प्रस्थान : द्विवेदी जी का प्रथम प्रेम
नामवर सिंह की “अपनी खोज” के प्रसंग में सबसे पहले ध्यातव्य है उक्त ‘अनुकरण’ में मौलिकता के उन्मेष की पहचान। द्विवेदी जी की कथा और कथेतर कृतियों पर लिखते हुए नामवर सिंह ने शीर्षक दिया है ‘प्रेमा पुमर्थो महान’ और ‘त्वं खलु कृति’। रोचक बात यह है कि उन्होंने द्विवेदी जी के उपन्यासों को ‘प्रेम कथा’ की संज्ञा दी है। इससे भी रोचक एक और बात है। वैष्णव कवियों और सूरदास पर उनके आरंभिक लेखन का ज़िक्र करते हुए उसे ‘प्रथम प्रेम’ की संज्ञा दी है। वहीं से उन्होंने जाना कि प्रेम ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है।
यों तो ‘प्रेमा पुमर्थो महान’ प्राचीन शास्त्र कथन है, लेकिन द्विवेदी जी की रचनात्मक आलोचना में ढलने पर शास्त्र भी व्यावहारिक और प्राचीन भी नवीन रूप ग्रहण कर लेता है। यों हजारी प्रसाद द्विवेदी शास्त्र को आलोचना में ही नहीं, जीवन-दृष्टि में भी पिघला-पिघला कर ढाल लेने वाले आलोचक हैं। और शास्त्र को पिघलाने वाला वही होगा जिसमें पांडित्य के साथ-साथ सहानुभूति, संवेदना और सहृदयता भी होगी, अपने अध्ययन और आलोचना-कर्म में गहरी नैतिक निष्ठा होगी।
द्विवेदी जी के आरंभिक लेखन का उल्लेख करते हुए नामवर सिंह ने लिखा है, “बीस वर्ष बाद उन दिनों को याद करते हुए उन्होंने लिखा था कि उन दिनों इस महान भक्त [सूरदास] की कविता का नशा था। वैसा नशा फिर भले ही न हुआ हो, लेकिन बाद की रचनाएँ बतलाती हैं कि उसका असर कभी गया नहीं। शायद इसलिए कि वह प्रथम प्रेम था।”[xii]12 वह तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ‘प्रथम प्रेम’ था। लेकिन नामवर सिंह की स्थिति क्या है? ‘बकलम ख़ुद’ ख़ुद नामवर सिंह के हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रति प्रेम का आरंभिक दस्तावेज़ है। नामवर को वैसा नशा भले ही बार-बार न हुआ हो, लेकिन बाद की कृतियाँ बतलाती हैं कि “असर कभी गया नहीं”। बाद की इन कृतियों में ‘दूसरी परम्परा की खोज’ अन्यतम है। द्विवेदी जी के शताब्दी-वर्ष में लिखे गए मूल्यांकन-निबंध ‘द्वा सुपर्णा...’ और ‘पुनर्नवा की प्रतिमूर्ति’ तो अपने स्थान पर हैं ही।[xiii]13
जब हम किसी आलोचकीय व्यक्तित्व की बुनावट की ‘खोज’ करना चाहते हैं तो उस बुनावट में इस ‘प्रथम प्रेम’ को लक्षित किए बिना आगे बढ़ना कठिन है। प्रसंगतः विजय देव नारायण साही आलोचना-प्रक्रिया के जिस संदर्भ में ‘उधेड़बुन’ जैसी विशिष्ट शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं उसी संदर्भ में ‘बुनावट की खोज’ को भी जोड़ा जा सकता है। आलोचक के साक्ष्यानुसार द्विवेदी जी के ‘पहले प्रेम’ के प्रसंग में शांतिनिकेतन का भी उल्लेख होता है जिसका अंकुर फूटा है 7-8 नवंबर 1930 को। नामवर सिंह अक्सर द्विवेदी जी के व्यक्तिगत जीवन-प्रसंगों को सामने ला कर आलोचना-कर्म को बेहद निजी या आत्मीय बना देते हैं। ‘खोज’ के पहले अध्याय में शांति निकेतन का प्रसंग यों ही नहीं आया है। वह द्विवेदी जी की गंभीर आलोचना में प्रवेश कराने वाली एक सुगम पगडंडी की तरह हमारे सामने खुलती है। जहाँ-जहाँ व्यक्तिगत जीवन के प्रसंग आए हैं, उनमें आजकल प्रचलित तथाकथित संस्मरणात्मक आलोचना-सी हल्की मनोरंजकता या विपथन नहीं है, बल्कि “बिजली की कौंध” को पकड़ने जैसी प्रत्यक्षानुभूति है। बिजली की कौंध को पकड़ने और उसे महसूस करते हुए प्राण गँवाने का ख़तरा हो सकता है। इसलिए आत्यंतिक जोखिम उठा कर यह करना पड़ता है। (यदि किसी को ‘बिजली की कौंध’ को (अभिधा में ही) पकड़ने और महसूस करने का जीवंत और मर्मभेदी विवरण पढ़ना हो तो अज्ञेय की ‘स्मृति लेखा’ में हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखा हुआ उनका संस्मरण पढ़ना चाहिए जिसका शीर्षक है ‘बीसवीं सदी का बाणभट्ट’।)[xiv]14 नामवर सिंह भी लगभग वही आत्यंतिक जोखिम उठा कर उस कौंध को पकड़ते हैं। लेकिन अभिधा में ही नहीं, लक्षणा और व्यंजना के साथ।
स्वयं नामवर सिंह के आलोचक व्यक्तित्व की पहचान की दृष्टि से प्रस्तुत कृति का ‘त्वं खलु कृति’ नामक अध्याय अतिशय महत्त्वपूर्ण है। इस अध्याय में द्विवेदी जी की आत्मसमीक्षा की चर्चा के बहाने उनके व्यक्तित्व की चर्चा है और उनकी आलोचना की शैली पर बात करते हुए स्वयं नामवर सिंह का आलोचक व्यक्तित्व भी छन कर बाहर आ गया है। उनके बहुमूल्य शब्द हैं—“आत्मसमीक्षा के रूप में द्विवेदी जी की जिस कृती-दृष्टि का परिचय मिलता है उसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है, उनकी क्रीड़ाशीलता... उनके हाथों शास्त्र भी साहित्य बन जाता है... (वे) शब्द की व्याख्या नहीं करते, उसे उपयुक्त संदर्भ देते हैं।... वस्तुतः द्विवेदी जी की आलोचना में व्याख्या की भूमिका प्रधान नहीं है, प्रधान भूमिका है उद्धरणों के चयन की। प्रसंग के अनुकूल वे ऐसे उद्धरण चुन कर लाते हैं कि किसी अतिरिक्त युक्ति की आवश्यकता रह नहीं जाती।”[xv]15 इस उद्धरण में ‘द्विवेदी जी’ के स्थान पर ‘नामवर सिंह’ रख कर पढ़ें तो हमारा अभिप्राय स्पष्ट हो जाएगा। नामवर सिंह वस्तुतः एक कृती आलोचक हैं और ‘दूसरी परम्परा की खोज’ सचमुच एक ‘कृती व्यक्तित्व का अभिनव परिचय-पत्र।’[xvi]16
आलोचना में व्यक्तिगत जीवन-प्रसंगों की बहुलता अक्सर उसे संस्मरण की ओर ले जाती है—और जबकि आलोचना महज संस्मरण नहीं है, तब यह निश्चित है कि आलोचना को संस्मरण न बनने देने के लिए आत्यंतिक जोखिम उठाया जाय। नामवर सिंह व्यक्तिगत जीवन के प्रसंग भी लाते हैं और उनकी आलोचना निरा संस्मरण भी नहीं बनने पाती। यथास्थान इन प्रसंगों को वे इतनी सावधानी से पिरोते चलते हैं कि आत्मपरकता और वस्तुपरकता का अंतर मिट जाता है। यों ‘अष्टाध्यायी’ कही जाने वाली ‘दूसरी परम्परा की खोज’ के आठ अध्यायों में निहित आलोचना-कर्म आठ फूल की तरह हैं जिन्हें द्विवेदी जी के जीवन-प्रसंग के धागों में बेहद सलीके से टांक दिया गया है। इस सलीके का नाम है अंतदृष्टिपूर्ण सूझ और आलोचनात्मक विवेक। कहना चाहिए कि यह सूझ और विवेक नामवर सिंह में भरपूर है।
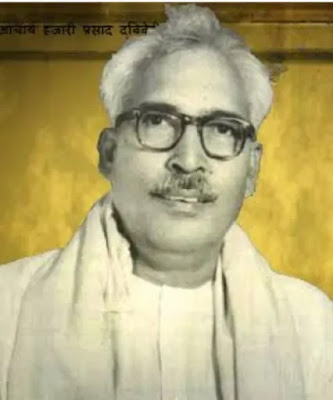 |
| हजारी प्रसाद द्विवेदी |
वस्तुनिष्ठ गर्वोक्ति
व्यक्तिगत जीवन-प्रसंगों के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के वृहत्तर योगदान पर भी नामवर सिंह ने गर्वोक्ति की है। आलोचना में स्वयं की गर्वोक्ति और स्वयं की भूमिका को ले कर आत्मश्लाघा तो बहुतों में देखी गई (जो किसी भी आलोचक के कच्चेपन का द्योतक है); लेकिन जिस पर लिखा जा रहा है या जिसे स्थापित किया जा रहा है, उस पर सच्ची गर्वोक्ति बहुत कम ही देखने को मिलती है। वैसे नकलची और अर्थहीन गर्वोक्ति करने वाले भी बहुत हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं। आचार्य शुक्ल की तुलसी और जायसी पर की गई गर्वोक्ति सच्ची गर्वोक्ति है। राम विलास शर्मा की निराला को ले कर की गई गर्वोक्तियाँ। नामवर सिंह की हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुक्तिबोध केंद्रित गर्वोक्तियाँ।
गर्वोक्ति, नामवर सिंह ने स्वयं के बारे में कम-से-कम की है, न के बराबर। वैसे भी इस तरह की गर्वोक्ति प्राचीन प्रातिभ और महान रचनाकारों को ही शोभा देती है। भवभूति की ‘उत्पत्स्यन्ते मम् तु कोSपि समानधर्मा’ या निराला की ‘मैं अलक्षित हूँ / यही कवि कह गया है’ जैसे उनके उदात्त जीवन संघर्ष की काव्यात्मक साक्ष्य हैं, वैसे ही स्वयं कविता के उदात्त मूल्यों की संवाहिका भी। हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित नामवर सिंह की गर्वोक्तियाँ भी वस्तुतः दोनों (आलोच्य और आलोचक) की आलोचना के उदात्त मूल्यों की साक्ष्य हैं। नामवर सिंह की गर्वोक्ति के शब्द देखिए—“‘चौरासी वैष्णवों की वार्ता’ तो बहुतों ने पढ़ी और वल्लभाचार्य से सूरदास के मिलन का उल्लेख भी किया; किन्तु द्विवेदी जी के लिए यह घटना इतनी महत्त्वपूर्ण थी कि उसका उल्लेख उन्होंने अनेक बार किया है और रस ले कर किया है।”[xvii]17 यहाँ ‘बहुतों’ को नीचा दिखाना उद्देश्य नहीं। उद्देश्य है ‘बहुतों’ के समानांतर जिसे खड़ा किया जा रहा है, उसकी अपेक्षित विशिष्टता को उजागर करना।
 |
| नंद दुलारे वाजपेयी |
आलोचना में, ‘गर्वोक्ति’ में गर्व दूसरों के प्रति किया जाता है, ‘उक्ति’ अपनी होती है। इसलिए गर्वोक्ति को निजी या व्यक्तिगत समझने का भ्रम न रखना चाहिए। यह ‘आत्म’ और ‘पर’ का समन्वय है। आलोचना-कर्म में यह समन्वय बेहद ज़रूरी है। एक सजग आलोचक हमेशा ‘आत्मनिष्ठ गर्वोक्ति’ और ‘वस्तुनिष्ठ गर्वोक्ति’ में अंतर समझेगा। ‘आत्मनिष्ठ गर्वोक्ति’ बहुधा प्रतिभाशाली कवियों का पक्ष होता आया है, जबकि ‘वस्तुनिष्ठ गर्वोक्ति’ आलोचकों का। नामवर सिंह इसी श्रेणी में हैं।
उक्त ‘वस्तुनिष्ठ गर्वोक्ति’ के बीज शब्द हैं—“द्विवेदी जी के लिए यह घटना इतनी महत्त्वपूर्ण थी”। ध्यातव्य है कि कोई घटना सबके लिए समान रूप से महत्त्वपूर्ण नहीं होती। इस प्रसंग में प्रो. एडवर्ड हैलेट कार की विश्वविख्यात पुस्तक ‘इतिहास क्या है’ का ध्यान आता है जिसमें उन्होंने बतलाया है कि “लाखों लोगों ने रूबीकान नदी को पार किया था लेकिन इतिहासकार हमें विश्वास दिलाता है कि केवल सीजर का रूबीकान नदी के पार जाना महत्त्वपूर्ण था। वस्तुतः ऐतिहासिक तथ्य जिस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं वे अपने युग के मूल्यों से प्रभावित इतिहासकार द्वारा अभीप्सित व्याख्या के लिए किए गए चुनाव का ही प्रतिफलन होते हैं। भले ही पूर्ण वस्तुनिष्ठता असंभव हो, इतिहासकार की भूमिका न तो कम होती है, न इतिहास का सम्मोहन कम होता है...”[xviii]18 ई. एच. कार विश्व इतिहास की विभिन्न घटनाओं की तथ्यात्मक व्याख्या की ओर संकेत करते हुए उस व्याख्या के आधार पर किसी भी घटना के साधारण या असाधारण होने की प्रवृत्ति पर ध्यान दिला रहे हैं, लेकिन उनकी यह स्थापना इतिहास के ऐसे किसी भी समानधर्मी तथ्य के लिए उतनी ही प्रासंगिक है। कार के इस उद्धरण में यदि हम ‘ऐतिहासिक तथ्य’ की जगह ‘आलोचनात्मक तथ्य’ और ‘इतिहासकार’ की जगह ‘आलोचक’ पढ़ें तो अभिप्राय स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा।
वल्लभाचार्य-सूरदास प्रसंग पर दृष्टि तो बहुतों की गयी, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए वह घटना विशेष महत्त्वपूर्ण हो उठी। ‘वस्तुनिष्ठ गर्वोक्ति’ में इस तथ्य पर ध्यान होना चाहिए कि कोई घटना या विषय किसी के लिए क्यों सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो उठी? आचार्य शुक्ल के लिए तुलसी दास, राम विलास शर्मा के लिए निराला, राम स्वरूप चतुर्वेदी के लिए अज्ञेय, नामवर सिंह के लिए मुक्तिबोध या हजारी प्रसाद द्विवेदी के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो उठने के पीछे केवल इन आलोचकों की वस्तुनिष्ठ गर्वोक्तियाँ ही नहीं हैं, बल्कि वे अपने युग के मूल्यों से प्रभावित आलोचक द्वारा अभीप्सित व्याख्या के लिए किए गए चुनाव के परिणामस्वरूप भी महत्त्वपूर्ण हैं। इस प्रक्रिया में कहीं-कहीं वस्तुनिष्ठता में कमी आ सकती है, लेकिन आलोचक या आलोचना की भूमिका कभी न्यून नहीं होती, न होनी चाहिए। वल्लभाचार्य-सूरदास प्रसंग द्विवेदी जी के लिए इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं है कि उसमें केवल उनकी व्यक्तिगत रुचि है, बल्कि इसलिए कि उनका इतिहास-बोध इस विशिष्ट प्रसंग पर आ कर अत्यंत उर्वर और मुखर हो जाता है। विचारधारा का प्रश्न उसके बाद आता है। यों, इतिहास-बोध : वैयक्तिक रुचियाँ : वैचारिक परिप्रेक्ष्य— इस क्रम में आलोचना की रचना-प्रक्रिया क्रियाशील होती है। व्यक्तिगत अध्ययन, तैयारी और अभ्यास तो इसमें अंतर्निहित हैं ही।
 |
| नेहरू |
नेहरू की ‘डिस्कवरी’ और नामवर की ‘खोज’
‘दूसरी परम्परा की खोज’ पुस्तक में जितना महत्त्व ‘परम्परा’ का है, उससे कम महत्त्व ‘खोज’ का नहीं। यह ‘खोज’ विशुद्ध एकेडमिक ‘रिसर्च’ का पर्याय नहीं है। एकेडमिक ‘खोज’ की गतानुगतिकता की अपेक्षा श्रेष्ठ समालोचना में ‘खोज’ का महत्त्व नवीन दृष्टि और मौलिकता के कारण अधिक होता है। ‘शुद्ध कविता की खोज’ तो दिनकर ने भी की थी, लेकिन उनकी खोज आज यदि गंभीरता से नहीं ली जा रही तो इसका एक कारण यह भी है कि बहुतों के लिए वह आलोचना की दृष्टि से कम, अकादमिक शोध की दृष्टि से अधिक उपयोगी प्रतीत होती हो। हालाँकि इस प्रसंग में विश्व साहित्य को पहचानने वाली दिनकर की सूक्ष्म दृष्टि हमें कायल करती है। दिनकर की विद्वता के साथ-साथ वक्तृता को मिलाने पर उनकी आलोचना या वैचारिक निबंधों का रूप संभव होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि एक विद्वान या मनीषी-कवि आलोचना लिखता है तो वह ‘शुद्ध कविता की खोज’ जैसी पुस्तक लिख सकता है। नामवर सिंह की ‘दूसरी परम्परा की खोज’ से गुज़रने पर ‘परम्परा’ और ‘खोज’ दोनों पर बराबर हमारा ध्यान केन्द्रित रहता है जब कि दिनकर के वैदुष्य के कारण उनकी ‘खोज’ पर से हमारी दृष्टि हट-सी जाती है क्योंकि वहाँ हम उनकी जानकारी के आग्रही होते हैं। यों दिनकर की ‘खोज’ और नामवर की ‘खोज’ में एक विद्वान-कवि और सुलझे हुए आलोचक का ही नहीं, वरन एक कवि की स्वच्छंद विदग्धता और आलोचक के अर्जित अनुशासन का अंतर भी है।
इस प्रसंग में और अन्यत्र भी दिनकर (‘संस्कृति के चार अध्याय’ आदि में), नेहरू की ‘द डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ के कुछ करीब हैं : प्रेरणा और प्रभाव-ग्रहण की दृष्टि से, विषयवस्तु की दृष्टि से भी, लेकिन प्रतिपादन या प्रस्तुति की दृष्टि से नहीं। नामवर सिंह की ‘दूसरी परम्परा की खोज’ भी नेहरू की ‘द डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ के बहुत करीब है : प्रेरणा और प्रभाव-ग्रहण की दृष्टि से, प्रतिपादन या प्रस्तुति की दृष्टि से भी, किन्तु विषयवस्तु की दृष्टि से नहीं। आशय यह है कि जिस तरह ‘भारत की खोज’ के प्रसंग में नेहरू की अपनी खोज भी निहित है उसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी की खोज में नामवर सिंह की भी अपनी खोज निहित है।
‘डिस्कवरी’ और ‘खोज’ वस्तुनिष्ठ शैली में लिखी गयी कृतियाँ हैं, लेकिन दोनों में आत्मीयता अथवा विषय से आत्मीय लगाव की एक मुकम्मल बुनियाद भी है। ध्यान से पढ़ने पर हिन्दुस्तान के प्रति नेहरू का और द्विवेदी जी के प्रति नामवर सिंह का लगाव महसूस किया जा सकता है। अनेक स्थानों पर विषय-निरूपण की प्रकृति के कारण नेहरू पूर्ण वस्तुनिष्ठता का निर्वाह नहीं कर पाए हैं, नामवर सिंह ने फिर भी यथासंभव वस्तुनिष्ठता का निर्वाह किया है। इस दृष्टि से ‘खोज’ के मर्म को समझने के लिए ‘डिस्कवरी’ को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मेरा विनम्र प्रस्ताव है कि ‘दूसरी परंपरा की खोज’ और ‘द डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ को साथ-साथ पढ़ा जाना चाहिए। कोई चाहे तो ‘खोज’ को पढ़ने से पहले भी ‘डिस्कवरी’ को पढ़ सकता है।
‘द डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ शुरू होती है भारत के अतीत की खोज से। यह ‘खोज’ जिसे नेहरू प्रायः ‘Quest’ भी कहते हैं, क्रमशः ‘Discovery’ का अर्थ ग्रहण करती जाती है। नेहरू के लिए अतीत कोई एकल सत्ता नहीं, वर्तमान का पूरक है। इसलिए वे पहले अध्याय के उपशीर्षक ‘अतीत का वर्तमान से संबंध’ में कहते हैं, “उस वर्तमान की जड़ें अतीत में स्थित हैं और इसलिए हमेशा किसी सूत्र की खोज में मैंने अतीत की यात्राएँ (voyages of discovery) की हैं—कोई ऐसा सूत्र जो वर्तमान को समझने के लिए उसमें मौजूद रहा हो।”[xix]19 नेहरू की खोज और खोज के लिए यह यात्रा कोई बैठे-ठाले का धंधा नहीं है, बल्कि उनके मन में भारत को ले कर अनवरत चलने वाली बेचैनी का नतीजा है, आत्मसंघर्ष का परिणाम है। तीसरे अध्याय का शीर्षक ही है ‘The Quest’। अध्याय के आरंभ में ही नेहरू भारत के प्रति अपने लगाव का अत्यंत साहित्यिक वर्णन करते हैं—“चिंतन और सक्रियता के इन वर्षों में मेरा मन भारत से भरा-पूरा रहा है : उसे जानने की कोशिश में और उसके प्रति मेरी अपनी प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण में... जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया और उन गतिविधियों में संलग्न हुआ जो भारतीय स्वाधीनता के नेतृत्व के लिए प्रतिश्रुत हुईं, वैसे ही मैं भारत के बारे में सोचते हुए अभिभूत होने लगा।... हिन्दुस्तान मेरे खून में था और उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो सहज ही मुझे रोमांचित (thrilled me) करता था।”[xx]20
ध्यान दें, ‘इंडिया’ जवाहर लाल को ‘थ्रिल’ करती है। यदि जवाहर लाल नेहरू को एक आलोचक मानें तो ‘इंडिया’ उनके लिए आलोच्य है, ठीक उसी तरह जिस तरह नामवर सिंह के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी विवेच्य हैं। कोई विवेच्य विषय विवेचक में ‘थ्रिल’ कैसे पैदा करता है, इस बात को समझने के लिए अपने भीतर बिजली की कौंध को महसूस करना पड़ेगा। पुनः मूल संदर्भ की ओर ध्यान देते हुए यह जानना चाहिए कि असल में भक्ति-आंदोलन के उदय को ‘बिजली की चमक के समान’ बतलाने वाली स्थापना जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन की है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ‘मध्यकालीन धर्म-साधना’ में उद्धृत किया है और ‘आलोक पर्व’ में संकलित अपने निबंध ‘हिन्दी पर वैष्णव धर्म का प्रभाव’ में व्याख्यायित भी किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रियर्सन के मत को अपने अनुकूल पाते हैं, इसलिए उसकी व्याख्या करते हैं।
 |
| दिनकर |
जवाहर लाल नेहरू ने भारत का न केवल अनुभव किया, बल्कि उसके बारे में पढ़ा और समझा भी। नेहरू को जो ‘थ्रिल’ अध्ययन के साथ-साथ अनुभव से प्राप्त हुआ था, हजारी प्रसाद उसे अध्ययन द्वारा अर्जित कर रहे थे। या यों कहें कि द्विवेदी जी अपने अध्ययन को अपने अनुभव का हिस्सा बना रहे थे और इसी बहाने भक्ति आंदोलन की समूची परम्परा को आत्मसात कर रहे थे। उन्हें भक्ति आंदोलन को अपने अनुभव का विषय इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि वह उनके लिए समकालीन आंदोलन नहीं था, ऐतिहासिक आंदोलन था। द्विवेदी जी के इस अनुभव को बल मिल रहा था उनके इतिहास-बोध से जिसे उन्होंने ‘मनुष्य की तीसरी आँख’ की संज्ञा दी है।[xxi]21 इसी प्रकार ‘दूसरी परम्परा की खोज’ तक आते-आते नामवर सिंह को भी एक बार फिर अनुभव को अध्ययन का और अध्ययन को अनुभव का विषय बनाना पड़ा। यों हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्थिति जवाहर लाल नेहरू और नामवर सिंह के बीच में कहीं प्रतीत होती है। नेहरू के लिए भारत ऐतिहासिक तो था ही, समकालीन भी था। ऐतिहासिक भारत अध्ययन का विषय था और समकालीन भारत अनुभव का। नामवर सिंह के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी समकालीन थे। वृद्ध समकालीन। उन्होंने द्विवेदी जी का अध्ययन भी किया और उनकी उपस्थिति/सान्निध्य का अनुभव भी। ऐसे ही अध्ययन और अनुभव के निचोड़ से नेहरू ‘डिस्कवरी’ लिखते हैं और नामवर सिंह ‘खोज’। नेहरू के लिए यदि ‘थ्रिल’ के कारण हैं, तो नामवर के लिए भी ‘बिजली की कौंध’ महसूस करने के। यद्यपि नामवर सिंह इसे परम्परा से पाते हैं, जिसकी कौंध ग्रियर्सन, नेहरू और हजारी प्रसाद द्विवेदी से होती हुई उन तक पहुँची है। और परम्परा से इतने गहरे ‘आत्म’ संघर्ष के बाद जो चीज़ पाई जाती है वह केवल वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती। उसका एक अंतर्निहित आभ्यांतर भी होता है जो हमेशा ‘खोज’ की प्रेरणा देता रहता है।
नेहरू तीसरे अध्याय के ‘The Search for India’ उपशीर्षक में लिखते हैं, “इसलिए हमारे लिए भारत—जैसा कि यह था—की खोज (discovery) शुरू हुई, और इसने हमारे भीतर समझ और संघर्ष दोनों पैदा की।”[xxii]22 इसलिए नामवर सिंह की ‘भूमिका’ की पहली ही पंक्ति है, “परंपरा के समान खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया है।” और “फिर भी इस यात्रा में पड़ाव आते हैं। यह पड़ाव, दुर्भाग्य से, तभी आया, जब पण्डित जी नहीं रहे। यह छोटी-सी पुस्तक उस पड़ाव का अनुचिंतन है।”[xxiii]23 ध्यान से देखें तो नामवर सिंह का ‘अनुचिंतन’ नेहरू के “समझ और संघर्ष” का पर्याय प्रतीत होगा। नामवर सिंह का यह ‘अनुचिंतन’ बेहद निजी भी है, इसलिए “संभव है, इसमें मेरी अपनी खोज भी मिल जाय!”
इस बेहद निजी ‘खोज’ और ‘अनुचिंतन’ का ब्यौरा नामवर सिंह ने अपनी खोज-यात्रा में भले न दिया हो, लेकिन नेहरू ने दे दिया है। पहले अध्याय के अंतिम हिस्से अर्थात् ‘The Burden of the Past’ उपशीर्षक में। नामवर सिंह की ‘अपनी खोज’ के ‘एक्सटेंशन’ के रूप में भी इसे पढ़ा जा सकता है—“अनिवार्यतः कई बार मेरा दृष्टिकोण निजी भी होगा, कि कैसे मेरे मन में यह विचार पनपा, इसने कौन सा रूप धारण किया, मुझे कैसे प्रभावित किया और मेरे कामों पर भी असर डाला। पूरी तरह कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी होंगे, जिनका व्यापक पैमाने पर विषय से कोई सरोकार न होगा, लेकिन जिन्होंने मेरे मन को रँग दिया और पूरी समस्या के प्रति मेरे दृष्टिकोण को प्रभावित किया।”[xxiv]24
‘डिस्कवरी’ के आरंभिक तीन अध्याय वस्तुतः व्यापक पटल पर लिखी गई उसकी भूमिका हैं। पहले अध्याय के अंत में नेहरू आशंका ज़ाहिर करते हैं कि उनकी ‘आत्मकथा’ के आख़िरी पन्नों की तरह कहीं इस पुस्तक में भी आत्मकथात्मक तत्त्व न आ जाएँ—“मैं इस कहानी को पूरी तरह से एक व्यक्तिगत अध्याय के रूप में शुरू करूँगा, जो उस अवधि के तुरंत बाद की मेरी मनोदशा का संकेत भी देता है जिसके बारे में मैंने अपनी आत्मकथा के अंत में लिखा है। लेकिन यह कोई दूसरी आत्मकथा नहीं बनने जा रही है, हालाँकि मुझे डर है कि बहुधा इसमें निजी प्रसंग भी सामने आएँगे।”[xxv]25 एक बार फिर “बहुधा इसमें निजी प्रसंग भी सामने आएँगे” को “संभव है, इसमें मेरी अपनी खोज भी मिल जाय” के साथ मिला कर पढ़ें तो नामवर सिंह के ‘अनुचिंतन’ और ‘खोज’ का मर्म बेहतर समझ में आएगा। आगे, अपनी मनोभूमिका (तीसरे अध्याय ‘The Quest’) के बिल्कुल अंत में नेहरू लिखते हैं—“ऐसे तथा अन्य तरीकों से मैंने भारत की खोज (Discover India) का यत्न किया है, अतीत और वर्तमान के भारत की... उस अंतहीन जुलूस में कुछ समय के लिए मैंने अपने आप को पहचानने की कोशिश की है, जिसके आख़िरी छोर पर सबके साथ संघर्ष करते हुए मैं भी कहीं था। और फिर मुझे ख़ुद को अलग कर लेना होगा, कुछ इस तरह कि जैसे अकेले ही किसी पर्वत की ऊँचाई से नीचे की घाटी को देख रहा होऊँ।”[xxvi]26 यही वह स्थान है जहाँ से नेहरू वस्तुनिष्ठ विवेचन आरंभ करते हैं। उनका यह विवेचन भी “अंतहीन जुलूस” है जैसे नामवर के लिए ‘खोज’ एक “गतिशील प्रक्रिया”।
जिस प्रकार नेहरू नाटकीय ढंग से सहसा अपने आप को झटकते हुए आत्मपरकता से दूर कर लेते हैं वैसे ही नामवर सिंह। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी और व्योमकेश शास्त्री के रूप में आपने आलोच्य की द्विधा-विभक्ति की वे बहुत गहरी छानबीन करते हैं। वस्तुतः नामवर सिंह को इस ‘छोटी-सी पुस्तक’ में निजी वस्तुनिष्ठता-आत्मपरकता की विवेचना का अवकाश ही नहीं है। जितने पृष्ठों में नेहरू की ‘डिस्कवरी’ की पट-भूमिका समाप्त होती है, कमोबेश उतने पृष्ठों में नामवर सिंह की पूरी पुस्तक समाप्त हो जाती है। इसलिए वे अपनी उद्घाटन कला का प्रयोग केवल अपने विवेच्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में ही कर पाते हैं।
‘दूसरी परम्परा की खोज’ के आठवें अध्याय ‘व्योमकेश शास्त्री उर्फ़ हजारी प्रसाद द्विवेदी’ में उन्होंने रूपंकर कलाओं में प्रचलित मुख़ौटा-सिद्धांत के हवाले से हजारी प्रसाद के अभिन्न व्योमकेश शास्त्री पर प्रकाश डाला है। इस प्रकाश में द्विवेदी जी का फक्कड़पन, उनकी कल्पना-कला, उनका अवगुंठन, अपने को कर्ता न मानने की उनकी विनयशीलता और उनकी प्रतिभा का मर्म—एक साथ ही भास्वर हो कर पाठकों के सामने प्रकट होते हैं। यदि हजारी प्रसाद एक कृती साहित्यकार हैं तो व्योमकेश उस कृती की अंतरात्मा। कभी साहित्यकार अंतरात्मा बन जाता है तो कभी अंतरात्मा साहित्यकार। इसे आप पारिभाषिक शब्दावली में ‘रूप’ और ‘अंतर्वस्तु’ की एकता भी कह सकते हैं। ‘दूसरी परम्परा की खोज’ में आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग और उनके सूत्रों की खोज तो अलग से अध्ययन का विषय है लेकिन यहाँ इतना ही पर्याप्त है कि साहित्यकार और उसकी अंतरात्मा के पक्ष-परिवर्तन की व्याख्या करते-करते नामवर सिंह एक मार्के की बात कह जाते हैं— “दरसअल मुखौटा इसलिए मूल्यवान है कि वह स्वयं एक कलाकृति है और कलाकृति स्वयं मनुष्य से ज़्यादा अभिव्यंजक होती है। विचित्र विरोधाभास है कि जो मुखौटा चेहरा छिपाता है, वही भावों को ज़्यादा से ज़्यादा उद्घाटित करता है।”[xxvii]27 जिस पक्ष-परिवर्तन के संबंध में ये बातें हैं, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी और व्योमकेश शास्त्री के बीच है। इस विवेचन के उपरांत ‘खोज’ के लेखक का अंतिम निष्कर्ष और खोज की अंतिम पंक्ति है—“इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी और व्योमकेश शास्त्री में अपने-आपको द्विधा विभक्त कर के द्विवेदी जी ने उस सृजनशीलता की रक्षा और विकास किया, जो हिन्दी साहित्य के लिए मूल्यवान उपलब्धि है।”[xxviii]28 नेहरू अपनी भूमिका के अंत में “I would separate myself” कहते हैं और नामवर सिंह अपने अंतिम विवेचन में “अपने-आपको द्विधा विभक्त कर के” लिखते हैं।
नामवर सिंह की मानें तो (द्विवेदी जी को ले कर उनकी खोज बहुत पहले शुरू हुई थी, पुस्तक लिखी जाने तक भी वह पूरी न हुई थी) उनकी यह पुस्तक उस “खोज की अंतरिम रिपोर्ट” है। यों उक्त उद्धरण ‘अंतरिम रिपोर्ट’ की अंतिम पंक्ति है। यदि यह पुस्तक ‘अंतरिम रिपोर्ट’ है तो द्विवेदी जी की खोज-यात्रा की भूमिका मात्र ही है। यों ‘खोज’ का अध्ययन भी ‘डिस्कवरी’ की (मनो) भूमिका की तरह किया जा सकता है। यदि एक व्यतिक्रमी अध्ययन-पद्धति के रास्ते हम ‘खोज’ के अंतिम अध्याय से शुरू कर के पहले अध्याय तक आएँगे तो भी हमारे अर्थ-ग्रहण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। उसी तरह ‘डिस्कवरी’ के तीसरे अध्याय से शुरू कर के पहले अध्याय तक आने में भी कोई हानि नहीं। कारण वही है—द्विधा-विभक्ति। हाँ, यदि इस द्विधा-विभक्ति या द्वैत का समंजन पहले न किया जाय तो खोजी के मूल मंतव्यों के अर्थ-ग्रहण में कठिनाई हो सकती है। हमारे यहाँ एक चिंतन-परंपरा द्वैत से अद्वैत की ओर जाने वाली रही है जहाँ मूल विवेचन से पहले द्वैत-बोध का समाहार अनिवार्य माना गया है। अतः उक्त प्रस्ताव में दोनों कृतियों को इस दृष्टि से व्यतिक्रम में पढ़ने का आशय है : आत्मनिष्ठता-वस्तुनिष्ठता के जटिल प्रसंगों को पहले सुलझा लें फिर आगे मुख्य अध्ययन में प्रवृत्त हों।
बहुत से अध्येता और विद्वान ‘दूसरी परम्परा की खोज’ को आलोचक नामवर की उपलब्धियों में महत्तम मानते हैं। कुछ लोग इसे उनके उत्तरकाल की श्रेष्ठतम कृति स्वीकार करते हैं। विद्वानों की पसंद चाहे जो हो, पर जैसा कहा गया, स्वयं नामवर सिंह के लिए यह कृति तो ‘अंतरिम रिपोर्ट’ ही है। और जब अंतरिम रिपोर्ट है तो अंतिम नहीं, अनंतिम ही है। किसी भी परियोजना के इस पड़ाव पर आ कर ‘रिपोर्टर’ को सिंहावलोकन करना पड़ता है, जैसे कि नेहरू ने अपने ग्रंथ के अंत में किया है—समाहार या निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए, ‘पोस्टस्क्रिप्ट’ लिखते हुए। जैसे कि नेहरू ने यह प्रश्न उठाया है—“भारत की खोज—आखिर मैंने खोजा क्या है?”[xxix]29 ‘अंतरिम रिपोर्ट’ के बाद भी यही एक प्रश्न है जो अंततः शेष रह जाता है। यही वह प्रश्न है जिसकी गूँज-अनुगूँज दूसरे रूपों में मुक्तिबोध में सुनाई पड़ती है और जो बार-बार नामवर के शब्दों में हम तक प्रतिध्वनित होती रहती है : “अंत में पीछे मुड़ कर अपने पूरे जीवन का सिंहावलोकन करता हूँ तो अन्दर-अन्दर वही प्रश्न उठता है जिससे मुक्तिबोध बेचैन रहते थे : अब तक क्या किया? / जीवन क्या जिया?”[xxx]30 उन्होंने अपने ‘आत्मकथ्य’ का नामकरण भी किया तो यही—‘जीवन क्या जिया!’ यह भी महज संयोग नहीं कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण के अवसर पर नामवर सिंह ने जो वक्तव्य दिया उसे भी ‘अब तक क्या किया...’ शीर्षक से संपादित-प्रकाशित किया गया है। वास्तव में जवाहर लाल नेहरू नाम के इस विश्वविद्यालय के निर्माण में नामवर सिंह और स्वयं नामवर के विकास में इस विश्वविद्यालय की भूमिका को मणि-कांचन संयोग वाली घटना कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वस्तुतः जो विश्वविद्यालय नेहरू के सपनों को ले कर निरंतर प्रगतिकामी रहा; समय के हर मोड़ पर विद्या, ज्ञान और बौद्धिकता के क्षेत्र में सामासिक संस्कृति को ले कर अपनी प्रतिबद्धता की छाप छोड़ता रहा और इन सबके बीच एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व के रूप में नामवर सिंह का सान्निध्य पाता रहा, वह अलग से अध्ययन का विषय है। फिलहाल इस विषय पर सुमन केशरी द्वारा संपादित अनूठी पुस्तक ‘जे एन यू में नामवर सिंह’ से उनके उक्त वक्तव्य-अंश को देखें और इसे एक तरह से ‘पोस्टस्क्रिप्ट’ के रूप में भी पढ़ें : “इन अठारह वर्षों में जो कुछ किया, जो कुछ हुआ, जो कुछ लिखा; उसमें साल भर की सबेटिकल छुट्टी के दौरान लिखी हुई ‘दूसरी परम्परा की खोज’ मेरे लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस किताब के लिए मैं विश्वविद्यालय का ऋणी हूँ।”[xxxi]31 बहुतों के लिए यह किताब दूसरे कारणों से एक उपलब्धि है लेकिन स्वयं लेखक के लिए उपलब्धि है, तो—नेहरू के सपनों की सांस्कृतिक दुनिया में रहते हुए रचे जाने के कारण।
प्रस्तुत संदर्भ में किंचित विस्तार का ख़तरा उठाते हुए भी ‘दूसरी परम्परा की खोज’ के साथ ‘द डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ को आईने की तरह रख कर पढ़ने के प्रस्ताव के कुछ निहितार्थ हैं। कुछ कारणों और साम्य-वैषम्य की चर्चा यहाँ की गई। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नेहरू के प्रति स्वयं नामवर सिंह के एक परवर्ती आकलन का संज्ञान लेना भी प्रासंगिक होगा।
यह मात्र उद्धरण नहीं, बल्कि एक परिप्रेक्ष्य है। नामवर सिंह के इस उद्धरण के बाद नेहरू-नामवर के गहरे बौद्धिक अन्तःसूत्रों पर अलग से टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ‘खोज’ की चर्चा यहीं समाप्त नहीं होती। नामवर सिंह के उद्धरण के अंत में ‘पहचान’ शब्द साभिप्राय है। ‘पहचान’ हमारे पूर्व-विवेचित ‘खोज’ के पर्याय के रूप में तो है ही, यहाँ ‘अस्मिता’ का अर्थ भी दे रहा है। उनके एक और व्याख्यान का शीर्षक है ‘हमारी साहित्यिक परंपरा और भारतीयता की सही पहचान’ जो मार्च 1991 में भोपाल में दिया गया था। इतना ही नहीं, वर्ष 2012 में आशीष त्रिपाठी के संपादन में प्रकाशित उनकी चार पुस्तकों में से एक का नाम है ‘साहित्य की पहचान’। यह उनके वाचिक आलोचना-कर्म की पुस्तक है। हालाँकि यह कोई आत्यंतिक नियम तो नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि लेखन में नामवर सिंह अक्सर ‘खोज’ और वाचिक में प्रायः ‘पहचान’ शब्द का प्रयोग करते हैं।
इसी प्रसंग में स्मरणीय है प्रसिद्ध समाजविज्ञानी प्रो. श्यामाचरण दुबे का ‘भारतीयता की तलाश’ शीर्षक निबंध, जो एक अर्थ में ‘डिस्कवरी’, ‘खोज’ और ‘पहचान’ का ही अर्थ-विस्तार करता है।
वास्तव में परंपरा के सारभूत मूल्यों को जो समझता है वही उसकी पुनर्व्याख्या या पुनर्नवीकरण के लिए प्रस्तुत हो सकता है। कोई विरला ही कभी ‘क्वेस्ट’, ‘डिस्कवरी’, ‘सर्च’ या ‘री-डिस्कवरी’ शुरू करता है और कभी ‘खोज’ या ‘तलाश’ के लिए निकल पड़ता है। नामवर सिंह के आकाशधर्मा गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं अपने विपुल साहित्य के माध्यम से मध्यकालीन धर्म और संस्कृति, कालिदास-बाणभट्ट, छान्दोग्योपनिषद् और रवीन्द्र-सूर-कबीर, नाथ-सिद्ध साधकों और सिख गुरुओं के पुण्य स्मरण और मीमांसा के निमित्त भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अनंत राशि की खोज ही की है। पुनराविष्कार ही तो किया है! यदि ग़ौर से देखें तो हमारे साहित्य की महान प्रगतिशील परम्पराओं में ‘खोज’ करने वाले इतने जगमगाते मानव-नक्षत्र हैं कि समूचा परिदृश्य ही प्रदीप्त हो उठता है और यह सब घटित होता है ‘बिजली की कौंध’ की भाँति अनुभूत होने वाले किन्हीं अपूर्व पावन-पूत अत्यंत दुर्लभ क्षणों में!
ऐसे ही दुर्लभ क्षणों में याद आता है ‘कविता के नए प्रतिमान’ का निबंध ‘अँधेरे में : परम अभिव्यक्ति की खोज’ और फिर कौंध उठते हैं कृती कवि मुक्तिबोध के ये शब्द :
उसको तू खोज अब
उसका तू शोध कर!
वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति,
उसका तू शिष्य है (यद्यपि पलातक...)
वह तेरी गुरु है
गुरु है...[xxxiii]33
संदर्भ / टिप्पणियाँ
[i] विस्तार के लिए देखिए, नामवर सिंह की पुस्तक ‘दूसरी परम्परा की खोज’ का पहला अध्याय ‘दूसरी परम्परा की खोज’। हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केन्द्रित यह पुस्तक 1982 में प्रकाशित हुई लेकिन इसी शीर्षक से एक निबंध उन्होंने तीन वर्ष पूर्व भी लिखा था जो ‘आलोचना’ पत्रिका के अप्रैल-जून/जुलाई-सितम्बर 1979 अंक में प्रकाशित हुआ था और अब उनकी पुस्तक ‘आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय-यात्रा’ में संकलित है। ऐसा प्रतीत होता है कि 1979 वाला निबंध वस्तुतः हजारी प्रसाद द्विवेदी (19 अगस्त 1907-19 मई 1979) के निधन के बाद उनके पहले जन्मदिन के निमित्त लिखा गया स्मृति-लेख है। है वह स्मृति-लेख, लेकिन संस्मरणों की बजाय उसमें दूसरी परम्परा के पथीकृत विचारक के रूप में द्विवेदी जी के योगदान को रेखांकित किया गया है। निबंध के आरंभिक वाक्य हैं—“आज पंडित जी के पुण्य स्मरण का दिन है। मन स्मृतियों से आच्छन्न है। किन्तु जिसे संस्मरण कहते हैं, ऐसा लिखने लायक कुछ भी याद नहीं आता।” [नामवर सिंह (2017) : 45] इसके बाद शान्ति निकेतन में उनके ‘द्विजत्व-प्राप्ति के दिन’ का प्रसंगोल्लेख और फिर द्विवेदी जी के उद्धरणों द्वारा ‘दूसरी परम्परा’ की कतिपय विशिष्टताओं का आलेखन। वस्तुतः नामवर सिंह की “दूसरी परम्परा” की अवधारणा ‘दूसरी परम्परा की खोज’ पुस्तक से पहले की है और उनकी अन्तर्यात्रा में यह द्विवेदी जी के मृत्यु-बोध के फलस्वरूप पैदा हुए रिक्तता-बोध की एक अनिवार्य परिणति भी है। एक और प्रमाण है ‘खोज’ वाली पुस्तक की ‘भूमिका’ की ये पंक्तियाँ—“परम्परा के समान खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया है। फिर भी इस यात्रा में पड़ाव आते हैं। यह पड़ाव, दुर्भाग्य से, तभी आया, जब पंडित जी न रहे। यह छोटी-सी पुस्तक उस पड़ाव का अनुचिंतन है।” [नामवर सिंह (1983) : 7]
[ii] नामवर सिंह (1983) : 18
[iii] नामवर सिंह (1983) : वही
[iv] हमने यहाँ ‘दूसरी परम्परा’ के एक सामान्य किन्तु प्रस्तुत लेख के लिए प्रासंगिक अर्थ की ओर ध्यान दिलाया है। अनेक विद्वानों ने इस कृति की विवेचना करते हुए ‘दूसरी परम्परा’ के अन्य अर्थों का भी संधान किया है, उन पर बहसें भी हुई हैं। प्रस्तुत लेख के मूल भाग में विस्तार-भय के कारण हमने इन बहसों का उल्लेख नहीं किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पुस्तकों को देखा जा सकता है :
(I) सुधीश पचौरी (सं.) - नामवर के विमर्श; प्रवीण प्रकाशन; 1995
(II) अशोक वाजपेयी (सं.) - परम्परा की आधुनिकता : हजारी प्रसाद द्विवेदी; पूर्वोदय प्रकाशन; 2002
(III) भगवान सिंह - भारतीय परम्परा की खोज, सस्ता साहित्य मंडल; 2011
(IV) सुधीश पचौरी - तीसरी परम्परा की खोज; वाणी प्रकाशन; 2019
[v] मुकुन्द द्विवेदी (सं.) (2007) : 195
[vi] भारत यायावर (सं.) (2003) : 508
[vii] नामवर सिंह (2012) : 142
[viii] नामवर सिंह (1983) : 13
[ix] नामवर सिंह (1983) : 17
[x] नामवर सिंह (1983) : 7
[xi] इस दृष्टि से उनकी उसी समय की उनकी एक रम्य रचना ‘आषाढस्य प्रथम दिवसे...’ पढी जा सकती है जिसमें आषाढ़ के पहले दिन रचनाकार और बादल का एक काल्पनिक किन्तु व्यंग्यात्मक संवाद है।
बादल कहता है, “बन्धु, सोचते क्या हो? आज आषाढ़ का पहला दिन है! आज आदमी बादल से बोलता है और बादल आदमी से।... तुम्हें काव्य-रसिक समझ कर ही बात कर रहा हूँ। बंगाल, बिहार से होते हुए यहाँ तक आया हूँ। आगे पंजाब की सीमा तक जाने का हौसला है। बीच में कोई संदेश हो तो कहो।”
संदेश से पहले बादल की अभ्यर्थना करनी चाहिए, लेकिन कैसे करें ये उलझन है, “लेकिन तुम्हारी पूजा करूँ भी तो किन फूलों से? फूल यहाँ नहीं रहे क्योंकि फूलदान बहुत हो गए हैं। (यहाँ दान माने आदान ही समझना।)... हरित कपिश अर्द्धरूढ़ केसर वाले कदम्ब कुसुम की ऋतु तो अभी आई ही नहीं। उसकी जगह तो कदंब की तरह नेताओं के गदगद बोल ही मिलेंगे। और प्रत्यग्र कुटज कुसुम? यहाँ कहाँ? अब तो वैसे फूल ‘पोज’ देते समय कैमरे के सामने मंत्रियों के अधखुले ओठों से झरते हैं अथवा निबंधों में द्विवेदी जी की कलम से।”
आगे बादल को काशीपुरी से दिल्ली तक का मार्ग बतलाया जाता है और वह भी पूरे कालीदासीय लय में, द्विवेदीय शैली में।
“शीघ्र ही तुम उस काशीपुरी में पहुँचोगे जो पहले कैलाशपति शिव के त्रिशूल पर थी लेकिन अब कमलापति विष्णु के चक्र पर है। पहुँचते ही वेणीमाधव का धौरहरा अथवा काटन मिल की चिमनी तुम्हारा स्वागत करेगी। नगरद्वार पर हँसों के धवल बंदनवार की तरह लटका हुआ मालवीय पुल तुम्हारा अभिनन्दन करेगा।... यहाँ से आगे के मार्ग तुम्हें वही सफेदपोश राजहंस बताएँगे जो राजधानियों तक जाने के लिए पाथेय के जोगाड़ में कुछ ही दिनों तक काशी में होंगे। इनमें से तुम केवल प्रयाग की ओर जाने वालों का साथ पकड़ना। इनकी पहचान यह है कि लखनऊ जाने वालों की अपेक्षा इनके पंख अधिक उजले होते हैं।... प्रयाग पहुँचते ही प्रसाद के अभाव में भी हिन्दी की वह काव्य त्रिवेणी मिलेगी जिसमें स्नान करके तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध हो जाएगा। परुन्तु कुछ और धाराओं और नालों के संगम को उमड़ते हुए देख कर त्रिवेणी का भ्रम न कर लेना।... प्रान्त की राजधानी और विशाल श्री वाली लखनऊ नगरी का मार्ग यहाँ से कुछ टेढ़ा है परन्तु वहाँ न जा कर तुम स्वर्ग का एक कान्तिमान टुकड़ा छोड़ दोगे, क्योंकि वर्तमान भूमि-भोगियों ने अपने पुण्य के भावी स्वर्ग-फल के बदले इस स्वर्ग-खंड को माँग लिया है। मार्ग में कलयुगी राघव की कीर्ति रूप में बिखरे हुए अनेक तालाब मिलेंगे जो वस्तुतः कागज पर ही खोदे गए हैं, परन्तु जादू से जमीन पर भी निकल गए हैं। इन तालाबों की मृगतृष्णा से तृप्त हो कर तुम लखनऊ पहुँचना।... लखनऊ कोई छोड़ता नहीं; छोड़ना पड़ता है। इसलिए हे मीत मेघ! तुम्हें पहले ही संभल जाना है। शीघ्र ही दिल्ली जाने के लिए कानपुर का रास्ता लेना।... दिल्ली पहुँचते ही सबसे पहले राजघाट की वह विभूति अपने शरीर में मल लेना जिसके रंग से कितने काले कारनामे मोटे दिख रहे हैं।... खादी की चाँदनी में गोरे मेघ-खंडों की क्रीड़ा के साथ लहराते हुए ज़रा दूतावासों का भी चक्कर लगा लेना और विदेशी बोतल पर फिट देशी ‘कागों’ को उछालते जाना। वहाँ से जान बुल की उस तोंद पर चढ़ जाना जो कभी वायस रीगल लॉज कहलाता था। और वहाँ से उचक कर कुतुबमीनार की ओर देखना कि नेहरू जी खड़े हैं या उतर गए। जब फाइल की ठंढी सीढ़ियों पर खट-खट चढ़ती हुई नौकरशाही तुम्हें चौंक कर देखे तो कह देना कि यह जनता है जो स्वयं अपने शरीर की सीढियाँ चढ़ कर दिल्ली के स्वर्ग पर आ बैठी है। फिर हमारे प्यारे प्रधानमंत्री को सोते से जगा कर धीरे से कह देना कि कुतुबमीनार नहीं एवरेस्ट पर चढ़ कर देखिए—यह है आपका बहका सपना!” [नामवर सिंह (2013) : 128-134]
[xii] नामवर सिंह (1983) : 57
[xiii] दिलचस्प है कि इन दो निबंधों में नामवर सिंह ने प्रच्छन्न रूप से द्विवेदी जी के समकक्ष उनके समकालीन जिस रचनाकार की ओर संकेत किया है वे हैं अज्ञेय। ‘द्वा सुपर्णा...’ निबंध के आरम्भ में ही वे लिखते हैं, “वैसे, साहित्य की रचना करने वाले और साथ ही साथ उसकी आलोचना लिखने वाले लेखक अनेक हुए, लेकिन इनमें से अधिकांश रचनाकारों के लिए आलोचना-कर्म हाशिए पर लिखा जाने वाला दूसरे दर्जे का काम रहा है। इसी तरह कुछ आलोचकों ने भी कथा-कविता आदि की रचना की है लेकिन उन्हें मुख्यतः आलोचक ही माना जाता है।... इस दृष्टि से हिन्दी कथाकारों में उनके निकट कोई लेखक कुछ-कुछ पहुँचता है तो एक अज्ञेय ही।” [नामवर सिंह (2010 क) : 173]
[xiv] ‘स्मृति-लेखा’ में संकलित अज्ञेय के संस्मरण ‘बीसवीं सदी का बाणभट्ट’ का संदर्भित अंश यों है :
“शान्ति निकेतन की खोवाई नदी, नदी तो नाम की ही है। पर उस के लाल-पीले, ढले-कटे, कंकरीले-मटीले कगार का एक आकर्षण है जिसे विश्वभारती के कई चित्रकारों ने चित्रित किया है। वर्षा ऋतु की घिरती घटाएँ इस आकर्षण को और बढ़ा देती हैं। पर घटाएँ लाने वाली वे आँधियाँ जब आतीं तो पेड़-पौधे मानो उन के जुहार के लिए बार-बार नीचे तक झुक जाते।
“उस दिन ऐसी ही आँधी के आसार दिखे तो मैंने एकाएक घोषणा की : “मैं घूमने जा रहा हूँ।”
“पंडित जी ने कुछ चौंक कर पूछा : “अन्धड़ में?”
“पंडितानी ने भी कमरे से बाहर आ कर डपटते हुए कहा, “नहीं, अन्धड़ में घूमने नहीं जाना है। यहीं बैठे रहिए।”
“पर हठ तो हठ है। घटा तेजी से घिर रही थी और गड़गड़ाहट स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। अँधेरा नहीं हुआ था इसलिए बिजली चमक चौंधाती तो नहीं थी पर वायुमंडल में एक नया तनाव भर जाती थी।
“बड़ा तूफान आने वाला है—यहाँ पेड़-वेड़ भी टूटते हैं और गिरती डालों से ख़तरा रहता है। मत जाइए।”
“अन्धड़ का, बालों में सनसनाती हवा का, पिंडलियों पर चिकोटी काटती कंकरियों का आनंद कैसे समझाया जा सकता है? पर नादान अतिथि के लिए वात्सल्य-भरे आतिथेय की चिन्ता भी शायद समझायी नहीं जा सकती अगर समझी न गयी हो... मैंने अपनी धृष्टता को कुछ कम करने के खयाल के कहा, “अभी पानी में तो देर है!” और तेजी से बाहर निकल गया।
“सचमुच अन्धड़ विचित्र था। मैं थोड़ी ही दूर गया हूँगा कि घटा मानो घुमड़ कर बिलकुल नीचे झुक आयी, अँधेरा हो गया और जोर से गड़गड़ाहट होने लगी। बजरी की कनियाँ मेरी पिंडलियों पर चिकोटी काटती हुई मुझे दौड़ाये लिए जा रही थीं। एकाएक दूर पर बिजली की तीखी कौंध हुई और उसके बाद एक बिलकुल दूसरे ढंग की कड़क : मैंने जाना कि बिजली गिरी है। मैं सुन चुका था कि ऐसे आँधियों में वहाँ अक्सर बिजली गिरती है। उस से झुलसे हुए पेड़ भी मैंने देखे थे। पर मैं तो बढ़ता ही जा रहा था।
“अँधेरा बढ़ गया था और उड़ती हुई बजरी के कारण आँखें खुली रखना भी कठिनतर होता जा रहा था। जब-तब मेरे चश्मे के शीशे पर भी कंकड़ बज उठते थे। एकाएक फिर वैसी ही तीखी कौंध और साथ ही साथ वह तीखी कड़क : बिजली बिलकुल मेरे पास ही गिरी—इतनी निकट कि मुझे लगा, मैं हाथ बढ़ाये होता तो उसे छू लेता। लेकिन उसी क्षण मैंने यह भी जाना कि बिजली पास के एक छोटे गाछ पर गिरी है जो उसकी चोट से चिर कर दो टुकड़े हो गया है।
“वैसा सुन्दर दृश्य जीवन में कदाचित् ही देखा होगा। मैं थोड़ी देर स्तब्ध खड़ा रहा। बड़ी-बड़ी बूँदों की चपत ने मुझे जगाया तो मैं घर की ओर बढ़ा। डर मुझे नहीं लगा था, न यही खयाल हुआ कि मैं किसी बड़े जोखम से बच गया हूँ—पर उस अनिर्वचनीय सौन्दर्य की सिहरन मन में थी।” [अज्ञेय (1982) : 124-125]
[xv] नामवर सिंह (1983) : 108-109, 110-111
[xvi] ये शब्द ‘दूसरी परम्परा की खोज’ के तीसरे संस्करण (2008) के ब्लर्ब से लिए गए हैं। नामवर सिंह के पाठकों को ध्यान देना चाहिए कि आरंभिक संस्करणों की तुलना में नए कलेवर में प्रकाशित इस तीसरे संस्करण के ब्लर्ब की सामग्री पूर्णतः संशोधित-संवर्द्धित है। इसमें अद्यतन रूप में दिए गए पुस्तक-परिचय के अंश हैं—“आलोचना कितनी सर्जनात्मक हो सकती है, इस कृति की प्रच्छन्न भाषा-शैली जैसे उसका एक प्रीतिकर उदाहरण है। नामवर जी की यह कृति द्विवेदी जी के इस कथन को पूरी तरह चरितार्थ करती है कि पंडिताई जब जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है और तब वह बोझ भी नहीं रहती। यह सहज रचना एक सुपरिचित आलोचक के कृति-व्यक्तित्व का अभिनव परिचयपत्र है।”
[xvii] नामवर सिंह (1983) : 57
[xviii] इस पूरी स्थापना के मूल संदर्भों का विवेचन ई. एच. कार ने ‘व्हाट इज हिस्ट्री’ के अपने पहले व्याख्यान ‘इतिहासकार और उसके तथ्य’ में किया है। वे इतिहासकार द्वारा तथ्यों के उपयोग को लेकर अपनाई गई रणनीति की चर्चा करते हुए कहते हैं, “कहा जाता था कि तथ्य खुद बोलते हैं, मगर यह बात सही नहीं है। तथ्य तभी बोलते हैं जब इतिहासकार उन्हें बुलाता है। यह वही तय करता है कि किन तथ्यों को किस क्रम और संदर्भ में वह मंच पर बुलाएगा। मेरा खयाल है कि पिरांदेली के एक चरित्र ने कहा था कि तथ्य बोरे की तरह होते हैं, जब तक उनमें कुछ भरा न जाए वे खड़े नहीं होते। हेस्टिंग्स की लड़ाई 1066 में लड़ी गई—इस जानकारी में हमारी दिलचस्पी का कारण यही है कि इतिहासकार इसे एक बड़ी ऐतिहासिक घटना मानते हैं। इतिहासकार ने निजी कारणों से यह तय किया कि रूबीकान नामक उस मामूली सी नदी का सीजर द्वारा पार किया जाना एक ऐतिहासिक तथ्य है बल्कि उसके पहले और बाद में जिन करोड़ों लोगों ने उसे पार किया उनमें किसी की दिलचस्पी नहीं है। इतिहासकारों ने उन्हें ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। दरअस्ल एक घंटा पहले पैदल, साइकिल या कार पर आप लोग इस भवन में आए : यह अतीत का वैसा ही तथ्य है जैसा सीजर का रुबीकान नदी पार करना है मगर इतिहासकार संभवतः इसकी उपेक्षा कर जाएँगे। प्रो. टैलकाट पार्सन्स ने एक बार विज्ञान के बारे में कहा था कि वह यथार्थ के अनुभवाश्रयी स्थिति ज्ञान की विशिष्ट प्रक्रिया है। इसे और सरल शब्दों में कहा जा सकता था मगर और दूसरी चीजों के साथ इतिहास की भी वही प्रक्रिया है। इतिहासकार आवश्यक रूप से चुनाव पर बल देता है। एक कुतर्क यह दिया जाता है कि ऐतिहासिक तथ्य वस्तुगत तथा इतिहासकार की व्याख्या से एकदम स्वतंत्र अलग अस्तित्व रखते हैं। मगर इस असंगत विश्वास को तोड़ना कठिन है।” [ई. एच. कार (1976) : 4-5]
[xix] Jawaharlal Nehru (2004) : 10
प्रस्तुत लेख में प्रयुक्त ‘द डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ के उद्धरणों का अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद लेखक द्वारा किया गया है। चूँकि लेख के अंतिम हिस्से में नामवर सिंह की ‘खोज’ को स्पष्ट करने के लिए नेहरू की ‘खोज’ की अवधारणा का उपयोग किया गया है, अतः ‘खोज’ के लिए स्वयं नेहरू द्वारा प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों जैसे Quest, Discovery, Search आदि की अर्थच्छवियों पर ध्यान दिलाने के उद्देश्य से उन्हें मूल रूप में ही रखा गया है।
[xx] Jawaharlal Nehru (2004) : 40, 41
[xxi] द्विवेदी जी ने अपने निबंधों और सर्जनात्मक कृतियों में इस धारणा को व्याख्यायित तो किया ही, लेकिन हमें इसका सबसे रोचक-रोमांचक और अपूर्व प्रमाण मिलता है मनोहर श्याम जोशी से हुई उनकी भेंटवार्ता में। यह तथ्य तब और भी स्मृत्य हो जाता है जब हमें पता चलता है कि वार्ता की मूल योजना नामवर सिंह की ही थी, आचार्य की षष्टि-पूर्ति के उपलक्ष्य में ‘आलोचना’ में उसके प्रकाशन के निमित्त। यह एक ऐसी भेंटवार्ता थी जिसके बारे में न तो द्विवेदी जी को कोई पूर्वसूचना थी और न ही प्रश्न पूछने अथवा उत्तर प्रस्तुत करने की कोई औपचारिक योजना। और तो और पर्याप्त और अनुकूल समय भी नहीं। लेकिन फिर भी वार्ता हुई और बेहद दिलचस्प हुई। अनायास संवाद में प्रश्नकर्ता ने उनसे सारगर्भित प्रश्न भी पूछ लिए और उत्तर देने वाले को कभी भान ही नहीं हुआ कि वह किसी साक्षात्कार के लिए सायास उत्तर दे रहा है। जैसे इतिहास और इतिहास-बोध पर जोशी जी का यह प्रश्न (और फिर द्विवेदी जी का उत्तर) : “आपको इतिहास से इतना प्रेम क्यों है? क्या यह भी एक तरह का पलायन नहीं?”
“इतिहास मनुष्य की तीसरी आँख है। एक गुजराती छात्र था वहाँ शान्तिनिकेतन में, ज़रा सिरफिरा-सा। एक दिन पूछ बैठा कि अगर ईश्वर को बुद्धि है तो उसने मनुष्य को दोनों आँखें सामने क्यों दीं? एक पीछे क्यों नहीं दे दी? इसका एक जवाब फौरन यह सूझा कि ईश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य पीछे की ओर देखे। लेकिन बाद में सोचा कि ईश्वर ने मनुष्य को पीछे की ओर देख सकने वाला नेत्र दिया है और वह है उसका इतिहास-बोध। इतिहास-प्रेम की बात मैं नहीं जानता मगर इतिहास-बोध को पलायन समझना आधुनिकता नहीं, आधुनिकता-विरोध है। आधुनिकता की तीन शर्तें हैं—एक इतिहास-बोध, दूसरी इहलोक में ही कल्याण होने की आस्था और तीसरी व्यक्तिगत कल्याण की जगह सामूहिक कल्याण की एषणा। मैं आग्रहपूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि जो इतिहास को स्वीकार न करे वह आधुनिक नहीं और जो चैतन्य को न माने वह इतिहास नहीं।” [मनोहर श्याम जोशी (1983) : 15]
[xxii] Jawaharlal Nehru (2004) : 50
[xxiii] नामवर सिंह (1983) : 7
[xxiv] Jawaharlal Nehru (2004) : 26
[xxv] Jawaharlal Nehru (2004) : 26
[xxvi] Jawaharlal Nehru (2004) : 62
[xxvii] नामवर सिंह (1983) : 115
[xxviii] नामवर सिंह (1983) : 121
[xxix] Jawaharlal Nehru (2004) : 627
[xxx] भारत यायावर (सं.) (2003) : 485
[xxxi] सुमन केशरी (सं.) (2009) : 17
[xxxii] नामवर सिंह (2010 ख) : 147-148
मूल रूप में यह व्याख्यान ‘वागर्थ’ (दिसंबर 2008) में प्रकाशित हुआ और बाद में इसे आशीष त्रिपाठी द्वारा नामवर सिंह के व्याख्यानों की संपादित पुस्तक ‘ज़माने से दो दो हाथ’ में संकलित किया गया। इसी प्रसंग में नेहरू-नामवर सिंह के अन्तःसूत्रों को समझने की दृष्टि से उनकी एक और टिप्पणी ध्यातव्य है जो उन्होंने ‘द डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ पर आधारित और श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित धारावाहिक ‘भारत : एक खोज’ पर की है। इस टिप्पणी में उन्होंने भारत के व्यापक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में नेहरू के दाय को स्वीकार करते हुए उनके उक्त ग्रंथ की सराहना की है। टिप्पणी के कुछ अंश देखें :
“दूरदर्शन द्वारा प्रस्तुत ‘भारत : एक खोज’ एक तरह से भारतीय संस्कृति का एक विराट बहुरंगी ‘कोलाज’ या ‘मोज़ेक’ है जिसके एक-एक रंग की अपनी पहचान है—‘भिन्नता में एकता’ की भावना की मनोहर प्रतिच्छाया।’
“1936-37 के देशव्यापी चुनावों के दौरान जब नेहरू जी पूरे भारत के तूफानी दौरे पर निकले तो वे दूर-दराज के छोटे कस्बे और गाँव तक पहुँचे। इस तरह उन्होंने असली भारत को आँख भर देखा। अपने भारत को गहराई से खोजने की चाह नेहरू जी में यहीं से जागी, लेकिन वह चाह पूरी हुई सितंबर, 1944 में अहमदनगर किले की कैम्प जेल में। चार महीने तक कलम घिसने के बाद नेहरू जी ने महसूस किया कि ‘जिस तरह मेरा दिमाग लिखित इतिहास से प्राप्त चित्रों और कमोबेश सुनिश्चित तथ्यों से भरा हुआ था, उसी तरह एक बिना पढ़े-लिखे किसान के मन में भी एक चित्रदीर्घा होती है। हालाँकि ये चित्र अधिकांशतः मिथकों, परम्पराओं, महाकाव्यों के नायकों-नायिकाओं की देन होते हैं और इनमें इतिहास का योगदान बहुत कम होता है, फिर भी यह चित्रदीर्घा काफी सजीव होती है।’
“इस प्रक्रिया में नेहरू जी को भारत ‘एक ऐसे प्राचीन भोजपत्र की तरह प्रतीत हुआ जिस पर विचारों और दिवास्वप्नों की परतें एक दूसरे पर कुछ इस तरह अंकित होती रही हैं कि कोई भी नई परत पहले से अंकित इबारत को पूरी तरह मिटा नहीं सकी।’
“जेल की एकान्त कोठरी में धीरे-धीरे इस प्राचीन भोजपत्र के पन्ने एक के बाद एक खुलते चले जाते हैं और भारत के पाँच हजार वर्षों का इतिहास आँखों के सामने सजीव चित्रों के रूप में उभरने लगता है और सबसे पहले सुनाई पड़ती है वेद वाणी—ऋग्वेद का नासदीय सूक्त, जिसके आरम्भिक शब्द हैं : नासदासीन्नो सदासीत् तदानीं...’ सृष्टि से पहले सत् नहीं था, असत् भी नहीं...। xxx
“कहना न होगा कि पाँच हजार वर्षों के जीवन्त इतिहास से गुजरते हुए हमें निश्चय ही जीवन के कुछ महत्त्वपूर्ण मूल्य मिलते हैं, जैसे—तर्क की स्थापना, त्याग का महत्त्व, अनुष्ठानों-पाखंडों का विरोध, सत्य की स्थापना, सद्भाव, भाईचारा, सामाजिक जड़ता का प्रतिरोध, दृढ़ निश्चय आदि।” [नामवर सिंह (2018) : 176-177]
[xxxiii] नेमिचन्द्र जैन (सं.) (1980) : 326
संदर्भ ग्रंथ
अज्ञेय (1982) 1999 : स्मृति-लेखा (नई दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस)।
अशोक वाजपेयी (2002) : परम्परा की आधुनिकता : हजारी प्रसाद द्विवेदी (सं.) (नई दिल्ली : पूर्वोदय प्रकाशन)।
ई. एच. कार (1976) 2007 : इतिहास क्या है (अनु. अशोक चक्रधर) (नई दिल्ली : मैकमिलन)।
नामवर सिंह (1983) 2000 : दूसरी परम्परा की खोज (नई दिल्ली : राजकमल पेपरबैक्स)।
................ (2010 क) : हिन्दी का गद्यपर्व (सं. आशीष त्रिपाठी) (नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन)।
................ (2010 ख) : ज़माने से दो दो हाथ (सं. आशीष त्रिपाठी) (नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन)।
................ (2012) : आलोचना और विचारधारा (सं. आशीष त्रिपाठी) (नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन)।
................ (2013) : प्रारंभिक रचनाएँ (सं. भारत यायावर) (नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन)।
................ (2017) : आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की जय-यात्रा (सं. ज्ञानेंद्र संतोष) (नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन)।
................ (2018) : पूर्वरंग (सं. आशीष त्रिपाठी), (नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन)।
नेमिचंद्र जैन (1980) 2007 : मुक्तिबोध रचनावली - खंड 2 (सं.) (नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन)।
भगवान सिंह (2011) : भारतीय परंपरा की खोज (नई दिल्ली : सस्ता साहित्य मंडल)।
भारत यायावर (2003) : आलोचना के रचना-पुरुष : नामवर सिंह (सं.) (नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन)।
मनोहर श्याम जोशी (1983) 2008 : बातों बातों में (नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन)।
मुकुन्द द्विवेदी (1981) 2007 : हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली – खंड - 4 (सं.) (नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन)।
रामधारी सिंह दिनकर (1956) 2005 : संस्कृति के चार अध्याय (इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन)।
............................ (1966) 1987 : शुद्ध कविता की खोज (नई दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस)।
विजय देव नारायण साही (1987) 2007 : छठवाँ दशक (इलाहाबाद : हिन्दुस्तानी एकेडेमी)।
श्यामा चरण दुबे (1991) 2008 : परम्परा, इतिहास-बोध और संस्कृति (नई दिल्ली : राधाकृष्ण प्रकाशन)।
सुधीश पचौरी (1995) : नामवर के विमर्श (सं.) (नई दिल्ली : प्रवीण प्रकाशन)।
................. (2019) : तीसरी परम्परा की खोज (नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन)।
सुमन केशरी (2009) : जे एन यू में नामवर सिंह (सं.) (नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन)।
Jawaharlal Nehru (1946, 2004) 2010: The Discovery of India (New Delhi: Penguin Books).
Theodor Adorno (1951, 1974) 2005: Minima Moralia: Reflections on a Damaged Life (London: Verso).
सम्पर्क-




आपकी इस प्रस्तुति का लिंक 29-07-2021को चर्चा – 4,140 में दिया गया है।
जवाब देंहटाएंआपकी उपस्थिति मंच की शोभा बढ़ाएगी।
धन्यवाद सहित
दिलबागसिंह विर्क
विस्तृत और शोधपरक समालोचना।
जवाब देंहटाएंअप्रतिम।