मार्कण्डेय जी की कविताएँ
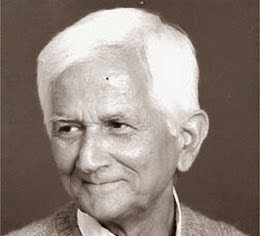 |
| मार्कण्डेय |
मार्कण्डेय जी ने कहानियों के अतिरिक्त अन्य विधाओं जैसे उपन्यास, एकांकी, कविता, आलोचना, समीक्षा आदि में भी सफलतापूर्वक अपनी लेखनी चलायी। रचनाधर्मिता के लिए जीवन-जगत के सूक्ष्म अवलोकन को वे जरुरी मानते थे। अपने अंतिम दिनों में वे मुझे अपनी पुरानी डायरी के पीले पड़ चुके और बिखर से गए पन्नों से अपनी कविताएँ बड़ी तन्मयता के साथ सुनाते थे। उनके दो कविता संग्रह प्रकाशित हैं- 'सपने तुम्हारे थे' और 'यह पृथ्वी तुम्हें देता हूँ'। आज मार्कण्डेय जी का जन्मदिन है। सन 1930 में जौनपुर के बराई गाँव में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। इस अवसर पर दादा को नमन करते हुए हम प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी कुछ कविताएँ। 'पहली बार' के लिए इन कविताओं का चयन किया है डॉ. हिमांगी त्रिपाठी ने। हिमांगी ने हाल ही में महात्मा गाँधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना (मध्य प्रदेश) से मार्कण्डेय जी की रचनाधर्मिता पर अपना शोध कार्य पूरा किया है। तो आइए आज पढ़ते हैं मार्कण्डेय जी की कुछ कविताएँ।
मार्कण्डेय जी की कविताएँ
चोर को चोर कहना
चोर को चोर कब नहीं कहना चाहिए
कभी मैंने पूछा था चाचा से,
तब वे चुप रह गये थे,
कल एकाएक अपनी धंसी आँखे
मुलमुलाते हुए बोले -
चोर को उस समय चोर नहीं कहना चाहिए
जब वह ऊंची मेड़ पर खड़ा हो
और उसके हाथ में लाठी हो
जब वह भाग रहा हो और सामने
ठाकुर की बखरी की अँधेरी कोली हो,
जब गाँव का मुखिया उसे
अपना मौसेरा भाई कहता हो
जब वह राजा का मित्र या साला हो
अथवा अफसर अदना
या आला हो
या गाँव का नाई हो
जिससे तुम्हें छिलवानी
हो खोपड़ी
बाप के शुद्धक में
अथवा उसे भी जिससे कहीं
दबती हो तुम्हारी नस
उस प्रोफेसर को तो कत्तई नहीं
जो तुम्हारा परीक्षक भी हो,
उस औरत को भूल कर भी नहीं
जो गुंडों अथवा डाकुओं की रखैल हो,
तस्कर अथवा शराब के व्यापारी को तो
सपने में भी नहीं,
किसी थानेदार को चोर कहना
सिर पर है आफत का लेना,
बस बस समझ गया चाचा
अब यह बताइए कि
चोर को कब चोर कहना चाहिए
तो सुनो बेटा
इस दो पाये आदमी की
मोटामोटी दो ही कोटियां हैं
अगर वह हीन है
तो उस चोर को उछल कर मारेगा चाँटा
जो लाचार और बेचारा हो
और दुखों में बुरी तरह कल्हारा हो
लेकिन श्रेष्ठ जन चोर को चोर
हुँकार कर तब कहते हैं
जब उस चोर का सरदार
देश का आलमबदार हो
चाहे उसके हाथ में मोटा डण्डा हो
चाहे फांसी का मोटा फंदा।
नेता के नगर आने पर
उनके आते ही
सारा शहर बस्साने लगता है, नाबदानों के फब्बारे
हवा में उछल-उछल कर
अपने रंग उगलने लगते हैं, दीवारें रंगीन छिपकलियों-सी
तख्तियों से अट जाती हैं, नारों का झूठ बिलबिलाने लगता है
मैला ढोते गुबरैलों की तरह,
चिढ़ाने लगता है मुँह
गृहस्थी का भार ढोते
बेबस, लाचार नागरिकों का,
एक अनचाहा आतंक रिसने लगता
धीमे-धीमे जहर की तरह, सोचिए कितना भयावह होगा
खोखला बनना
मरी हुई आत्मा के डांगर का
या झण्डे ढोना किसी ऐसे धोखा का
जो हैवान के लिए नहीं
इन्सान के लिए
उसकी ही फसलों में
रोप दिया गया हो।
स्मृति का छाता
आज सुबह-सुबह
अचानक हवा महक उठी है
कली जो बन्द थी डाल पर कब से
विहस पड़ी है
चिड़िया जो आती थी
खिड़की पर चुपचाप बैठ चली जाती थी
चहक उठी है
पता नहीं बाहर
आसमान का क्या हाल है
वह जरूर घिरा होगा
काले बादल दौड़े आए होंगे
जल्दी ही बूंदें पड़ेंगी
तीर की तरह
फिर क्या होगा!
स्मृति का छाता पुराना पड़ गया है
जगह-जगह छेद हो गये हैं उसमें
फिर भी उसे सीता हूँ बार-बार
जीता हूँ भीगना...।
बया और कौवा
बया के घोंसले से
निकला एक कौवा
मैंने पूछा बया से
यह कैसे हुआ
बोली जरा देखिए
कैसा जमाना है
मेरे जैसे लोगों का
अब कहाँ ठिकाना है
रात-दिन जग कर
मर कर, खप कर
तृण-तृण तोड़ कर
चोंच से जोड़ कर
घोंसला बनाया
न जाने कहाँ से
डाकू यह आया
बकने लगा कांव कांव
हो गयी झांव झांव
बच्चों को खा गया
मुझको बहला गया
उड़ती हूँ दिन रात
डार-डार पात-पात
घोंसले को देखती हूँ
रोती हूँ, बिसूरती हूँ
बोलो कहाँ जाऊं
किसको बुलाऊं
किससे कहूँ दुख-दर्द
किससे कहूँ सपना
अब इस दुनिया में
कोई नहीं अपना।
मुझे तुमने सीपियों में देखा है
नीली जलराशि के
सुहाने, नवरंगों में,
सूर्य की प्रताड़ित
सतरंगी लघु किरणों में
तीराक्ष, चंचल चंचरीक के घेरों में
जल की अतल गहराइयों में :
नहीं देखा तुमने किन्तु
टूटी चट्टानों की
शोख, शमित धारों को,
जो कभी छवि-मण्डित
हिम-शिखरों सी थीं
लेकिन वे टूट गयीं
प्रबल जल-प्लावन में
खंडित उन्हें कर दिया
भ्रमर दिया रग-रग
मधुर स्पर्शों से,
शीतल थपकियों से
कण-कण को निर्मल निखार कर
पैना मुझे कर दिया :
इसलिए जाग्रत हूँ,
टूटा हूँ,
लेकिन समादृत हूँ,
आऊंगा,
तट का अभिलाषी मुक्त नागरिक हूँ।
मौन
आराधना का मौन :
जैसे साँझ की मुरली मधुर बजती,
उखड़ती बज्र-सी धरती,
रम्हाते गो-पदों के चिन्ह में
लिख दे कहानी मोह की,
आह, तेरे छोह की
ऐसी कथा है,
और मेरे मौन की
तैसी व्यथा है।
तुम कुछ वैसी ही हो,
कैसी, अगर कोई पूछे तो
बता न सकूं
तुम कुछ वैसी ही हो
जैसी एक बात, जिसमें अर्थ नहीं
जैसी अंधेरे के बगैर रात,
लेकिन अगर कोई चाहे तो दिखा न सकूं,
जब कभी बेहोश में होता हूँ
इसलिए पल भर
अर्थ और अंधेरे से
लय और चांदनी निकालता हूँ,
पाता हूँ, बेसुध हो जाता हूँ
तो तुम क्या लय हो, धमनी से!
तब तो मैं गाऊंगा
शब्दहीन चाहनी की माला बनाऊंगा
धरती पर घूमूंगा, सबको पिन्हाऊंगा!
सूली पर कवि
जब कोई बेन्जामिन
जनता का प्रेम गीत गाता है
लोगों को नींद से जगाता है
बताता है प्रेयसी से
धरती की गंध
रूप-रंग माटी का
कहता है देह में तुम्हारे है
वही गंध, वही रंग
वही हो तुम, बिल्कुल वही
जुल्म की कहानी सुनाता है
गर्भस्थ शिशुओं को
लोगों को दिखाता है
रक्त-सिक्त थूथुन
गोरे आदम खोरी भेड़ियों का,
माँओं की चिथी हुई छातियां,
बिजली से दाग-दाग
मारे गए बच्चों को
फंसे हुए पंजों में गिद्धों के,
सड़कों से अनायास पकडे़ गये
युवकों के जख्मी पुट्ठों को,
पत्थरों से पीसे गये
भुरकुस हाथों को,
तब कविता, कविता नहीं रहती
वह फसल बन जाती है,
गीत गाये नहीं जाते
लोगों की सांसों में
चुपके से उतर जाते हैं
वे समझ नहीं पाते
घबराते हैं
पसीने-पसीने हो जाते हैं
और चढ़ा देते हैं
कवि को सूली पर.... ।
 |
| हिमांगी त्रिपाठी |
सम्पर्क
ई-मेल : tripathihimangi@gmail.com





आपकी इस प्रस्तुति का लिंक 04-05-2017 को चर्चा मंच पर चर्चा - 2627 में दिया जाएगा
जवाब देंहटाएंधन्यवाद
पहली बार मार्कण्डेय जी से अवगत हुआ
जवाब देंहटाएंप्रस्तुति शानदार
आभार
व्यवस्था पर जबरदस्त प्रहार करती मार्कण्डेय जी की रचनाएँ पढ़वाने हेतु धन्यवाद!
जवाब देंहटाएंसटीक रचनाएँ
जवाब देंहटाएं